
समयसीमा 263
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1018
मानव व उसके आविष्कार 790
भूगोल 257
जीव - जन्तु 299
समयसीमा 263
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1018
मानव व उसके आविष्कार 790
भूगोल 257
जीव - जन्तु 299
| Post Viewership from Post Date to 08- Jun-2025 (31st) Day | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Subscribers (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 2320 | 38 | 0 | 2358 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

जौनपुर के नागरिकों, मैंग्रोव पेड़ ऐसे खारे पानी वाले तटीय क्षेत्रों में उगते हैं, जहां सामान्य पौधे नहीं बढ़ सकते। इन पेड़ों को जीने के लिए, उनकी जड़ें ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करके समुद्र के पानी से नमक छानती हैं, ताकि केवल मीठा पानी ही पौधों में प्रवेश कर सके। इससे मैंग्रोव को उनके कठोर वातावरण में भी ताज़गी और सेहतमंद बने रखने में मदद मिलती है। कुछ मैंग्रोव तो अधिक नमक को अपनी पत्तियों तक भेजते हैं, जो बाद में गिर जाती हैं, ताकि संतुलन बनाए रखा जा सके। ऑस्मोसिस का यह शानदार तरीका मैंग्रोव को तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने, मिट्टी के कटाव को रोकने और समुद्री जीवन का समर्थन करने में मदद करता है, जिससे यह पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
आज हम मैंग्रोव पेड़ों के बारे में बात करेंगे, और जानेंगे कि ये तटीय वातावरण में कैसे अनुकूलित होते हैं। इसके बाद हम मैंग्रोव के जंगलों की महत्ता पर चर्चा करेंगे और इनके तटीय सुरक्षा और जैव विविधता में योगदान को समझेंगे। फिर हम भारत में मैंग्रोव के बारे में जानेंगे।
मैंग्रोव के पौधों की बोटैनिकल विशेषताएँ
मैंग्रोव जंगलों का महत्व
भारत में मैंग्रोव
भारत में मैंग्रोव का क्षेत्रफल 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसके बाद गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। सुंदरबन, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह जंगल रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और खाराजल मगरमच्छ का घर है।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल ओडिशा के भितरकनिका में स्थित है, जो ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के डेल्टा द्वारा निर्मित है। यह भारत के महत्वपूर्ण रामसर आर्द्रभूमि में शामिल है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा में फैला हुआ मैंग्रोव जंगल ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक फैला है। केरल के बैकवाटर्स में भी मैंग्रोव वन की उच्च घनता पाई जाती है। तमिलनाडु के पिचावरम में पानी से ढके हुए विशाल मैंग्रोव जंगल हैं, जो कई जल पक्षी प्रजातियों का घर हैं।
पश्चिम बंगाल भारत के मैंग्रोव क्षेत्र का 42.45% हिस्सा है, इसके बाद गुजरात का 23.66% और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का 12.39% हिस्सा है।
संदर्भ
मुख्य चित्र में सूर्यास्त के समय मैंग्रोव का स्रोत : Wikimedia
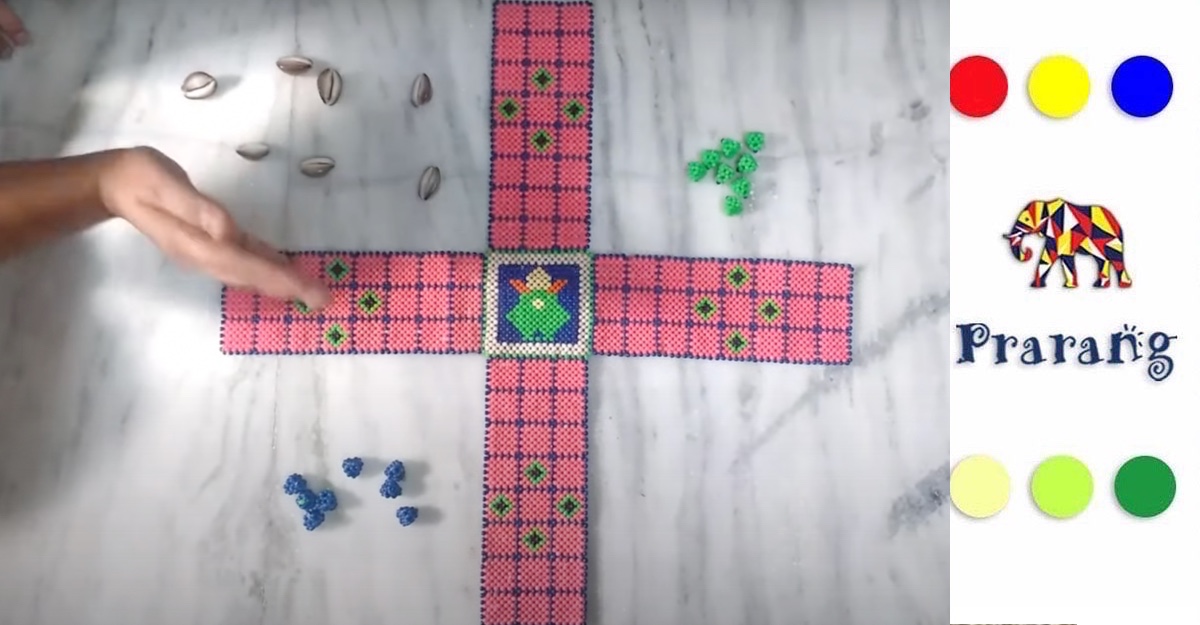




A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.
