
समयसीमा 267
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1029
मानव व उसके आविष्कार 799
भूगोल 263
जीव - जन्तु 303

जौनपुरवासियों, हमारी ज़िंदगी की रफ्तार आज इतनी तेज़ हो चुकी है कि हम सुबह से रात तक काम, जिम्मेदारियों और सोशल मीडिया (Social Media) की भागदौड़ में उलझे रहते हैं। ऐसे में कब हमारा मन थकने लगता है, कब भीतर एक ख़ामोशी घर करने लगती है - हमें खुद भी पता नहीं चलता। हम मुस्कुराते रहते हैं, दूसरों के साथ सामान्य व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कोई तकलीफ़ चुपचाप गहराती जाती है। देशभर में आत्महत्या के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो सिर्फ संख्या नहीं हैं - वे हज़ारों अनकही पीड़ाओं, टूटी उम्मीदों और सुनी-अनसुनी कहानियों की निशानियाँ हैं। कई बार व्यक्ति अपनी परेशानी किसी से कह भी नहीं पाता, क्योंकि उसे डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। यही सोच उसे और अकेला कर देती है। आज समय आ गया है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को भी उसी तरह गंभीरता से लें जैसे बुखार या कोई शारीरिक बीमारी को लेते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक मानवीय स्थिति है, जिसका इलाज और सहयोग - दोनों संभव हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हमें यह याद दिलाने का मौका है कि हम एक-दूसरे के मन की हालत को समझें, समय पर बात करें, और अगर ज़रूरत हो तो मदद लेने या देने से बिल्कुल न हिचकें। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि कभी-कभी सिर्फ किसी का हालचाल पूछ लेना भी किसी के टूटते मन को थाम सकता है।
इस लेख में हम सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में आत्महत्या की स्थिति क्या है और हाल के वर्षों में आंकड़े किस ओर इशारा कर रहे हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह अलग-अलग वर्ग - जैसे छात्र, गृहिणियां, किसान और दैनिक मजदूर - आज मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। फिर हम यह समझेंगे कि कैसे बड़े शहरों की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। इसके साथ ही, हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की भूमिका, जागरूकता अभियानों की ज़रूरत और आत्महत्या की रोकथाम के लिए समाज और सरकार की साझा ज़िम्मेदारी पर भी बात करेंगे। अंत में, हम यह जानेंगे कि कैसे प्रकृति के संपर्क में आकर मानसिक शांति पाई जा सकती है ।
भारत में आत्महत्या से जुड़ी वर्तमान स्थिति: आँकड़ों की दृष्टि से एक समीक्षा
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 2021 में भारत में 1,64,033 आत्महत्याएं दर्ज की गईं - जो 2020 की तुलना में 7.2% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक बेचैनी का संकेत है। आत्महत्या, जो कभी व्यक्तिगत दुर्भाग्य मानी जाती थी, अब एक राष्ट्रव्यापी मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल का रूप लेती जा रही है। विशेष रूप से महाराष्ट्र (22,207), तमिलनाडु (18,925), मध्य प्रदेश (14,965), पश्चिम बंगाल (13,500), और कर्नाटक (13,056) जैसे राज्य, जो कुल आत्महत्याओं का 50% से अधिक वहन करते हैं - ये आंकड़े देश के मानसिक स्वास्थ्य ढांचे की गंभीर कमज़ोरियों को उजागर करते हैं। उत्तर प्रदेश, जो देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, वहां आत्महत्या की दर 3.6% है - यह अपेक्षाकृत कम ज़रूर लगती है, लेकिन इस राज्य की विशाल जनसंख्या को देखते हुए वास्तविक संख्या कहीं अधिक भयावह हो सकती है। इन आंकड़ों के पीछे वे अनसुनी कहानियाँ छिपी हैं - जो कभी नौकरी छूटने से शुरू हुईं, तो कभी रिश्तों की टूटन से। हर एक आत्महत्या अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है - और यह केवल संबंधित परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की ज़िम्मेदारी है कि वह इन मौन पीड़ाओं को सुने और समझे।

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मानसिक दबाव की स्थिति
भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में आत्महत्या अब किसी एक वर्ग या तबके की त्रासदी नहीं रही। नसीआरबी (NCRB) की रिपोर्ट साफ़ बताती है कि दैनिक वेतनभोगी, गृहिणियां, स्वरोज़गार करने वाले, छात्र और किसान - हर वर्ग में मानसिक तनाव और निराशा की लहर फैल रही है। 2021 में स्वरोज़गार करने वालों में ही 20,231 आत्महत्याएं दर्ज की गईं। यह संख्या दर्शाती है कि व्यापार में अस्थिरता, ऋण का बोझ, और भविष्य की अनिश्चितता अब आम बात हो गई है। गृहिणियों की आत्महत्याएं एक अलग कहानी कहती हैं - एक ऐसी कहानी जिसमें आर्थिक निर्भरता, घरेलू हिंसा, भावनात्मक अकेलापन और सामाजिक चुप्पी शामिल हैं। 2021 में 23,000 से अधिक गृहिणियों ने आत्महत्या की, जिनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक घटनाएं हुईं। इसी तरह, छात्रों की आत्महत्याएं भी लगातार बढ़ रही हैं। केवल परीक्षा में असफलता नहीं, बल्कि करियर का डर, माता-पिता की अपेक्षाएं, सोशल मीडिया की तुलना और आत्म-संदेह जैसे कारक उन्हें अंदर से खा रहे हैं। किसान, जो कभी भारत की आत्मा माने जाते थे, आज वे फसल की विफलता, कर्ज़ और प्राकृतिक आपदाओं के चलते खुद को असहाय पा रहे हैं। जब एक किसान आत्महत्या करता है, तो उसके साथ उसकी ज़मीन, उसके बच्चों का भविष्य और पूरे गांव की उम्मीदें भी टूट जाती हैं। यह स्थिति हमें साफ़ चेतावनी देती है कि अब मानसिक स्वास्थ्य केवल "शहरी" चिंता नहीं रह गई है - यह गाँव से लेकर शहर तक हर व्यक्ति का सवाल बन चुका है।
शहरों में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों की बढ़ती प्रवृत्ति
शहरों में जीवन की रफ्तार जितनी तेज़ हुई है, मानसिक शांति उतनी ही पीछे छूटती जा रही है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और बेंगलुरु जैसे महानगरों में आत्महत्या के मामले सबसे अधिक दर्ज हो रहे हैं - और यह कोई संयोग नहीं है। उच्च प्रतिस्पर्धा, काम का अत्यधिक दबाव, नौकरी की अस्थिरता, और सामाजिक अकेलापन - ये सभी कारक मिलकर एक भयावह मानसिक स्थिति बना देते हैं। यहां तक कि जब हम परिवार और दोस्तों के बीच होते हैं, तब भी कई लोग खुद को अंदर से बेहद अकेला महसूस करते हैं। कॉलेज के छात्र, युवा प्रोफेशनल्स (professional) और यहां तक कि गृहिणियां भी अब उस तनाव का सामना कर रही हैं जो पहले सिर्फ मेट्रो (metro) शहरों में देखा जाता था। इंटरनेट (internet) और सोशल मीडिया ने भले ही सूचना को नज़दीक कर दिया हो, लेकिन इंसानी रिश्तों की गर्माहट को कहीं दूर ले गया है। अब 'डिजिटल संवाद' (Digital Dialogue) तो है, लेकिन 'संवेदनशील संवाद' नहीं। शहरों में खुलेपन की कमी, प्रकृति से दूरी, और हमेशा उपलब्ध रहने की अपेक्षा ने लोगों को मानसिक थकावट की स्थायी स्थिति में डाल दिया है। मानसिक स्वास्थ्य अब केवल एक वैकल्पिक विषय नहीं - यह शहरी जीवन की अनिवार्यता बन चुकी है।

मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का महत्व
हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाने वाला विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं - बल्कि एक सामाजिक संकल्प का प्रतीक है। यह दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने मानसिक स्वास्थ्य को उतना महत्व दिया, जितना हम शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं? क्या हम अपने आस-पास किसी उदास व्यक्ति को पहचानते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में अब भी काफी भ्रांतियां हैं। कई लोग इसे 'कमज़ोरी' समझते हैं, या फिर इसे छिपाकर रखने लायक विषय। लेकिन सच यह है कि मानसिक बीमारियां भी उतनी ही वास्तविक हैं, जितनी डायबिटीज़ (diabetes) या ब्लड प्रेशर (blood pressure)। इस दिन का उद्देश्य है - लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करने, मदद मांगने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, कॉलेजों में काउंसलिंग सेंटर (counselling center), और कार्यस्थलों पर तनाव प्रबंधन कार्यक्रम - ये सब जागरूकता के ठोस उपाय हैं। जब हम यह समझेंगे कि 'मन' भी 'तन' की तरह बीमार हो सकता है, तब हम सही मायनों में स्वस्थ समाज की ओर बढ़ सकेंगे। जागरूकता सिर्फ पोस्टर (poster) या अभियान नहीं - यह जीवन बचाने का माध्यम बन सकती है।

आत्महत्या की रोकथाम हेतु समाज और प्रणाली की साझा जिम्मेदारी
जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो हम अक्सर यह सोचते हैं - "उसने ऐसा क्यों किया?" लेकिन सही सवाल यह होना चाहिए - "हमने ऐसा होने से पहले क्या किया?" आत्महत्या को केवल व्यक्ति की निजी विफलता समझना हमारी सबसे बड़ी सामाजिक चूक है। यह एक संरचनात्मक संकट है - जो समाज, परिवार, नीति और संवाद के स्तर पर हमारी विफलता को दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा लागू मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मानसिक रूप से बीमार लोगों को गरिमा और अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, इलाज की गोपनीयता, और ज़बरदस्ती इलाज पर रोक जैसे प्रावधान शामिल हैं। लेकिन कानून तभी कारगर होता है जब समाज उसे अपनाए। मीडिया को आत्महत्या की रिपोर्टिंग में अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार होना होगा। विद्यालयों और कॉलेजों में परामर्शदाता अनिवार्य किए जाने चाहिए। पंचायत स्तर तक सामुदायिक सहायता समूह बनने चाहिए। ये समस्या अकेले एक डॉक्टर नहीं सुलझा सकता - हमें पूरी सामाजिक व्यवस्था को उत्तरदायी बनाना होगा।

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रकृति का सकारात्मक प्रभाव
आज जब जीवन तकनीक से बंधा हुआ है - जहां हर पांच मिनट में एक नोटिफिकेशन (notification) आता है, हर काम की डेडलाइन (deadline) है, और हर चेहरे पर मुस्कान नकली लगती है - वहां प्रकृति एक वास्तविक राहत बनकर सामने आती है। शोध बताते हैं कि प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से मस्तिष्क शांत होता है, तनाव कम होता है और आत्म-संयम बढ़ता है। टहलना, हरे-भरे पेड़ों के बीच कुछ समय बिताना, या पानी के किनारे बैठना - यह सब सिर्फ गतिविधियाँ नहीं, मानसिक पुनर्स्थापनाएं हैं। हरे-भरे पार्कों की हरियाली, नदियों या झीलों के किनारे का वातावरण, और गांव के प्राकृतिक नज़ारे - ये सभी मानसिक सुकून के सहज माध्यम हैं। आज जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो यह भी याद रखना चाहिए कि हर इलाज दवाओं से नहीं होता - कभी-कभी मन को बस कुछ खुला आसमान, थोड़ी धूप और हरियाली चाहिए होती है। प्रकृति हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल दौड़ नहीं, कभी-कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है। अगर हम अपने दिन में 15 मिनट भी पेड़ों के नीचे बैठ लें, तो शायद मन कुछ हल्का हो जाए।
संदर्भ-
https://tinyurl.com/j4pwmejw
https://tinyurl.com/yc3uvcny



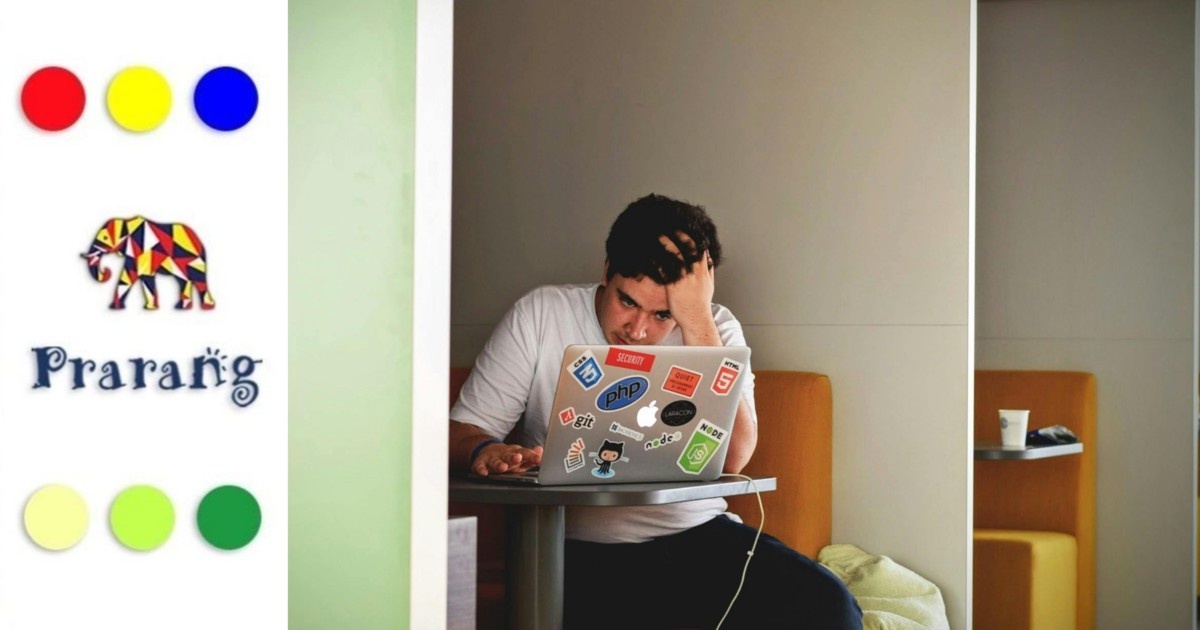
A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.