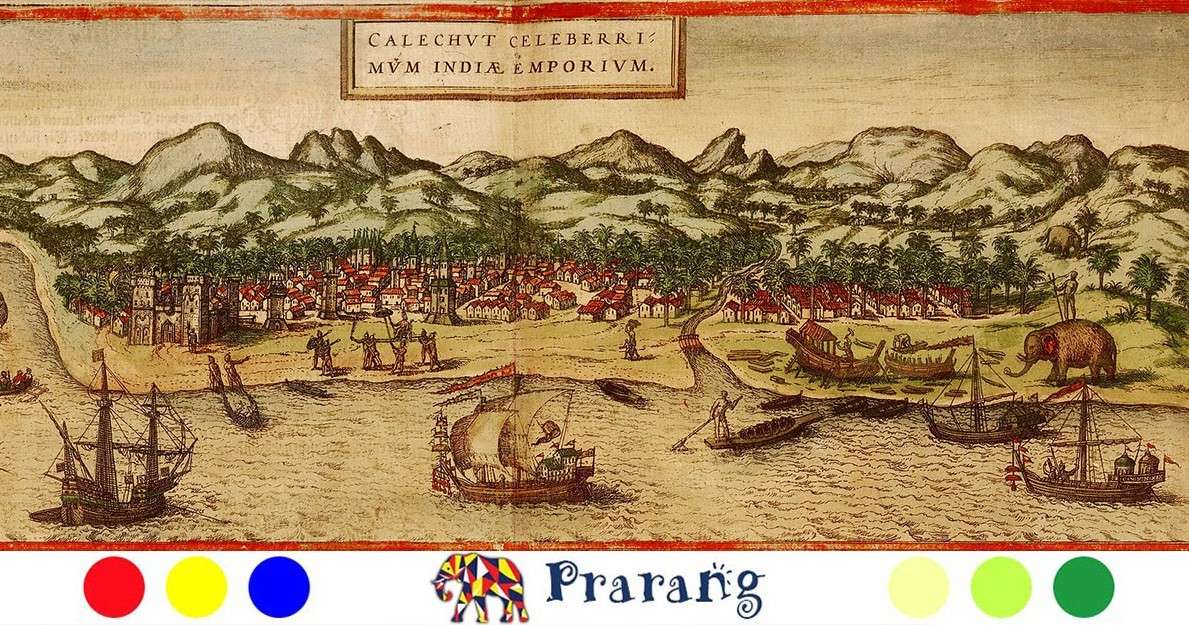समय - सीमा 268
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1036
मानव और उनके आविष्कार 802
भूगोल 264
जीव-जंतु 306
समय - सीमा 268
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1036
मानव और उनके आविष्कार 802
भूगोल 264
जीव-जंतु 306

भारतीय अर्थव्यवस्था को असंगठित श्रम रोजगार के विशाल बहुमत के अस्तित्व से वर्णित किया जा सकता है। 2009-10 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश में कुल 46.5 करोड़ रोजगार थे, जिसमें संगठित क्षेत्र में लगभग 2.8 करोड़ और असंगठित क्षेत्र में 43.7 करोड़ श्रमिक शामिल थे। असंगठित क्षेत्र के इन श्रमिकों में से, कृषि क्षेत्र में 24.6 करोड़ श्रमिक कार्यरत थे और लगभग 4.4 करोड़ निर्माण कार्य में और शेष विनिर्माण और सेवा में थे।

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने चार समूहों के अंतर्गत असंगठित श्रम रोजगार वर्गीकृत किया है, जो कुछ इस प्रकार हैं :-
व्यवसाय की शर्तों के तहत
छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, फसल काटने वाले, मछुआरे, पशुपालन में लगे लोग, बीड़ी बनाने वाले, भवन और निर्माण कामगार, चमड़े के मजदूर, बुनकर, कारीगर, नमक कर्मचारी, ईंट भट्टों और पत्थर की खदानों में काम करने वाले, आरा मिलों, तेल मिलों आदि के श्रमिक इसी श्रेणी में आते हैं।
रोजगार की प्रकृति की शर्तों के तहत
संलग्न कृषि मजदूर, बंधुआ मजदूर, प्रवासी श्रमिक, अनुबंध और आकस्मिक मजदूर इस श्रेणी में आते हैं।
विशेष रूप से व्यथित श्रेणियों की शर्तों के तहत
सामान ढोने वाले, पशु चालित वाहनों के ड्राइवर और आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
इन चार श्रेणियों के अलावा, असंगठित श्रमिक बल का एक बड़ा वर्ग मौजूद है जैसे कि मोची, हस्तशिल्प के कारीगर, हथकरघा बुनकर, महिला टेलर, शारीरिक रूप से विकलांग स्वरोजगार वाले व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चालक, पावर लूम श्रमिकों आदि।

असंगठित श्रमिकों को कई पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए भारत के श्रम मंत्रालय द्वारा प्रवासी, स्थायी या बंधुआ मजदूरों और बाल श्रमिकों के साथ होने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को पहचाना है, जो निम्न हैं :-
प्रवासी श्रमिकबंधुआ श्रमिक
बंधुआ श्रम एक नियोक्ता और एक कर्मचारी के बीच एक मजबूर संबंध होता है, जिसमें बाध्यता बकाया ऋण के बदले ली जाती है। अक्सर ब्याज की दरें इतनी अधिक होती है कि बंधुआ श्रम बहुत लंबे समय तक या अनिश्चित काल तक रहता है। सर्वेक्षण विधियों, मान्यताओं और स्रोतों के आधार पर भारत में बंधुआ मजदूरी का अनुमान व्यापक रूप से भिन्न होता है। जैसे कि आधिकारिक भारत सरकार का दावा है कि कुछ सौ हजार मजदूर बंधुआ मजदूर हैं।
बाल श्रम
2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में 5 से 14 साल के 12.6 मिलियन बच्चे अंशकालिक या पूर्णकालिक काम करते हैं। इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक असंगठित कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, और बाकी असंगठित श्रम बाजारों में। गरीबी, स्कूलों की कमी, खराब शिक्षा के बुनियादी ढांचे और असंगठित अर्थव्यवस्था की वृद्धि ने भारत में बाल श्रम को बढ़ावा दिया है।
 वहीं भारत में कई श्रम कानून हैं जैसे कि भेदभाव और बाल श्रम पर रोक लगाने वाले, जो सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, संगठित करने का अधिकार देते हैं, ट्रेड यूनियनों का गठन करते हैं और सामूहिक सौदेबाजी को लागू करते हैं। साथ ही भारत में श्रमिकों के लिए कई कठोर नियम भी लागू किए गए हैं जैसे कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में प्रति कंपनी कर्मचारियों की अधिकतम संख्या, कागजी कार्रवाई की आवश्यकता, नौकरशाही प्रक्रिया और कंपनियों में श्रम में बदलाव के लिए सरकार की मंजूरी। श्रम भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है और इसलिए श्रम मामले केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने श्रम संबंधों और रोजगार के मुद्दों पर कानून बनाए हैं।
वहीं भारत में कई श्रम कानून हैं जैसे कि भेदभाव और बाल श्रम पर रोक लगाने वाले, जो सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, संगठित करने का अधिकार देते हैं, ट्रेड यूनियनों का गठन करते हैं और सामूहिक सौदेबाजी को लागू करते हैं। साथ ही भारत में श्रमिकों के लिए कई कठोर नियम भी लागू किए गए हैं जैसे कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में प्रति कंपनी कर्मचारियों की अधिकतम संख्या, कागजी कार्रवाई की आवश्यकता, नौकरशाही प्रक्रिया और कंपनियों में श्रम में बदलाव के लिए सरकार की मंजूरी। श्रम भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है और इसलिए श्रम मामले केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने श्रम संबंधों और रोजगार के मुद्दों पर कानून बनाए हैं।
भारत में श्रम से संबंधित कुछ प्रमुख कानून निम्नलिखित हैं:
कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 :- श्रमिक की क्षतिपूर्ति अधिनियम किसी भी कर्मचारी को उसके रोजगार के दौरान हुई उसकी मृत्यु के मामले में उसके आश्रितों को हुई चोट के लिए मुआवजा देना होगा है। यह अधिनियम कर्मचारी को मुआवजा दिया जाने के संबंध में काफी लाभदायक है और साथ ही यह भारत में सामाजिक सुरक्षा कानूनों में से एक है।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965 :- यह अधिनियम सभी कारखानों और प्रत्येक उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है, जो 20 अथवा इससे अधिक श्रमिकों को नियुक्त करता है। बोनस संदाय अधिनियम,1965 में मजदूरी के न्यूनतम 8.33 प्रतिशत बोनस का प्रावधान है।
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 :- मातृत्व लाभ अधिनियम कानून द्वारा अनिवार्य महिलाओं के रोजगार और मातृत्व लाभ को नियंत्रित करता है। कोई भी महिला कर्मचारी जिसने अपनी अपेक्षित प्रसव की तारीख से पहले 12 महीनों के दौरान कम से कम 80 दिनों की अवधि के लिए किसी भी प्रतिष्ठान में काम किया, अधिनियम के तहत मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार है।
संदर्भ :-
1. https://bit.ly/336WVDC
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Labour_in_India#Unorganised_labour_issues
3. https://bit.ly/2BUh3gr
4. http://www.aajeevika.org/labour-and-migration.php