
समय - सीमा 285
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1051
मानव और उनके आविष्कार 824
भूगोल 261
जीव-जंतु 315
| Post Viewership from Post Date to 03- Jan-2025 (31st) Day | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 2791 | 124 | 0 | 2915 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

मेरठ में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित हुआ, इसका सटीक विवरण ज्ञात नहीं है, लेकिन 1850 तक, यहाँ दो प्रिंटिंग प्रेस, सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि 1870 में, पंडित गौरी दत्त का उपन्यास, ‘देवरानी-जेठानी की कहानी’ पहली बार लिथोग्राफ़ी प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करते हुए मेरठ के जैनन प्रिंटिंग रूम में छापा गया था?
इस लेख में, हम सबसे पहले मेरठ में प्रिंटिंग के इतिहास पर चर्चा करेंगे। इसके बाद, आधुनिक प्रिंटिंग तकनीकों पर बात करेंगे। इन तकनीकों में से एक है फ़्लेक्सोग्राफ़िक प्रिंटिंग, जिसे फ़्लेक्सो भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रिंटिंग तकनीक है, जो लचीली प्लेटों और तेज़ी से सूखने वाली स्याही का उपयोग करती है। यह तकनीक, विभिन्न प्रकार की सतहों पर प्रिंटिंग के लिए उपयोगी है। फ़्लेक्सो को लेटरप्रेस प्रिंटिंग का आधुनिक संस्करण माना जाता है, और इसका उपयोग अक्सर पैकेजिंग, लेबल, और उन उत्पादों के लिए किया जाता है, जिन्हें टिकाऊ और अनुकूलनीय होना चाहिए।
आज, हम इस प्रिंटिंग तकनीक और इसके उपयोगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके बाद, हम भारत में व्यावसायिक रूप से उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रिंटिंग मशीनों पर भी चर्चा करेंगे।
मेरठ में प्रिंटिंग का इतिहास
1857 के गदर से पहले ही देश के कई हिस्सों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जनमत का माहौल बनने लगा था। मेरठ से प्रकाशित किताबों, अख़बारों और पैम्फ़लेट्स ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1894 में सिविल पब्लिशिंग हाउस की स्थापना हुई, जिसने मासिक पत्र ‘देवनगर’ का प्रकाशन शुरू किया। ये सभी पत्र उसी प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते थे। इसके अलावा, पंडित जी ने उपन्यास ‘देवरानी-जेठानी की कहानी’ लिखी। पहली बार 1870 में इसका प्रकाशन मेरठ के जैनन प्रिंटिंग रूम में लिथो तकनीक (Leitho Method) से किया गया।
आचार्य कामचंद्र सुमन के अनुसार, दूसरा उपन्यास ‘हिंदी टीचर’ 1872 में मुंशी कल्याण राय और मुंशी ईश्वरी प्रसाद ने लिखा। यह उपन्यास लगभग 11 साल बाद, 1883 में, मेरठ के विद्यार्थी दर्पण पत्रिका के प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया। 19वीं सदी के अंत तक, इन साहित्यकारों के प्रयासों से, जो ख़ड़ी बोली और देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध था, बूलंदशहर ज़िले में हिंदी प्रकाशनों का एक प्रमुख केंद्र बन गया और उनका प्रसार तेज़ी से बढ़ने लगा।
प्रारंभिक समय में, मेरठ के अधिकतर प्रकाशक, पुराने तहसील क्षेत्र के आस-पास केंद्रित थे। इसके अलावा, वर्तमान सुभाष बाज़ार (सिपट बाज़ार) भी एक प्रमुख प्रकाशन केंद्र था।
मेरठ के प्रकाशन उद्योग में स्वामी तुलसीराम स्वामी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने, 1885 में, मेरठ में स्वामी प्रेस की स्थापना की। शुरू में यहाँ लिथो तकनीक से ही छपाई होती थी। स्वामी तुलसीराम, आर्य समाज के अध्यक्ष भी थे और समाज सुधार के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते थे।

फ़्लेक्सोग्राफ़िक प्रिंटिंग का परिचय
फ़्लेक्सोग्राफ़िक प्रिंटिंग, जिसे आमतौर पर फ़्लेक्सो कहा जाता है, प्रिंटिंग की सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली और बहुउपयोगी तकनीकों में से एक है। इस तकनीक का उपयोग अक्सर बड़ी मात्रा में छपाई (हाई-वॉल्यूम प्रिंटिंग) के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से पैकेजिंग सामग्री की छपाई के लिए उपयुक्त है, जहाँ इसकी लोकप्रियता काफ़ी अधिक है।
फ़्लेक्सोग्राफ़ी को रोटरी वेब लेटरप्रेस का एक आधुनिक रूप माना जाता है, जो लेटरप्रेस और रोटोग्रैवुर प्रिंटिंग दोनों की विशेषताओं को जोड़ती है। इस प्रक्रिया में लचीली फ़ोटोपॉलिमर प्रिंटिंग प्लेट्स का उपयोग किया जाता है, जिन्हें घुमने वाले सिलिंडरों पर लपेटा जाता है। ये स्याही से भरी प्लेटें, जिनमें छपाई के लिए हल्की उभरी हुई छवि होती है, तेज़ गति से घुमाई जाती हैं और छवि को सामग्री (सब्सट्रेट) पर स्थानांतरित करती हैं।
इस प्रिंटिंग तकनीक की सबसे बड़ी ख़ासियत, इसकी तेज़ी से सूखने वाली स्याही का उपयोग है, जो आमतौर पर पानी आधारित (वॉटर-बेस्ड) या यूवी-क्युरेबल होती है। इसकी वजह से यह तकनीक विभिन्न प्रकार की सतहों, चाहे वे छिद्रयुक्त हों या न हों, दोनों पर छपाई के लिए उपयुक्त बन जाती है।
फ़्लेक्सोग्राफ़िक प्रिंटिंग के अनुप्रयोग
फ़्लेक्सोग्राफ़िक प्रिंटिंग, अत्यधिक लचीली होती है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए किया जा सकता है। इसमें खाद्य पैकेजिंग, पेय पदार्थों के कार्टन, वॉलपेपर, और फ़्लोरिंग के लिए लैमिनेट्स जैसी वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा, विशेष टैग्स और लेबल्स—साधारण स्टिकर्स से लेकर जटिल सुरक्षा टैग्स तक—भी फ़्लेक्सो प्रिंटिंग की सीमा में आते हैं।
यह तकनीक विभिन्न प्रकार की सतहों पर छपाई का समर्थन करती है, जैसे कागज़, फ़ॉयल्स, फ़िल्म्स, और नॉन-वोवन्स, जिससे फ़्लेक्सो मशीनें पैकेजिंग और डेकोर अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनती हैं। तेज़ी से चलने वाली उपभोक्ता वस्तुओं (FMCG) के क्षेत्र में कंपनियाँ अपनी पैकेजिंग के लिए अक्सर फ़्लेक्सोग्राफ़ी पर निर्भर रहती हैं, क्योंकि इसका लचीलापन, छपाई की गुणवत्ता, और दक्षता इसे एक आदर्श विकल्प बनाती है।
भारत में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रिंटिंग मशीनें

1.) डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस: यह छोटे से मध्यम रन के लिए बिल्कुल सही है। इस प्रकार के प्रिंटरों को कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत कम समय लगता है और फिर भी वे पूर्ण-रंगीन प्रिंट का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। डिजिटल इंकजेट प्रिंटर, कागज़, प्लास्टिक, कैनवास, या यहां तक कि दरवाज़े और फ़र्श की टाइलों सहित विभिन्न प्रकार के सबस्ट्रेट्स पर प्रिंट कर सकते हैं।
डिजिटल प्रिंटिंग की सेटअप लागत कम है जो इसे छोटे प्रिंट रन के लिए भी एक बढ़िया विकल्प बनाती है। हालांकि, किसी भी प्रिंटिंग प्रेस की तरह, आपके प्रिंट की गुणवत्ता मशीन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, और ऐसी मशीनों की तलाश करना महत्वपूर्ण है जो सब्सट्रेट को लगातार फीड कर सकें।
इन-लाइन इंकजेट प्रिंटर को कभी-कभी वैरिएबल डेटा प्रिंट करने के लिए अन्य प्रकार के प्रेस के साथ जोड़ा जाता है, (जैसे डायरेक्ट मेल पीस पर मेलिंग एड्रेस) प्रिंट किया जा सके।
2.) स्क्रीन प्रिंटिंग प्रेस: 1960 के दशक से, स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में तकनीकी और सामग्री के सुधार के साथ काफ़ी बदलाव आए हैं। इस प्रक्रिया में एक स्क्रीन का उपयोग किया जाता है जिसे कपड़े के एक टुकड़े में बुना जाता है। इस जाल के कुछ हिस्सों को एक गैर-प्रवेशी सामग्री से कोट किया जाता है, जिससे स्याही को जाल के खुले हिस्सों से सब्सट्रेट पर डाला जा सकता है।
स्क्रीन प्रिंटिंग की विशेषता यह है कि प्रिंटिंग, सतह समतल नहीं होनी चाहिए और स्याही विभिन्न प्रकार की सामग्री, जैसे कागज़, वस्त्र, कांच, सिरेमिक, लकड़ी और धातु पर चिपक सकती है। स्क्रीन प्रिंटिंग के दो प्रकार होते हैं: फ़्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग और रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग, जिनमें प्रक्रिया में हल्का अंतर होता है।
- फ़्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग: इस प्रक्रिया के दौरान, उजागर स्क्रीन को चुने हुए सब्सट्रेट के शीर्ष पर व्यवस्थित किया जाता है। फिर स्याही को स्क्वीजी के सामने जमा किया जाता है। स्क्वीजी (squeegee) फिर स्क्रीन पर चलती है, इस प्रकार स्याही को जाल के माध्यम से धकेलती है और एक प्रिंट बनाती है।
- रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग: रोटरी स्क्रीन प्रक्रिया थोड़ी भिन्न होती है। स्क्वीजी को स्क्रीन के ऊपर ले जाने के बजाय, यह स्क्रीन के अंदर स्थिर होता है। स्क्वीजी और स्क्रीन पर आई टी आर लगाया जाता है, और स्याही डाली जाती है। जब लगा हुआ सिलेंडर घूमता है, तो स्याही को स्क्वीजी के माध्यम से जाली के माध्यम से धकेला जाता है। सब्सट्रेट स्क्रीन के बाहर चला जाता है और स्याही प्राप्त करता है, जिससे एक प्रिंट बनता है।

3.) इंकजेट प्रिंटिंग: यह औद्योगिक प्रिंटिंग मशीनों का एक वर्ग है, जिसमें इंकजेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें डिजिटल छवि को कागज़, प्लास्टिक, या अन्य सामग्री पर स्याही की बूंदों को फेंककर बनाया जाता है। ये प्रिंटर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्रकार के प्रिंटर होते हैं, जो छोटे, सस्ते उपभोक्ता मॉडल से लेकर महंगे पेशेवर मशीनों तक उपलब्ध होते हैं।
इंकजेट प्रिंटर सस्ते और उपयोग में आसान होते हैं। ये जल्दी चालू हो जाते हैं और इनकी कार्यप्रणाली बहुत शांत होती है। हालांकि, इनकी एक कमी यह है कि प्रिंट हेड की टिकाऊपन कम होती है और यह जल्दी सूख सकता है, जिससे स्याही की बर्बादी और प्रिंटर में ब्लॉकेज हो सकता है। ये उच्च वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त नहीं होते।
4.) लेटरप्रेस प्रिंटिंग मशीनें: इन्हें राहत या टाइपोग्राफ़िक प्रिंटिंग मशीन भी कहा जाता है। ये इमेजेज की प्रतियां बनाने के लिए स्याही लगी उभरी हुई सतह को कागज़ की शीट्स या रोल्स पर बार-बार सीधे दबाकर उपयोग की जाती हैं। लेटरप्रेस प्रिंटिंग में प्रयुक्त पदार्थों में वही सामग्री होती है जो लिथोग्राफ़ी में इस्तेमाल होती है, जैसे फिल्म डेवेलपर्स, स्याही, और ब्लैंकेट और रोलर वॉशेस।
आजकल, ऑफ़सेट प्रिंटिंग मशीनें, लिथोग्राफ़िक प्रेस और फ़्लेक्सोग्राफ़िक प्रेस जैसे अधिक कुशल और उन्नत प्रिंटिंग प्रेस की वजह से लेटरप्रेस का उपयोग घट गया है, लेकिन फ़ोटोपॉलिमर प्लेट्स के उपयोग ने इसे 21वीं सदी में फिर से लोकप्रिय बना दिया है।
5.) ऑफ़सेट प्रिंटिंग: ऑफ़सेट प्रिंटिंग मशीनों का व्यापक रूप से उपयोग, विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। इसकी वॉल्यूम प्रोडक्शन और कागज़ की लागत के मामले में बेजोड़ गुणवत्ता के कारण, यह व्यावसायिक प्रिंटिंग तकनीक का सबसे प्रमुख रूप है। हालांकि इन मशीनों की सेटअप लागत अधिक होती है, प्रिंटिंग प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से सस्ती होती है।
ऑफ़सेट प्रिंटिंग मशीन को लिथोग्राफ़िक प्रिंटिंग भी कहा जाता है, और यह स्पष्ट, तेज़ और उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों के साथ उच्च वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए आदर्श है।
6.) 3D प्रिंटिंग: 3D प्रिंटिंग, नवीनतम तकनीक है और यह प्रिंटिंग की कई नई संभावनाओं को खोलता है। 3D प्रिंटिंग पारंपरिक रूप से कागज़ पर चित्र या टेक्स्ट प्रिंट करने के बजाय त्रि-आयामी वस्तुएं प्रिंट कर सकता है। यह कार्यात्मक हाथ के उपकरण या किसी भी ऐसी वस्तु को प्रिंट कर सकता है जो प्रिंटर में फ़िट हो।
3D प्रिंटर, वस्तुओं को समान आकार में पुन: उत्पन्न करने की क्षमता के कारण विशेष हैं। सबसे उन्नत 3D प्रिंटरों में लेज़र और धातु की धूल का उपयोग कर त्रि-आयामी वस्तुएं बनाई जाती हैं। 3D प्रिंटिंग तकनीक के विकास के साथ, हम शायद जल्द ही कुछ भी प्रिंट करने में सक्षम होंगे।
संदर्भ
https://tinyurl.com/yp6ykx9w
https://tinyurl.com/4c5x2p26
https://tinyurl.com/4kcmt793
https://tinyurl.com/4hkpvx5n
चित्र संदर्भ
1. बड़े प्रारूप के डिजिटल प्रिंटर (Large format digital printer) को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
2. एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. फ़्लेक्सोग्राफ़िक प्रिंटिंग प्रेस (Flexographic printing press) को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4 स्वचालित माउंटिंग मशीन पर लेज़रपॉइंटर्स (laser pointers) की सहायता से टेप पर फ़्लेक्सो



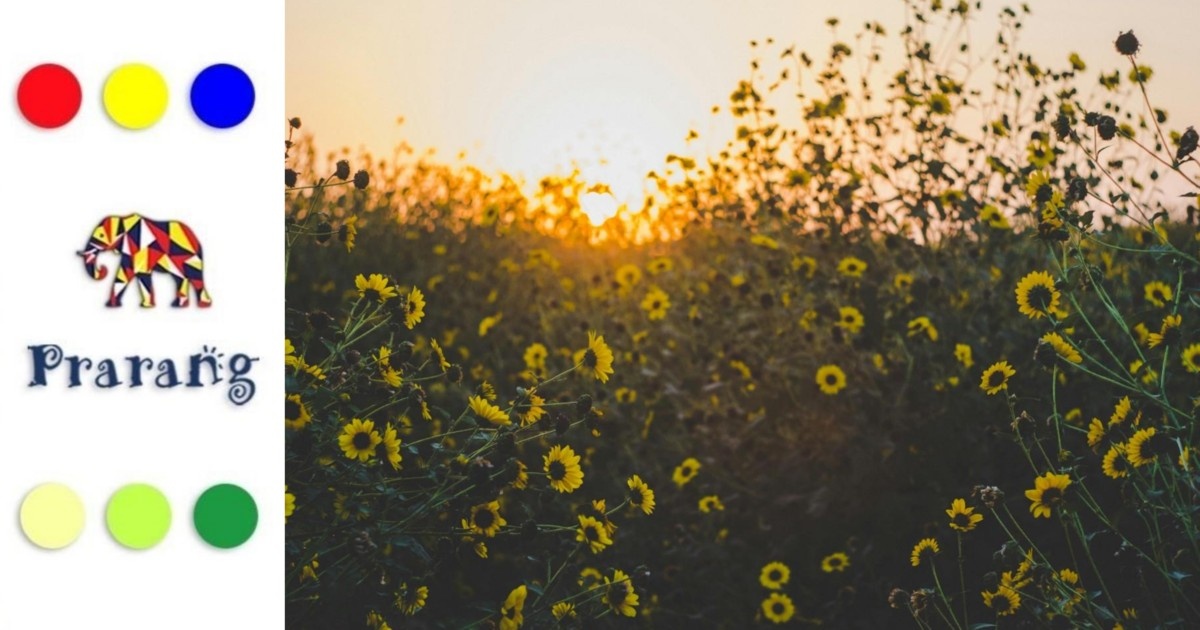

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.