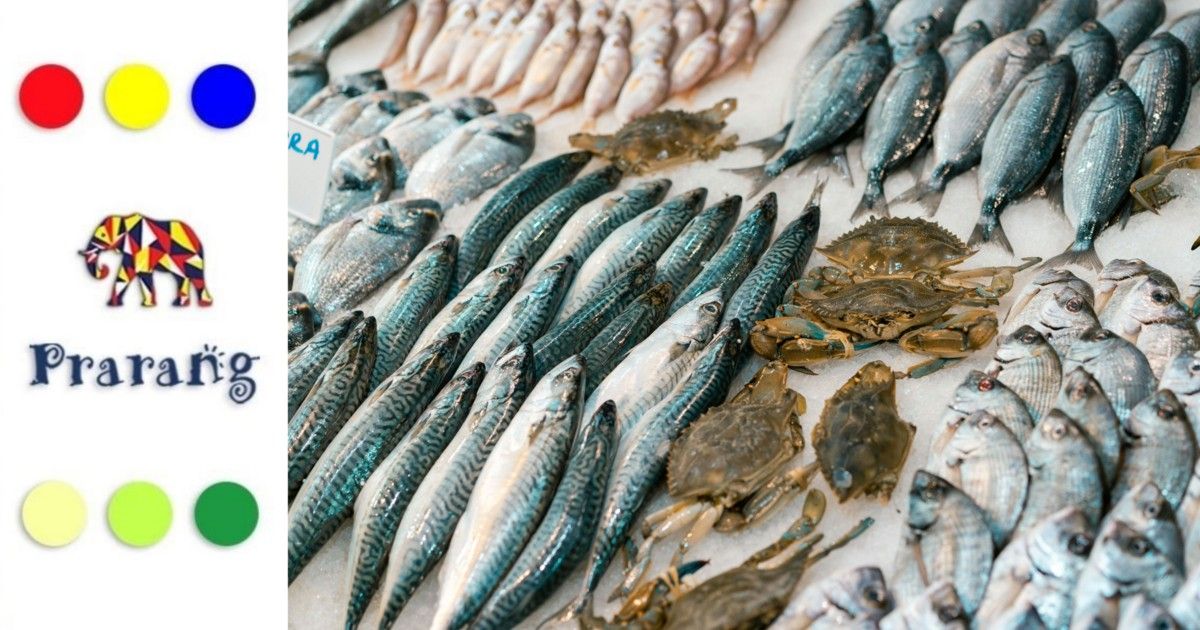2011 की जनगणना के अनुसार, मेरठ की लगभग 84% आबादी हिंदी बोलती है। इसका मतलब है कि, उस समय, कुल 13,05,429 की जनसंख्या में से 10,96,316 लोग हिंदी का उपयोग करते थे। हम सभी जानते हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में 48 मुख्य वर्ण होते हैं, जिनमें 14 स्वर और 34 व्यंजन शामिल हैं। यह लिपि प्राचीन ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अस्तित्व में थी। 8वीं शताब्दी ईस्वी तक यह लिपि, विकसित होकर सामान्य उपयोग में आ गई, और 1000 ईस्वी तक इसका आधुनिक रूप विकसित हुआ। आज देवनागरी, दुनिया में चौथी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली लिपि है, जिसका उपयोग 120 से अधिक भाषाओं में किया जाता है, जैसे मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत आदि।
तो, इस विश्व हिंदी दिवस पर, आइए हम देवनागरी लिपि और इसके उद्भव के बारे में विस्तार से जानें। इसके बाद, हम इस लिपि में प्राचीनतम मुद्रित ग्रंथों के बारे में जानेंगे। फिर, हम देवनागरी लिपि के ऐतिहासिक विकास पर ध्यान देंगे। इसके बाद, हम भारत में लिपि सुधारों के युग और 20वीं शताब्दी में देवनागरी में हुए परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे।
 देवनागरी लिपि का उद्भव
देवनागरी लिपि का उद्भव
देवनागरी लिपि का मूल ब्राह्मी लिपि से है, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में थी। इसका पूर्ववर्ती रूप नागरी लिपि था, जिसने नंदिनागरी को भी जन्म दिया। नागरी लिपि में मिले शुरुआती लेखों का काल, 1 से 4 शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है और इन्हें गुजरात, भारत में पाया गया है।
आधुनिक मानकीकृत देवनागरी का सबसे पुराना प्रमाण, लगभग 1000 ईस्वी का माना जाता है। इसके कुछ संस्करण भारत के बाहर भी पाए गए हैं, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, और इंडोनेशिया में।
शुरुआत में, देवनागरी का उपयोग, धार्मिक रूप से शिक्षित व्यक्तियों द्वारा जानकारी रिकॉर्ड करने और आदान-प्रदान करने के लिए किया जाता था।
संयुक्ताक्षर बनाने वाली क्षैतिज पट्टी की उपस्थिति, 992 ई.पू. में मानी जाती है, जिसका प्रमाण, बरेली के कुटिला शिलालेख में पाया गया है। कुटिला लिपि में देवनागरी का प्रारंभिक संस्करण शामिल है।
देवनागरी लिपि के शुरुआती मुद्रित उदाहरण
देवनागरी लिपि का सबसे पुराना मुद्रित उदाहरण 1667 में प्रकाशित ‘चाइना इलस्ट्रेटा’ (China Illustrata) नामक ग्रंथ में है, जिसे जर्मन मिशनरी अथानासियस किर्चर ने संकलित किया था। इस ग्रंथ में देवनागरी लिपि के उदाहरण मिलते हैं, जिनमें व्यक्तिगत अक्षर, अक्षरों के साथ जोड़ने वाली मात्राएँ, और छोटे उदाहरणात्मक पाठ शामिल हैं।
एक और महत्वपूर्ण शुरुआती मुद्रित उदाहरण 1678 के ‘हॉर्टस इंडिकस मलाबरिकस’ नामक ग्रंथ में है, जो एम्स्टर्डम में मुद्रित हुआ था और इसमें देवनागरी लिपि में लिखी हुई कोंकणी भाषा की एक धारा शामिल है।
देवनागरी लिपि का पहला धातु प्रकार 1740 में भारत से हजारों मील दूर रोम में कैथोलिक धर्म स्वीकार करने वाले भारतीयों द्वारा ढाला गया था। इसे 1771 में ‘ अल्फ़ाबेटम ब्राह्मणिकम’ नामक ग्रंथ में मुद्रित किया गया, जो देवनागरी फ़ॉन्ट में छपा हुआ हमारा सबसे पुराना प्रमाणित पाठ है। इस ग्रंथ में जो स्थानीय उदाहरण हैं, वे उस भाषाई विविधता को दर्शाते हैं, जिसे ब्रिटिश ‘हिंदुस्तानी’ के रूप में संदर्भित करते थे।
 देवनागरी लिपि का ऐतिहासिक विकास
देवनागरी लिपि का ऐतिहासिक विकास
जो देवनागरी लिपि आज के रूप में है (जो 7वीं सदी ईस्वी तक उभरने लगी थी), उसे संस्कृत से गहरे जुड़ाव के कारण विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। यह स्पष्ट नहीं है कि, यदि मुद्रित और आधुनिक समाज के लिए आवश्यक मानकीकरण प्रक्रिया न होती, तो भारतीय लिपियों का विकास, नए रूपों में कभी रुकता या नहीं। उदाहरण के लिए, हाल ही में, देवनागरी ने नए, क्षेत्रीय रूपों को जन्म दिया, जैसे कि गुजराती लिपि, जो यह संकेत करता है कि भारतीय लेखन में अक्षरों के आकार के विकास में कोई “अंतिम रूप” नहीं था। यह स्थिति, तब भी बनी रही, जब भारतीय लिपि उपयोगकर्ताओं को रोमन और अरबी वर्णमालाओं से परिचित कराया गया था, जो अपेक्षाकृत स्थिर थीं।
अक्षर रूपों में बदलाव, जो नई लिपियों की ओर बढ़ा, जो इतना धीमा था कि, पीढ़ी दर पीढ़ी, यह प्रक्रिया, एक लिपि से दूसरी लिपि में जानबूझकर परिवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि अक्षरों के निर्माण में धीरे-धीरे अंतर के रूप में दिखाई देती थी, जैसा कि समय के साथ, ग्रंथों की प्रतियां बनाई जाती थीं। इसी प्रकार का विकास मध्यकालीन यूरोप में लैटिन लिपि में हुआ था, लेकिन मुद्रण प्रेस के आविष्कार और पुनर्जागरण के विचारों ने यह सुनिश्चित किया कि लैटिन लिपि को कैसे दिखना चाहिए, जिससे टाइपोग्राफ़िक समरूपता आई।

ब्रिटिश भारत में लिपि सुधार और देवनागरी में बदलाव
भारत में जो मैकेनिकल प्रेस शुरू की गईं, उन्हें लैटिन लिपि को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, जिसमें बहुत छोटा वर्ण सेट है। सेट के आकार के अलावा, देवनागरी बहुत अधिक जटिल लिपि है। टाइपोग्राफ़रों को पूर्ण अक्षरों और संयुक्ताक्षरों के निर्माण के लिए आवश्यक सभी ग्रैफेम्स और संयोजनों को तैयार करने में एक चुनौती का सामना करना पड़ा। वे देवनागरी के डिज़ाइन और कार्यक्षमता के प्रति सच्चे बने रहने की कोशिश करते हुए, न्यूनतम संख्या में मैट्रिक्स के साथ काम कर रहे थे।
समस्याएँ तब बढ़ गईं जब मशीने, जैसे मोनोटाइप, लिनोटाइप और टाइपराइटर, सामने आईं। अब वे सीमित संख्या में मैट्रिक्स या टाइपराइटर के कीबोर्ड पर उपलब्ध सीमित संख्या में वर्णों से चुनौती का सामना कर रहे थे। असल में, देवनागरी लिपि के लिए, इस तकनीक के पास बहुत अधिक वर्ण थे। परिणामस्वरूप, मुद्रण, हस्तलेखन और टाइपिंग के लिए लिपि को मानकीकरण करने का दबाव बढ़ा। और इसी तरह देश में ‘लिपि सुधारों का युग’ की शुरुआत हुई।
लिपि सुधारकों ने सम्मेलनों और समितियों के माध्यम से कई विचारों और प्रणालियों का प्रस्ताव किया। वे थे:
1.) उन भाषाओं के लिए रोमन या लैटिन लिपि को अपनाना, जो वर्तमान में देवनागरी का उपयोग करती हैं।
2.) यांत्रिक प्रेसों पर काम करने के लिए देवनागरी लिपि में संशोधन और सरलीकरण।
3.) मशीनों को इस लिपि के अनुरूप बनाने और देवनागरी अक्षरों की विशेषताओं को समायोजित करने के लिए बदलाव।
संदर्भ
https://tinyurl.com/ct8u243t
https://tinyurl.com/3p5tekvh
https://tinyurl.com/ykdvvat4
https://tinyurl.com/5tnpph3e
चित्र संदर्भ
1. देवनागरी लेखन और एक उपनिषद को संदर्भित करता एक चित्रण (प्रारंग चित्र संग्रह, wikimedia)
2. देवनागरी लिपि के अक्षरों को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. हिंदी साहित्य की एक हस्तलिपि को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. हिंदी में टाइप करने के लिए एक कीबोर्ड को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)