
समय - सीमा 289
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1064
मानव और उनके आविष्कार 837
भूगोल 267
जीव-जंतु 321
समय - सीमा 289
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1064
मानव और उनके आविष्कार 837
भूगोल 267
जीव-जंतु 321
| Post Viewership from Post Date to 08- May-2025 (31st) Day | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 3112 | 46 | 0 | 3158 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

मेरठ के कई निवासी इस तथ्य से सहमत होंगे कि, पूरे इतिहास में पृथ्वी का बढ़ता तापमान, हिमनदों को पिघलाने के लिए ज़िम्मेदार है। विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित विज्ञान जर्नल – नेचर (Nature) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में दुनिया भर के हिमनद, ग्रीनलैंड (Greenland) या अंटार्कटिक हिम विस्तार (Antarctic ice sheets) की तुलना में अधिक द्रव्यमान खो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि, 2000 से 2019 के बीच दुनिया के सभी हिमनदों ने, हर वर्ष लगभग 267 बिलियन टन बर्फ़ खो दिया है। तो आज, हम हिमनदों के पिघलने के पीछे मौजूद कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा, हम दुनिया भर में विभिन्न हिमनदों द्वारा खोए हुए बर्फ़ द्रव्यमान का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद, हम पर्यावरण पर इनके पिघलने से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर कुछ प्रकाश डालेंगे। अंत में, हम इस समस्या से निपटने के लिए, कुछ समाधानों और उपायों का सुझाव देंगे।
हिमनद क्यों पिघल रहे हैं ?
1900 के दशक की शुरुआत से, दुनिया भर के कई हिमनद तेज़ी से पिघल रहे हैं। मानव गतिविधियां इस घटना की जड़ हैं। विशेष रूप से, औद्योगिक क्रांति के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैस (Greenhouse gas) उत्सर्जन ने पृथ्वी का तापमान बढ़ा दिया है। यह तापमान ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक बढ़ा है, और परिणामस्वरूप, हिमनद तेज़ी से पिघल रहे हैं। इससे इनका पानी समुद्र में जा रहा है, और हिमनद भूमि पर अपनी जगह से पीछे हट रहे हैं।
अगर हम आने वाले दशकों में गैस उत्सर्जन पर अंकुश भी लगाते हैं, तो भी दुनिया के शेष हिमनदों का एक तिहाई से अधिक हिस्सा, वर्ष 2100 से पहले पिघल जाएगा। जब समुद्री बर्फ़ के पिघलने की बात आती है, तो आर्कटिक (Arctic) में सबसे पुरानी और मोटी बर्फ़ का 95% पहले से ही चला गया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि, यदि उत्सर्जन अनियंत्रित रूप से बढ़ता रहता है, तो 2040 तक आर्कटिक गर्मियों में बर्फ़ मुक्त हो सकता है।
पिछले दो दशकों में, हिमनदों ने दुनिया भर में कितना द्रव्यमान खो दिया है ?
| क्षेत्र | ग्लेशियर हानि में प्रतिशत योगदान (% में) | द्रव्यमान की हानि (गीगाटन(Gt) में) |
| अलास्का(Alaska) | 25 | 68 |
| ग्रीनलैंड(Greenland) के बाहरी क्षेत्र | 13 | 36 |
| उत्तरी आर्कटिक कनाडा(Arctic Canada) | 10 | 31 |
| दक्षिणी आर्कटिक कनाडा (Southern Arctic Ecozone) | 10 | 27 |
| अंटार्कटिक(Antarctic) और उप-अंटार्कटिक क्षेत्र | 8 | 21 |
| एशिया(Asia) के उच्च पर्वतीय क्षेत्र | 8 | 21 |
| दक्षिणी एंडीज़ पर्वत(Andes mountains) | 8 | 21 |
मनुष्यों और समाज पर हिमनद के पिघलने के प्रभाव:
1.) समुद्र स्तर में वृद्धि और तटीय क्षेत्रों में बाढ़:
ग्लेशियरों का सबसे बड़ा और सबसे उल्लेखनीय प्रभाव, पिघलना है। 1960 के दशक के बाद से कुल समुद्र स्तर, 2.7 सेंटीमीटर बढ़ गया है। दुनिया के ग्लेशियरों में अभी भी, समुद्र स्तर को 1.5 मीटर तक बढ़ाने की क्षमता है, जो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बन सकता है।
2.) महासागर-आधारित उद्योगों का पतन:
इन धाराओं और जेट स्ट्रीमों (Jet streams) के भंग के माध्यम से, एक बड़े पैमाने पर महासागर को बदला जा रहा है। यह प्रभाव, मछली पकड़ने के उद्योगों के पतन जैसे परिणामों के साथ, हमारे सामने खड़ा है।
3.) प्रजातियों का नुकसान:
विभिन्न प्राणी व वनस्पति प्रजातियां भी जोखिम में हैं। कई भूमि और समुद्री जानवर, ग्लेशियरों पर अपने प्राकृतिक आवासों के रूप में निर्भर हैं, और जब वे गायब हो जाते हैं, तो समृद्ध पारिस्थितिक जीवन को खतरा होता हैं।
4.) मीठे पानी की हानि:
ग्लेशियर पिघलने का एक अन्य प्रभाव, मीठे पानी का नुकसान है। कम बर्फ़ मतलब, मीठे पानी का कम संचय है। फिर चाहे वह पानी, पीने के लिए हो, पनबिजली के लिए हो या सिंचाई के लिए हो।
ग्लेशियरों के पिघलने से बचने हेतु समाधान:
1.)जलवायु परिवर्तन को रोकें: जलवायु परिवर्तन को रोकने और ग्लेशियरों को बचाने के लिए, यह अपरिहार्य है कि, अगले दशक में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (Carbon dioxide emissions) 45% कम हो जाए, और 2050 के बाद यह शून्य हो जाए।
2.)ग्लेशियरों के कटाव को धीमा करना: वैज्ञानिक पत्रिका – नेचर (Nature) ने याकबशौवेन ग्लेशियर(Jakobshavn glacier)(ग्रीनलैंड) के सामने, एक 100 मीटर लंबे बांध का निर्माण करने का सुझाव दिया। यह ग्लेशियर आर्कटिक बर्फ़ पिघलने से सबसे खराब प्रभावित है।
3.)कृत्रिम हिमखंडों को मिलाएं: इंडोनेशियाई वास्तुकार (Indonesian architect) फ़ारिस राजक कोतहातुहा (Faris Rajak Kotahatuhaha) ने एक परियोजना पर काम किया, जिसमें आर्कटिक को फिर से बनाया गया था। इसमें पिघले हुए ग्लेशियरों से पानी इकट्ठा करना शामिल है, जिसे डीसैलिनेट (Desalinating) करना और बड़े बर्फ़ ब्लॉकों को बनाने के लिए उन्हें जमाना शामिल है। इन हिमखंडों को तब, जमे हुए द्रव्यमान बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है।
4.)ग्लेशियरों की मोटाई बढ़ाएं: एरिज़ोना विश्वविद्यालय (University of Arizona) ने एक सरल समाधान प्रस्तावित किया है: अधिक बर्फ़ का निर्माण। उनके प्रस्ताव में ग्लेशियर के नीचे से बर्फ़ इकट्ठा करना होता है। इसे ऊपरी बर्फ़ छादन पर फ़ैलाने के लिए, पवन ऊर्जा द्वारा संचालित पंपों का उपयोग किया जाता है।
संदर्भ
मुख्य चित्र: नॉर्वे में स्थित ब्रिक्सडल ग्लेशियर (Briksdal glacier) का एक दृश्य, जिसमें ग्लेशियर के पिघलने और उजागर चट्टानों के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं (Wikimedia)




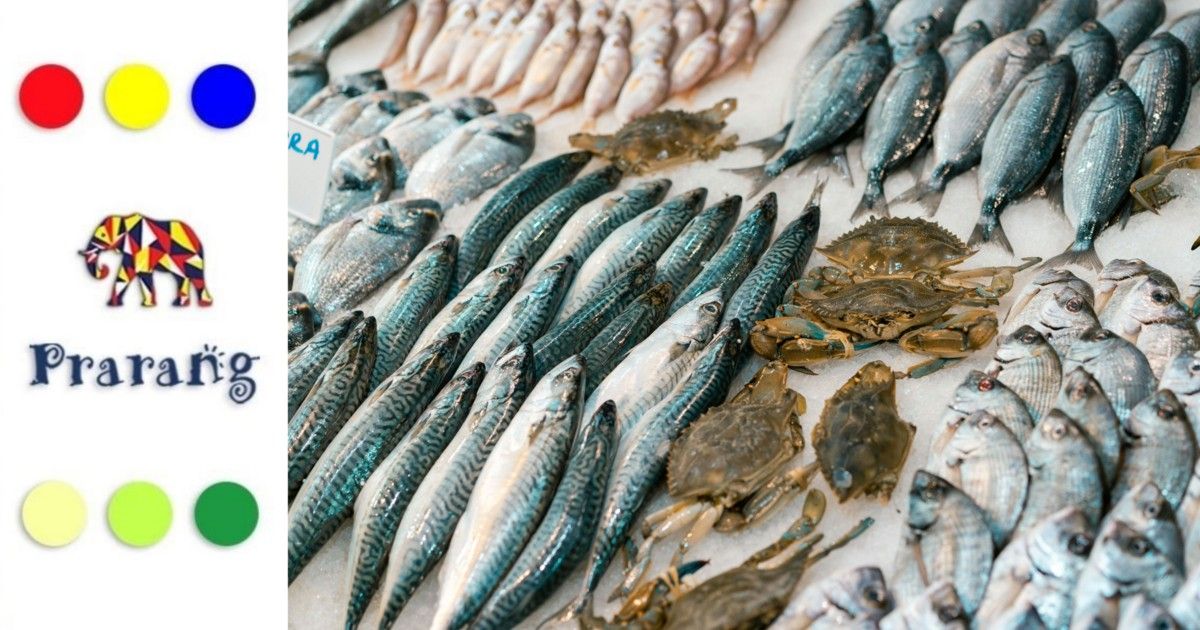
A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.