
समय - सीमा 289
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1064
मानव और उनके आविष्कार 837
भूगोल 267
जीव-जंतु 321
| Post Viewership from Post Date to 27- Jul-2025 (31st) Day | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 2829 | 54 | 10 | 2883 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

वन हमारे पारिस्थितिक तंत्र का आधार स्तंभ हैं। वे न केवल जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करते हैं, बल्कि मानव जीवन के लिए आवश्यक अनेक सेवाएं भी प्रदान करते हैं — जैसे जलवायु संतुलन, जल संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण, और स्वच्छ वायु। इसके साथ ही वन आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे लाखों लोगों की आजीविका का साधन हैं और जैव-अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। बदलते समय में वनों की भूमिका सिर्फ पारंपरिक उपयोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे नीति, निवेश और आजीविका से जुड़े मुद्दों का भी प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। आज हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे कि वनों की जैव विविधता में भूमिका क्या है और ये विभिन्न प्रजातियों के लिए जीवनदायिनी स्थान कैसे प्रदान करते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि वन अर्थव्यवस्था में वनों का आर्थिक योगदान किस प्रकार से होता है और इसमें राज्य सरकारों की क्या योजनाएँ हैं। फिर, हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में राज्य स्तरीय निवेश और योजनाओं के माध्यम से किस तरह हरित आवरण बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, हम जानेंगे कि सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय आजीविका वनों के सतत विकास में कैसे सहायक सिद्ध हो रही है। अंत में, हम विश्लेषण करेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों में वन क्षेत्र की स्थिति क्या है और वर्तमान वन प्रबंधन में क्या चुनौतियाँ हैं तथा सुधार की क्या आवश्यकता है।

वनों की जैव विविधता में भूमिका
वन केवल पेड़ों का समूह नहीं हैं, बल्कि ये जैव विविधता के सबसे प्रमुख आश्रय स्थल हैं। वनों में हजारों प्रकार के पौधे, जीव-जंतु, सूक्ष्म जीव और कीट रहते हैं, जो पृथ्वी की पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अनुमान के अनुसार, विश्व की लगभग 80% स्थलीय प्रजातियाँ वनों में निवास करती हैं। इसमें स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर और कीट वर्ग के लाखों जीव सम्मिलित हैं।
वनों में जैव विविधता का संरक्षण न केवल पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से आवश्यक है, बल्कि यह मानव समाज की खाद्य सुरक्षा, औषधियों की उपलब्धता और जलवायु नियंत्रण में भी सहायक है। जैव विविधता जलचक्र को संतुलित रखने, मृदा अपरदन को रोकने तथा प्रदूषण नियंत्रण में योगदान देती है।
वनों की विविधता में उष्णकटिबंधीय वर्षावन (Tropical Rainforests) सबसे आगे हैं। उदाहरणस्वरूप, अमेज़न वर्षावन अकेले ही लगभग 16,000 वृक्ष प्रजातियों और 390 अरब वृक्षों का घर है। भारत में भी पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र अत्यधिक जैव विविध वनों के रूप में चिन्हित किए गए हैं।
वनों की जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक प्राकृतिक कवच है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ग्रीनहाउस गैसों को संतुलित करती है। इसलिए, जैव विविधता को बनाए रखना वैश्विक जलवायु लक्ष्य हासिल करने के लिए अनिवार्य है।
वन अर्थव्यवस्था में वनों का आर्थिक योगदान
वनों का आर्थिक महत्व केवल लकड़ी तक सीमित नहीं है। वनों से प्राप्त गैर-काष्ठ वन उत्पाद (NTFPs) जैसे शहद, बांस, लाख, औषधीय पौधे, रेजिन, गोंद, और जड़ी-बूटियाँ ग्रामीण वनों पर निर्भर समुदायों के लिए एक स्थायी आय का स्रोत हैं। भारत में लगभग 275 मिलियन लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वनों से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं।
वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो वनों का सालाना आर्थिक मूल्य लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर आँका गया है। यह मूल्य केवल उत्पादों के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि वनों की पर्यावरणीय सेवाओं जैसे जल संरक्षण, मृदा सुरक्षा, पर्यटन और जलवायु नियंत्रण से जुड़ा है।
भारत सरकार के अनुसार, वन उत्पादों का संग्रहण और विपणन अबतक अनौपचारिक रूप से होता आया है, जिससे इसका आर्थिक योगदान स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाया। लेकिन हाल के वर्षों में सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा वन आधारित उद्योगों में निवेश करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इससे वन उत्पादों का स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन संभव हुआ है और ग्रामीण समुदायों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।
जैव-अर्थव्यवस्था, जिसमें जैव संसाधनों का उपयोग कर नवाचार और उत्पादन किया जाता है, वन आधारित संसाधनों की संभावनाओं को और भी बढ़ा रही है। उदाहरण के लिए, बांस आधारित उद्योगों में चीन और भारत में तेजी से वृद्धि हो रही है।

राज्य स्तरीय निवेश और योजनाएँ (विशेष रूप से उत्तर प्रदेश)
उत्तर प्रदेश सरकार ने वन अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं और निवेश पहलों की शुरुआत की है। 2030 तक राज्य के हरित क्षेत्र को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। वर्तमान में राज्य का कुल वनावरण लगभग 9.23% है, जिसे बढ़ाने हेतु सरकार ने बहुपक्षीय रणनीति अपनाई है।
राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में 350 मिलियन पौधे लगाने का संकल्प लिया था, जिसमें सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दिया गया। इसके लिए 600 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान बजट में किया गया था। इसके अतिरिक्त, नर्सरी प्रबंधन योजना के अंतर्गत 175 करोड़ रुपये, पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 10 करोड़ रुपये तथा कुकरैल वन क्षेत्र में रात्रि पर्यटन हेतु 50 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे।
‘ग्रीन इंडिया मिशन’ के तहत उत्तर प्रदेश को 100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इसके माध्यम से पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना, जैव विविधता संरक्षण और आजीविका संवर्द्धन के कार्य किए जा रहे हैं।
वन आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु 'राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन' के अंतर्गत 114 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ, कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपये का निवेश भी प्रस्तावित है, जिससे युवा नवप्रवर्तकों को कृषि-वानिकी से जोड़ने का अवसर मिलेगा।
सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय आजीविका
वनों के सतत प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार ने 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी है, जिससे ग्राम स्तरीय समितियाँ वनों का प्रबंधन कर सकती हैं।
वन संसाधनों पर निर्भर समुदाय, जैसे कि आदिवासी, अन्य परंपरागत वनवासी और सीमांत किसान, वनों से न केवल खाद्य, औषधि, ईंधन और चारा प्राप्त करते हैं, बल्कि इनके माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता भी हासिल करते हैं।
भारत में लगभग 200 मिलियन लोग वनों से प्राप्त संसाधनों पर निर्भर हैं। यह समुदाय अक्सर मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से कटे रहते हैं, अतः वन उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन में सामुदायिक उद्यमों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।
‘कृषक उत्पादक संगठन’ (FPO) जैसे मॉडल को अपनाकर वन उत्पादकों को बाज़ार से जोड़ा जा सकता है। वन आधारित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को प्रशिक्षण, वित्त और विपणन समर्थन प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है।
गुजरात जैसे राज्यों में सामुदायिक वन प्रबंधन के तहत बांस उत्पादन और आपूर्ति में समुदायों की भागीदारी से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। ऐसे मॉडल अन्य राज्यों में भी लागू किए जा सकते हैं।

राज्यों के अनुसार वन क्षेत्र की स्थिति
भारत ने 2011-2021 के दशक में वन क्षेत्र में 3.14% की वृद्धि दर्ज की है। कुल वन आवरण अब 7,13,789 वर्ग किमी है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24% है।
वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, मध्य प्रदेश (11%) का वन क्षेत्र सबसे अधिक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश (9%), छत्तीसगढ़ (8%), ओडिशा (7%) और महाराष्ट्र (7%) का स्थान है।
वन आवरण के प्रतिशत के अनुसार देखें तो पूर्वोत्तर के राज्य शीर्ष पर हैं – मिजोरम (85%), अरुणाचल प्रदेश (79%), मेघालय (76%), मणिपुर (74%) और नागालैंड (74%)।
बहुत घने जंगलों की वृद्धि सर्वाधिक रही है – 2011 से 2021 के बीच लगभग 20% की वृद्धि। खुले वनों में 7% की वृद्धि जबकि मध्यम घने जंगलों में गिरावट देखी गई है।
हालांकि यह वृद्धि आंशिक रूप से वृक्षारोपण और गैर-पारंपरिक वन क्षेत्रों में वृक्षों की गणना के कारण भी हुई है, जिस पर कुछ विशेषज्ञों ने आलोचना भी की है। फिर भी, भारत की वैश्विक स्थिति सुदृढ़ हुई है – विश्व स्तर पर वन क्षेत्र वृद्धि दर में भारत तीसरे स्थान पर है।
वन प्रबंधन में चुनौतियाँ और सुधार की आवश्यकता
वन प्रबंधन में कई जटिलताएँ विद्यमान हैं। इनमें प्रमुख हैं – अवैध कटाई, वनों का क्षरण, वन भूमि का अन्य उपयोगों में परिवर्तन, और वनवासियों की उपेक्षा।
वन उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला का पहला स्तर आज भी अनौपचारिक और बिखरा हुआ है, जिससे न तो उत्पादकों को उचित मूल्य मिल पाता है और न ही सरकार को राजस्व।
वन विभागों में आधुनिक तकनीकी ज्ञान, भू-स्थानिक सूचना प्रणालियों (GIS), रिमोट सेंसिंग, और डेटा एनालिटिक्स का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। इससे नीति निर्माण और निगरानी प्रभावित होती है।
वन कानूनों और नीतियों में पारदर्शिता तथा विकेंद्रीकरण की कमी भी एक प्रमुख समस्या है। वनों की रक्षा में लगे स्थानीय संरक्षकों को अधिकार और संसाधन देने की आवश्यकता है।
इसके लिए निम्नलिखित सुधार आवश्यक हैं:
निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश को प्रोत्साहन।



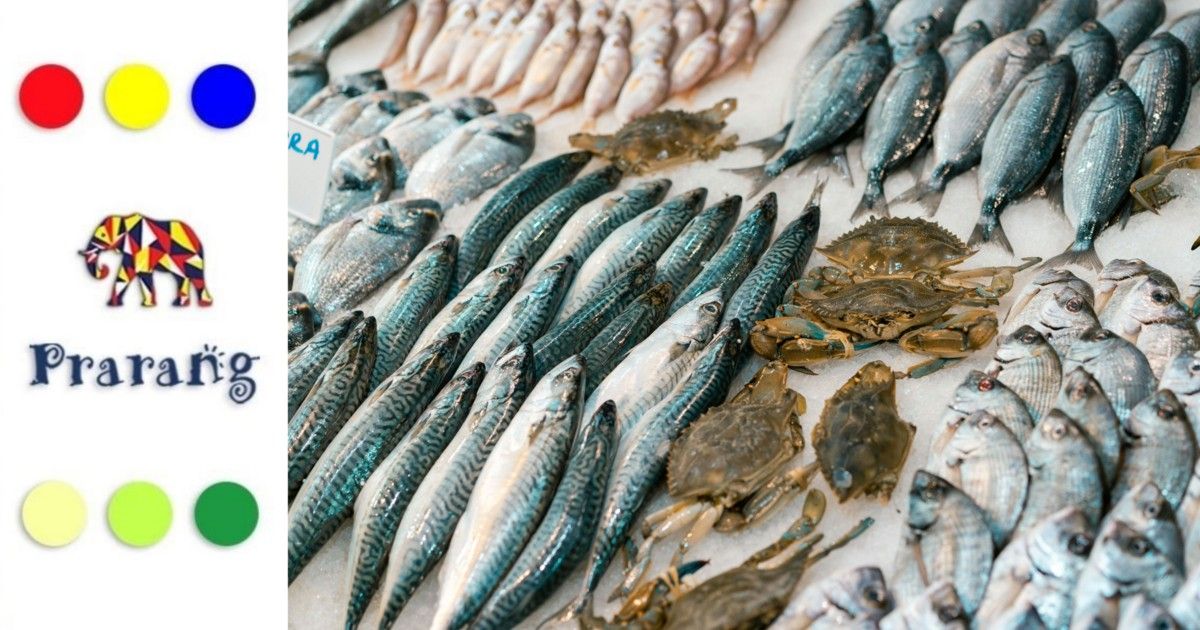

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.