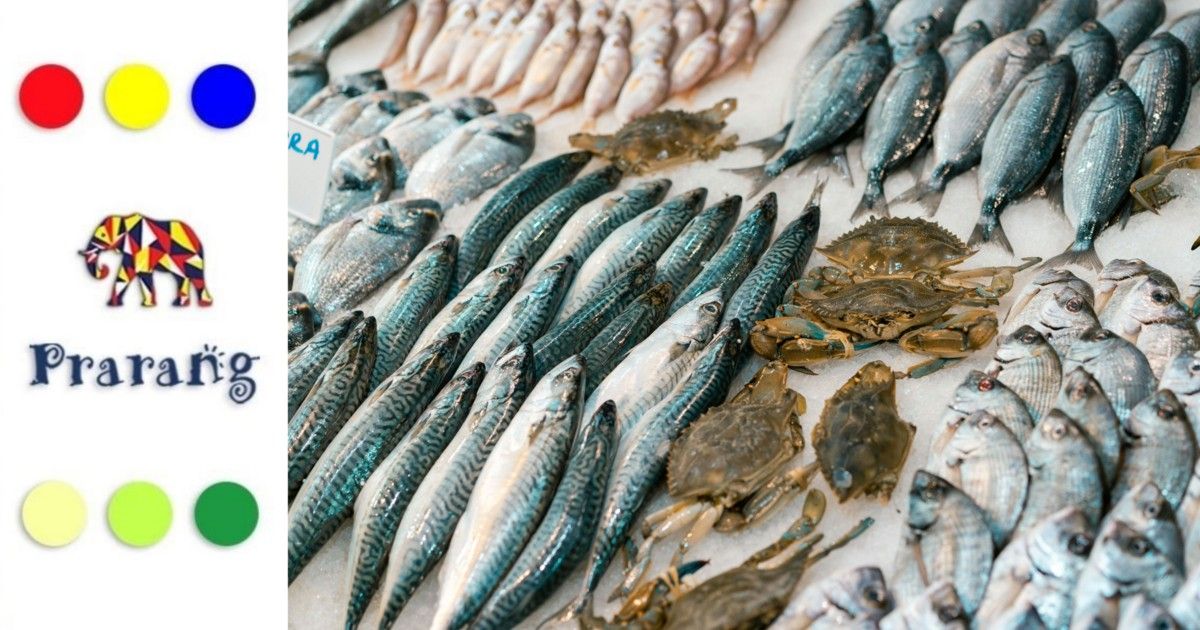समय - सीमा 289
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1064
मानव और उनके आविष्कार 836
भूगोल 267
जीव-जंतु 321
समय - सीमा 289
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1064
मानव और उनके आविष्कार 836
भूगोल 267
जीव-जंतु 321
| Post Viewership from Post Date to 05- Oct-2025 (31st) Day | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 2776 | 96 | 9 | 2881 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

मेरठवासियो, क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर कुछ ऐसे जीव भी हैं जो करोड़ों साल से अस्तित्व में हैं, लेकिन आज उनकी पहचान खतरे में पड़ गई है? इन्हीं रहस्यमय जीवों में से एक है बटागुर बास्का कछुआ, जिसे उत्तरी नदी टेरापिन (northern river terrapin) भी कहा जाता है। यह दुर्लभ और बेहद सुंदर कछुआ मुख्य रूप से सुंदरबन और ओडिशा की नदियों और मैंग्रोव (mangrove) इलाकों में पाया जाता है। कभी बड़ी संख्या में नदियों में तैरने वाला यह जीव अब सिर्फ गिनती के कुछ सौ कछुओं तक सिमट चुका है। प्रकृति की नाजुकता और मानव हस्तक्षेप के कारण ये कछुए आज विलुप्ति की कगार पर हैं।
इस लेख में हम बटागुर बास्का कछुए से जुड़ी पाँच प्रमुख बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले, हम इस दुर्लभ कछुए के परिचय और उसकी भौतिक विशेषताओं को जानेंगे, जिसमें इसका आकार, रंग और अन्य विशिष्ट गुण शामिल हैं। इसके बाद हम इसके प्राकृतिक आवास और जीवन शैली पर नज़र डालेंगे, जहां यह कछुआ मीठे और खारे पानी के बीच अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है। तीसरे भाग में हम इसके प्रजनन चक्र और अंडे देने की प्रक्रिया को समझेंगे, जो इसकी प्रजाति के अस्तित्व में अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद चौथे हिस्से में उन प्रमुख खतरों पर बात करेंगे, जिनकी वजह से यह प्रजाति आज विलुप्ति के कगार पर पहुँच गई है। अंत में, हम उन संरक्षण प्रयासों और उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे, जिनकी बदौलत इस अनोखे कछुए को बचाने की उम्मीद अब भी बनी हुई है।
बटागुर बास्का कछुए का परिचय और भौतिक विशेषताएँ
बटागुर बास्का कछुआ दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया की नदियों में पाया जाने वाला एक अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत जीव है। यह कछुआ अपने आकार और अनोखी शारीरिक बनावट के कारण अन्य प्रजातियों से अलग दिखाई देता है। इसकी लंबाई लगभग 55 से 60 सेंटीमीटर तक हो सकती है और वज़न 15 से 18 किलोग्राम तक पहुँचता है। इसके मजबूत और थोड़ा उभरे हुए खोल का रंग जैतून या भूरा होता है, जो इसे प्राकृतिक परिवेश में घुलने-मिलने में मदद करता है। नीचे का हिस्सा हल्के पीले रंग का होता है। सिर छोटा और थूथन आगे से नुकीला और हल्का ऊपर उठा होता है, जिससे यह आसानी से पानी में सांस लेने और भोजन खोजने में सक्षम होता है। इनकी सबसे खास बात यह है कि प्रजनन काल के दौरान इनका रंग बदल जाता है, नर कछुओं का सिर और गर्दन काले हो जाते हैं और पैरों पर लाल या नारंगी रंग की आभा आ जाती है। उनकी आंखों की पुतलियां भी इस समय बदलकर और चमकीली हो जाती हैं। यह बदलाव सिर्फ इन्हीं कछुओं में देखा जाता है, जिससे इनका स्वरूप अत्यंत आकर्षक और अनूठा हो जाता है।

प्राकृतिक आवास और जीवन शैली
बटागुर बास्का कछुआ मीठे और खारे दोनों तरह के पानी में रहने में सक्षम है। यह प्रजाति मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश के सुंदरबन डेल्टा (delta), ओडिशा के भितरकनिका अभयारण्य, म्यांमार, मलेशिया (Malaysia) और कंबोडिया (Cambodia) के तटीय इलाकों और बड़ी नदियों के मुहानों पर पाई जाती है। कभी ये सिंगापुर और थाईलैंड (Thailand) में भी पाए जाते थे, लेकिन अब वहां पूरी तरह लुप्त हो चुके हैं। ये कछुए सामान्य दिनों में नदी के शांत मीठे पानी में रहते हैं और प्रजनन के मौसम में खारे पानी वाले ज्वारीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। इनका भोजन पौधों के कोमल हिस्सों, बीजों और जलीय छोटे जीवों से बना होता है। इन्हें देखने का मौका बेहद दुर्लभ होता है क्योंकि ये स्वभाव से बहुत शर्मीले और सतर्क होते हैं। ये अक्सर पानी के भीतर या मैंग्रोव की झाड़ियों में छिपकर रहते हैं। इनकी धीमी चाल और सतर्क स्वभाव इन्हें इंसानों से दूर रखता है, और शायद इसी कारण यह प्रजाति हमारे लिए अब भी रहस्यमयी बनी हुई है।
प्रजनन चक्र और अंडे देने की प्रक्रिया
बटागुर बास्का का प्रजनन समय दिसंबर से मार्च तक चलता है। इस अवधि में नर कछुए रंग बदलकर और भी आकर्षक हो जाते हैं ताकि मादा को आकर्षित कर सकें। प्रजनन के बाद, मादा कछुआ नदी के किनारे पर किसी सुरक्षित रेतीले स्थान की तलाश करती है। वह एक बार में 10 से 34 अंडे देती है, जिसे वह तीन अलग-अलग बार में पूरा करती है। अंडे देने के बाद मादा उन्हें रेत में अच्छी तरह ढक देती है और अपने भारी शरीर से दबाकर मजबूत करती है। यह स्वाभाविक व्यवस्था अंडों को शिकारी जानवरों और लहरों से बचाती है। यह पूरा व्यवहार इस बात का उदाहरण है कि प्रकृति अपने हर जीव को जीवन देने का अवसर किस तरह देती है। अंडे देने के बाद मादा कछुआ बिना पीछे देखे पानी की ओर लौट जाती है और प्रकृति पर भरोसा करती है कि अगली पीढ़ी सुरक्षित रूप से जन्म लेगी।
इस प्रजाति के अस्तित्व के सामने प्रमुख खतरे
आज बटागुर बास्का का अस्तित्व कई गंभीर खतरों से जूझ रहा है। अतीत में इनके मांस और अंडों का बड़े पैमाने पर शिकार हुआ, जिससे इनकी संख्या तेजी से घट गई। औपनिवेशिक समय में इनका मांस एक खास व्यंजन माना जाता था। वर्तमान समय में इनके आवास का लगातार खत्म होना सबसे बड़ा खतरा है। प्रदूषण, नदियों में फैला प्लास्टिक कचरा, मैंग्रोव का कटना और जलवायु परिवर्तन से समुद्र का बढ़ता जल स्तर इनके प्राकृतिक घर को तेजी से नष्ट कर रहा है। इसके अलावा, अक्सर ये मछली पकड़ने के जाल में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। तापमान में लगातार वृद्धि ने इनकी प्रजनन प्रक्रिया को भी प्रभावित किया है क्योंकि ज्यादा तापमान पर अंडों से अधिक मादाएं पैदा हो रही हैं, जिससे नर-मादा का संतुलन बिगड़ रहा है। इस असंतुलन के कारण प्रजाति की आगे की पीढ़ियां संकट में हैं।

संरक्षण के लिए किए गए प्रयास और सफलताएँ
2018 में जब इनकी संख्या केवल 100 के आसपास रह गई, तब पश्चिम बंगाल के वन विभाग और कई संस्थाओं ने मिलकर इन कछुओं को बचाने की बड़ी मुहिम शुरू की। सजनेखाली द्वीप पर मिले कुछ कछुओं को सुरक्षित वातावरण में रखा गया और वहां कृत्रिम ऊष्मायन तकनीक (Artificial incubation) का उपयोग करके इनके अंडों को सेने का काम शुरू किया गया। इस प्रयास के बाद धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी। आज 2024 तक लगभग 430 कछुए नियंत्रित और सुरक्षित स्थानों पर पाले जा रहे हैं। 2022 में 10 कछुओं को उपग्रह निगरानी के साथ खुले जंगल में छोड़ा गया ताकि उनके व्यवहार और अनुकूलन क्षमता को समझा जा सके। परिणाम उत्साहजनक रहे, हालांकि बढ़ती लवणता और आवास के नुकसान जैसी चुनौतियां अब भी बाकी हैं। इन प्रयासों से उम्मीद की किरण जगी है कि यदि लगातार प्रयास किए जाएं तो एक दिन ये कछुए फिर से स्वतंत्र रूप से सुंदरबन की नदियों और मैंग्रोव में लौट सकते हैं।
संदर्भ-
A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.