
समय - सीमा 289
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1064
मानव और उनके आविष्कार 837
भूगोल 267
जीव-जंतु 321
समय - सीमा 289
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1064
मानव और उनके आविष्कार 837
भूगोल 267
जीव-जंतु 321
| Post Viewership from Post Date to 09- Oct-2025 (31st) Day | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 2547 | 102 | 13 | 2662 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

मेरठवासियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे शहर के पार्क, बाजार, स्कूल या सरकारी दफ्तरों में रखे गए रंग-बिरंगे कूड़ेदान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते? इनका असली उद्देश्य हमारे घरों और सार्वजनिक स्थानों से निकलने वाले कचरे को सही तरीके से अलग करना और उसे पुनर्चक्रण (recycling) के लिए तैयार करना है। आज जब मेरठ तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण का सामना कर रहा है, तो कचरे की मात्रा भी पहले से कई गुना बढ़ गई है। ऐसे में रंगीन कूड़ेदान व्यवस्था न केवल हमारे शहर की सफाई बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और संसाधनों के दोबारा इस्तेमाल की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इस तरह की प्रणाली से न केवल हमारे आस-पास की गंदगी कम होती है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ मेरठ बनाने की नींव भी रखी जाती है।
इस लेख में हम जानेंगे कि शहरों में बढ़ते कचरे से निपटने के लिए रंगीन कूड़ेदान क्यों और कैसे बनाए गए हैं। इसमें हम भारत में कचरे की स्थिति और उसके प्रकार, रंगीन कूड़ेदान के सही इस्तेमाल, आम गलतियों और जागरूकता की कमी, दुनिया भर में अपनाई गई रंगीन कूड़ेदान प्रणाली, अपशिष्ट प्रबंधन में 4R (4 आर) सिद्धांत की अहमियत, और सही निस्तारण से स्वच्छ शहर के लक्ष्य तक पहुँचने की बात करेंगे।

भारत में शहरी कचरे की स्थिति और प्रकार
भारत में शहरीकरण की रफ़्तार पिछले कुछ दशकों में इतनी तेज़ हुई है कि इसके साथ जुड़ी कचरे की समस्या भी दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है। आज हमारे शहर प्रतिदिन करीब 1.5 लाख टन ठोस कचरा पैदा करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 40–50% जैविक कचरे का होता है, जैसे सब्जियों के छिलके, बचे हुए खाने के टुकड़े, बगीचे की पत्तियाँ वगैरह। इसके अलावा 8–12% प्लास्टिक (plastic) कचरा है, जो सबसे कठिन चुनौती है क्योंकि यह न तो जल्दी नष्ट होता है और न ही मिट्टी में घुलता है। करीब 1% जैव-चिकित्सीय कचरा (दवाइयों के अवशेष, अस्पतालों का कचरा, प्रयोगशालाओं का कचरा) सीधे तौर पर स्वास्थ्य के लिए खतरा है। बाकी हिस्से में धातु, कांच, कपड़े, ई-कचरा (पुराना मोबाइल (mobile), लैपटॉप (laptop), बैटरी आदि) और अन्य ठोस अवशेष आते हैं। ई-कचरे में मौजूद सीसा (Lead), पारा (Mercury), कैडमियम (Cadmium) जैसे रसायन नदियों और भूजल को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे गंभीर बीमारियाँ फैल सकती हैं।

भारत में रंगीन कूड़ेदान प्रणाली और उनका उपयोग
भारत में चार मुख्य रंग के कूड़ेदान अपनाए गए हैं, और इनका सही उपयोग कचरा प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी जैसा है।
सामान्य गलतियां और जागरूकता की कमी
कई बार देखा जाता है कि लोग नियम जानते हुए भी उनका पालन नहीं करते। हरे कूड़ेदान में प्लास्टिक की बोतल डालना या नीले कूड़ेदान में बचा हुआ खाना डालना, ये छोटी-सी लगने वाली गलतियाँ पूरी व्यवस्था बिगाड़ देती हैं। जब गीला और सूखा कचरा मिल जाता है, तो पुनर्चक्रण करना मुश्किल हो जाता है और अंत में वह सब लैंडफिल (landfill) में चला जाता है। समस्या का एक बड़ा कारण जागरूकता की कमी है। कुछ लोग मानते हैं कि "कचरा तो बाद में सब मिला दिया जाता है, तो अलग करने का क्या फ़ायदा?" जबकि सच यह है कि सही तरह से अलग किया गया कचरा रीसायक्लिंग यूनिट (recycling unit) में सीधा इस्तेमाल हो सकता है। आलस्य और आदत में बदलाव की अनिच्छा भी एक वजह है।

अंतर्राष्ट्रीय रंगीन कूड़ेदान प्रणाली
दुनिया के कई विकसित देशों में कचरे को और अधिक बारीकी से अलग करने के लिए पाँच रंगों वाली प्रणाली अपनाई जाती है:
इस तरह की विस्तृत प्रणाली से न केवल पुनर्चक्रण की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि खतरनाक कचरे को समय पर और सुरक्षित तरीके से निपटाया जा सकता है। भारत में भी भविष्य में इस मॉडल (model) को अपनाने की संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए जनता में उच्च स्तर की जागरूकता और सरकारी बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी।
अपशिष्ट प्रबंधन में पृथक्करण और 4R सिद्धांत
कचरे के सही प्रबंधन का पहला कदम गीले और सूखे कचरे का अलगाव है। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर 4R सिद्धांत को अपनाना चाहिए:
अगर स्कूल, दफ्तर, और आवासीय सोसायटी (Residential Society) इस सिद्धांत पर काम करें, तो कचरे की मात्रा में 30–40% तक कमी आ सकती है।
सही कचरा निस्तारण और स्वच्छ शहर का लक्ष्य
कचरे का सही निस्तारण सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है। अगर हर व्यक्ति यह आदत डाल ले कि सही कचरा सही कूड़ेदान में ही डाले, तो न केवल हमारा शहर साफ़ रहेगा, बल्कि पर्यावरण पर दबाव भी कम होगा। सरकार और नगर निगम को चाहिए कि अधिक रंगीन कूड़ेदान लगाएं, समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाएं और कचरे को पुनर्चक्रण इकाइयों तक सही तरीके से पहुंचाएं। यह छोटा-सा बदलाव “स्वच्छ भारत मिशन” और “स्मार्ट सिटी” (Smart City) दोनों के सपनों को साकार कर सकता है।
संदर्भ-




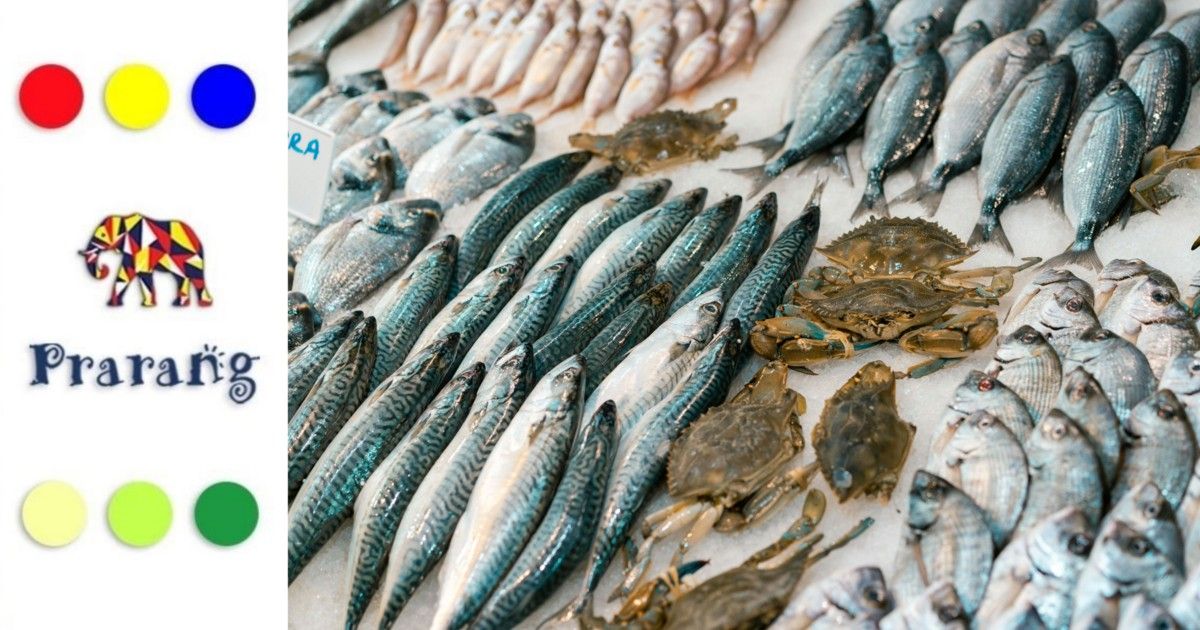
A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.