
समय - सीमा 288
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1058
मानव और उनके आविष्कार 829
भूगोल 262
जीव-जंतु 317
| Post Viewership from Post Date to 14- Nov-2025 (31st) Day | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 3360 | 76 | 5 | 3441 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

मेरठवासियो, आप सभी जानते हैं कि हमारा यह क्षेत्र खेती-बाड़ी, पशुपालन और दूध उत्पादन की परंपरा के लिए लंबे समय से प्रसिद्ध रहा है। गाँवों की गलियों से लेकर शहर की डेयरियों (dairies) तक, यहाँ के परिवारों का जीवन दूध और दुग्ध उत्पादों से गहराई से जुड़ा है। यही कारण है कि मेरठ न केवल शिक्षा और खेलों में अपनी पहचान रखता है, बल्कि दुग्ध उत्पादन में भी एक अहम योगदान देता है। भारत आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन चुका है, और इस उपलब्धि के पीछे मेरठ जैसे क्षेत्रों की मेहनत और परंपराएँ शामिल हैं। समय के साथ, दूध उत्पादन की पद्धतियों में बड़े बदलाव आए हैं - जहाँ पहले केवल परंपरागत गाय-भैंसों पर निर्भरता थी, वहीं अब पशु संकरण और आधुनिक ट्रांसजेनिक (Transgenic) तकनीकें सामने आई हैं। इन नई विधियों ने किसानों के लिए अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक दूध की राह खोली है।
इस लेख में हम क्रमवार समझेंगे कि भारत में दूध उत्पादन क्यों महत्वपूर्ण है और पशु संकरण ने इसमें कैसी भूमिका निभाई है। फिर हम जानेंगे कि विदेशी और संकरित गायों की हिस्सेदारी कैसे लगातार बढ़ रही है। इसके बाद हम स्वदेशी और संकर गायों के बीच उत्पादन की तुलना करेंगे और इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। आगे चलकर हम ट्रांसजेनिक गायों और उनके दूध की पौष्टिकता के बारे में विस्तार से देखेंगे, साथ ही यह भी जानेंगे कि इस तकनीक को बनाने के कौन-कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। अंत में, हम इसकी संभावनाओं और इससे जुड़ी नैतिक चुनौतियों पर विचार करेंगे।

भारत में दूध उत्पादन और पशु संकरण की भूमिका
भारत में दूध उत्पादन केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का आधार है। ‘एफएओस्टेट’ (FAOSTAT) के आँकड़ों के अनुसार, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। यह उपलब्धि अचानक नहीं मिली, बल्कि वर्षों से चली आ रही मेहनत, परंपरा और वैज्ञानिक तरीकों के मेल से संभव हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दूध न केवल पोषण का प्रमुख स्रोत है, बल्कि यह किसानों के लिए नक़दी कमाने का भी अहम साधन है। बढ़ती आबादी और बदलते खानपान की आदतों के कारण दूध की माँग लगातार बढ़ रही है। इस चुनौती को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों और किसानों ने मिलकर पशु संकरण की तकनीक को अपनाया। संकरण के ज़रिए अलग-अलग नस्लों के गुणों को जोड़ा गया, जिससे गायों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसी वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि दूध उत्पादन के मामले में गायों ने भैंसों को पीछे छोड़ दिया। यह बदलाव भारत के दुग्ध क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ है।

विदेशी और संकरित गायों की बढ़ती हिस्सेदारी
भारतीय किसानों का रुझान अब तेजी से विदेशी और संकरित गायों की ओर बढ़ रहा है। जर्सी और होल्स्टाइन फ्रीज़ियन (Holstein Friesian) जैसी नस्लें आज भारत के गाँव-गाँव में देखी जा सकती हैं। 2012 से 2019 के बीच इनकी आबादी में लगभग 26% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह आँकड़ा सिर्फ़ एक संख्या नहीं है, बल्कि किसानों के भरोसे और बदलते नजरिए का प्रमाण है। आज कुल दूध उत्पादन का लगभग 31% हिस्सा इन्हीं गायों से आता है, जबकि कुछ साल पहले यह केवल 26.5% था। यानी, कम समय में ही इन नस्लों ने किसानों को अधिक उत्पादन देकर बड़ा लाभ पहुँचाया। इन गायों की ख़ासियत यह है कि यह कम समय में अधिक दूध देती हैं और इनका दूध बाज़ार में ऊँचे दाम पर बिकता है। यही वजह है कि किसानों की आय में सुधार हो रहा है और दुग्ध व्यवसाय एक व्यावसायिक दृष्टि से और भी आकर्षक बन गया है।

स्वदेशी बनाम संकर गायें: उत्पादन और चुनौतियाँ
भारत में हमेशा से देसी गायों का महत्व रहा है। वे हमारी संस्कृति, परंपरा और धार्मिक आस्था से गहराई से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब दूध उत्पादन की बात आती है तो यहाँ एक बड़ी चुनौती सामने आती है। देसी गायें कुल आबादी का लगभग 38% हिस्सा हैं, लेकिन उनका दूध उत्पादन केवल 20% है। इसके उलट विदेशी और संकर गायें आबादी का केवल 20.5% हैं, लेकिन उनका योगदान दूध उत्पादन में 28% है। यह असंतुलन चिंता का विषय है, क्योंकि इससे हमारी देसी नस्लें धीरे-धीरे कमज़ोर हो रही हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने 2014 में ‘राष्ट्रीय गोकुल मिशन’ की शुरुआत की। इसके तहत किसानों को कृत्रिम निषेचन, आईवीएफ जैसी तकनीकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। रेड सिंधी, थारपारकर, साहीवाल और गिर जैसी नस्लों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे भी आधुनिक तकनीकों की मदद से अधिक दूध दे सकें। यह प्रयास केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी परंपरा और जैव विविधता को बचाने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।
ट्रांसजेनिक गायें और दूध की पौष्टिकता
वैज्ञानिक प्रगति ने दुग्ध उत्पादन को एक नए युग में प्रवेश करा दिया है। हाल के वर्षों में ट्रांसजेनिक गायें विकसित की गई हैं जिनका दूध मानवीय दूध के समान गुणकारी और पौष्टिक होता है। इन गायों के दूध में ऐसे विशेष प्रोटीन पाए जाते हैं जो शिशुओं की प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत करते हैं और उन्हें विभिन्न संक्रमणों से बचाते हैं। लगभग 300 डेयरी गायों में मानव जीन डालकर उन्हें आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है। इनसे प्राप्त दूध न केवल शिशुओं के लिए, बल्कि बुज़ुर्गों और रोगियों के लिए भी बेहद फायदेमंद हो सकता है। यह तकनीक भविष्य में शिशु आहार और फ़ॉर्मूला मिल्क (formula milk) का विकल्प बन सकती है। कहा जा सकता है कि यह नवाचार पोषण विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता रखता है।

ट्रांसजेनिक तकनीक की विधियाँ
ट्रांसजेनिक गायें बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल और वैज्ञानिक है। इसके लिए तीन प्रमुख तकनीकों का उपयोग किया जाता है - डीएनए माइक्रोइंजेक्शन (DNA microinjection), रेट्रोवायरस-मध्यस्थता जीन (Retrovirus-mediated gene) स्थानांतरण और भ्रूण स्टेम सेल-मध्यस्थता जीन (Embryonic stem cell-mediated gene) स्थानांतरण। इनमें से डीएनए माइक्रोइंजेक्शन सबसे ज़्यादा प्रचलित और सफल मानी जाती है। इन विधियों में गायों के डीएनए में विशेष जीन डाले जाते हैं, ताकि उनका दूध अधिक पौष्टिक और उपयोगी बन सके। यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है और इसमें उच्चस्तरीय लैब व वैज्ञानिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। हालांकि यह सुनने में जटिल लगता है, लेकिन इसका लक्ष्य सीधा है - ऐसा दूध तैयार करना जो मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक से अधिक लाभकारी हो।

संभावनाएँ और नैतिक चुनौतियाँ
ट्रांसजेनिक गायों का दूध केवल भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई औषधीय उपयोग भी हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे इंसुलिन (insulin), ग्रोथ हार्मोन (growth hormone) और कई अन्य दवाएँ तैयार की जा सकती हैं। यदि यह तकनीक व्यापक स्तर पर अपनाई गई, तो यह स्वास्थ्य और पोषण विज्ञान दोनों में नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। लेकिन इसके साथ ही कई नैतिक सवाल भी उठते हैं। क्या जानवरों को आनुवंशिक रूप से बदलना सही है? क्या इससे उनकी प्राकृतिक जीवन शैली प्रभावित होगी? और क्या इससे पर्यावरण और जैव विविधता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है? इन सवालों पर समाज में गंभीर बहस जारी है। इसके बावजूद, यदि इस तकनीक को सावधानी और ज़िम्मेदारी के साथ अपनाया जाए, तो यह भविष्य में मानव स्वास्थ्य की बड़ी समस्याओं का समाधान बन सकती है। यह विज्ञान, कृषि और चिकित्सा का संगम है, जो सही संतुलन के साथ हमारे जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है।
संदर्भ-
https://shorturl.at/dyyfe
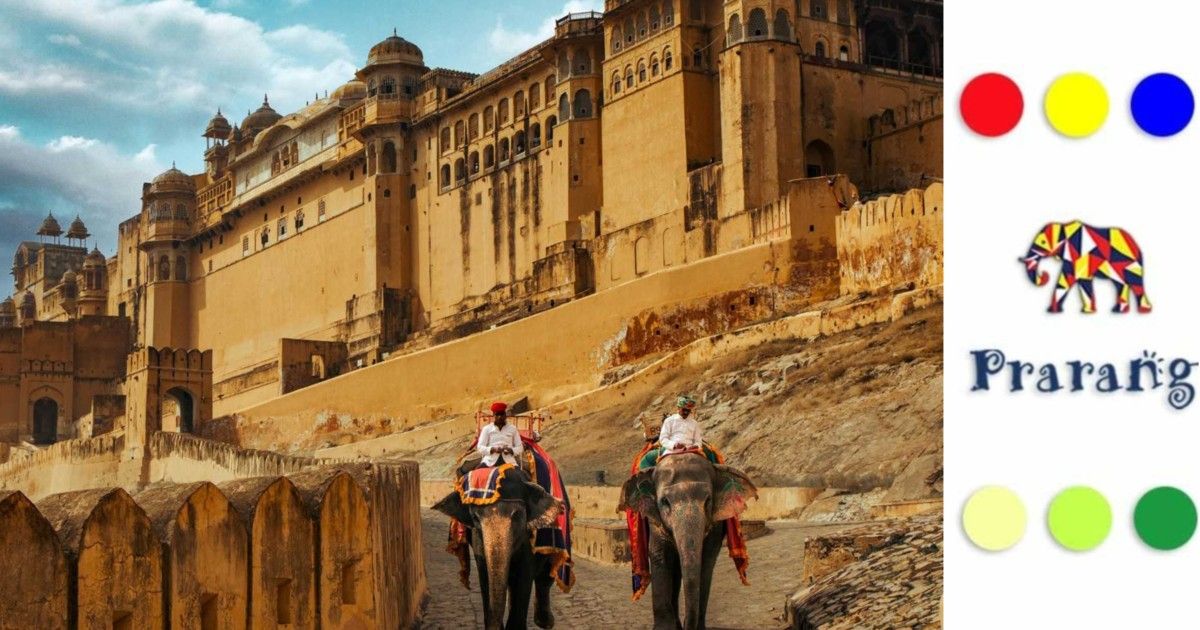
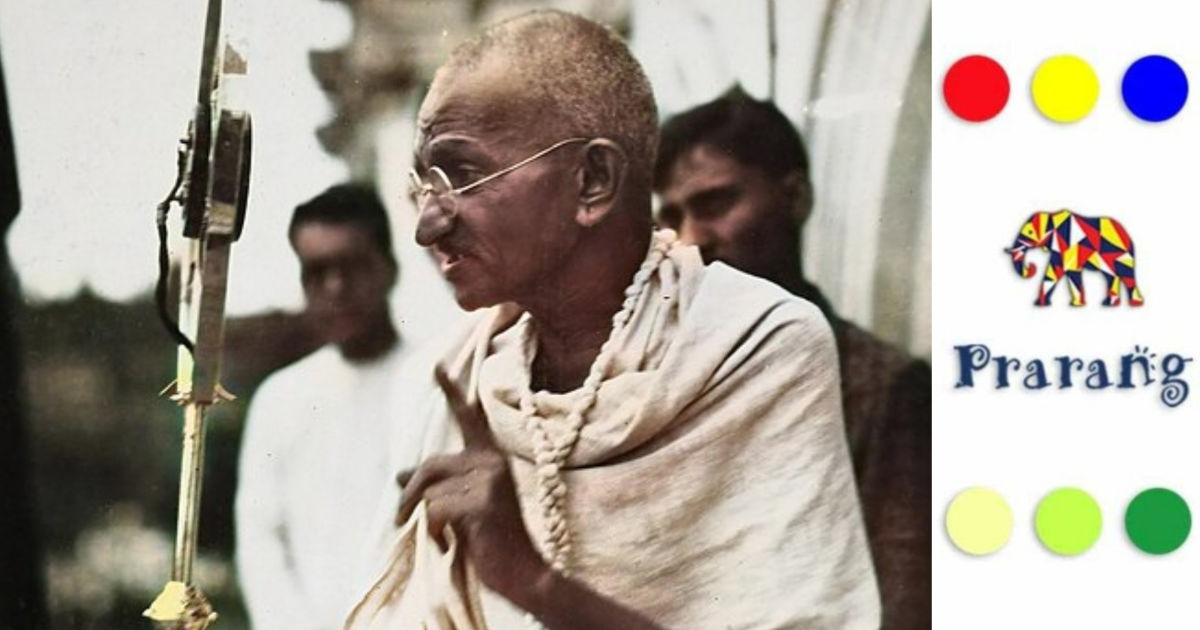



A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.