
समय - सीमा 288
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1058
मानव और उनके आविष्कार 829
भूगोल 262
जीव-जंतु 317
| Post Viewership from Post Date to 18- Nov-2025 (31st) Day | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 2148 | 78 | 5 | 2231 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

मेरठवासियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब खेतों में नई कोपलें फूटती हैं, जब मिट्टी से सोंधी खुशबू आती है और जब फसलें झूमकर हवा से बातें करती हैं - तो इसके पीछे सिर्फ किसान की मेहनत नहीं, बल्कि मिट्टी के भीतर एक अदृश्य दुनिया भी सांस ले रही होती है? यह दुनिया है सूक्ष्मजीवों की - वो नन्हे जीव जो आंखों से तो नहीं दिखते, लेकिन खेत की हर हरियाली में उनकी भूमिका अटूट है। आज मेरठ की खेती एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है - एक तरफ रासायनिक खादों और कीटनाशकों की लत, तो दूसरी तरफ मिट्टी की थकान और घटती उपज। लेकिन इसी बीच, हमारी पुरखों की ज़मीन में ही एक समाधान भी छिपा है - सूक्ष्मजीव, जो न केवल मिट्टी को फिर से जिंदा कर सकते हैं, बल्कि खेती को टिकाऊ और सुरक्षित भी बना सकते हैं। राइज़ोबियम (Rhizobium) जैसे जीवाणु नाइट्रोजन (Nitrogen) को पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं, जैव उर्वरक बिना रसायन के खेतों को पोषण देते हैं, और ट्राइकोडर्मा (Trichoderma) जैसे जैविक कीटनाशक फ़सलों को बीमारियों से बचाते हैं। इतना ही नहीं, घर के कचरे और गोबर से बनने वाली खाद में भी यही जीव मिट्टी को जीवन देते हैं। ये सब मिलकर मिट्टी को फिर से जीवंत, सांस लेने वाली और उत्पादक बनाते हैं।
इस लेख में हम जानेंगे कि खेती में सूक्ष्मजीव कितने उपयोगी होते हैं। सबसे पहले, राइज़ोबियम और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को समझेंगे, जो पौधों को प्राकृतिक नाइट्रोजन देते हैं। इसके बाद जैव उर्वरक, पीजीपीआर (PGPR) और एएमएफ (AMF) जैसे सूक्ष्मजीवों की भूमिका पर नज़र डालेंगे, जो फसल की वृद्धि और पोषण को बढ़ाते हैं। फिर जैविक कीटनाशक और ट्राइकोडर्मा जैसे कवकों की अहमियत समझेंगे, जो बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही, सूक्ष्मजीवों द्वारा खाद निर्माण, मृदा के जैविक पदार्थों की भूमिका और मिट्टी की संरचना में सुधार पर भी चर्चा करेंगे। अंत में, हम पीजीपीआर देखेंगे कि सूक्ष्मजीवों की विविधता टिकाऊ खेती और स्वस्थ मिट्टी का आधार है।

राइज़ोबियम और नाइट्रोजन स्थिरीकरण: मिट्टी को जीवन देने वाली प्रक्रिया
खेती की बुनियाद मानी जाने वाली मिट्टी को असली जीवन राइज़ोबियम जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं से मिलता है। यह एक गतिशील, ग्राम-नेगेटिव (Gram-Negative) जीवाणु है जो खासतौर पर फलीदार पौधों - जैसे चना, मूँग, लोबिया और अरहर - की जड़ों में पाए जाने वाले रूट नोड्यूल्स (nodules) में सहजीवी संबंध बनाता है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधा अमोनिया में बदलता है, जिसे पौधे सरलता से ग्रहण कर पाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया नाइट्रोजनेज़ नामक विशेष एंजाइम (enzyme) द्वारा संचालित होती है, जो केवल राइज़ोबियम जैसे जीवाणु ही उत्पन्न कर सकते हैं। इन रूट नोड्यूल्स के अंदर जब यह एंजाइम सक्रिय होता है, तो वह नाइट्रोजन गैस को एक उपयोगी जैविक यौगिक में परिवर्तित कर देता है, जो पौधों के लिए प्रोटीन, क्लोरोफिल (chlorophil) और अन्य आवश्यक तत्वों का निर्माण करने में सहायक होता है। राइज़ोबियम और पौधे के बीच यह सहजीवी रिश्ता ऐसा होता है कि पौधा उसे प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त कार्बनिक ऊर्जा देता है, जबकि बदले में जीवाणु उसे प्राकृतिक पोषण प्रदान करता है। यह प्रक्रिया न केवल उर्वरता बढ़ाती है, बल्कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता भी कम करती है, जिससे मिट्टी की दीर्घकालिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है।
जैव उर्वरकों का चमत्कारी असर: पीजीपीआर और एएमएफ की भूमिका
कृषि में जैव उर्वरक आधुनिक जैवप्रौद्योगिकी और पारंपरिक प्राकृतिक तकनीकों का अद्भुत मेल हैं। ये ऐसे सूक्ष्मजीवों का समूह होते हैं जो पौधों की वृद्धि को बिना किसी रासायनिक दुष्प्रभाव के तेज़ी से बढ़ाते हैं। इनमें पीजीपीआर (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) प्रमुख हैं, जैसे एज़ोटोबैक्टर (Azotobacter), बैसिलस (Bacillus) और स्यूडोमोनास (Pseudomonas), जो मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन, फॉस्फोरस (Phosphorus) और पोटैशियम (Potassium) जैसे पोषक तत्वों को पौधों के लिए अधिक सुलभ और घुलनशील बनाते हैं। यह केवल पोषण में नहीं, बल्कि पौधों की जड़ प्रणाली को मजबूत करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और जल धारण क्षमता को सुधारने में भी सहायक होते हैं। इनके साथ ही AMF (Arbuscular Mycorrhizal Fungi) जैसे फफूंद - जैसे ग्लोमस वर्सीफॉर्म (Glomus versiforme) और ग्लोमस मैक्रोकार्पम (Glomus macrocarpum) - पौधों की जड़ों से सहजीवी संबंध बनाकर पोषक तत्वों के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देते हैं। इन सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति मिट्टी में जैविक क्रियाओं को सक्रिय करती है और पौधों को विभिन्न जैविक व अजैविक तनावों से निपटने की ताकत देती है। जैव उर्वरकों का निरंतर प्रयोग न केवल रासायनिक खादों की लागत को घटाता है, बल्कि मिट्टी को दीर्घकालिक रूप से उर्वर और स्वस्थ बनाए रखता है, जिससे टिकाऊ खेती की नींव और मजबूत होती है।
ट्राइकोडर्मा जैसे जैविक कीटनाशकों की ताकत
जब हम कीटनाशकों की बात करते हैं, तो आमतौर पर रासायनिक विकल्पों की कल्पना करते हैं, जो फसल को तो बचाते हैं लेकिन मिट्टी, जल और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे में ट्राइकोडर्मा जैसे जैविक कीटनाशक एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं। ट्राइकोडर्मा एसपीपी (SPP) नामक फफूंद मिट्टी में मौजूद हानिकारक रोगजनकों - जैसे फ्यूज़ेरियम (Fusarium), स्क्लेरोटीनिया (Sclerotinia), फाइटोफ्थोरा (Phytophthora) - को निष्क्रिय कर देते हैं और फसलों को बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कवक विशेष एंजाइम का स्रवण करता है जो हानिकारक फफूंद की कोशिका भित्तियों को तोड़ता है और उनके विकास को रोकता है। इसके अलावा, ट्राइकोडर्मा पौधों में तनाव-रोधी प्रोटीन के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, जिससे पौधे तापमान, सूखा और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्वस्थ बने रहते हैं। ट्राइकोडर्मा हरज़ियानम (Trichoderma harzianum) जैसे प्रकारों का प्रयोग विशेषकर सब्ज़ी उत्पादन, बागवानी और नर्सरी खेती में अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुआ है। यह न केवल उत्पादन बढ़ाता है, बल्कि मिट्टी की जैविक सक्रियता को भी बनाए रखता है और खेती को पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक उत्तरदायी बनाता है।
खाद निर्माण में सूक्ष्मजीवों की भागीदारी
खाद बनाना एक जैविक कला है, और इसमें सूक्ष्मजीवों की भूमिका मुख्य है। चाहे वह वर्मी-कम्पोस्ट (vermi-compost) हो, जीवामृत हो या पारंपरिक गोबर खाद - सभी के निर्माण में बैक्टीरिया और फफूंद जैसे सूक्ष्मजीव अवश्य होते हैं, जो कचरे को पोषण में बदलने का काम करते हैं। ये जीवाणु जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल यौगिकों में तोड़ते हैं, जिससे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर (shulfur) जैसे पोषक तत्व पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। रसोई के अपशिष्ट, खेतों से निकले पत्ते, गोबर और अन्य जैविक सामग्री जब इन सूक्ष्मजीवों के संपर्क में आती है, तो वह धीरे-धीरे सड़ती और विघटित होती है। यह प्रक्रिया न केवल खाद को समृद्ध बनाती है, बल्कि उससे निकलने वाले एंजाइम और जीवाणु मिट्टी की बनावट, जलधारण और जैव विविधता में भी योगदान देते हैं। जब किसान स्वयं जैविक खाद बनाते हैं, तो वे एक साथ तीन समस्याओं का हल करते हैं - कचरे का प्रबंधन, उर्वरता में वृद्धि और रासायनिक निर्भरता की कमी। खाद निर्माण एक जीवंत प्रक्रिया है, जिसमें प्रकृति खुद किसान की सबसे बड़ी सहयोगी बन जाती है।
मृदा कार्बनिक पदार्थ: मिट्टी की संरचना को मज़बूत करने वाला आधार
मिट्टी की सेहत का असली रहस्य उसके भीतर छिपे कार्बनिक पदार्थों में निहित होता है। ये पदार्थ - जैसे हरी खाद, सूखे पत्ते, पौधों के अवशेष, गोबर खाद - मिट्टी को केवल पोषण नहीं, बल्कि जीवन देते हैं। जब कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मिलते हैं, तो वे उसकी जलधारण क्षमता, वायु संचार और संरचना को बेहतर बनाते हैं। इससे जड़ों को फैलने के लिए अधिक जगह और पोषक तत्वों तक बेहतर पहुँच मिलती है। साथ ही ये पदार्थ मिट्टी में सूक्ष्मजीवों के लिए भोजन का काम करते हैं, जिससे उनका समुदाय समृद्ध होता है। यह जैविक सक्रियता ही मिट्टी को रोगों से लड़ने योग्य बनाती है और पोषक चक्रण को बनाए रखती है। विशेषकर बाढ़ प्रभावित या अधिक दोहन वाली मिट्टियों में, कार्बनिक पदार्थ मिट्टी के ढांचे को सुदृढ़ करते हैं और उसे जल कटाव, क्षरण व थकावट से बचाते हैं। जब किसान नियमित रूप से कार्बनिक सामग्री डालते हैं, तो मिट्टी में एक सतत ऊर्जा प्रवाह बना रहता है जो उसे उत्पादक और टिकाऊ बनाए रखता है।
टिकाऊ खेती के लिए सूक्ष्मजीवों की विविधता क्यों ज़रूरी है?
कृषि विज्ञान की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मिट्टी केवल एक माध्यम नहीं, बल्कि एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है, और इसकी ताक़त इसमें निवास करने वाले सूक्ष्मजीवों की विविधता पर निर्भर करती है। यह विविधता जितनी अधिक होती है, मिट्टी उतनी ही अधिक रोग प्रतिरोधी, पोषक और टिकाऊ बनती है। सूक्ष्मजीवों की यह विविधता - जिसमें बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ (protozoa) और एक्टिनोमाइसेट्स (Actinomycetes) शामिल होते हैं - न केवल पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं, बल्कि रोगजनकों से रक्षा करते हैं और पर्यावरणीय उतार-चढ़ाव के समय पौधों को सहनशील बनाते हैं। विविधता बनाए रखने के लिए फसल चक्रण, कवर क्रॉपिंग (cover cropping), जैविक खाद, न्यूनतम जुताई और प्राकृतिक मल्चिंग (mulching) जैसी तकनीकों का प्रयोग आवश्यक है। यह जैविक विविधता मिट्टी में संतुलन बनाए रखती है, जिससे उसमें आवश्यक एंजाइम, पोषक यौगिक और रोगनिरोधी तत्वों का निरंतर उत्पादन होता है। यदि यह विविधता नष्ट हो जाए, तो मिट्टी धीरे-धीरे निष्प्राण हो जाती है। इसलिए हर किसान को यह समझना ज़रूरी है कि मिट्टी की गहराई में मौजूद ये अदृश्य जीवन-रक्षक ही खेती को भविष्य के लिए तैयार करते हैं।
संदर्भ-
https://shorturl.at/KFYwC
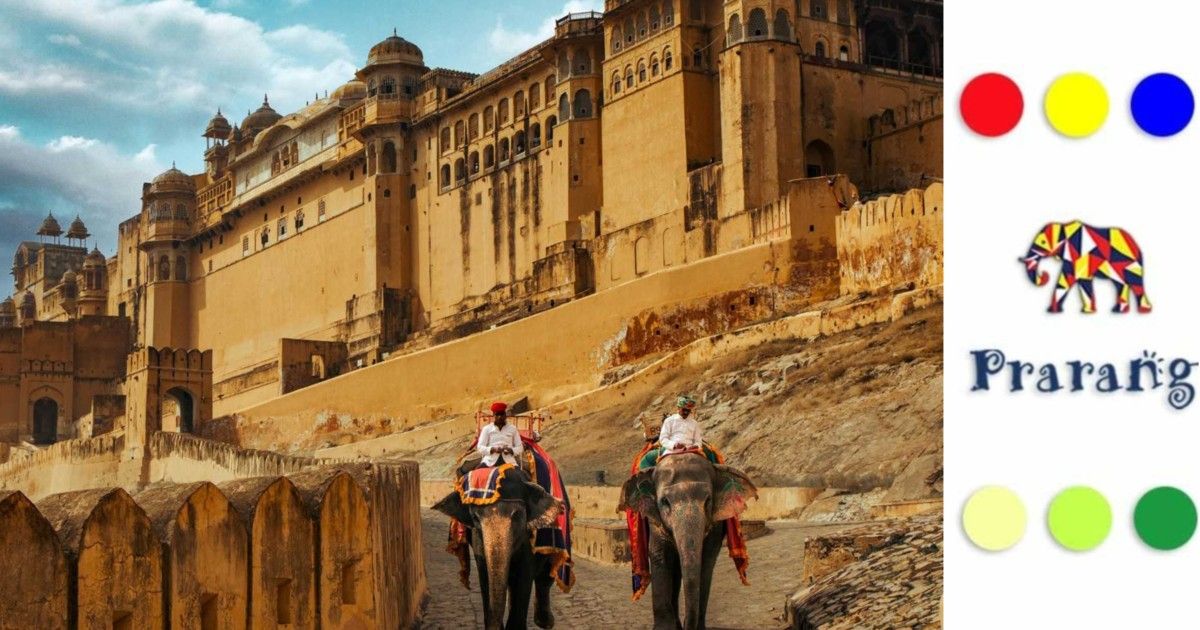
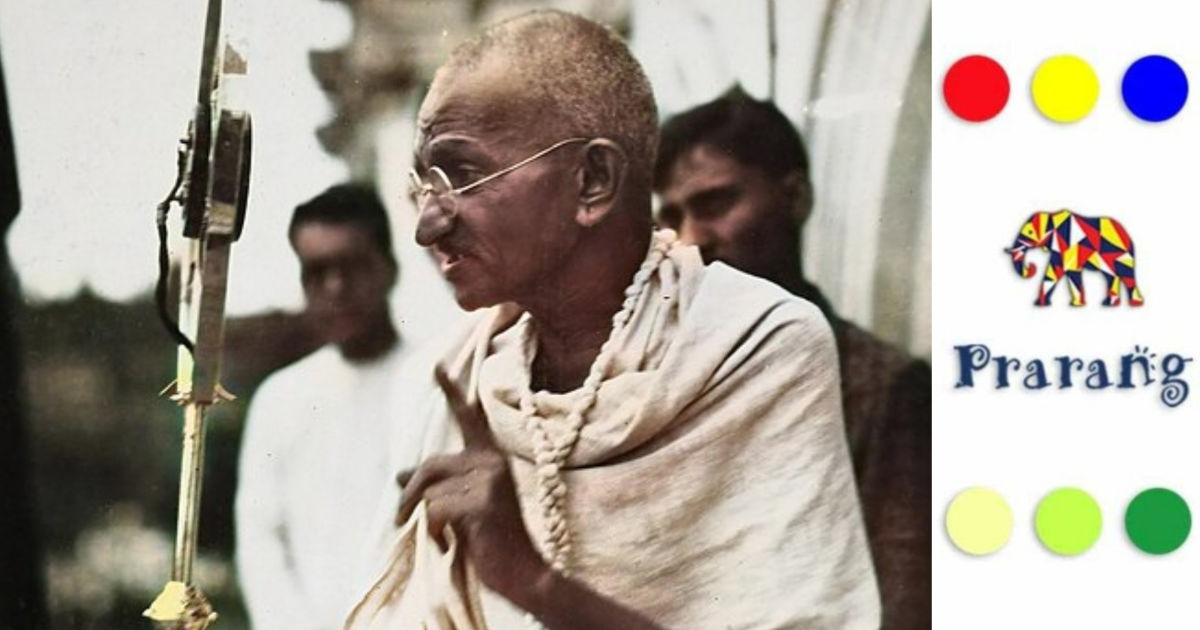



A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.