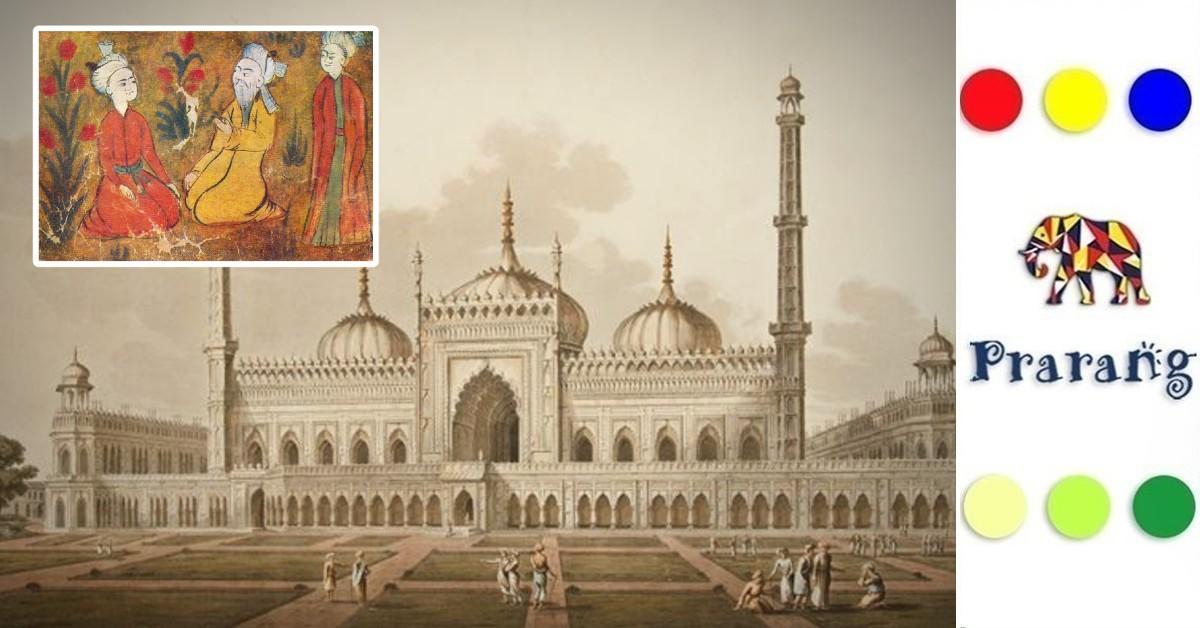
समयसीमा 258
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1041
मानव व उसके आविष्कार 823
भूगोल 238
जीव - जन्तु 302
| Post Viewership from Post Date to 05- Jun-2025 (31st) Day | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Subscribers (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 2732 | 58 | 0 | 2790 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||
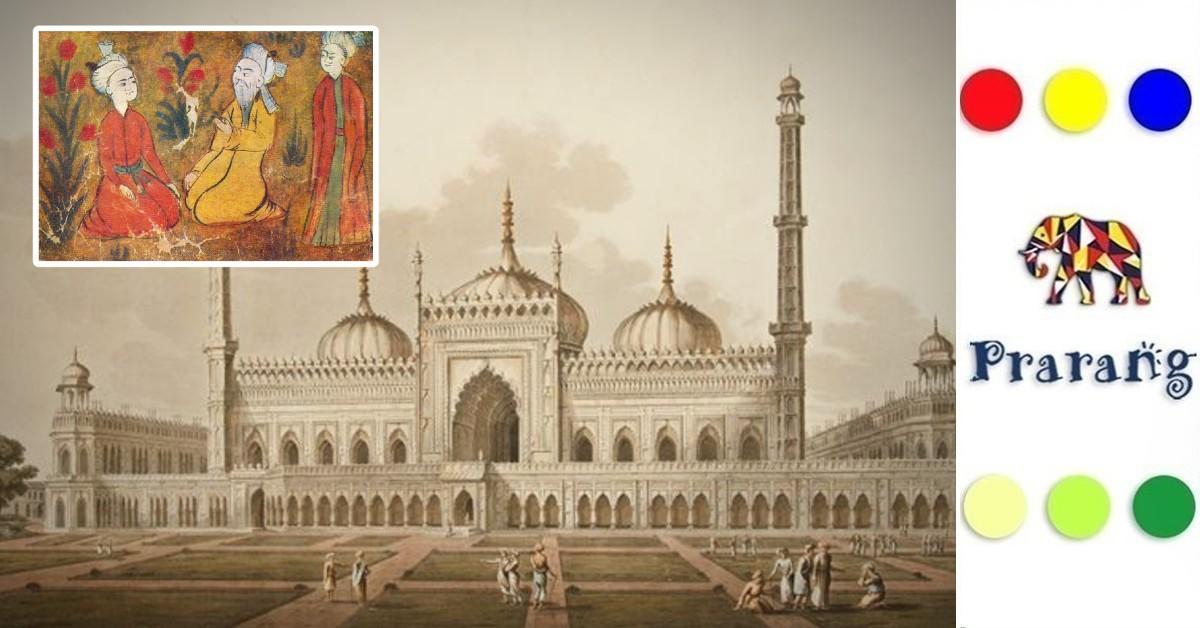
अपनी छवि बनाइ के जो मैं पी के पास गई,
जब छवि देखी पीहू की तो अपनी भूल गई।
छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाइ के
बात अघम कह दीन्हीं रे मोसे नैना मिलाइ के।
इन पंक्तियों को आपने अनेकों बार सूफ़ी संगीत समारोहों, दरगाहों और दर्जनों फ़िल्मी गानों में सुना होगा! लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कव्वाली के मूल लेखक अमीर ख़ुसरों थे! लखनऊ की गलियों में गूंजती कव्वाली की धुनें और सुरों की मिठास हमें एक ऐसे दौर की याद दिलाती हैं, जब शब्दों और संगीत ने मिलकर इतिहास रच दिया था। अमीर ख़ुसरो, इसी इतिहास का एक चमकता सितारा थे। उनका नाम केवल साहित्य और संगीत तक सीमित नहीं है, बल्कि वे एक सांस्कृतिक सेतु की तरह आज भी जीवंत हैं। उन्हें "भारत का तोता" कहा जाता है, और वे दिल्ली सल्तनत के दौर के एक महान कवि, विद्वान और संगीतकार थे। उनकी रचनाओं में फ़ारसी और हिंदवी का अनूठा संगम देखने को मिलता है, जो प्रेम, भक्ति और सांस्कृतिक एकता का संदेश देता है। लेकिन अमीर ख़ुसरो केवल लेखक या संगीतकार नहीं थे। वे एक क्रांतिकारी कलाकार थे, जिन्होंने नई संगीत शैलियों को जन्म दिया और कव्वाली को एक नई पहचान दी। उनकी कविताएँ और संगीत सदियों से हमारी संस्कृति को समृद्ध कर रहे हैं। इसलिए आज के इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण बच्चा, जिसने बचपन में ही अपनी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता से सबको चौंका दिया, आगे चलकर इतिहास का एक अमिट नाम बन गया। सबसे पहले, हम उनके शुरुआती जीवन पर नज़र डालेंगे। फिर देखेंगे कि सूफ़ी संत निज़ामुद्दीन औलिया से उनकी मुलाकात ने उनके विचारों और लेखनी को कैसे नया आयाम दिया। इसके बाद, हम बात करेंगे कि खिलजी और तुग़लक़ सल्तनत के दौर में शाही दरबार में उनकी भूमिका कैसी रही। आख़िर में, हम जानेंगे कि अमीर ख़ुसरो का वह योगदान क्या है, जो सदियों बाद भी हमें जोड़ता है और हमारी सांस्कृतिक जड़ों को और मज़बूत करता है। तो आइए, इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं!
अमीर ख़ुसरो का बचपन और प्रारंभिक जीवन कैसा था?
1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाली (ज़िला कासगंज) में जन्मे अबुल हसन यामिनुद्दीन ख़ुसरो का जीवन शुरू से ही असाधारण था। उनके पिता, अमीर सैफ़ुद्दीन महमूद, सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश के दरबार में एक सम्मानित अधिकारी थे। उनकी माँ, बीबी दौलतनाज़, भारतीय राजपूत परिवार से थीं। बचपन से ही ख़ुसरो असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनके दो भाई और एक बहन थे, लेकिन उनमें कुछ ख़ास था। छोटी उम्र में ही उन्हें कविता और संगीत में गहरी रुचि हो गई। दुर्भाग्यवश, जब वे केवल नौ साल के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनके नाना, नवाब इमादुल मुल्क, ने उनका पालन-पोषण किया। अमीर ख़ुसरो के पिता, अमीर सैफ़ उद-दीन महमूद, तुर्क मूल के थे, जबकि उनकी माँ, बीबी दौलतनाज़, भारतीय थीं। अमीर ख़ुसरो के पिता का जन्म मध्य एशिया के केश गाँव में हुआ था, जो आज उज्बेकिस्तान में है। यह जगह समरकंद के पास स्थित थी। जब चंगेज़ ख़ान ने मध्य एशिया पर हमला किया, तो वहाँ के कई लोग अपनी जान बचाने के लिए पलायन करने लगे। भारत उन लोगों की पसंदीदा जगहों में से एक बन गया। अमीर सैफ़ उद-दीन भी अपने परिवार के साथ उज्बेकिस्तान छोड़कर बल्ख (वर्तमान उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान) आ गए। लेकिन वहाँ भी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं हुआ, तो उन्होंने दिल्ली के सुल्तान से शरण मांगी।
दिल्ली के शासक सुल्तान इल्तुतमिश भी तुर्क मूल के थे। उन्होंने शरणार्थियों का न सिर्फ़ स्वागत किया, बल्कि कई लोगों को महत्वपूर्ण पद और जागीरें भी दीं। 1230 में, अमीर सैफ़ उद-दीन को उत्तर प्रदेश के पटियाली में एक जागीर मिली। यहीं पर उनकी शादी बीबी दौलतनाज़ से हुई। बीबी दौलतनाज़ एक प्रतिष्ठित भारतीय परिवार से थीं। उनके पिता रावत अर्ज दिल्ली के नौवें सुल्तान ग़ियास उद-दीन बलबन के सैन्य मंत्री थे। उनका परिवार उत्तर प्रदेश के राजपूत समुदाय से संबंध रखता था। अमीर ख़ुसरो की परवरिश एक ऐसी पृष्ठभूमि में हुई, जहाँ तुर्की और भारतीय संस्कृतियाँ आपस में घुल-मिल गई थीं। यही कारण है कि वे आगे चलकर भारत की गंगा-जमुनी तहज़ीब के सबसे बड़े प्रतीक बने।
ख़ुसरो की शिक्षा और आध्यात्मिक सफर कैसा था?
ख़ुसरो में शिक्षा और ज्ञान के प्रति अद्वितीय प्यास देखने लायक थी! ख़ुसरो का शिक्षा के प्रति झुकाव असाधारण था। उन्होंने साहित्य, कला, खगोल विज्ञान, दर्शन, तर्कशास्त्र, धर्म, रहस्यवाद और इतिहास में गहरी समझ विकसित की। तुर्की, फ़ारसी और अरबी भाषाओं में वे पूरी तरह दक्ष हो गए। दिल्ली के विविध सांस्कृतिक माहौल में उन्होंने भारतीय भाषाओं में भी निपुणता हासिल कर ली। लेकिन उनका सफ़र केवल किताबों तक सीमित नहीं था। 1310 में ख़ुसरो की ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने प्रसिद्ध सूफ़ी संत निज़ामुद्दीन औलिया को अपना गुरु बना लिया। यह रिश्ता केवल गुरु-शिष्य का नहीं था, बल्कि आत्मा तक जुड़ा हुआ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध था। सूफ़ी विचारधारा ने उनकी सोच और रचनाओं को नया रूप दिया। उनकी कविता और संगीत में एक अनोखा आध्यात्मिक प्रवाह दिखने लगा। 1325 में जब निज़ामुद्दीन औलिया का निधन हुआ, तो ख़ुसरो यह आघात सह नहीं सके। अपने प्रिय गुरु को खोने के कुछ ही समय बाद वे भी इस दुनिया से विदा हो गए।
तुग़लक़ वंश और अमीर ख़ुसरो: इतिहास का एक अनोखा संगम:-
जब भी तुग़लक़ वंश का ज़िक्र होता है, अमीर ख़ुसरो का नाम स्वाभाविक रूप से उभर आता है। उनकी मौजूदगी ने न सिर्फ़ इस दौर की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया, बल्कि सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लक़ के शासन में भी उनकी भूमिका बेहद अहम रही। अमीर ख़ुसरो तुग़लक़ दरबार के प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने शाही प्रशासन में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। उनकी कलम से लिखा गया "तुग़लक़नामा" उस समय की राजनीतिक और सामाजिक हलचलों को दर्शाने वाला एक अमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज़ माना जाता है। इसमें सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लक़ के शासन की घटनाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है, साथ ही यह तत्कालीन समाज की झलक भी पेश करता है। सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लक़ खुद कला और साहित्य के संरक्षक माने जाते थे। उन्होंने अमीर ख़ुसरो की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया। इस सहयोग ने तुग़लक़ काल की सांस्कृतिक विरासत को और भी समृद्ध बना दिया।
ख़िलजी वंश और अमीर ख़ुसरो: कला और काव्य का स्वर्ण युग:-
ख़िलजी वंश के दौर में, अमीर ख़ुसरो का योगदान एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की तरह था। वे न केवल एक प्रमुख दरबारी थे, बल्कि शासकों के विश्वासपात्र भी थे। अलाउद्दीन ख़िलजी के शासनकाल में, अमीर ख़ुसरो ने कवि और सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलाउद्दीन, जो कला और साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखते थे, उन्होंने ख़ुसरो की रचनाओं को न केवल सराहा, बल्कि उन्हें भरपूर संरक्षण भी दिया। इसी काल में अमीर ख़ुसरो ने "ख़ज़ाइन-उल-फुतूह" (विजय का ख़ज़ाना) की रचना की। यह ग्रंथ अलाउद्दीन ख़िलजी के सैन्य अभियानों और विजय गाथाओं का एक ऐतिहासिक विवरण है। लेकिन उनका योगदान सिर्फ़ इतिहास लेखन तक सीमित नहीं था। अमीर ख़ुसरो ने संगीत की दुनिया में भी एक नया अध्याय लिखा। उन्होंने फ़ारसी और भारतीय संगीत के अद्भुत मेल से कव्वाली को एक नई पहचान दी। आगे चलकर, यही कव्वाली भारतीय उपमहाद्वीप में सूफ़ी संगीत की पहचान बन गई।
आइए अब आपको अमीर ख़ुसरों की एक ऐसी अमर कृति से रूबरू कराते हैं, जिसकी रचना अमीर ख़ुसरों ने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया को प्रसन्न करने के लिए की थी। कहा जाता है कि जब निजामुद्दीन औलिया अपने भांजे की मृत्यु से दुखी थे, तो अमीर ख़ुसरों ने उनकी मुस्कान लौटाने के लिए बसंत के पीले फूल लेकर दरगाह पर नृत्य किया, जिससे उनके गुरु के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। तभी से यह रस्म परंपरा के रूप में चिश्तिया दरगाहों में प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गई। आज भी यह रस्म अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह सहित कई सूफी स्थलों पर मनाई जाती है। जब कव्वाल अमीर खुसरो के कलाम गाते हैं, तो यह सदियों पुरानी परंपरा सजीव हो उठती है।
ख़ुसरों द्वारा अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया को प्रसन्न करने के लिए रचा गया गीत निम्नवत दिया गया है:
आज बसंत मना ले सुहागन
आज बसंत मना ले ...
अंजन–मंजन कर पिया मोरी
लंबे नेहर लगाए
तू क्या सोवे नींद की माटी
सो जागे तेरे भाग सुहागन
आज बसंत मना ले...
ऊंची नार के ऊंचे चितवन
ऐसो दियो है बनाय
शाहे अमीर तोहे देखन को
नैनों से नैना मिलाय
आज बसंत मना ले…
संदर्भ
https://tinyurl.com/26tflwab
https://shorturl.at/SySnA
https://tinyurl.com/24dm9ejb
https://tinyurl.com/23u93w69
https://tinyurl.com/22ekedl8
मुख्य चित्र में अमीर खुसरो अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए और लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा परिसर के दृश्य का स्रोत : Wikimedia, प्रारंग चित्र संग्रह




A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.