
समयसीमा 258
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1041
मानव व उसके आविष्कार 823
भूगोल 238
जीव - जन्तु 302
| Post Viewership from Post Date to 03- Jun-2025 (31st) Day | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Subscribers (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 2494 | 61 | 0 | 2555 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

हमारा शहर लखनऊ सिर्फ़ एक शहर नहीं है, तहज़ीब और इल्म की जीती-जागती मिसाल है। यहाँ की गलियों में इत्र की ख़ुशबू बसी है, और अख़बारों की सुर्खियाँ भी सुबह-सुबह लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाती हैं। यहाँ घटने वाली एक छोटी से छोटी घटना भी ख़बर में तब्दील हो जाती है! अब्दुल मियां सुबह की पहली चाय के साथ ही अख़बार की सारी ताज़ा ख़बरों को टटोल लेते हैं! अख़बार पढ़ने के बाद वे गली के सबसे ‘ख़बरदार’ आदमी लगने लगते हैं, जो हर बड़ी-छोटी ख़बर से वाक़िफ़ रहते हैं। इससे पता चलता है कि प्रेस महज़ ख़बरों का ज़रिया नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने और बदलाव लाने का हथियार है। अख़बार, टी वी और डिज़िटल मीडिया (Digital Media) ही वो कड़ी हैं, जो आम आदमी को राजनीति से लेकर गली-मोहल्ले की हलचल तक, हर अहम मुद्दे से जोड़े रखते हैं। एक स्वतंत्र और ज़िम्मेदार प्रेस न केवल जनता की आवाज़ बनती है, बल्कि सरकार को जवाबदेह ठहराकर शासन में पारदर्शिता भी लाती है।
लखनऊ की पत्रकारिता का इतिहास भी कम रोशन नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ के पत्रकारों ने अपनी कलम को हथियार बना लिया था। ‘अवध पंच’ जैसे अख़बारों ने अपने तीखे व्यंग्य और बेख़ौफ़ लेखनी से ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। आज भी लखनऊ की पत्रकारिता सामाजिक मुद्दों को उठाकर नागरिकों को जागरूक करती है और उन्हें सही फ़ैसले लेने की ताकत देती है। लोकतंत्र में प्रेस को यूँ ही "चौथा स्तंभ" नहीं कहा जाता। यह सरकार और जनता के बीच संतुलन बनाए रखने वाला अहम माध्यम है। इसकी मौज़ूदगी एक स्वस्थ, निष्पक्ष और मज़बूत समाज के लिए बेहद ज़रूरी है।
इसलिए आज के इस लेख में हम भारत में प्रेस के इतिहास को समझेंगे! इसके तहत हम देखेंगे कि समय के साथ इसका विकास कैसे हुआ। फ़िर, हम औपनिवेशिक शासन के दौर में प्रेस के योगदान पर नज़र डालेंगे और जानेंगे कि कैसे इसने स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक जागरूकता में अहम भूमिका निभाई। अंत में, हम देखेंगे कि आधुनिक दौर में पत्रकारिता का समाज, लोकतंत्र और शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
भारतीय पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी?
भारत में पत्रकारिता की नींव 18वीं सदी में रखी गई थी। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी (James Augustus Hickey) ने देश का पहला समाचार पत्र 'बंगाल गजट' (Bengal Gazette) प्रकाशित किया। यह अख़बार अंग्रेज़ी में था और इसकी केवल 400 प्रतियाँ ही छपती थीं। हालाँकि इसे पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन इसने भारतीय प्रेस के लिए नई राह खोल दी।
शुरुआती दौर में ज़्यादातर समाचार पत्रों का संचालन ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के हाथ में था। ये अख़बार मुख्यतः अंग्रेज़ शासकों के समर्थन में प्रकाशन करते थे, जिसमें आम भारतीयों की समस्याओं के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन जैसे-जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन तेज़ हुआ, वैसे-वैसे भारतीय पत्रकारों ने ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती देनी शुरू कर दी। उन्होंने ऐसे समाचार पत्र निकाले, जो भारतीय जनता की आवाज़ बनने लगे।
1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय पत्रकारिता के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। उस समय तक मीडिया पर अंग्रेज़ों का पूर्ण नियंत्रण था, लेकिन विद्रोह के बाद भारतीयों द्वारा संचालित अख़बारों की संख्या बढ़ने लगी।
इन अख़बारों ने अंग्रेज़ों के अत्याचारों को उज़ागर किया और जनता को उनके ख़िलाफ़ जागरूक किया। पत्रकारों ने विद्रोह की ख़बरें और ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियाँ लोगों तक पहुँचाईं, जिससे विरोध की भावना और अधिक भड़क उठी। इस दौर में प्रेस, स्वतंत्रता संग्राम का एक मज़बूत हथियार बन गया।
20वीं सदी में भारत में राष्ट्रवादी पत्रकारिता ने तेज़ रफ़्तार पकड़ी। इस दौर में 'द हिंदू (The Hindu)', 'द इंडियन एक्सप्रेस (The Indian Express)' और 'अमृत बाज़ार पत्रिका' जैसे अख़बारों ने ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई।
इन समाचार पत्रों ने भारतीयों की समस्याओं, संघर्षों और आकांक्षाओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया। उन्होंने जनता को स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागरूक किया और समर्थन जुटाने में अहम भूमिका निभाई।
20वीं सदी के मध्य में पत्रकारिता के माध्यमों में बड़ा बदलाव आया। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो (All India Radio) की स्थापना हुई, जिसने समाचार और सूचनाओं को देशभर में पहुँचाने का काम किया। रेडियो की वजह से ख़बरें तेज़ी से लोगों तक पहुँचने लगीं। 1950 के दशक में भारत में टेलीविज़न (Television) आया, जिसने पत्रकारिता का दायरा और भी बढ़ा दिया। दृश्य और ध्वनि के माध्यम से ख़बरें दिखाने का यह तरीक़ा जनता तक सूचना पहुँचाने में बेहद प्रभावी साबित हुआ।
ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन (1870-1918) के दौर में भारतीय प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम को गति देने में अहम भूमिका निभाई। उस समय भारतीय मीडिया का मुख्य उद्देश्य जनता में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना था। प्रेस ने न केवल सरकार की राजनीतिक नीतियों पर चर्चा की, बल्कि निरक्षरता के खिलाफ़ जागरूकता फ़ैलाने, जन आंदोलनों को प्रेरित करने और सरकार के खिलाफ़ खुली बहस का मंच भी तैयार किया।
आइए अब जानते हैं कि आधुनिक समय में भारत में पत्रकारिता क्या भूमिका निभा रही है?
पत्रकारिता का मक़सद लोगों तक सही, सटीक़ और निष्पक्ष जानकारी पहुँचाना, उन्हें जागरूक रखना और शिक्षित करना है। आज के समय में, जब राजनीति, सत्ता और भ्रष्टाचार के खेल में हिंसा और नफ़रत बढ़ रही है, तब पत्रकारिता "बेज़ुबानों की आवाज़" बनकर उभर रही है। मीडिया सच को सामने लाकर जनता को हकीकत से रूबरू कराता है, जिससे लोग सही-गलत का फ़र्क़ समझ पाते हैं। पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण काम लोगों के नज़रिए को आकार देना भी है। यह समाज में रोज़ हो रही घटनाओं और मुद्दों पर जागरूकता फ़ैलाता है। चाहे सड़क हादसे की ख़बर हो या सरकार की नई नीति – मीडिया लोगों को हर महत्वपूर्ण जानकारी से जोड़ता है।
भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में पत्रकारिता का योगदान अहम है। यह राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करती है। अन्याय और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है। समाज में बदलाव लाने में सहायक होती है। मीडिया भ्रष्टाचार को उज़ागर कर समाज में जवाबदेही तय करने में मदद करता है। पत्रकारिता की ख़ासियत यह है कि यह जटिल और तकनीकी जानकारियों को आम लोगों की भाषा में पेश करती है। उदाहरण के लिए, जब सरकार बजट पेश करती है, तो उसमें कई जटिल आँकड़े और तकनीकी शब्द होते हैं, जिन्हें आम जनता आसानी से नहीं समझ पाती। ऐसे में पत्रकारों की ज़िम्मेदारी होती है कि वे विशेषज्ञों से बातचीत करके बजट के फ़ायदे-नुकसान को सरल भाषा में समझाएँ। पत्रकारिता केवल ख़बरें दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनता की आवाज़ को सत्ता तक पहुँचाने का काम भी करती है। सही मायनों में, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो समाज को जागरूक, ज़िम्मेदार और सशक्त बनाता है।
संदर्भ
मुख्य चित्र में लखनऊ से प्रकाशित उर्दू व्यंग्य साप्ताहिक 'अवध पंच', 1878 और मोबाइल चलाते व्यक्ति का स्रोत : Wikimedia. Pexels
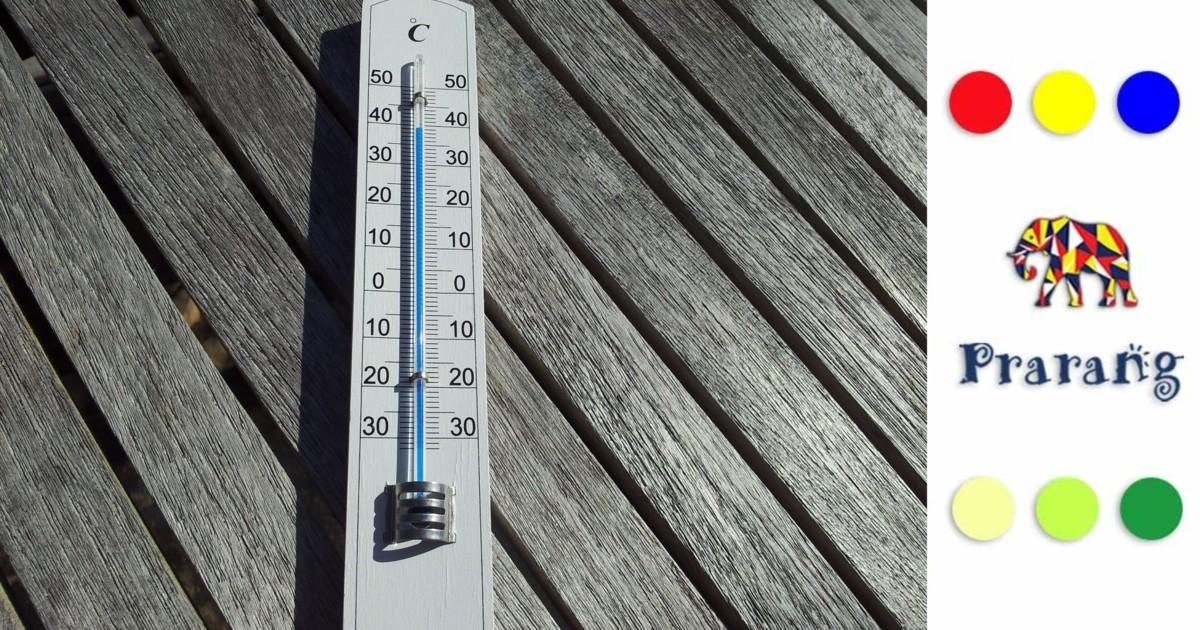




A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.