
समयसीमा 257
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1038
मानव व उसके आविष्कार 821
भूगोल 236
जीव - जन्तु 300
समयसीमा 257
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1038
मानव व उसके आविष्कार 821
भूगोल 236
जीव - जन्तु 300

लखनऊवासियो, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति का भी अहम हिस्सा है - विमानन उद्योग। जब भी हम हवाई जहाज़ों की उड़ान देखते हैं, तो यह केवल यात्रा का साधन नहीं होता बल्कि आधुनिक भारत की उभरती ताक़त और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी होता है। हाल के वर्षों में भारत ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। लेकिन लखनऊवासियो, यह भी सच है कि अभी हमारी यात्रा अधूरी है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कड़ी है और भारत की हिस्सेदारी अभी भी सीमित है। जहाँ चीन और अमेरिका जैसे देश प्रति व्यक्ति कई गुना अधिक हवाई यात्राएँ करते हैं, वहीं भारत इस मामले में पीछे है। ऐसे में "मेक इन इंडिया" (Make in India) और "आत्मनिर्भर भारत" जैसी पहलें इस अंतर को कम करने और भारत को विमान निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं।
इस लेख में हम भारत के विमानन उद्योग को कुछ प्रमुख पहलुओं से समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है और वैश्विक स्तर पर यह कहाँ खड़ा है। इसके बाद "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" जैसी पहलों के तहत स्वदेशी विमान निर्माण के प्रयासों पर नज़र डालेंगे। फिर एयरबस (Airbus) और बोइंग (Boeing) जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका और उनके योगदान की चर्चा करेंगे। आगे चलकर एमएसएमई (MSMI) यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी और उनसे जुड़ी चुनौतियों को समझेंगे। इसके साथ ही वित्तीय कठिनाइयों और ऋण की सीमित पहुँच जैसे मुद्दों पर भी विचार होगा। अंत में, हम भविष्य की संभावनाओं और एक मज़बूत औद्योगिक विमान नीति की ज़रूरत को देखेंगे, जो इस उद्योग को नई उड़ान दे सकती है।
भारत का विमानन उद्योग: वैश्विक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान स्थिति
भारत का विमानन उद्योग बीते दो दशकों में तेजी से उभर कर सामने आया है। आज यह 16 अरब डॉलर के बाज़ार आकार के साथ दुनिया का नौवां सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाज़ार है और लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या, मध्यम वर्ग की बढ़ती आय और यात्रा की बदलती आदतों ने इस उद्योग को नई गति दी है। सालाना 15.2% की वृद्धि दर इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भारत का हवाई सफर और भी आम होता जाएगा। साल 2013-14 में घरेलू विमान यात्रियों की संख्या 10 मिलियन (million) थी, जो मात्र तीन वर्षों में बढ़कर 158.4 मिलियन तक पहुँच गई। यह रफ़्तार दर्शाती है कि भारत में लोगों की यात्रा प्राथमिकताओं में हवाई यात्रा की ओर बड़ा बदलाव आया है। हालाँकि, कोविड-19 (Covid-19) महामारी ने इस क्षेत्र की वृद्धि को अचानक रोक दिया और यात्रियों की संख्या में गिरावट आई। फिर भी, 2023 में अनुमान लगाया गया कि यह संख्या 152 मिलियन तक पहुँच जाएगी। लेकिन अगर हम वैश्विक तुलना करें तो भारत अभी भी पीछे है। प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा की दर भारत में प्रति वर्ष केवल 0.04 है, जबकि चीन में यह 0.3 और अमेरिका में 2 से भी अधिक है। यह अंतर साफ दर्शाता है कि भारत में अपार संभावनाएँ मौजूद हैं, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल
भारत सरकार का लक्ष्य केवल हवाई यात्रा की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि विमानन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाना भी है। "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" जैसी योजनाओं के तहत घरेलू स्तर पर विमानों और उनके पुर्जों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्पष्ट कहा था कि भारत को जल्द ही अपना स्वदेशी यात्री विमान बनाने और वैश्विक बाजार में उतारने की दिशा में काम करना होगा। इस दिशा में राष्ट्रीय एयरोस्पेस लैब्स (National Airports Labs) द्वारा "सारस" विमान का विकास एक महत्वपूर्ण कदम है। यह स्वदेशी विमान भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया बड़ा प्रयास है। हालांकि यह परियोजना अभी शुरुआती चरण में है और वाणिज्यिक स्तर पर इसकी पूरी सफलता साबित नहीं हुई है, लेकिन यह निश्चित है कि यह भविष्य के लिए आधार तैयार कर रहा है। आज वैश्विक वाणिज्यिक विमान आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी केवल 1-1.5% ही है। यह आँकड़ा छोटा जरूर है, लेकिन इसमें सुधार की अपार संभावनाएँ हैं। यदि भारत स्वदेशी उत्पादन को गति देता है, तो यह हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ सकती है।
वैश्विक कंपनियों की भारत में भूमिका
भारत के विमानन उद्योग में विदेशी कंपनियों की भूमिका भी काफी अहम है। एयरबस और बोइंग जैसी बड़ी वैश्विक कंपनियाँ भारत से लगभग 1.6 बिलियन (billion) डॉलर मूल्य के उत्पाद हर साल खरीदती हैं। इसमें विमान के विभिन्न पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम (electronic system), और इंजीनियरिंग (engineering) सेवाएँ शामिल हैं। भारतीय कंपनियों की आपूर्ति से यह साबित होता है कि भारत वैश्विक कंपनियों के लिए भरोसेमंद साझेदार बनता जा रहा है। फिर भी, एक बड़ी सच्चाई यह है कि भारत में सीधे आपूर्ति करने वाली कंपनियों की संख्या बेहद कम है - मुश्किल से 10। इनमें से अधिकांश कंपनियाँ एमएसएमई हैं, जो अपने छोटे स्तर पर विमान घटकों और स्पेयर पार्ट्स (spare parts) का उत्पादन करती हैं। इसका मतलब यह है कि भारत का योगदान अभी भी सीमित है और बड़े स्तर पर विस्तार की जरूरत है। यदि सरकार नीतिगत सहयोग दे और कंपनियाँ उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाएँ, तो भारत इस क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति का अहम केंद्र बन सकता है।
एमएसएमई और विमानन उद्योग में उनकी भागीदारी
भारत का विमानन उद्योग एमएसएमई क्षेत्र के बिना अधूरा है। देश में 20,000 से अधिक एमएसएमई कंपनियाँ इस क्षेत्र से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई हैं। लेकिन इनमें से केवल 642 ही ऐसी हैं जो सीधे तौर पर विमान घटकों के निर्माण में लगी हुई हैं। इसका अर्थ यह है कि बाकी अधिकतर कंपनियाँ सहायक सेवाओं जैसे एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग (Airport Ground Handling), विमानों की मरम्मत और रखरखाव (MRO) जैसी गतिविधियों में योगदान देती हैं। एमएसएमई का काम करने का तरीका भी चुनौतीपूर्ण है। अधिकांश कंपनियाँ उपठेका प्रणाली (sub-contracting) पर काम करती हैं और वे मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) पर निर्भर रहती हैं। इसका असर यह होता है कि वे स्वतंत्र रूप से बड़े स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पातीं। इसके बावजूद, इन कंपनियों ने रोजगार सृजन और लागत प्रभावी सेवाएँ देने में बड़ी भूमिका निभाई है।
वित्तीय चुनौतियाँ और ऋण तक सीमित पहुँच
एमएसएमई के सामने सबसे बड़ी समस्या पूँजी की कमी है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल 15% एमएसएमई ही बैंकों से ऋण प्राप्त कर पाती हैं। इसके विपरीत, कई अन्य देशों में यह आँकड़ा 45% तक पहुँचता है। यह अंतर इस बात को दर्शाता है कि भारतीय एमएसएमई वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वित्तीय दृष्टि से कमज़ोर हैं। बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयाँ, उच्च ब्याज दरें, और लंबी प्रक्रियाएँ छोटे व्यवसायों के विकास में बड़ी बाधा बनती हैं। नतीजतन, ये कंपनियाँ नई तकनीक अपनाने या अपने उत्पादन को बड़े स्तर तक ले जाने में पिछड़ जाती हैं। यदि सरकार समर्थित ऋण योजनाओं को और आसान बनाए और एमएसएमई को वित्तीय सहायता देने के नए तरीके निकाले, तो भारत का विमानन उद्योग कहीं अधिक मजबूत हो सकता है।
भविष्य की संभावनाएँ और औद्योगिक विमान नीति की ज़रूरत
भारत का विमानन उद्योग अभी संभावनाओं से भरा हुआ है। यदि सही दिशा में कदम उठाए जाएँ, तो यह क्षेत्र न केवल भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है, बल्कि देश को वैश्विक स्तर पर विमान निर्माण का एक प्रमुख केंद्र भी बना सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि एक ठोस और दीर्घकालिक औद्योगिक विमान नीति बनाई जाए। यह नीति निवेश आकर्षित करने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और एमएसएमई को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित होनी चाहिए। साथ ही, विदेशी निर्भरता को कम करके घरेलू अनुसंधान और विकास (R&D) पर ध्यान देना अनिवार्य है। यदि ऐसा हुआ, तो भारत आने वाले दशकों में न केवल घरेलू मांग पूरी करेगा, बल्कि दुनिया भर में विमानों और उनके पुर्जों का निर्यातक भी बन सकता है।
संदर्भ-

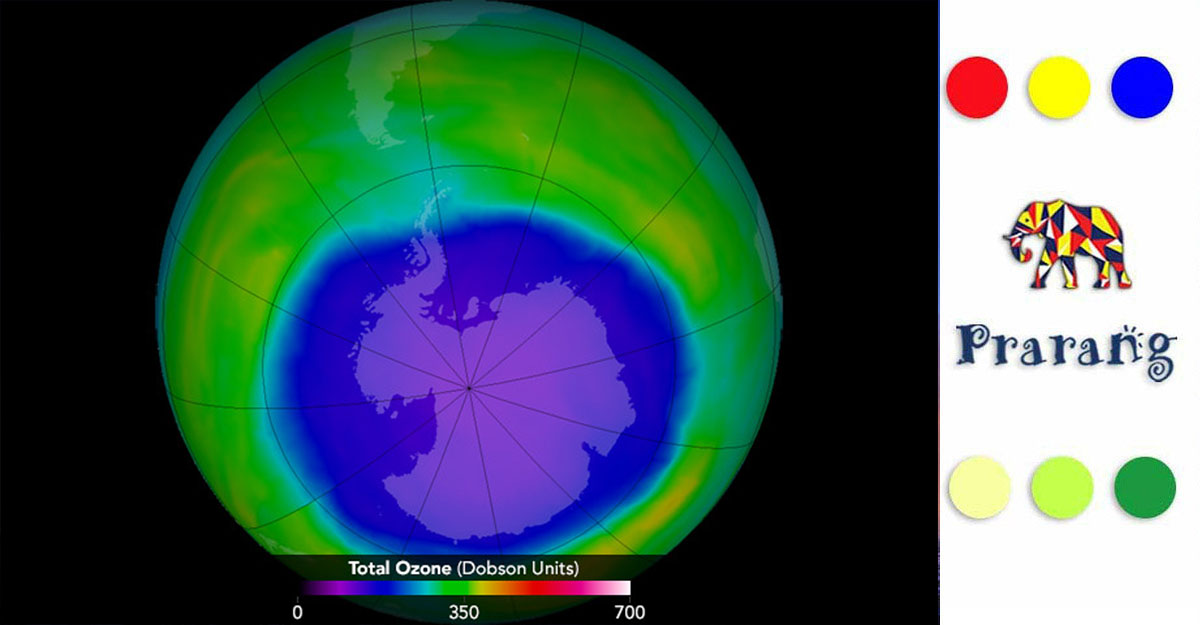


A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.
