
समय - सीमा 280
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1062
मानव और उनके आविष्कार 819
भूगोल 276
जीव-जंतु 319
| Post Viewership from Post Date to 23- Sep-2025 (31st) Day | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 1965 | 73 | 11 | 2049 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

जौनपुरवासियों, क्या आप जानते हैं कि समुद्र सिर्फ तटीय इलाकों तक सीमित नहीं हैं, वहाँ की लहरों और ज्वार-भाटों से मिलने वाली ऊर्जा आने वाले समय में हमारे जैसे ज़िलों तक भी पहुँच सकती है? पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग महासागरों से ढका है, और अब वैज्ञानिक इस अनंत जल-शक्ति को बिजली में बदलने की दिशा में तेज़ी से काम कर रहे हैं। महासागर थर्मल (thermal) ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति और लहरों से बनने वाली ऊर्जा को ‘समुद्री ऊर्जा’ कहा जाता है, जो पूरी तरह अक्षय, कार्बन-तटस्थ (carbon-neutral) और लगातार मिलने वाला स्रोत है। भले ही जौनपुर समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन देश के समुद्री किनारों पर तैयार हो रही ये ऊर्जा परियोजनाएँ आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय ग्रिड (grid) के ज़रिए पूरे देश को प्रभावित करेंगी। ऐसे में यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि समुद्र से पैदा की जाने वाली यह नई ऊर्जा हमारे जैसे कृषि-प्रधान जिलों में भी एक दिन डीज़ल (diesel) और गैस (gas) पर निर्भरता को कम कर सकती है, खासकर सिंचाई, परिवहन और घरेलू ऊर्जा के लिए। यही कारण है कि समुद्री ऊर्जा को अब केवल समुद्र किनारे की तकनीक नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक साझा भविष्य माना जा रहा है।
आज हम विस्तार से समझेंगे कि महासागर में छुपी ऊर्जा के स्रोत कौन-कौन से हैं और ये पारंपरिक ऊर्जा से कैसे अलग हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि महासागर की ऊर्जा की खासियत क्या होती है और यह कैसे काम करती है। फिर हम तीन प्रमुख प्रकारों, ज्वारीय, तरंग और तापीय ऊर्जा, की कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे। इसके बाद, हम देखेंगे कि समुद्र से पेट्रोलियम (petroleum) और प्राकृतिक गैस कैसे निकाली जाती है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। अंत में, हम भारत में समुद्री ऊर्जा की संभावनाओं और भविष्य की योजनाओं को समझने की कोशिश करेंगे।
महासागर: अनंत ऊर्जा का स्रोत
जब नवीकरणीय ऊर्जा की बात होती है, तो अधिकांश लोग सौर और पवन ऊर्जा को ही प्रमुख मानते हैं। लेकिन समुद्र, जो पृथ्वी की सतह के दो-तिहाई से अधिक भाग को घेरे हुए है, ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसकी क्षमता अभी तक पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाई गई है। समुद्र की थर्मल (ऊष्मीय), ज्वारीय और तरंग ऊर्जा, ये तीनों मिलकर एक ऐसी अक्षय ऊर्जा प्रणाली की नींव रख सकती हैं जो 24x7 उपलब्ध हो। विशेष रूप से महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण (OTEC) तकनीक, समुद्र की सतह और गहराई में मौजूद तापमान के अंतर का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करती है। इस तकनीक की खास बात यह है कि यह लगातार और बिना किसी मौसम की निर्भरता के ऊर्जा दे सकती है। यह प्रणाली पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है क्योंकि इसमें ग्रीनहाउस गैसों (greenhouse gases) का उत्सर्जन नहीं होता और यह समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचाए बिना संचालित की जा सकती है। आने वाले समय में, यह तकनीक छोटे द्वीप राष्ट्रों, तटीय क्षेत्रों और ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए एक क्रांतिकारी विकल्प बन सकती है।
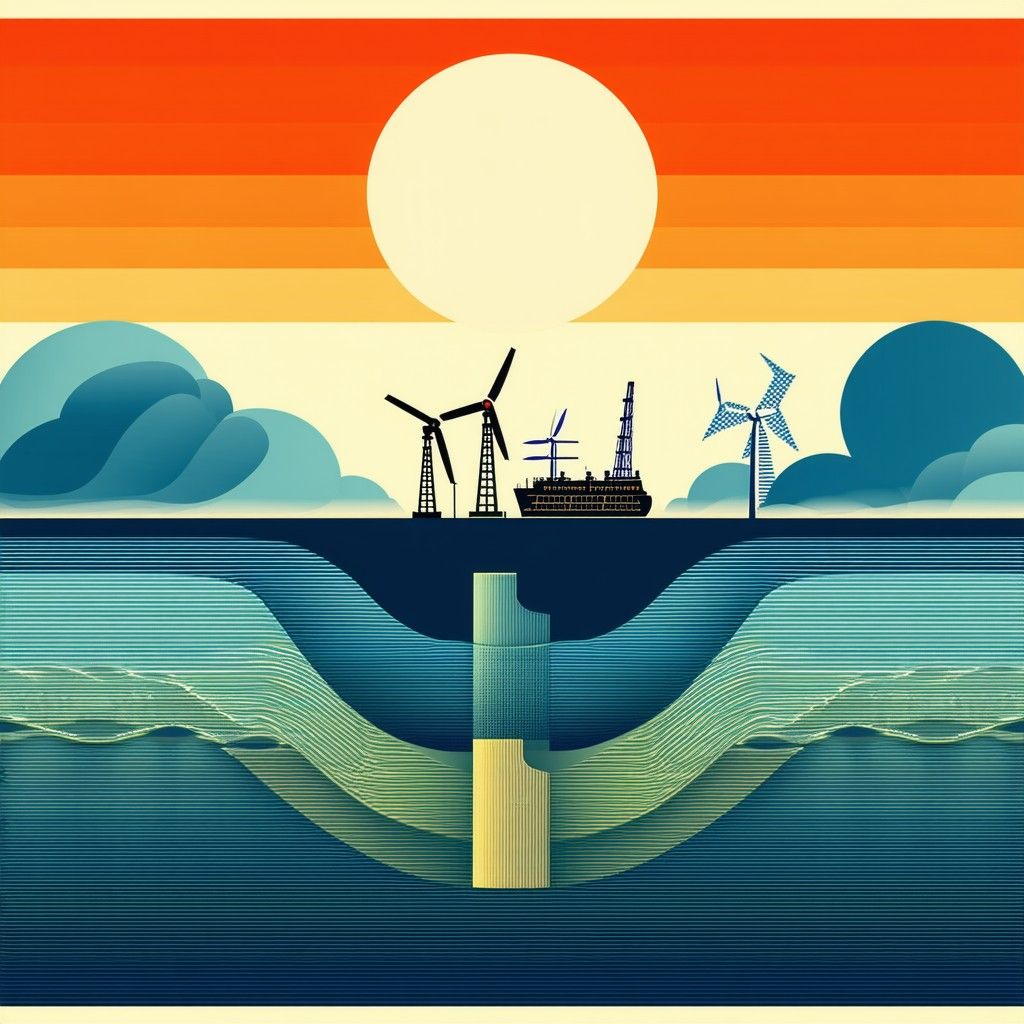
तरंगें, धाराएँ और तापमान: समुद्र में छुपे ऊर्जा के तीन आयाम
समुद्री ऊर्जा की विविधता इसकी सबसे बड़ी ताकत है। समुद्र की लहरें, ज्वारीय धाराएँ, और सतही व गहरे जल के बीच का तापमान, ये सभी विभिन्न तकनीकों से विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र के पानी के चढ़ने-उतरने की नियमित प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, जो पूरी तरह पूर्वानुमानित होती है और इस कारण बेहद विश्वसनीय मानी जाती है। लहरों की गति से उत्पन्न ऊर्जा, जिसे वेव एनर्जी कहा जाता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी होती है जहाँ समुद्र लगातार सक्रिय रहता है। इसके अतिरिक्त, गहरे और सतही समुद्री जल के तापमान में अंतर से ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया (OTEC) उन क्षेत्रों के लिए आदर्श है जहाँ जलवायु गर्म है। जापान, जो प्राकृतिक संसाधनों में सीमित है, अब समुद्री धाराओं जैसे कुरोशियो करंट (Kuroshio Current) से 200 गीगावाट (gigawatt) तक ऊर्जा निकालने की दिशा में काम कर रहा है, जो उसके वर्तमान राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 60% है। यूरोप में स्कॉटलैंड (Scotland) और स्वीडन (Sweden) जैसी जगहों पर टाइडल टरबाइन (tidal turbine) पहले ही व्यावसायिक स्तर पर कार्यरत हैं। इससे पता चलता है कि महासागर ऊर्जा केवल भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि वर्तमान की हकीकत बनती जा रही है।

समुद्र से निकला काला सोना: पेट्रोलियम और गैस की कहानी
समुद्र की ऊर्जा का मतलब केवल नवीकरणीय स्रोत ही नहीं है; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे पारंपरिक ईंधन भी बड़ी मात्रा में समुद्र के गर्भ में छिपे हैं। यह कोई आधुनिक खोज नहीं है, इतिहास में भी समुद्री संसाधनों से ऊर्जा निकाली जाती रही है, जैसे कि व्हेल का तेल, जिसका उपयोग दीपक जलाने, जहाजों के निर्माण और युद्धों में होता था। आज समुद्र तल के नीचे तेल और गैस के विशाल भंडारों का उत्खनन आधुनिक तकनीकों के ज़रिए किया जाता है। विशेष रूप से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारत के अपतटीय तेल और गैस परियोजनाएँ देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती दे रही हैं। गहरे समुद्र में ड्रिलिंग (drilling), सागरमंथन जैसा प्रयास है, जहाँ अत्याधुनिक तकनीकें और जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों के दोहन से आर्थिक समृद्धि तो मिलती है, लेकिन यह आवश्यक है कि पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हुए इनका दोहन किया जाए। यही कारण है कि आज सतत ऊर्जा विकास की दृष्टि से नवीकरणीय और पारंपरिक दोनों स्रोतों को संतुलित रूप से अपनाना महत्वपूर्ण हो गया है।

समुद्री ऊर्जा का राष्ट्रीय महत्व
भारत जैसे देश, जहाँ जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है, के लिए समुद्री ऊर्जा एक लंबी अवधि का समाधान बन सकती है। इससे न केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता भी घटेगी। देश के कई क्षेत्र, चाहे वे समुद्र से लगे हों या दूरस्थ मैदानी हों, ऊर्जा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे लाभान्वित हो सकते हैं। यदि समुद्री ऊर्जा को एक केंद्रीकृत ग्रिड से जोड़ा जाए और उसे स्मार्ट नेटवर्कों (smart networks) के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों तक पहुँचाया जाए, तो यह नवीकरणीय ऊर्जा का एक मजबूत आधार बन सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुँच सकती है, जो ग्रामीण विकास और हरित अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है।
भविष्य की दिशा: तकनीक, निवेश और नीतियाँ
महासागर ऊर्जा की तकनीकें अभी नवाचार के दौर में हैं, लेकिन इनमें तेजी से प्रगति हो रही है। यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे देश समुद्री ऊर्जा को अपने राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति का हिस्सा बना चुके हैं। कई देश विशेष फंडिंग प्रोग्राम (funding program) और अनुदान देकर इन तकनीकों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में भी कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स (pilot projects) शुरू किए गए हैं, लेकिन इन्हें और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। साथ ही, नीति-निर्माताओं को चाहिए कि वे समुद्री ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा मिशन (mission) में समाहित करें और इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश व निवेश वातावरण तैयार करें। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ जैसे आईरेना (IRENA) और यूएनडीपी (UNDP) भी समुद्री ऊर्जा पर वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित कर रही हैं। अगर वैज्ञानिक शोध, औद्योगिक निवेश और सरकारी सहयोग साथ आएँ, तो महासागर भारत के ऊर्जा भविष्य को बदल सकते हैं।
संदर्भ-





A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.