
समय - सीमा 289
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1064
मानव और उनके आविष्कार 837
भूगोल 267
जीव-जंतु 321
| Post Viewership from Post Date to 15- Jul-2025 (31st) Day | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 3138 | 79 | 0 | 3217 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

कपड़ा, मानव सभ्यता के सबसे पुराने आविष्कारों में से एक है, जो केवल तन ढकने का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति, पहचान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी रहा है। भारत जैसे देश में, जहाँ परंपराएं और इतिहास जीवन का अभिन्न अंग हैं, वहाँ वस्त्र उद्योग एक समृद्ध विरासत के साथ जुड़ा हुआ है। मेरठ, जो उत्तर भारत का एक प्रमुख ऐतिहासिक नगर है, खादी और वस्त्र उत्पादन में विशेष स्थान रखता है। इस लेख में हम सबसे पहले प्राचीन भारत में वस्त्रों की शुरुआत और बुनाई की परंपरा को समझेंगे। इसके बाद भारत के कपड़ा उद्योग के विकास, उत्पादन क्षमताओं और रोजगार में इसकी भूमिका पर चर्चा होगी। फिर स्वदेशी आंदोलन में खादी के महत्व और गांधीजी के योगदान को जानेंगे। इसके बाद मेरठ में खादी आंदोलन की ऐतिहासिक घटनाओं और स्थानीय सहभागिता को विस्तार से देखेंगे। लेख के अंतिम भागों में मेरठ के वर्तमान वस्त्र उद्योग की स्थिति और खादी व भारतीय कपड़ों के भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला जाएगा।
प्राचीन भारत और कपड़ा उद्योग की पृष्ठभूमि
कपड़ों का इतिहास मानव सभ्यता की शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है। पुरातत्व साक्ष्यों के अनुसार, लगभग 27,000 वर्ष पूर्व मनुष्यों ने जानवरों की खाल से तन ढकना शुरू किया और धीरे-धीरे बुने हुए वस्त्रों का उपयोग होने लगा। भारत में वस्त्रों की परंपरा अत्यंत पुरानी है, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में भी सूती कपड़े के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। ऋग्वेद, महाभारत और अन्य ग्रंथों में वस्त्रों के उल्लेख मिलते हैं, जो दर्शाते हैं कि भारत के लोगों को वस्त्र निर्माण में दक्षता थी। प्राचीन काल में भारतीय बुनकरों की कलात्मकता विश्वप्रसिद्ध थी, विशेषकर काशी, पटना और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। रेशमी और सूती वस्त्रों का निर्यात मिस्र, रोम और चीन तक होता था। भारत के पारंपरिक कपड़े न केवल आस्थावान धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा रहे, बल्कि वैश्विक व्यापार में भी इनकी अहम भूमिका रही। इस दौर की विविध कढ़ाई और बुनाई तकनीकों, जैसे कि ‘जामदानी’, और ‘ब्रोकेड’ आज भी जीवंत हैं और भारतीय हस्तकला की अनूठी पहचान बन चुकी हैं।

भारत में कपड़ा उद्योग का विकास और वर्तमान स्थिति
भारत का कपड़ा उद्योग सदियों पुराना है और यह परंपरागत हथकरघा से लेकर आधुनिक मिलों तक विस्तृत है। कपास, जूट, रेशम और ऊन के साथ-साथ आज भारत पॉलिएस्टर, नायलॉन जैसे कृत्रिम फाइबरों का भी प्रमुख उत्पादक बन चुका है। यह उद्योग लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसमें 35 लाख से अधिक हथकरघा श्रमिक शामिल हैं। भारत में टेक्सटाइल क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 2.3% और कुल निर्यात का 11% हिस्सा प्रदान करता है। टेक्सटाइल पार्क, मेगा रीजन स्कीम, और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड जैसी सरकारी योजनाओं ने इस उद्योग को मजबूती दी है। इसमें महिला श्रमिकों की भागीदारी भी उल्लेखनीय है, जो सामाजिक-सांस्कृतिक रूपांतरण की दिशा में अहम योगदान देती है। अनुमान है कि 2025-26 तक भारत का कपड़ा बाज़ार 190 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो इसे विश्व स्तर पर एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाता है। भारत का वस्त्र उद्योग न केवल रोजगार सृजन का साधन है, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए आर्थिक संबल का स्रोत भी बन चुका है।

स्वदेशी आंदोलन और खादी की शुरुआत
महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक जागरूकता की भी क्रांति था। खादी, जिसे 'खादर' भी कहा जाता है, इस आंदोलन का मुख्य प्रतीक बनी। यह कपड़ा हाथ से काता और बुना गया होता था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश मिलों के उत्पादों का बहिष्कार कर भारतीय मजदूरों और बुनकरों को समर्थन देना था। गांधीजी मानते थे कि खादी केवल कपड़ा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सपना है, जिसे हर नागरिक अपने श्रम से साकार कर सकता है। उन्होंने चरखे को स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया और इसे हर घर में अपनाने की अपील की। खादी का प्रयोग एक सांस्कृतिक आंदोलन बन गया, जिससे गाँव-गाँव में चरखा चलने लगा। यह आंदोलन केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह गाँवों, महिलाओं, विद्यार्थियों और युवा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनांदोलन का रूप ले चुका था। इसके माध्यम से स्वदेशी भावना और आत्मसम्मान को पुनर्जीवित किया गया।

मेरठ में खादी आंदोलन का प्रभाव और ऐतिहासिक योगदान
मेरठ में खादी आंदोलन ने विशेष गति पकड़ी। 1922 में मेरठ जिले में करीब 60,000 चरखे कार्यरत थे और लगभग 65% आबादी खादी पहनने लगी थी। महिलाओं की भूमिका भी इस आंदोलन में उल्लेखनीय रही—लाला लाजपत राय की भतीजी पार्वती देवी ने महिलाओं से अपील की थी कि जब तक उनके पति खादी न पहनें, उन्हें भोजन न दिया जाए। मेरठ में देवनागरी स्कूल के छात्रों द्वारा खादी प्रदर्शनी, चरखा क्लब की स्थापना, तथा कताई प्रतियोगिताओं जैसे आयोजन इस आंदोलन को जन-जन तक ले गए। 3 मार्च 1928 को मेरठ में होली की जगह विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, जो इस आंदोलन के प्रति जनता के उत्साह को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त मेरठ के खादी प्रेमियों ने गांव-गांव जाकर खादी के लिए प्रचार किया, जनसभाएं आयोजित कीं, और आत्मनिर्भरता का संदेश फैलाया। खादी की बिक्री के लिए स्थानीय मेलों और हाट बाजारों का प्रयोग किया गया, जिससे ग्रामीण जनता भी इस अभियान से जुड़ सकी। मेरठ की भूमिका ने खादी को एक लोकप्रिय लोक आंदोलन में परिवर्तित कर दिया।

मेरठ का वस्त्र उद्योग: वर्तमान परिदृश्य
वर्तमान में मेरठ का वस्त्र उद्योग आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है। यहाँ 30,000 से अधिक पावरलूम कार्यरत हैं, जो इसे उत्तर भारत के बड़े टेक्सटाइल क्लस्टरों में से एक बनाते हैं। खादी के अतिरिक्त मेरठ में तैयार वस्त्र, रेडीमेड परिधान और अन्य कपड़ों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। शहर में छोटे और मध्यम उद्योगों की भरमार है जो विभिन्न प्रकार के कपड़ों—जैसे जर्सी, स्पोर्ट्सवेयर, बेडशीट, टॉवेल, और सूती वस्त्र—का निर्माण करते हैं। मेरठ का टेक्सटाइल क्लस्टर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है और उद्यमियों के लिए कपड़ा व्यवसाय में निवेश का एक आकर्षक केंद्र बन चुका है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही MSME योजनाएँ, स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम, और डिजिटलीकरण ने इस क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी और आधुनिक बना दिया है। मेरठ न केवल घरेलू मांग को पूरा करता है, बल्कि इसके उत्पाद अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी निर्यात किए जा रहे हैं।
खादी और भारतीय कपड़ों का भविष्य
आज खादी और भारतीय पारंपरिक वस्त्रों की वैश्विक मांग बढ़ रही है। विदेशी ब्रांड भारतीय बाजार में आ रहे हैं और खादी के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। खादी अब केवल ग्रामीण भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह अब एक फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। भारत सरकार द्वारा अनुसंधान एवं विकास के लिए करोड़ों रुपए की निधियाँ स्वीकृत की गई हैं, जिससे इस क्षेत्र में नवाचार और गुणवत्ता बढ़ेगी। डिजिटल मीडिया और ई-कॉमर्स के माध्यम से खादी अब वैश्विक उपभोक्ताओं तक पहुँच रहा है। खादी ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में खादी की बिक्री में 33% की वृद्धि हुई है, जो इसका बढ़ता आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व दर्शाता है। उपभोक्ताओं की स्थायित्व और पर्यावरण मित्रता के प्रति बढ़ती रुचि के कारण खादी अब एक "सस्टेनेबल फैशन" के रूप में भी देखा जाने लगा है। आने वाले वर्षों में खादी और भारतीय कपड़ों का बाज़ार और अधिक विस्तृत और सशक्त होने की संभावना है। अगर सही रणनीतियाँ अपनाई जाएँ तो भारत वैश्विक टेक्सटाइल नवाचार और परंपरा का नेतृत्व कर सकता है।



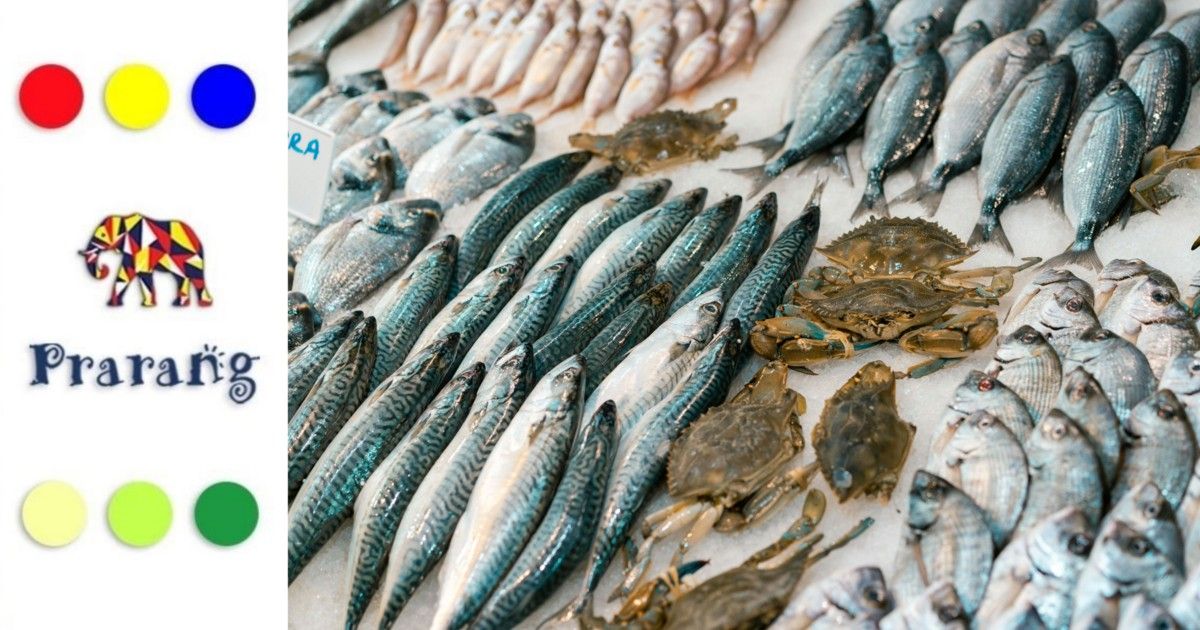
A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.