
समयसीमा 268
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1009
मानव व उसके आविष्कार 801
भूगोल 239
जीव - जन्तु 297
| Post Viewership from Post Date to 07- Aug-2025 (31st) Day | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Subscribers (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 1975 | 239 | 0 | 2214 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

मेरठवासियों, क्या कभी आपने सोचा है — वो चॉकलेट जो आप अपने बच्चों को ख़ुशी में देते हैं, त्योहारों पर मिठाई की जगह रखते हैं, या अकेले में दिल बहलाने के लिए खा लेते हैं… उसकी शुरुआत कितनी दूर से हुई होगी? आज जो चॉकलेट हमारी ज़िंदगी का मीठा हिस्सा बन चुकी है, एक समय पर वह भारत के लिए एक अजनबी स्वाद थी। ब्रिटिश राज के ज़माने में जब पहली बार कोको से बनी चॉकलेट भारत आई, तब यह सिर्फ अंग्रेज़ों और बड़े घरों की रसोई में दिखती थी। लेकिन ज़माना बदला, ज़ायके बदले — और अब ये चॉकलेट मेरठ के हर कोने में, हर उम्र के लोगों की पसंद बन चुकी है।
आज शहर के सुपरमार्केट्स, मिठाई की दुकानों और कैफ़े में आपको चॉकलेट की दर्जनों किस्में मिल जाएंगी। बच्चे हों या बड़े, सबका एक फेवरिट फ्लेवर है — मिल्क चॉकलेट बच्चों की हँसी का हिस्सा है, डार्क चॉकलेट युवाओं की स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है, और त्योहारों में चॉकलेट गिफ्ट पैक्स अब रिश्तों की मिठास का ज़रिया हैं। लेकिन चॉकलेट की कहानी सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। आज भारत न सिर्फ इसे खा रहा है, बल्कि उगा भी रहा है। दक्षिण भारत के राज्य जैसे केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश अब ऐसी कोको फसल उगा रहे हैं जिसकी क्वॉलिटी अफ्रीका जैसे बड़े उत्पादक देशों को टक्कर दे रही है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है, और देश में नए देसी ब्रांड्स जन्म ले रहे हैं।
इस लेख में हम सबसे पहले जानेंगे कि भारत में चॉकलेट की ऐतिहासिक शुरुआत कैसे हुई और कोको की खेती की बुनियाद कैसे पड़ी। फिर बात करेंगे कि किस तरह भारत के दक्षिणी राज्यों में कोको का उत्पादन होता है और खेती की कौन-कौन सी नई प्रवृत्तियाँ सामने आ रही हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि प्रीमियम और जैविक कोको उत्पादन में क्या सीमाएँ हैं और क्यों अधिकांश किसान इससे दूरी बनाए रखते हैं। इसके बाद हम भारत की वैश्विक कोको बाजार में सीमित भागीदारी पर प्रकाश डालेंगे। फिर, भारत में उपभोक्ता बाजार के विस्तार और बदलती प्राथमिकताओं को देखेंगे। अंत में, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स की प्रतिस्पर्धा को समझेंगे और उनका भारतीय बाजार पर क्या प्रभाव है, यह जानेंगे।
भारत में चॉकलेट का ऐतिहासिक आगमन और कोको की शुरुआत
ब्रिटिशों ने 1798 में कोको कोरटालम (तमिलनाडु) में क्रिओल किस्म के पौधों के ज़रिए पहली बार लाया। शुरुआती समय में इसे केवल अभिजात वर्ग ने अपनाया। वहीं, श्रीलंका में भी कोको का प्रचलन था, लेकिन भारत में यह धीमी गति से पैर पसार रहा था। 1960-70 के दशक में कैडबरी ने कोको की खेती को प्रोत्साहित किया, किसानों को उच्च उपज वाले पौधे दिए। इसके साथ खेती तेज़ी से बढ़ी, खासकर दक्षिण भारत में। इस दौर में डेयरी मिल्क चॉकलेट और बॉर्नविटा जैसे उत्पादों ने चॉकलेट को आम भारतीयों के बीच नाम कमाया। इसके पीछे कैडबरी का उद्देश्य था—कच्चा माल स्थानीय रूप से उपलब्ध कराना ताकि लागत और आपूर्ति बेहतर हो जाए। 1979 में केरल कृषि विश्वविद्यालय ने विश्व बैंक की मदद से कोको प्रजनन कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसने और ज्यादा उपज देने वाली संकर प्रजातियाँ विकसित कीं। 1987 में कैडबरी के सहयोग से ये बीज बाज़ार में उपलब्ध कराए गए। इससे कृषि प्रक्रिया वैज्ञानिक बन गई और किसानों की आय भी बेहतर हुई। भारत में चॉकलेट संस्कृति का आरंभ धीरे-धीरे तब हुआ जब अनुभवी लोगों ने इसे त्योहारों, उपहारों और खास मौकों पर अपनाना शुरू कर दिया। इसके बाद यह मिठाई रेगुलर उपयोग वाली वस्तु बन गई। धीरे‑धीरे यह ऐश्वर्य और ग्लैमर से मुक्त होकर घर-घर की रोजमर्रा की स्वादिष्ट वस्तु बन गया।

भारत के कोको उत्पादक राज्य और बदलती खेती की प्रवृत्तियाँ
दक्षिण भारत में कोको खेती का मूल आधार अनुकूल जलवायु और भूमि संरचना है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में वर्षा, तापमान और मृदा इन फसलों से जुड़ी लागत कम करती है। अलग-अलग क्षेत्रों में किसानों ने रणनीतियाँ बदली हैं—राज्य-स्तर पर सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और प्रशिक्षण ने किसानों को प्रोत्साहित किया है। आंध्र प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोको-कैस्केड फार्मिंग को बढ़ावा मिला है, जहां नारियल, सुपारी और पौधे के बीच कोको के पेड़ लगाए जा रहे हैं जिससे उपयोग भूमि की बनावट कई गुना बढ़ रही है। तमिलनाडु में विशेष रूप से पोलाची क्षेत्र ने सफल मॉडल पेश किए हैं—जिसमें किसानों ने नारियल की जगह कोको लगाया। वहीं कर्नाटक में शहरी किसानों ने इंटरक्रॉपिंग मॉडल अपनाया, जहां कम भूमि पर ज्यादा पैदावार होती है। केरल में किसान अब ग्रीन हाउस में कोको की खेती उत्पादन गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं। इन प्रवृत्तियों से न केवल पैदावार बढ़ी है, बल्कि किसानों के आय-सहारे में भी सुधार आया है। व्यक्तिगत स्तर पर किसानों ने इस बदलते मॉडल को अपनाया और अपनी फसल विविधता में कोको को एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में जोड़ा।
प्रीमियम कोको और जैविक खेती की सीमाएँ
प्रीमियम मार्केट में कोको की गुणवत्ता—फ्लेवर प्रोफाइल, नमी स्तर, और प्रसंस्करण विधियाँ—बहुत सख्त होती हैं। लागत अधिक होती है, गांव‑गांव में लेबर का खर्च बढ़ता है, और समय‑समय पर बाज़ार की मांग बदलने से जोखिम भी बड़ा होता है। साथ ही, जैविक कोको के निवेश पर वापस फसल लागत की तुलना में काफी समय में लाभ आता है, इसलिए बहुत से किसान इससे जुड़ने से कतराते हैं। सरकार की योजनाएं अभी सुचारु रूप से प्रभावी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि सब्सिडी और मार्केट लिंकेज का महत्त्व नहीं समझा गया है। इस क्षेत्र में सीधी खरीद प्रणाली, सहकारी मॉडल और अनुदान संबंधी जानकारी किसान तक नहीं पहुंच पा रही। इसी कारण प्रीमियम और जैविक खेती अपेक्षा पूरी न कर पाने के कारण सीमित बनी हुई है।

वैश्विक कोको आपूर्ति में भारत की सीमित भागीदारी
दुनिया भर का लगभग 70% कोको उत्पादन आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया और कैमरून से होता है। आइवरी कोस्ट अकेले वैश्विक उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा नियंत्रित करता है। इसके विपरीत, भारत वैश्विक कोको आपूर्ति का केवल 1% का मामूली हिस्सा उत्पादन करता है। जबकि वैश्विक उपभोग में भारत की भूमिका जबरदस्त रूप से बढ़ी है—यह खपत मात्रा दोगुनी है—लेकिन उत्पादन में यह पीछे रह गया है। सीमित उत्पादन के कारण भारत में कोको मूल्य अस्थिर होता है। इससे उत्पादन लागत अधिक लगती है और किसानों के लिए स्थिर मार्केट नहीं बन पाता। वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका अभी तक मामूली है—यह इस समय इम्पोर्ट-डिपेंडेंट देश की भूमिका निभा रहा है। हालाँकि, सरकार और निजी क्षेत्र अब इसे बदलने की दिशा में पहल कर रहे हैं—उदाहरणस्वरूप, टेक्निकल ट्रेनिंग, वैज्ञानिक अनुसंधान, और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में गुणवत्ता प्रमाणन के माध्यम से भारत की भूमिका बढ़ाने की कोशिशें तेज हुई हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में कोको की खेती अधिकतर छोटे किसानों द्वारा की जाती है, जिनके पास आधुनिक तकनीक या वैश्विक मांगों की जानकारी नहीं है। प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी और निर्यात केंद्रों की दूरी के कारण भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार बाधित होता है। यदि भारत को वैश्विक कोको आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भागीदारी बढ़ानी है, तो नीति निर्माताओं को बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण में भारी निवेश करना होगा। इससे न केवल किसानों को अधिक लाभ मिलेगा बल्कि भारत की आयात निर्भरता भी कम होगी।
भारत में चॉकलेट उपभोक्ता बाजार का तेजी से विस्तार
भारत में चॉकलेट अब सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि जीवनशैली का हिस्सा बन गया है। मध्यवर्गीय परिवारों के अलावा, शहरी युवाओं और वृद्धों में भी इसकी खपत बढ़ी है। डार्क चॉकलेट, जिसकी कोको सामग्री ज्यादा होती है और चीनी कम, स्वास्थ्य‑चेतक उपभोक्ता वर्ग में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। छोटे पैकेट्स, नए फ्लेवर (जैसे मिर्च-कारमेल, इलायची-डार्क), और शुगर-फ्री विकल्प जैसे ट्रेंड्स युवाओं को लुभा रहे हैं।
मिंटेल (Mintel) और बिज़नेस वायर (BusinessWire) के आँकड़े बताते हैं कि 2019–24 के बीच भारत में चॉकलेट बाज़ार की वार्षिक वृद्धि लगभग 12–13% रही—जो वैश्विक औसत से अधिक है। ऑनलाइन बिक्री ने ग्रामीण कस्बों और छोटे शहरों तक पहुंच प्रदान की है। धीरे-धीरे त्योहारों से ऊपर उठकर चॉकलेट रोज़मर्रा के जीवन में ईंधन का काम करने लगी है।
इसके साथ ही, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने भी चॉकलेट की लोकप्रियता को एक नया आयाम दिया है। बड़े-बड़े ब्रांड्स युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, जिनके पास अब खर्च करने की स्वतंत्रता और स्वाद में विविधता की चाह है। हेल्दी स्नैकिंग ट्रेंड, ऑफिस ट्रीट कल्चर और ‘गिल्ट-फ्री डेज़र्ट’ जैसे कॉन्सेप्ट्स भी इस खपत को बढ़ावा दे रहे हैं। यह मांग भारतीय उत्पादन और मार्केटिंग रणनीतियों को लगातार रूपांतरित कर रही है।

भारतीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स का प्रभाव और प्रतिस्पर्धा
कैडबरी की मार्केट हिस्सेदारी लगभग 65–70% है, नेस्ले 20% पर स्थिर है। प्रीमियम ब्रांड जैसे अमूल, आई टी सी, और लोटस ने लोकल फ्लेवर को अपनाकर अपनी छाप छोड़ी है। ड्यूक ऑफ़ दिल्ली (Duke of Delhi) जैसे ब्रांड्स ने नारियल-डार्क, इलायची-डार्क जैसे मिश्रणों के साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों पर ग्रामीण भारतीय स्वाद दिया है।
स्थानीय ब्रांड्स की रणनीति है—स्थानीय फ्लेवर + वैश्विक क्वॉलिटी टोन्ड = ग्लोबल अपील। इंडस्ट्री विश्लेषक मानते हैं कि 2026 तक भारतीय चॉकलेट मार्केट 12.1% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर से बढ़ेगा। इससे किसानों से लेकर ब्रांड्स, स्टार्टअप और पैकेजिंग इंडस्ट्री—सभी को फायदा होगा।
इन प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों ने नवाचार को जन्म दिया है—अब छोटे स्तर के ब्रांड्स भी क्राफ्ट चॉकलेट, शुगर-फ्री, वेगन और फेयर-ट्रेड लेबल के साथ बाज़ार में अपनी जगह बना रहे हैं। भारतीय ब्रांड्स न केवल गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं, बल्कि पैकेजिंग और स्टोरीटेलिंग में भी अंतर ला रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को स्थानीय स्वाद के साथ वैश्विक अनुभव मिल रहा है। यह प्रतिस्पर्धा भारत को न केवल एक बड़ा बाजार बना रही है, बल्कि एक इनोवेशन हब की ओर भी ले जा रही है।
संदर्भ-




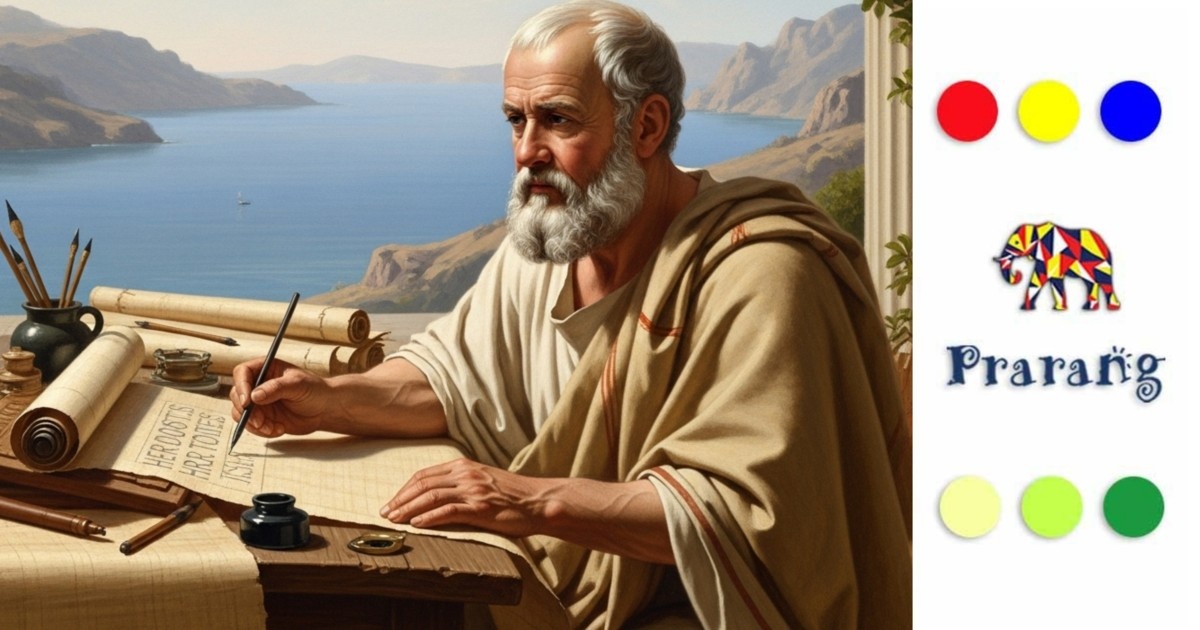
A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.