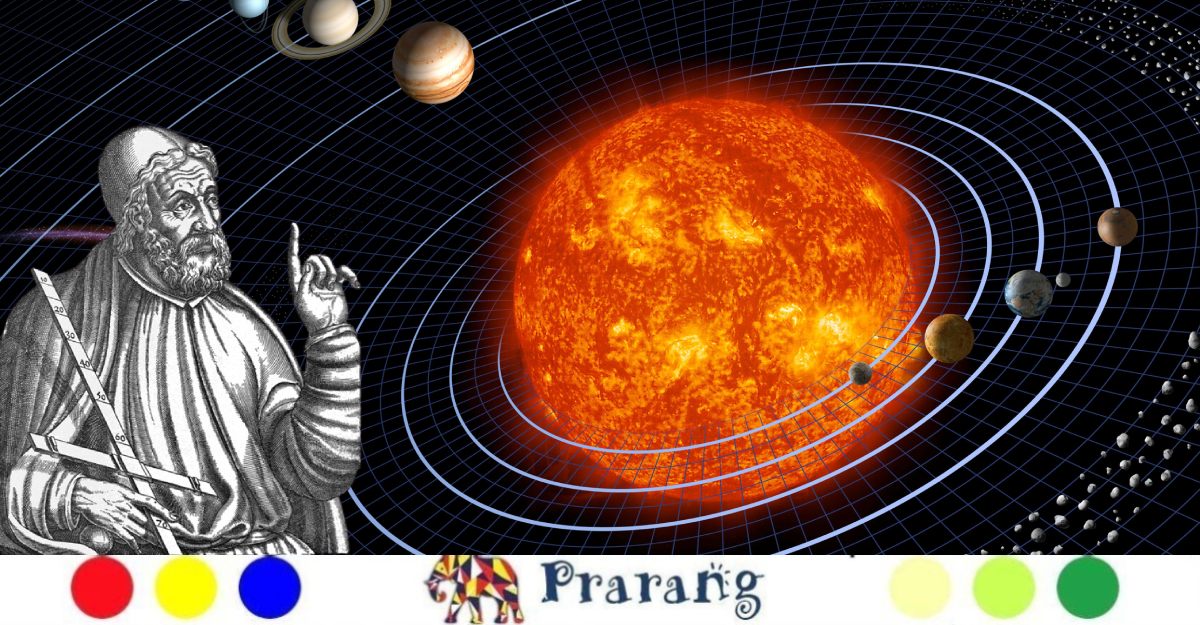समयसीमा 261
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1031
मानव व उसके आविष्कार 801
भूगोल 252
जीव - जन्तु 308
समयसीमा 261
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1031
मानव व उसके आविष्कार 801
भूगोल 252
जीव - जन्तु 308

रामपुरवासियो, क्या आपने भी हाल के दिनों में उस तेज़ आंधी की गूंज सुनी है, जो अचानक आई और पेड़-पौधों को उखाड़ ले गई? क्या आपने उस धूल भरी तूफ़ानी शाम को महसूस किया है जब आसमान पीला हो गया था और घर की खिड़कियां तक थरथरा उठीं? और फिर आई मूसलधार बारिश, जो सड़कें बहा ले गई और ज़िंदगी कुछ देर के लिए ठहर सी गई। ये सब घटनाएं अब कोई इत्तेफाक नहीं हैं, बल्कि बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन की खुली चेतावनी हैं। मौसम वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि उत्तर भारत, विशेषकर रामपुर जैसे इलाके, अब चरम मौसम की घटनाओं के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। ये बदलते हालात सिर्फ मौसम नहीं बदल रहे, बल्कि हमारी खेती, रोज़मर्रा की ज़िंदगी और शहर की बुनियादी संरचनाओं पर गहरा असर डाल रहे हैं।
इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि उत्तर भारत, खासकर रामपुर और उसके आस-पास, किस तरह से बदलते मौसम के प्रभाव में है। सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्तर भारत में हाल के वर्षों में किस प्रकार की चरम मौसम की घटनाएं देखी गई हैं और इनकी वर्तमान तस्वीर क्या है। फिर हम समझेंगे कि मौसम विभाग इस पर किस तरह की चेतावनियां दे रहा है और उनके पीछे कौन से वैज्ञानिक कारण हैं। इसके बाद हम जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानसून में आ रहे असंतुलन पर चर्चा करेंगे। अंत में, हम देखेंगे कि कैसे शहरी क्षेत्रों की अव्यवस्था और खेती पर इस मौसमी बदलाव का सीधा और गंभीर असर हो रहा है।

उत्तर भारत में चरम मौसम की घटनाओं की वर्तमान तस्वीर
पिछले कुछ सालों में, उत्तर भारत के मौसम में एक अजीब सा तनाव देखा जा रहा है, एक ऐसा तनाव जो अब केवल तापमान में उतार-चढ़ाव नहीं रहा, बल्कि तूफानों, भारी बारिश, और असमय बेमौसम घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है। इस साल लखनऊ में 36 घंटे के भीतर 228 मिमी बारिश हुई, जो शहर की सामान्य व्यवस्था को चरमरा देने के लिए काफी थी। वहीं रामपुर में धूल भरी तेज़ आंधियों ने कई दिनों तक आकाश को ढँक रखा और जनजीवन पर गहरा असर डाला। बरेली जैसे शहरों में अचानक बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं, और कई किसान खेतों में काम करते समय इसकी चपेट में आ गए। ये घटनाएं अब एक-दो बार की बात नहीं रहीं। पिछले दो दशकों में उत्तर भारत में ‘एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स’ (Extreme Weather Events - चरम मौसमीय घटनाएं) की संख्या दोगुनी हो चुकी है। यह सब केवल मौसम की मार नहीं है, यह संकेत हैं कि हमारा पर्यावरण कुछ गंभीर बदलावों से गुजर रहा है। हमें इन घटनाओं को एक सतही खबर की तरह नहीं, बल्कि भविष्य के लिए चेतावनी के रूप में देखना होगा।
मौसम विभाग की चेतावनियां और उनका वैज्ञानिक आधार
अक्सर जब मौसम विभाग किसी तूफान या भारी बारिश की चेतावनी देता है, तो आमजन उसे हल्के में ले लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन चेतावनियों के पीछे कितना गहरा और जटिल विज्ञान काम करता है? भारतीय मौसम विभाग (IMD) आज उपग्रहों, रडार (Radar), और अत्याधुनिक कंप्यूटर मॉडलिंग (computer modelling) की मदद से मौसम की बारीकियों को समझता है। उदाहरण के तौर पर, इस वर्ष लखनऊ और आस-पास के क्षेत्रों में जो आंधी आई, उसका कारण था - ‘पश्चिमी विक्षोभ’ (Western Disturbance) और ‘गर्त रेखा’ (Trough Line) का उत्तर भारत से टकराना। जब राजस्थान की तपती गर्मी से गर्म हवा ऊपर उठती है और पश्चिमी विक्षोभ से आई नमी से मिलती है, तो अचानक तूफान, बिजली और तेज़ बारिश की स्थिति बनती है। आईएमडी (IMD) के पूर्वानुमानों में अब “कलर कोडेड अलर्ट्स” (Color Coded Alerts) होते हैं - हरा (सामान्य), पीला (सावधानी), नारंगी (चेतावनी) और लाल (खतरा)। लेकिन फिर भी, स्थानीय प्रशासन और आम नागरिकों का इन पर भरोसा कम है, जिससे नुकसान की आशंका और बढ़ जाती है।

मानसून का असंतुलन और ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव
कभी मानसून को भारत की "जीवन रेखा" कहा जाता था, समय पर आता था, खेतों को सींचता था, और किसान मुस्कान के साथ अन्न उगाते थे। लेकिन अब मानसून एक अनिश्चित मेहमान बन गया है। कहीं यह बहुत पहले आता है और बहुत जल्दी चला जाता है, तो कहीं यह देरी से आता है और रिकॉर्डतोड़ बारिश कर जाता है। इस वर्ष के मानसून पैटर्न (pattern) पर गौर करें, लखनऊ और आसपास के इलाके जून के अंत तक सूखे पड़े रहे, लेकिन जुलाई में एक ही सप्ताह में मासिक औसत से दोगुनी वर्षा हो गई। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) है। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है, तो मानसून हवाओं की दिशा, गति और नमी की मात्रा बदल जाती है। इससे बारिश की प्रवृत्ति असंतुलित हो जाती है। इस असंतुलन का सबसे बड़ा असर यह है कि हम तैयारी नहीं कर पाते, किसान समय पर बीज नहीं डाल पाते, शहर जलनिकासी की व्यवस्था नहीं कर पाते, और आम जनता के लिए हर मानसून एक अनिश्चित संकट बन जाता है।
शहरी इलाकों पर मौसमीय बदलावों का सीधा प्रभाव
लखनऊ, रामपुर, बरेली जैसे शहरों में बढ़ती जनसंख्या और अनियोजित विकास के चलते जलवायु परिवर्तन का असर कहीं अधिक भयावह हो जाता है। भारी बारिश के दौरान नालों का जाम होना, बिजली की आपूर्ति बाधित होना और सड़कें जलमग्न होना अब आम दृश्य हैं। जुलाई माह में लखनऊ के गोमतीनगर, इंदिरा नगर और हजरतगंज जैसे क्षेत्रों में जलभराव ने जनजीवन को पूरी तरह ठप कर दिया। जिन कॉलोनियों में पहले कभी पानी नहीं भरता था, वहां अब गाड़ियां तक डूबने लगी हैं। वजह? अत्यधिक कंक्रीट (concrete), हरियाली की कमी, और प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था का नष्ट होना। यहां तक कि शहरों में बढ़ती गर्मी और घटती हवा की गुणवत्ता भी मौसमीय चरम स्थितियों को और अधिक नुकसानदायक बना देती है। गर्म हवा शहरी क्षेत्रों में ‘हीट आइलैंड’ (Heat Island Effect) बनाती है, जिससे बारिश के समय बादलों की ऊँचाई कम हो जाती है और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ जाती हैं।

कृषि और खाद्य सुरक्षा पर मौसम बदलाव का प्रभाव
जब बारिश की बूंदें खेतों को छूती हैं, तो वे केवल पानी नहीं बरसातीं, वे किसान के सपने, मेहनत और पूरे देश की खाद्य सुरक्षा का भविष्य तय करती हैं। लेकिन आज यही बारिश या तो समय पर नहीं आती, या इतनी ज़्यादा आती है कि फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार की असमय बारिश और तेज़ हवाओं ने धान, मक्का और सब्जियों की फसल को बहुत नुकसान पहुँचाया है। किसान दोहरी मार झेल रहे हैं, एक ओर कर्ज़ और महंगे बीजों का बोझ, दूसरी ओर मौसम की अनिश्चितता। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमराती है, बल्कि शहरी उपभोक्ताओं को भी खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी उछाल का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही, मिट्टी की गुणवत्ता और भूजल स्तर भी बिगड़ रहा है। अधिक बारिश से मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है, और सूखे में सिंचाई के लिए अधिक पानी खींचा जाता है, जिससे भूमिगत जल तेजी से कम होता है।
संदर्भ-
A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.