
समयसीमा 253
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1032
मानव व उसके आविष्कार 818
भूगोल 232
जीव - जन्तु 298
समयसीमा 253
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1032
मानव व उसके आविष्कार 818
भूगोल 232
जीव - जन्तु 298

लखनऊ की ज़मीन पर जब परंपरागत फ़सलों के साथ प्रयोग होने लगे तो एक नया नाम उभरा, मशरूम। आज लखनऊ न केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बल्कि धीरे-धीरे वह मशरूम उत्पादन की भी एक मजबूत इकाई बनता जा रहा है। लखनऊ, जो कभी सिर्फ तहज़ीब और तालीम के लिए जाना जाता था, आज मशरूम उत्पादन का एक नया केंद्र बनता जा रहा है। बदलते वक्त के साथ यहां के किसान अब सिर्फ गेहूं या धान पर निर्भर नहीं हैं, वे मशरूम को एक ऐसा विकल्प मान रहे हैं जो कम लागत, कम जगह और कम समय में ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। इस बदलाव की जड़ में हैं आईसीएआर-सीआईएसएच (ICAR-CISH) जैसे संस्थान, जिन्होंने स्थानीय युवाओं, महिलाओं और सीमित संसाधनों वाले किसानों को न केवल तकनीकी प्रशिक्षण दिया, बल्कि उन्हें एक नया आत्मविश्वास भी दिया है। खेती के नए विकल्पों की तलाश में लगे किसान, अब मशरूम को एक लाभकारी और टिकाऊ व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं। इस परिवर्तन में सीआईएसएच जैसी संस्थाओं का योगदान उल्लेखनीय है, जिन्होंने लखनऊ के युवाओं, महिलाओं और सीमित संसाधनों वाले किसानों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देकर मशरूम की खेती को व्यावसायिक रूप दिया है।
आज हम जानेंगे कि किस प्रकार लखनऊ और उत्तर प्रदेश में मशरूम उत्पादन एक व्यवहारिक व्यवसाय बनता जा रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लखनऊ में मशरूम की खेती किस प्रकार विस्तार पा रही है। फिर, हम संक्षेप में भारत और विश्व में इसकी खेती का इतिहास और पोषण मूल्य समझेंगे। इसके बाद, हम मशरूम की तीन लोकप्रिय किस्मों और उनकी खेती के अनुकूल मौसम व स्थितियों के बारे में जानेंगे। फिर, हम मशरूम से जुड़ी बीमारियों और उनके उपचार पर चर्चा करेंगे। अंत में, हम मशरूम से मिलने वाले आर्थिक लाभ, लागत का विश्लेषण और सरकारी प्रशिक्षण व सहायता योजनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे।
उत्तर प्रदेश व लखनऊ में मशरूम की खेती का विकास और बढ़ती संभावनाएं
उत्तर प्रदेश, विशेषकर लखनऊ और उसके आस-पास के जिले जैसे हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, शाहजहाँपुर और लखीमपुर, मशरूम की खेती के नए केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। पहले जहाँ किसान पारंपरिक फसलों पर निर्भर थे, वहीं अब वे वैकल्पिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और मशरूम इसमें सबसे लाभकारी विकल्पों में गिना जा रहा है। सर्दियों में बटन मशरूम (Button Mushroom) की मांग और उत्पादन दोनों बढ़ जाते हैं, जबकि गर्मियों में ऑयस्टर (Oyster Mushroom) और मिल्की मशरूम (Milky Mushroom) ने बाजार में अपनी अलग जगह बना ली है। ऑयस्टर और मिल्की मशरूम जैसे किस्में विशेष रूप से इस क्षेत्र के मौसम के अनुकूल हैं, जो कम लागत और कम जगह में भी अच्छी पैदावार देती हैं। इस परिवर्तन के पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आईसीएआर- सीआईएसएच, लखनऊ स्थित एक अग्रणी कृषि अनुसंधान संस्थान। यह संस्थान न केवल किसानों और युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देता है, बल्कि उन्हें व्हाट्सएप (WhatsApp) समूहों, ऑन-साइट विज़िट्स (On-site Visits)और वीडियो मार्गदर्शन के माध्यम से निरंतर समर्थन भी देता है। परिणामस्वरूप, कई छोटे उत्पादक भी अपने निवेश पर 5 से 10 गुना लाभ कमा रहे हैं। महिला स्व-सहायता समूह और बेरोजगार युवा इस खेती को एक स्थायी व्यवसाय के रूप में अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। यह स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश विशेषकर लखनऊ, मशरूम उत्पादन और नवाचार में देश का प्रमुख केंद्र बन सकता है।
भारत व विश्व में मशरूम की खेती का संक्षिप्त इतिहास और पोषण महत्त्व
मशरूम की खेती का इतिहास विश्व के अनेक हिस्सों में बहुत प्राचीन रहा है। चीन में लगभग 600 ईस्वी में इसका प्रचलन देखा गया था, जब शिटाके मशरूम (Shitake Mushroom) को औषधीय और खाद्य उपयोग के लिए उगाया जाता था। बाद में 17वीं सदी के दौरान फ्रांस (France) और अन्य यूरोपीय देशों में इसकी वैज्ञानिक खेती शुरू हुई, और 20वीं सदी की शुरुआत में यह अमेरिका में एक प्रमुख उद्योग बन गया। भारत में मशरूम की खेती अपेक्षाकृत देर से शुरू हुई, लेकिन बीते कुछ दशकों में इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी मशरूम उत्पादक राज्यों में है, और इसकी बढ़ती लोकप्रियता इसका प्रमाण है।
मशरूम का पोषण मूल्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका व्यावसायिक पक्ष। इसमें उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन (Protein) (20–40%), फाइबर (Fiber), विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स (Vitamin B-Complex), पोटेशियम (Potassium), कॉपर (Copper) और अन्य खनिज तत्व होते हैं, जबकि वसा और कैलोरी (Calorie) की मात्रा बहुत कम होती है। यह विशेष रूप से शाकाहारियों के लिए एक बेहतरीन प्रोटीन स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त, मशरूम में पाये जाने वाले बायोएक्टिव कंपाउंड (bioactive compound) मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। यही कारण है कि पोषण विशेषज्ञ और डॉक्टर इसे एक ‘सुपरफूड’ की श्रेणी में रखते हैं। कुपोषण की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में यह एक सस्ती और पौष्टिक खाद्य सामग्री बन सकती है।
मशरूम की लोकप्रिय किस्में और उनकी खेती की उपयुक्त परिस्थितियाँ
भारत में मशरूम की अनेक किस्में उगाई जाती हैं, लेकिन तीन प्रमुख प्रकार हैं जो किसानों के बीच सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं - बटन मशरूम, ऑयस्टर (ढींगरी) मशरूम, और स्ट्रॉ मशरूम (Straw Mushroom)।
बटन मशरूम सफेद रंग का होता है और इसे सबसे अधिक खपत किया जाता है। यह ठंडी जलवायु पसंद करता है और इसकी खेती नवम्बर से मार्च तक की जाती है। इसे 14–25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 85–90% आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इस किस्म की मांग होटल, रेस्टोरेंट और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री (processing industry) में बहुत अधिक है।
ऑयस्टर मशरूम की खेती अपेक्षाकृत आसान मानी जाती है, और यह उन किसानों के लिए आदर्श है जो सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। यह अक्टूबर से मार्च के बीच 20–30 डिग्री तापमान और लगभग 80% आर्द्रता में अच्छा उत्पादन देता है। इसका स्वाद उमामी (umami) होता है और यह चिकित्सकीय दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है।
स्ट्रॉ मशरूम, जिसे धान भूसे वाला मशरूम भी कहते हैं, गर्मी में उगाया जाता है और यह अप्रैल से सितंबर के बीच 30–35 डिग्री तापमान में भी बढ़ सकता है। इसकी खेती विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है क्योंकि इसमें लागत कम आती है और कचरे जैसे भूसे का उपयोग किया जा सकता है।

मशरूम की खेती से जुड़े सामान्य रोग और उनका नियंत्रण
मशरूम की खेती करते समय रोगों का प्रबंधन एक अत्यंत आवश्यक पहलू होता है, क्योंकि यह फसल कवक पर आधारित होती है और अत्यधिक नमी एवं तापमान में कई हानिकारक सूक्ष्मजीव पनप सकते हैं।
वर्टिसिलियम (Verticillium) रोग मशरूम की छतरी पर भूरे धब्बे पैदा करता है, जिससे उसकी गुणवत्ता और बाजार कीमत दोनों प्रभावित होती हैं। इससे बचाव के लिए स्वच्छता बनाए रखना और इंडोफिल एम-45 (Indofil M-45) जैसे कवकरोधी रसायन का छिड़काव आवश्यक है।
माइकोगोन (Mycogone) रोग सफेद कवक के रूप में फैलता है और मशरूम में दुर्गंध पैदा करता है। इसकी रोकथाम के लिए मिट्टी और कक्ष को पाश्चुरीकृत करना बेहद जरूरी है।
हरा कवक भी मशरूम की डंठल को नष्ट कर देता है। इसका उपचार डाइथियोकार्बोमेट (Dithiocarbamate) मिश्रण के प्रयोग से किया जा सकता है।
ट्रफल (Truffle) रोग, जो मशरूम की वृद्धि को रोक देता है, तब फैलता है जब तापमान और आर्द्रता का संतुलन बिगड़ता है। इसे नियंत्रित करने के लिए जलवायु प्रबंधन आवश्यक है।
बैक्टीरियल ब्लॉच (Bacterial Blotch), जो मशरूम की टोपी पर भूरे धब्बे डाल देता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट (sodium hypochlorite) के प्रयोग से रोका जा सकता है।
इन सभी रोगों से बचाव का मूल मंत्र है, उचित स्वच्छता, तापमान नियंत्रण, वेंटिलेशन (ventilation) और उन्नत खेती पद्धतियों का पालन। इन उपायों को अपनाकर किसान अपनी फसल को स्वस्थ और मुनाफेदार बना सकते हैं।

मशरूम उत्पादन में लाभ, लागत, प्रशिक्षण और सरकारी सहायता योजनाएं
मशरूम की खेती छोटे व मध्यम किसानों और नवोदित उद्यमियों के लिए एक लाभकारी और सुलभ व्यवसाय है, जो कम लागत और कम जगह में अधिक आय देने की क्षमता रखता है। औसतन 1 किलो मशरूम की उत्पादन लागत ₹100–₹120 तक आती है, जबकि बाज़ार में इसका मूल्य ₹150–₹300 प्रति किलो तक हो सकता है, जो किस्म और गुणवत्ता पर निर्भर करता है। प्रति बैग से 500–800 ग्राम तक उपज प्राप्त होती है और किसान साल में कई बार फसल ले सकते हैं। यदि कोई उत्पादक 1000 बैग लगाता है, तो वह ₹50,000 से ₹1,00,000 तक वार्षिक लाभ कमा सकता है। यदि कोई इसे 100–500 वर्ग फुट के क्षेत्र में शुरू करे, तो उसकी सालाना कमाई ₹1 लाख से ₹5 लाख तक हो सकती है। इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी कई योजनाएं चला रही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) मशरूम इकाई की लागत पर 50% तक सब्सिडी देता है। नाबार्ड (NABARD) और कृषि वित्त निगम (AFC) जैसे संस्थान उपकरणों की खरीद और कार्यशील पूंजी के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिसकी पुनर्भुगतान अवधि 7 वर्ष तक होती है। मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसायियों को ₹10 लाख तक का ऋण बिना गारंटी (Guarantee) दिया जाता है।
संदर्भ-
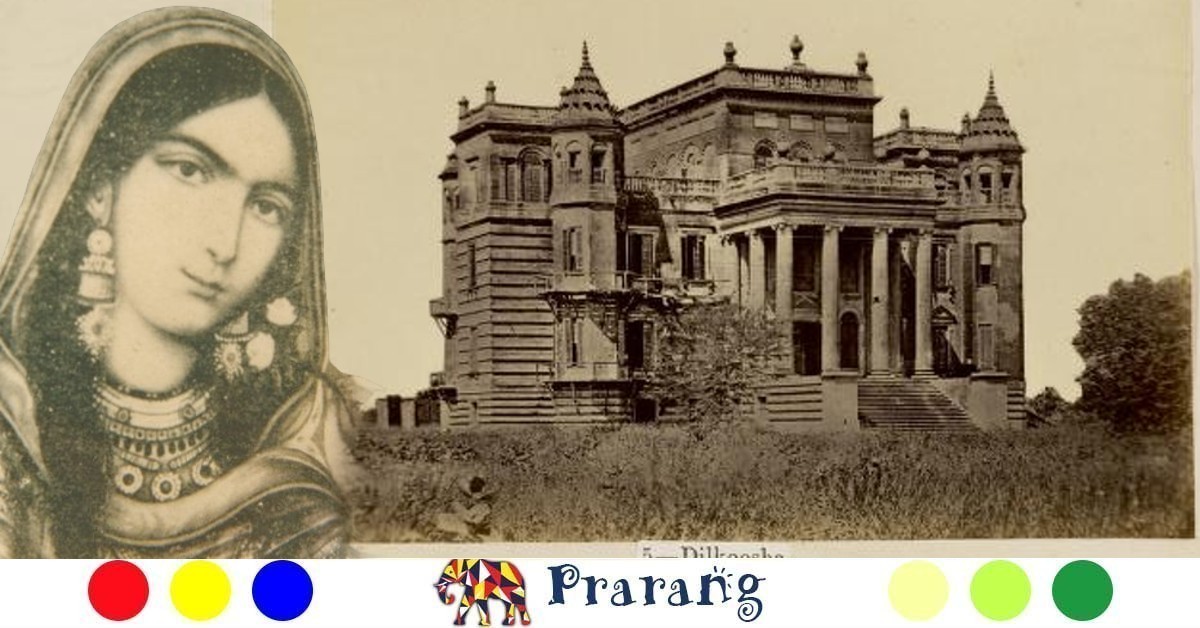
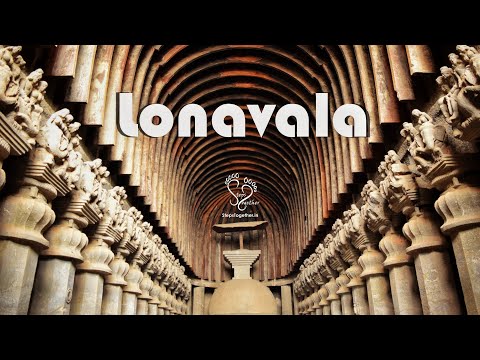


A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.
