
समयसीमा 263
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 998
मानव व उसके आविष्कार 792
भूगोल 237
जीव - जन्तु 292
समयसीमा 263
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 998
मानव व उसके आविष्कार 792
भूगोल 237
जीव - जन्तु 292

मेरठवासियो, क्या आपने कभी यह कल्पना की है कि कोई लोहे का खंभा बिना जंग लगे 1600 वर्षों से सीना ताने खड़ा रह सकता है? ऐसे समय में, जब हम अपनी आधुनिक तकनीक पर गर्व करते हैं और वैज्ञानिक प्रगति को विकास की सबसे ऊँची सीढ़ी मानते हैं — तब एक प्राचीन संरचना हमारे इस विश्वास को चुनौती देती है। यह कोई मिथक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से प्रमाणित तथ्य है। दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित लौह स्तंभ न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह भारत की पारंपरिक धातुकला और वैज्ञानिक सोच का एक ऐसा प्रमाण है, जिसे देखकर आज की पीढ़ियाँ भी आश्चर्यचकित रह जाती हैं। यह लौह स्तंभ सिर्फ एक खंभा नहीं है — यह उन कारीगरों, लुहारों और धातुविदों की मेहनत और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतिफल है, जिन्होंने बिना किसी आधुनिक मशीनरी के, ऐसा धातु निर्मित किया जो आज भी संक्षारण (जंग) से मुक्त है। यह स्तंभ हर उस भारतीय के लिए गर्व का कारण है, जो अपनी विरासत को जानने और समझने की इच्छा रखता है।
आज हम जानेंगे कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का ऐतिहासिक महत्त्व क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ। फिर, हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इस स्तंभ को जंग से बचाने वाला तत्व क्या है और वैज्ञानिक इसके पीछे कौन-से सिद्धांत मानते हैं। इसके बाद, हम अगरिया जनजाति की पारंपरिक लोहा निर्माण प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे, जिन्होंने सदियों तक इस धरोहर को जीवित रखा। अंत में, हम यह जानेंगे कि आज के आधुनिक युग में लोहा कहाँ-कहाँ उपयोग होता है, और क्यों प्राचीन तकनीकों की कमी हमें आज भी खलती है।

दिल्ली के लौह स्तंभ का इतिहास और निर्माण तकनीक
दिल्ली के महरौली स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में खड़ा यह लौह स्तंभ न सिर्फ एक अद्भुत धातु संरचना है, बल्कि प्राचीन भारत की तकनीकी दक्षता और वैज्ञानिक सूझबूझ का प्रतीक भी है। माना जाता है कि इसे गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल (लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी) में बनवाया गया था। स्तंभ की ऊँचाई लगभग 7.21 मीटर है और इसका वजन लगभग 6 टन के आसपास बताया गया है — और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह स्तंभ पूरी तरह लोहे से बना होने के बावजूद 1600 वर्षों में भी जंग से अछूता रहा है। उस दौर की सीमित तकनीक को देखते हुए, इसका ऐसा निर्माण किसी चमत्कार से कम नहीं। यह लौह स्तंभ फोर्ज वेल्डिंग (Forge Welding) नामक पारंपरिक तकनीक से बनाया गया था, जिसमें लोहे के टुकड़ों को ऊँचे तापमान पर गर्म करके आपस में ठोककर जोड़ा जाता था। यह तकनीक आज के उच्चतम औद्योगिक मानकों के सामने भी सिर ऊँचा करके खड़ी है। इस प्रक्रिया में न केवल लोहे को मजबूत बनाया गया, बल्कि उसका सतही ढांचा ऐसा तैयार किया गया जो समय और मौसम की मार झेलने में सक्षम हो। खास बात यह भी है कि इसमें इस्तेमाल किए गए लोहे में कार्बन की मात्रा बेहद कम है, जिससे उसकी संरचनात्मक स्थिरता और अधिक बनी रहती है। यह स्तंभ अपने आप में धातुकला, स्थापत्य और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इतना विशिष्ट है कि यह विश्वभर के धातु विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का केंद्र बन चुका है।

लौह स्तंभ के संक्षारण प्रतिरोध का रहस्य
अब प्रश्न उठता है कि आखिर यह लौह स्तंभ जंग से कैसे बचा रहा? इस रहस्य को समझने के लिए वर्षों तक शोध हुए हैं। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों ने स्तंभ की संरचना और उसकी सतह का गहराई से अध्ययन किया। शोध में पाया गया कि इस स्तंभ की सतह पर आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट (Iron Hydrogen Phosphate Hydrate) नामक एक रासायनिक परत विकसित हुई है, जो इसे वायुमंडलीय नमी और ऑक्सीजन के संपर्क से बचाती है। यही परत जंग की शुरुआत को रोकने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा एक और यौगिक, जिसे वैज्ञानिकों ने मिसवाइट (Misawite) नाम दिया है — जो लोहे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है — वह भी स्तंभ की सतह पर एक अतिसूक्ष्म परत बनाता है, जो बाहरी तत्वों से संरचना की रक्षा करता है। परंतु विज्ञान की तमाम कोशिशों के बावजूद, कोई भी एकमात्र सिद्धांत इस रहस्य को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर सका है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस स्तंभ के निर्माण में इस्तेमाल हुआ शुद्ध लोहा, और उसमें धातुमल (slag) की मात्रा, दिल्ली की अपेक्षाकृत शुष्क जलवायु और निर्माण के दौरान किया गया सतह परिष्करण (Surface Finishing) — ये सभी मिलकर इसके संक्षारण प्रतिरोध का रहस्य रचते हैं। इसके अतिरिक्त, निर्माण के बाद हुई प्राकृतिक ऑक्सीकरण प्रक्रिया ने भी इस पर स्थायी परत बना दी, जिससे यह मौसमीय प्रभावों से स्वयं को बचा सका।

अगरिया जनजाति और उनकी पारंपरिक लौह निर्माण तकनीक
भारत की प्राचीन धातुकला की समझ सिर्फ राजसी दरबारों या वास्तुकारों तक सीमित नहीं थी — यह ज्ञान उन समुदायों में भी मौजूद था जिन्हें आज हम “जनजातियाँ” कहते हैं। ऐसी ही एक प्रमुख जनजाति थी — अगरिया, जो मध्य भारत के कोरबा, छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करती थी। ये लोग सदियों से जंगलों में पारंपरिक भट्टियों का उपयोग करके लोहा बनाते आ रहे थे। इस प्रक्रिया की शुरुआत से पहले वे धार्मिक अनुष्ठान और पारंपरिक रीति-रिवाज़ों का पालन करते थे, जिससे यह साफ़ झलकता है कि उनके लिए धातु निर्माण केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कार्य भी था। उनकी यह पारंपरिक तकनीक बेहद प्रभावशाली थी — भले ही उन्होंने कभी आधुनिक रसायनशास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन उनका अनुभव और सूझबूझ असाधारण थी। वे लौह अयस्क को लकड़ी की कोयले के साथ मिट्टी की भट्टियों में गर्म करते थे और प्रक्रिया को सटीक तापमान नियंत्रण के साथ संचालित करते थे — यह एक पूर्ण विज्ञान था, जिसे वे पीढ़ियों से मौखिक परंपरा में सुरक्षित रखे हुए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान जब भारत की कई स्वदेशी परंपराओं पर प्रतिबंध लगाया गया, तब अगरिया जनजाति की यह परंपरा भी धीरे-धीरे दम तोड़ने लगी। अंग्रेजों ने उन्हें “असभ्य” और “अपराधी जाति” करार देकर सामाजिक हाशिये पर ढकेल दिया, जिससे उनका जीवन और ज्ञान दोनों ही संकट में आ गए।

आधुनिक युग में लोहा: उपयोग और प्राचीन तकनीकों की कमी की टीस
आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ लोहे के बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है। ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज़, पुल, इमारतें, मशीनें — हमारी पूरी औद्योगिक और तकनीकी दुनिया इस धातु पर निर्भर है। और इसके बावजूद, हम ऐसा लोहा नहीं बना पाए हैं जो दिल्ली के लौह स्तंभ जैसा समय की मार झेल सके। यह एक ऐसी विडंबना है जो बार-बार यह सवाल उठाती है: क्या आधुनिकता ने हमारी परंपरागत धरोहरों और तकनीकों को पीछे छोड़ दिया है? हमें यह मानना होगा कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान केवल कथाओं या किंवदंतियों तक सीमित नहीं था — वह अनुभवजन्य और व्यावहारिक था। आज हम कंप्यूटर और रोबोट की मदद से योजनाएँ बनाते हैं, लेकिन वह संवेदनशीलता और पर्यावरण के साथ सामंजस्य, जो पुराने कारीगरों के हाथों में थी, वह खोती जा रही है। विज्ञान और तकनीक की दिशा में हमारी तेज़ रफ्तार ने हमें स्थायित्व और टिकाऊपन (durability) की सोच से दूर कर दिया है। जहाँ पहले एक संरचना सदियों तक खड़ी रहती थी, वहीं आज निर्माण कार्य केवल 30–40 वर्षों की उम्र के हिसाब से किया जाता है। मेरठ जैसे सांस्कृतिक केंद्रों के लिए यह सिर्फ एक ऐतिहासिक सीख नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है — कि यदि हम अपनी जड़ों से जुड़कर पारंपरिक विज्ञान को फिर से समझने और उपयोग में लाने की कोशिश करें, तो हम कई आधुनिक समस्याओं का समाधान अपनी ही विरासत में पा सकते हैं। क्या हम तैयार हैं उस ज्ञान को फिर से अपनाने के लिए, जिसे हमने खुद पीछे छोड़ दिया? यह केवल इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य का भी रास्ता है — एक ऐसा रास्ता जो टिकाऊ, आत्मनिर्भर और संस्कृति से जुड़ा हुआ हो।
संदर्भ-
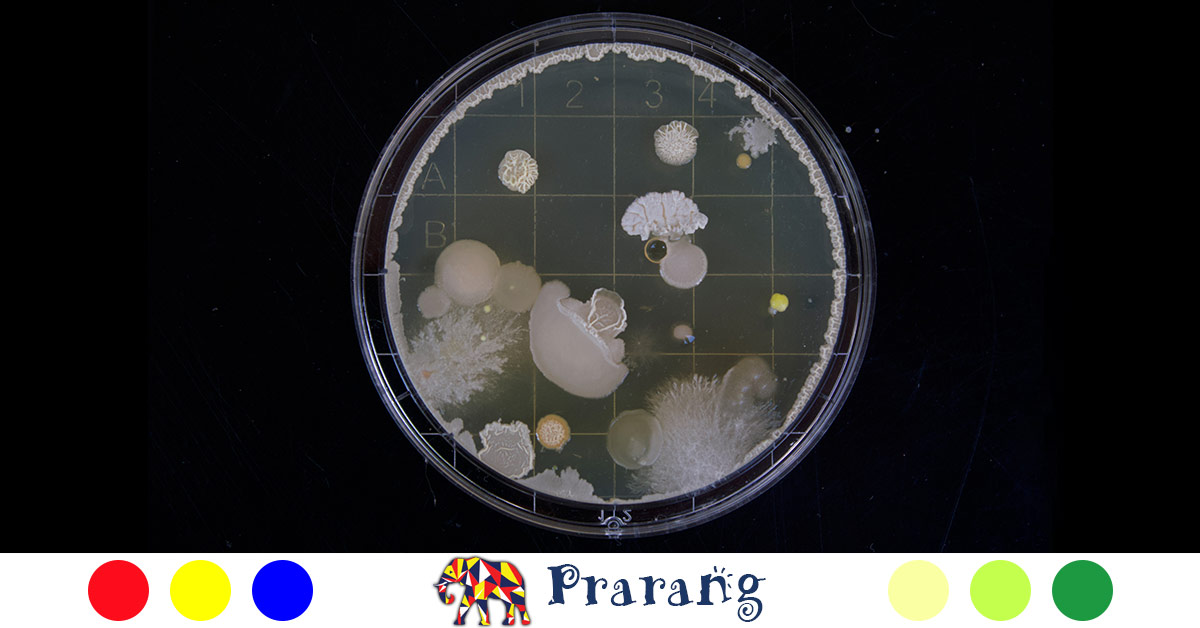



A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Total Viewership — This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.
D. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.
