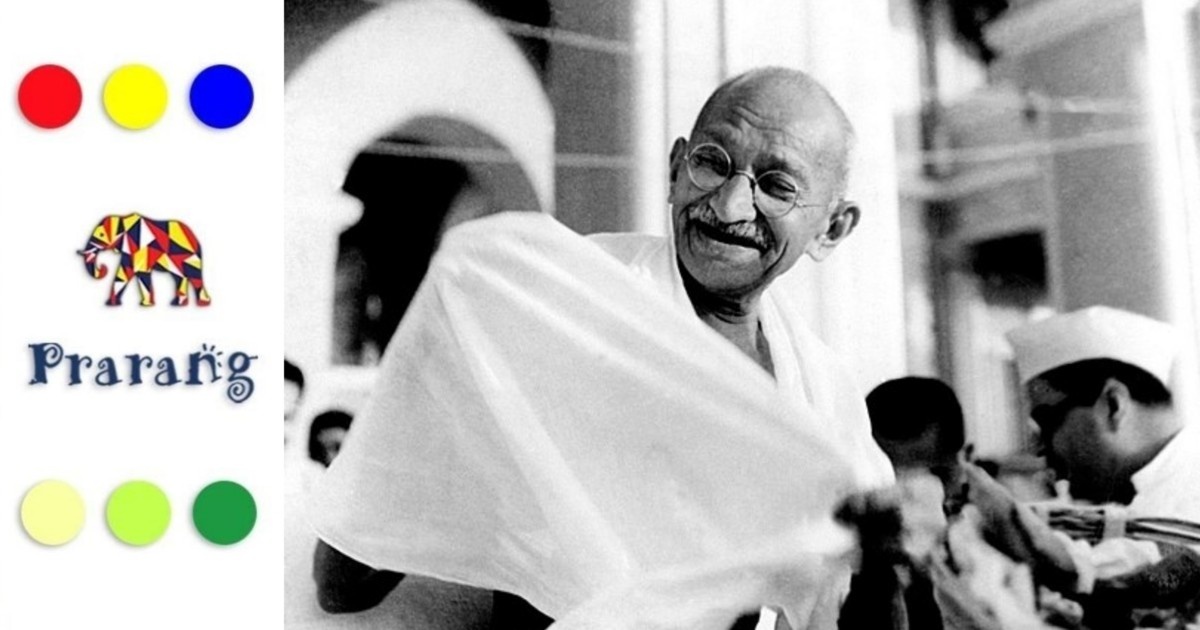भारत में जलवायु और भौगोलिक विविधता के कारण मिट्टी की कई प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर (ICAR)) ने भारत की मिट्टियों को आठ प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकार हैं—जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट और क्षारीय मृदा । उत्तर प्रदेश के कई अन्य शहरों की तरह, रामपुर में भी सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है।
इसके अलावा, खरीफ़ फ़सलें, पूरी तरह से मानसून पर निर्भर होती हैं। इन फ़सलों की बुवाई जुलाई से अक्टूबर के बीच होती है। उदाहरण के तौर पर—धान, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन और मूँगफली खरीफ़ फ़सलों में शामिल हैं। दूसरी ओर, रबी फ़सलें मानसून ख़त्म होने के बाद सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में काटी जाती हैं। इन फ़सलों की बुवाई का समय अक्टूबर से अप्रैल तक होता है। इनके उदाहरण हैं—गेहूँ, जौ, सरसों, जई, चना और अलसी।
आज हम भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों और उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही, हम इन मिट्टियों के भारत में वितरण, इनमें उगाई जाने वाली फ़सलों, इनके पोषक तत्वों और रासायनिक संरचना के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद, खरीफ़ और रबी फसलों के लिए आदर्श मिट्टी की आवश्यकताओं पर भी प्रकाश डालेंगे।
भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ
 1) जलोढ़ मृदा (Alluvial Soil):
1) जलोढ़ मृदा (Alluvial Soil):
जलोढ़ मृदा, नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट और तटीय क्षेत्रों की लहरों के कारण बनती है। यह मुख्य रूप से सिंधु-गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली और तटीय इलाकों में पाई जाती है। भारत की लगभग 46% भूमि पर जलोढ़ मिट्टी है, जो देश की 40% से अधिक जनसंख्या का समर्थन करती है।
जलोढ़ मृदा के रासायनिक गुण: यह मृदा, नाइट्रोजन की कमी से ग्रस्त होती है, लेकिन इसमें पोटाश, फ़ॉस्फ़ोरिक एसिड और क्षार प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसका लौह ऑक्साइड और चूने की मात्रा क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है।
भारत में जलोढ़ मृदा का वितरण: जलोढ़ मृदा मुख्यतः सिंधु-गंगा-ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, सिवाय उन इलाकों के जो रेगिस्तानी रेत से ढके हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा क्षेत्रों को डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा, नर्मदा और ताप्ती घाटियों के कुछ हिस्सों और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी यह मिट्टी पाई जाती है।
जलोढ़ मृदा में उगाई जाने वाली फ़सलें: यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। इसमें मुख्यतः धान, गेहूँ, गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट, मक्का, तिलहन, सब्ज़ियाँ और फल उगाए जाते हैं।
 2) लाल मृदा (Red Soil):
2) लाल मृदा (Red Soil):
लाल मृदा, पुरानी (आर्कियन) ग्रेनाइट चट्टानों पर विकसित होती है और भारत के एक बड़े हिस्से में पाई जाती है। इसकी विशेषताएँ वर्षा के आधार पर बदलती हैं, और कुछ प्रकार की लाल मिट्टी तेज़ जल निकासी के लिए उपयुक्त होती हैं। यह मृदा, लौह (आयरन) और पोटाश से भरपूर होती है, लेकिन अन्य खनिजों की इसमें कमी होती है।
लाल मिट्टी की रासायनिक संरचना: इस मिट्टी में फ़ॉस्फ़ेट, चूना, मैग्नीशिया, ह्यूमस और नाइट्रोजन की मात्रा सामान्यतः कम होती है।
भारत में लाल मृदा का वितरण: लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड तक, और राजमहल से काठियावाड़ तक फैली हुई है।
लाल मृदा में उगाई जाने वाली फ़सलें: यह मिट्टी धान, गन्ना, कपास, बाजरा और दालों की खेती के लिए उपयुक्त है। कावेरी और वैगई नदी घाटियाँ अपने लाल जलोढ़ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध हैं, जो विशेष रूप से धान की खेती के लिए आदर्श मानी जाती हैं।
 3) काली मृदा (Black Soil):
3) काली मृदा (Black Soil):
काली मिट्टी, अत्यधिक चिकनी होती है, जिससे यह बहुत उपजाऊ बनती है। यह मिट्टी नमी को अच्छी तरह से बनाए रखती है, गीली होने पर फैलती है, और गर्मियों में सूखकर दरारें बनाती है, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन प्रवाह होता है।
काली मृदा की रासायनिक संरचना: इस मिट्टी में लौह और चूना भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन और फ़ॉस्फ़ोरस की कमी होती है।
भारत में काली मृदा का वितरण: काली मिट्टी, मुख्य रूप से दक्कन के ज्वालामुखीय पठार क्षेत्र में पाई जाती है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में फैली हुई है।
काली मृदा में उगाई जाने वाली फ़सलें: यह मिट्टी कपास के लिए आदर्श है, इसलिए इसे “रेगर” और “ब्लैक कॉटन सॉयल” भी कहा जाता है। इसके अलावा, यह गेहूँ, ज्वार, अलसी, तंबाकू, अरंडी, सूरजमुखी, बाजरा, धान, गन्ना, सब्ज़ियाँ और फलों की खेती के लिए भी उपयुक्त है।
 4. रेगिस्तानी मृदा (Desert Soil):
4. रेगिस्तानी मृदा (Desert Soil): ये मृदा, शुष्क और अर्ध-शुष्क परिस्थितियों में विकसित होती है और मुख्य रूप से हवा के द्वारा जमा होती है।
भारत में वितरण: रेगिस्तानी मिट्टी, मुख्य रूप से राजस्थान, अरावली पर्वत की पश्चिमी दिशा, उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों और पंजाब के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है।
रासायनिक संरचना: रेगिस्तानी मिट्टी, रेत से लेकर बजरी तक होती है, जिनमें जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन की कमी होती है और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। इनमें घुलनशील लवणों की उच्च मात्रा होती है, लेकिन नमी कम और पानी को बनाए रखने की क्षमता भी कम होती है।
महत्वपूर्ण फ़सलें: इंदिरा-गांधी नहर से पानी की उपलब्धता ने पश्चिमी राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टियों के कृषि परिदृश्य को बदल दिया है। इन मिट्टियों में मुख्य रूप से बाजरा, दालें, ग्वार और चारा उगाए जाते हैं, जिनके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है।
 5. लैटराइट मृदा (Laterite Soil):
5. लैटराइट मृदा (Laterite Soil): ये मृदा मानसून जलवायु की विशेषता है, जो मौसमी वर्षा से उत्पन्न होती है । वर्षा के दौरान चूना और सिलिका धुलकर मिट्टी में लौह ऑक्साइड और ऐल्यूमीनियम की अधिकता छोड़ देती हैं, जिससे लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लैटराइट मिट्टी, वायुमंडल के संपर्क में आने पर तेज़ी से कठोर हो जाती है, जो इसे दक्षिण भारत में इमारतों की ईंटों के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है।
भारत में वितरण: ये मिट्टियाँ मुख्य रूप से पठारी इलाकों, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियां, सतपुड़ा, विंध्य, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम के उत्तर कचहरी पहाड़ियां और मेघालय के गारो पहाड़ों में पाई जाती हैं।
रासायनिक संरचना: ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.7% हिस्सा कवर करती हैं। मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। उच्च क्षेत्रों की मिट्टियाँ सामान्यतः निचले क्षेत्रों की मिट्टियों से अधिक अम्लीय होती हैं। ये मिट्टी, लौह और ऐल्यूमीनियम में समृद्ध होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन, पोटाश, कैल्शियम और जैविक पदार्थों में कमी होती है।
महत्वपूर्ण फ़सलें: इन मिट्टियों में मुख्य रूप से धान, रागी, गन्ना और काजू की खेती की जाती है।
 6. वन और पर्वतीय मिट्टी (Forest and Mountain Soils):
6. वन और पर्वतीय मिट्टी (Forest and Mountain Soils): ये मिट्टी, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.7% हिस्सा कवर करती है। इन मिट्टियों का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। उच्च क्षेत्रों की मिट्टियाँ निचले क्षेत्रों की तुलना में अधिक अम्लीय होती हैं। हालांकि, इनकी उर्वरता कम होती है, लेकिन ये अच्छे तरीके से खाद देने पर उपजाऊ हो जाती है।
रासायनिक संरचना: ये मिट्टियाँ लौह और ऐल्यूमीनियम में समृद्ध होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन, पोटाश, कैल्शियम और जैविक पदार्थों में कमी होती है।
भारत में वितरण: ये मिट्टियाँ मुख्य रूप से पठारी क्षेत्रों के ऊंचे इलाकों, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियां, सतपुड़ा, विंध्य, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम के उत्तर कचहरी पहाड़ियां और मेघालय के गारो पहाड़ों में पाई जाती हैं।
7. क्षारीय और लवणीय मृदा (Saline and Alkaline Soil): लवणीय मिट्टियाँ तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल के घुसने और शुष्क क्षेत्रों में कैल्सीफिकेशन के कारण पाई जाती हैं। ये मिट्टियाँ अपनी क्षारीयता के कारण अधिकांश फ़सलों के लिए अनुपयुक्त होती हैं। हालांकि, इन मिट्टियों को जल निकासी और मिट्टी सुधार उपायों के माध्यम से कृषि के लिए पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने चारा फसलों के लिए किया है।
 8. पीट / दलदली मृदा (Peaty / Marshy Soil):
8. पीट / दलदली मृदा (Peaty / Marshy Soil): यह मिट्टी उच्च वर्षा और आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां बहुत कम वनस्पति वृद्धि होती है। मृत जैविक पदार्थों की उच्च मात्रा के कारण यह मिट्टी क्षारीय और काली होती है। ये मृदा, उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों जैसे कि केरल के बैकवाटर्स, पूर्वोत्तर भारत आदि में पाई जाती है और ये अत्यधिक अम्लीय होती है। यह मिट्टी, गीली भूमि कृषि का समर्थन करती है और चावल तथा जलीय फसलों के लिए उपयुक्त होती है।
रबी फ़सलों के लिए आदर्श मिट्टी की आवश्यकताएँ
रबी फ़सलें अच्छी तरह से जल निकासी वाली उर्वर, चिकनी दोमट से लेकर मंझली काली मिट्टी में सबसे अच्छे से उगती हैं। हालांकि, किसान बालू-दोमट और काली मिट्टी में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। भारी मिट्टियाँ, जिनमें जल निकासी की समस्या हो, अनुकूल नहीं होतीं क्योंकि गेहूं जलभराव के प्रति संवेदनशील है।
इन फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मौसम शुष्क और ठंडा होता है। गेहूं जैसी रबी फ़सल के लिए आदर्श अंकुरण के लिए 20 से 25ºC का तापमान सर्वोत्तम होता है। बुवाई के तुरंत बाद होने वाली बारिश अंकुरण में रुकावट डालती है और अंकुर का सड़ना बढ़ाती है, जबकि उच्च आर्द्रता और कम तापमान जंग के हमले के लिए आदर्श होते हैं।
खरीफ़ फ़सलों के लिए आदर्श मिट्टी
उर्वर, अच्छी तरह से जल निकासी वाली जलोढ़ या सामान्य लाल दोमट मिट्टी, जो मोटे तत्वों से मुक्त हो और नाइट्रोजन से भरपूर हो, मक्के जैसे खरीफ़ फसलों की खेती के लिए आदर्श होती है। मक्का को विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, जिनमें बालू-दोमट से लेकर चिकनी दोमट तक शामिल हैं। हालांकि, उबड़-खाबड़ ज़मीनें इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती हैं, यह विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है। मिट्टी में अच्छा कार्बनिक पदार्थ और पानी को बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए, और pH 5.5-7.5 के बीच होना चाहिए, ताकि उपज बढ़ सके। भारी चिकनी मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती।
संदर्भ
https://tinyurl.com/5xmb9jcx
https://tinyurl.com/5e6kw4js
https://tinyurl.com/57vpdh2a
https://tinyurl.com/bd3dze87
https://tinyurl.com/7hpre3v5
चित्र संदर्भ
1. हल जोतते भारतीय किसान को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
2. जलोढ़ मृदा को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. लाल मृदा को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. काली मृदा को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
5. रेगिस्तानी मृदा को संदर्भित करता एक चित्रण (Pexels)
6. लैटराइट मृदा को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
7. कैलिफ़ोर्निया, यू इस ए में स्थित योजमाइट राष्ट्रीय उद्यान की पर्वतीय मृदा को संदर्भित करता एक चित्रण (pxhere)
8. जंगल में एक पोखर
(puddle) को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)