
समयसीमा 264
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1034
मानव व उसके आविष्कार 803
भूगोल 253
जीव - जन्तु 310
| Post Viewership from Post Date to 15- Aug-2025 (31st) Day | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Subscribers (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 2459 | 121 | 0 | 2580 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

राजस्थान की रेत में जब सूरज की किरणें चमकती हैं, तो वहां की संस्कृति में सबसे पहले जो दृश्य उभरता है, वह है — ऊँटों की कतारें, रंग-बिरंगे वस्त्रों में सजे रायका समुदाय के पशुपालक, और उनके जीवन में ऊँटों की अनोखी भूमिका। जैसलमेर से बीकानेर तक, जहां-जहां रेत के टीले फैले हैं, वहां ऊँटों की आहट और उनके साथ जुड़ी परंपराएँ सुनाई देती थीं। लेकिन आज, रेगिस्तान का यह गौरवमयी 'जहाज' खुद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। आधुनिक जीवनशैली, बदलती अर्थव्यवस्था और पारंपरिक रीति-नीतियों में आई दरारें इस संकट की मुख्य वजह बन गई हैं।
इस लेख में हम राजस्थान की ऊँट संस्कृति को करीब से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यह रायका समुदाय की पारंपरिक जीवनशैली में कैसी गहराई से रची-बसी है। हम इतिहास के उन दौरों पर नज़र डालेंगे जहाँ ऊँटों ने गंगा रिसाला से लेकर बीएसएफ तक अहम सैन्य जिम्मेदारियाँ निभाईं। साथ ही, यह भी देखेंगे कि आधुनिक बदलावों ने ऊँटों की उपयोगिता और उनसे जुड़ी परंपराओं को कैसे प्रभावित किया। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऊँटनी का दूध, जिसे कभी सिर्फ पारंपरिक मान्यताओं से जोड़ा जाता था, आज डेयरी उद्योग में कैसे एक नया रूप ले रहा है। अंत में, हम भारत में ऊँटों की अलग-अलग नस्लों और उनके संरक्षण से जुड़ी जटिल चुनौतियों पर भी बात करेंगे।

राजस्थान की ऊँट संस्कृति और रायका समुदाय की परंपराएँ
राजस्थान में ऊँट न केवल परिवहन और व्यापार का साधन रहा है, बल्कि वह समुदायों की संस्कृति और धर्म का अभिन्न अंग भी रहा है। विशेषकर रायका या रेबारी समुदाय ने ऊँटों के साथ ऐसा आध्यात्मिक रिश्ता जोड़ा, जिसे केवल 'पशुपालन' कहकर समझाया नहीं जा सकता। इन समुदायों की मान्यताओं के अनुसार, ऊँटों का मांस खाना, दूध बेचना, ऊन निकालना या मादा ऊँट को बाहर के किसी व्यक्ति को बेचना, वर्जित था। वे नर ऊँटों को ही बेचते थे, वह भी धार्मिक एवं पारंपरिक अनुमतियों के भीतर।
यह परंपरा दरअसल एक प्रकार की धार्मिक आस्था और सामाजिक अनुशासन का स्वरूप थी, जिसमें ऊँटों को वंशानुक्रम का हिस्सा माना जाता था। रायका मानते हैं कि ऊँट भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त हुए थे। यह विचारधारा ऊँटों के साथ उनके व्यवहार को मानव-जैसा बनाती थी — जिसमें पशु नहीं, परिवार का सदस्य देखा जाता था। इसीलिए उनके दूध या मादा ऊँट के व्यापार को सामाजिक अपराध के रूप में देखा जाता था। लेकिन वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण और युवाओं में पशुपालन के प्रति घटते रुझान के कारण यह संस्कृति संकट में है। आधुनिक शिक्षा और अन्य रोजगारों की ओर पलायन भी इस सांस्कृतिक विरासत के क्षरण में योगदान दे रहा है।

इतिहास में ऊँटों की सैन्य भूमिका: गंगा रिसाला से बीएसएफ तक
ऊँटों का प्रयोग सिर्फ व्यापार या यातायात तक सीमित नहीं था। भारतीय इतिहास में यह जानवर सैन्य व्यवस्था का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। 12वीं शताब्दी से व्यापारिक कारवाँ में ऊँटों का उपयोग होता रहा, लेकिन 16वीं शताब्दी में अकबर जैसे शासकों ने ऊँट वाहिनी स्थापित की। राजस्थान के महाराजाओं के पास ऊँटों की पूरी ‘तोला’ हुआ करती थी, जिनकी देखभाल रायका करते थे।
गंगा रिसाला, जिसे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1889 में स्थापित किया था, वह ब्रिटिश सेना के इंपीरियल सर्विस कॉर्प्स का हिस्सा बना। इस वाहिनी ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान, सोमालिया, मिश्र और ईराक जैसे देशों में भाग लिया। ऊँटों की लंबी दूरी तय करने की क्षमता, कम पानी में जीवित रहने और दुर्गम भू-भागों में चलने की अद्वितीयता के कारण इन्हें रेगिस्तानी युद्धों के लिए अनिवार्य माना गया। स्वतंत्र भारत में बीएसएफ (BSF (सीमा सुरक्षा बल) ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, विशेषकर भारत-पाकिस्तान सीमा पर। लेकिन अब सड़कों के जाल, निगरानी ड्रोन, जीप और मोटरसाइकिलों ने ऊँटों की भूमिका सीमित कर दी है। इससे एक परंपरा और पेशे दोनों का ह्रास हो रहा है।
आधुनिकरण के प्रभाव और ऊँटों की उपयोगिता में गिरावट
20वीं शताब्दी के मध्य तक ऊँटगाड़ियाँ भारत के ग्रामीण जीवन की रीढ़ थीं। विशेष रूप से 1960 के दशक में जब ऊँटगाड़ियों में हवाई जहाज के टायरों का प्रयोग हुआ, तब ऊँटों की मांग चरम पर पहुँच गई। लेकिन 1990 के दशक से सड़क नेटवर्क, ट्रैक्टर, और मोटरसाइकिलों ने ऊँटों की जगह लेना शुरू कर दिया।
आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवहन के वैकल्पिक साधनों की अधिकता ने ऊँटों की उपयोगिता घटा दी है। यही कारण है कि ऊँट पालने वाले अब अपने जानवरों को खुला छोड़ने लगे हैं ताकि चराई का बोझ न उठाना पड़े। परंतु वन क्षेत्रों और मैंग्रोव (विशेषकर कच्छ में) में ऊँटों के प्रवेश पर सरकारी रोक ने उन्हें चारागाह से वंचित कर दिया है। इसके साथ ही, पशु व्यापार कानूनों में सख्ती, पुष्कर जैसे मेलों में व्यापार गिरावट, और ऊँट अधिनियम ने भी ऊँट व्यवसाय को हतोत्साहित किया है। कृषि में यंत्रीकरण और मशीनीकरण के चलते अब ऊँटों को खेती में भी उपयोग नहीं किया जाता, जिससे यह पारंपरिक पशुधन अब अलाभकारी हो गया है।

ऊँटनी का दूध: परंपरागत वर्जनाओं से आधुनिक डेयरी नवाचार तक
पारंपरिक रूप से ऊँटनी के दूध को बेचना ‘बेटा बेचने’ जैसा समझा जाता था। लेकिन अब रायका समुदाय के पशुपालक भी जीविका चलाने के लिए इस दूध को बाजार में बेचने लगे हैं। खासकर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, अमूल ब्रांड के अंतर्गत ऊँटनी का दूध अब व्यावसायिक रूप से बेचा जा रहा है।
यह बदलाव आवश्यक था, क्योंकि पारंपरिक मान्यताएँ पशुपालकों को आर्थिक रूप से पीछे छोड़ रही थीं। ऊँटनी का दूध अब केवल धार्मिक या घरेलू उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि औषधीय गुणों से युक्त उत्पाद के रूप में उभर रहा है। इस दूध में पाई जाने वाली इम्युनोग्लोबुलिन (Immunoglobulin), लैक्टोफेरिन (lactoferrin) और इंसुलिन (insulin) जैसे घटक मधुमेह, हृदय रोग और ऑटिज़्म (autism) जैसी बीमारियों के लिए उपयोगी माने जाते हैं। आज ऊँटनी के दूध से कुल्फी, पनीर, घी, चॉकलेट और सौंदर्य प्रसाधन तक बनाए जा रहे हैं। हालाँकि इन उत्पादों का वितरण अब भी सीमित है, लेकिन इनका एक विशिष्ट बाजार वर्ग तैयार हो रहा है। यदि डेयरी क्षेत्र में निवेश और नीति समर्थन मिले, तो यह क्षेत्र ऊँट पालन को फिर से जीवनदान दे सकता है।

भारत में ऊँट नस्लों की विविधता और संरक्षण की चुनौतियाँ
भारत में कुल नौ प्रकार की ड्रोमेडरी (एक कूबड़ वाली) ऊँट नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें से बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, जालोरी और मेवाड़ी नस्लें राजस्थान से संबंधित हैं। इसके अलावा, लद्दाख में पाई जाने वाली बैक्ट्रियन ऊँट (दो कूबड़ वाली) की एक दुर्लभ नस्ल भी भारत में मौजूद है। यह नस्लें न केवल जैव विविधता का प्रतीक हैं, बल्कि प्रत्येक नस्ल की विशेष उपयोगिता होती है — जैसे बीकानेरी ऊँट लंबी दूरी तय करने में दक्ष है, जबकि मारवाड़ी ऊँट मजबूत और भारी वजन ढोने में सक्षम है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये नस्लें तेजी से लुप्त होती जा रही हैं। 1992 से 2019 तक भारत की ऊँट आबादी में लगभग 80% की गिरावट आई है। राजस्थान सरकार ने ऊँट को राज्य पशु घोषित किया है, लेकिन संरक्षण योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत सीमित रहा है। इन नस्लों के जीन पूल को सुरक्षित रखने के लिए अनुवांशिक अनुसंधान, प्रजनन केंद्रों और स्थानीय पशुपालकों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। यदि इस पर तुरंत और ठोस प्रयास न किए गए, तो भारत इन मूल्यवान ऊँट नस्लों को सदा के लिए खो सकता है।
संदर्भ-


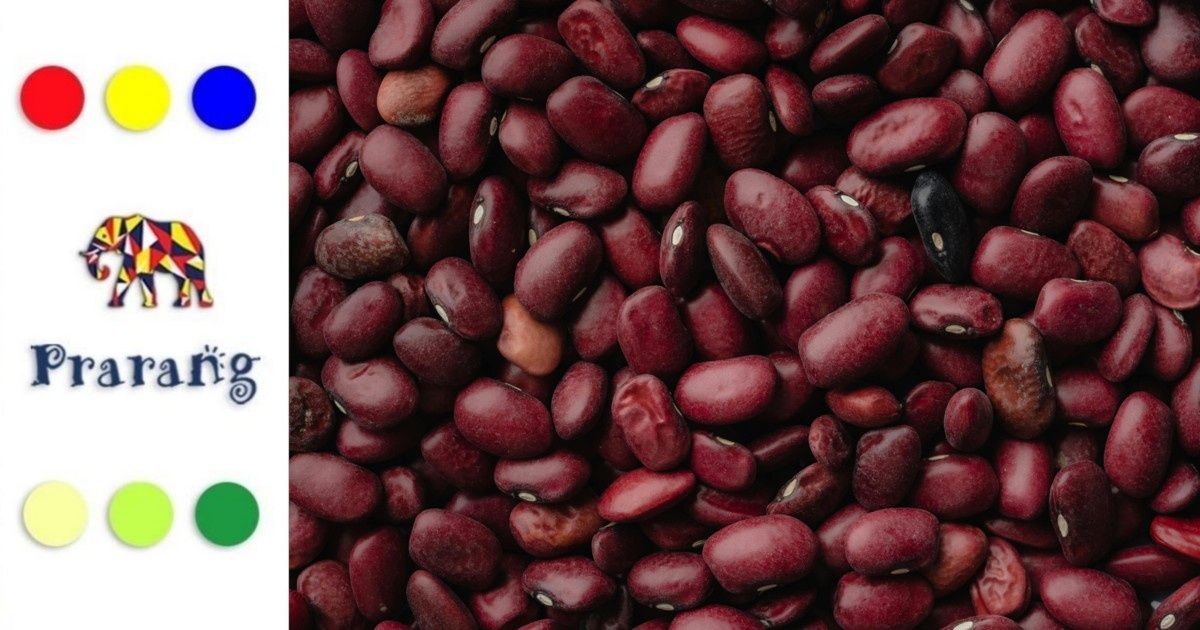
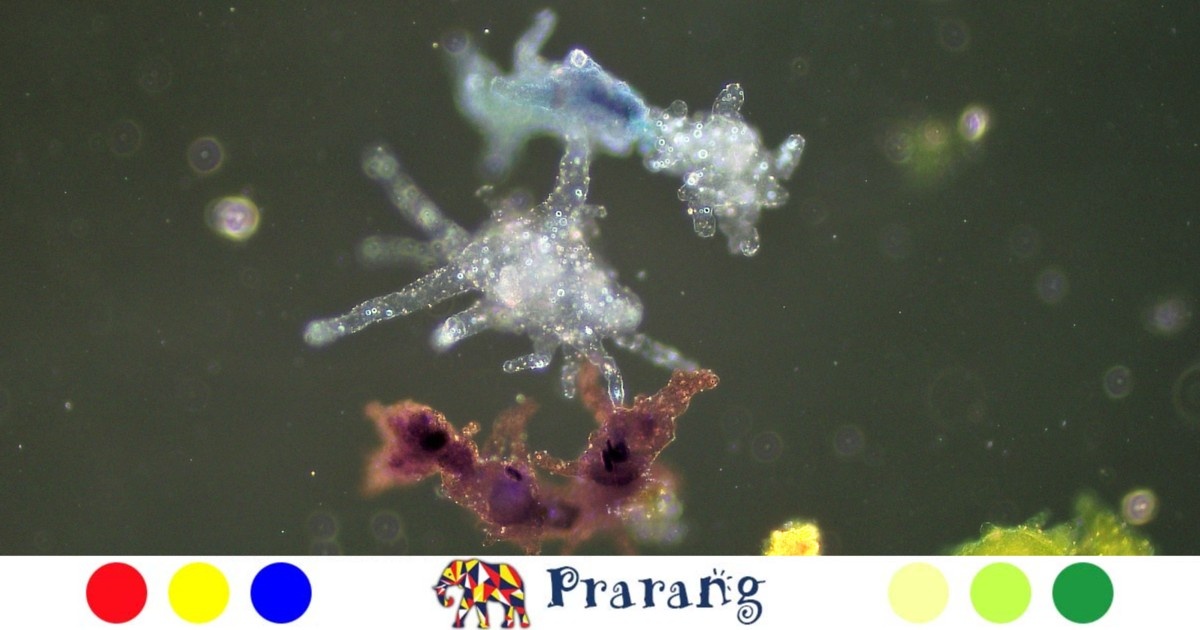

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.