
समय - सीमा 269
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1057
मानव और उनके आविष्कार 821
भूगोल 264
जीव-जंतु 317
समय - सीमा 269
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1057
मानव और उनके आविष्कार 821
भूगोल 264
जीव-जंतु 317

रामपुरवासियो, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी नदियों का जल आखिर कहाँ से आता है? जो रामगंगा नदी हमारे खेतों को सींचती है, हमारे घरों में जीवन का संचार करती है, उसका असली स्रोत कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर हमें ले जाता है हिमालय की उन ऊँचाइयों तक जहाँ जन्म लेते हैं हिमनद - बर्फ़ के ऐसे विशाल भंडार जो हमारे क्षेत्र के जल, कृषि और जलवायु संतुलन के मूल स्तंभ हैं। हिमनद केवल बर्फ़ नहीं, बल्कि धरती की स्मृति हैं - जो सदियों से जलवायु के हर उतार-चढ़ाव को अपने भीतर संजोए हुए हैं। जब ये पिघलते हैं, तो नदियाँ बहती हैं; जब ये ठहरते हैं, तो धरती को स्थिरता मिलती है। रामपुर जैसे क्षेत्रों के लिए, जहाँ जल जीवन का आधार है, इन हिमनदों का अस्तित्व सीधे-सीधे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है - खेतों की सिंचाई, मौसम का संतुलन, और नदियों की स्थिरता सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है।
आज हम जानेंगे कि हिमनद वास्तव में क्या होते हैं और यह कैसे बनते हैं। फिर हम भारत के प्रमुख हिमनदों - जैसे सियाचिन, गंगोत्री, ज़ेमू और मिलम - के भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व को समझेंगे। इसके बाद, हम यह भी देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण इन हिमनदों के पिघलने से क्या ख़तरे उत्पन्न हो रहे हैं और कौन-कौन से क्षेत्र सबसे अधिक संवेदनशील हैं। अंत में, हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) किस तरह नई तकनीकों और वैश्विक पहल के माध्यम से इन हिमनदों की निगरानी और संरक्षण के प्रयास कर रहे हैं।

हिमनद क्या हैं और ये कैसे बनते हैं
हिमनद (Glacier) पृथ्वी की सतह पर जमा हुई बर्फ़ का वह विशाल द्रव्यमान है जो समय के साथ अपने ही भार और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धीरे-धीरे नीचे की ओर बढ़ता रहता है। जब ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार कई वर्षों तक बर्फ़बारी होती है, तो हर नई परत पुरानी बर्फ़ पर दबाव डालती है। यह दबाव धीरे-धीरे बर्फ़ को ठोस, नीली और घनी संरचना में बदल देता है, जिसे हम हिमनद कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में दशकों, कभी-कभी सदियों का समय लग जाता है। हिमनदों का यह प्रवाह भले ही बेहद धीमा हो, लेकिन इसका भूगोल और पारिस्थितिकी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये पहाड़ों को काटते हैं, घाटियों को गढ़ते हैं और नदियों के मार्ग बनाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, हिमनद धरती के जलवायु संतुलन के “प्राकृतिक थर्मामीटर” हैं - जब तापमान बढ़ता है तो वे पीछे हटते हैं, और जब मौसम ठंडा होता है तो फैल जाते हैं। यही वजह है कि इन्हें “पृथ्वी की जलवायु डायरी” कहा जाता है, जो हमें बताती है कि हमारे ग्रह का मौसम किस दिशा में बदल रहा है।

भारत के प्रमुख हिमनद और उनका भौगोलिक महत्व
भारत हिमालय की गोद में स्थित है, जहाँ लगभग नौ हज़ार से अधिक हिमनद मौजूद हैं। ये न केवल देश की नदियों के उद्गम स्थल हैं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ हिमनद अपने आकार, स्थान और ऐतिहासिक योगदान के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। लद्दाख के पूर्वी काराकोरम क्षेत्र में स्थित सियाचिन हिमनद भारत का सबसे बड़ा और रणनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। यह नुबरा नदी को जल प्रदान करता है, जो आगे चलकर सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा बनती है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊँचा सक्रिय सैन्य क्षेत्र भी है, जहाँ सैनिक कठोर परिस्थितियों में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित गंगोत्री हिमनद गंगा नदी का स्रोत है और इसे हिंदू संस्कृति में माँ गंगा का जन्मस्थान माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु गौमुख पहुँचकर इस पवित्र हिमनद का जल ग्रहण करते हैं। ज़ेमू हिमनद, सिक्किम के उत्तर में, कंचनजंगा पर्वत की तलहटी में स्थित है। यह तीस्ता नदी को जल देता है, जो पूर्वोत्तर भारत की जीवनरेखा है। वहीं मिलम हिमनद, उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में, गोरीगंगा नदी का उद्गम स्थल है और कभी तिब्बत के प्राचीन व्यापार मार्ग का हिस्सा हुआ करता था।

हिमनदों के पिघलने से उत्पन्न खतरे और संवेदनशील क्षेत्र
आज हिमनदों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है - मानवजनित जलवायु परिवर्तन। औद्योगिक प्रदूषण, कोयला आधारित ऊर्जा, और जंगलों की कटाई ने पृथ्वी के औसत तापमान को लगातार बढ़ा दिया है। पिछले पचास वर्षों में हिमालय के अधिकांश ग्लेशियर 15% तक पीछे हट चुके हैं, जिससे नदियों के जल प्रवाह का स्वरूप बदल रहा है। जब हिमनद पिघलते हैं, तो उनके निचले हिस्से में झीलें बनने लगती हैं। इनमें से कई झीलें इतनी विशाल हो जाती हैं कि जरा-सी हलचल या भूकंप आने पर वे फट जाती हैं, जिससे नीचे के गाँव और कस्बे बह जाते हैं। ऐसी घटनाओं को वैज्ञानिक “ग्लेशियर झील फटने से बाढ़” (Glacial Lake Outburst Flood - GLOF) कहते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से इस ख़तरे की सबसे अधिक चपेट में हैं।
ग्लेशियर संरक्षण का वैश्विक और राष्ट्रीय महत्व
ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने वर्ष 2025 को “ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष” (International Year of Glaciers’ Preservation) घोषित किया है। इसका उद्देश्य है - लोगों को यह समझाना कि ग्लेशियर केवल ठंडी बर्फ़ की चट्टानें नहीं, बल्कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के जीवंत अंग हैं। भारत में भी कई वैज्ञानिक संस्थान, विश्वविद्यालय और पर्यावरण संगठन मिलकर ग्लेशियरों की निगरानी कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्रालय और जल संसाधन विभाग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नीति-स्तर पर कदम उठा रहे हैं। हिमनदों का संरक्षण केवल सरकारों की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य भी है। पेड़ लगाना, पानी की बर्बादी रोकना, और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना - ये छोटे कदम हमारे बड़े भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की तकनीकी पहलें
भारत ने हिमालयी ग्लेशियरों की स्थिति समझने और संरक्षित करने में विज्ञान की शक्ति का शानदार उपयोग किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने उन्नत उपग्रहों की मदद से देश के प्रमुख ग्लेशियरों की वास्तविक समय पर निगरानी कर रहा है। इन उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि किन क्षेत्रों में बर्फ़ पिघलने की रफ़्तार अधिक है, कहाँ नई झीलें बन रही हैं, और कौन-से ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (SAC) ने विशेष डिजिटल मॉडल (Digital Model) और सॉफ्टवेयर (software) विकसित किए हैं, जो ग्लेशियरों की गति, मोटाई और तापमान का विश्लेषण करते हैं। यह तकनीकी पहल न केवल विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह नीति निर्माताओं को आपदा प्रबंधन और जल संसाधन योजना में मदद करती है। इसरो का यह प्रयास साबित करता है कि यदि हम विज्ञान और प्रकृति को साथ लेकर चलें, तो पृथ्वी के सबसे नाज़ुक पारिस्थितिक तंत्रों को भी संरक्षित किया जा सकता है।
संदर्भ-
https://tinyurl.com/5n9azku4
https://tinyurl.com/2s3ah5w6
https://tinyurl.com/2mt43crh
https://tinyurl.com/mtj449b4
https://tinyurl.com/474mxrzt
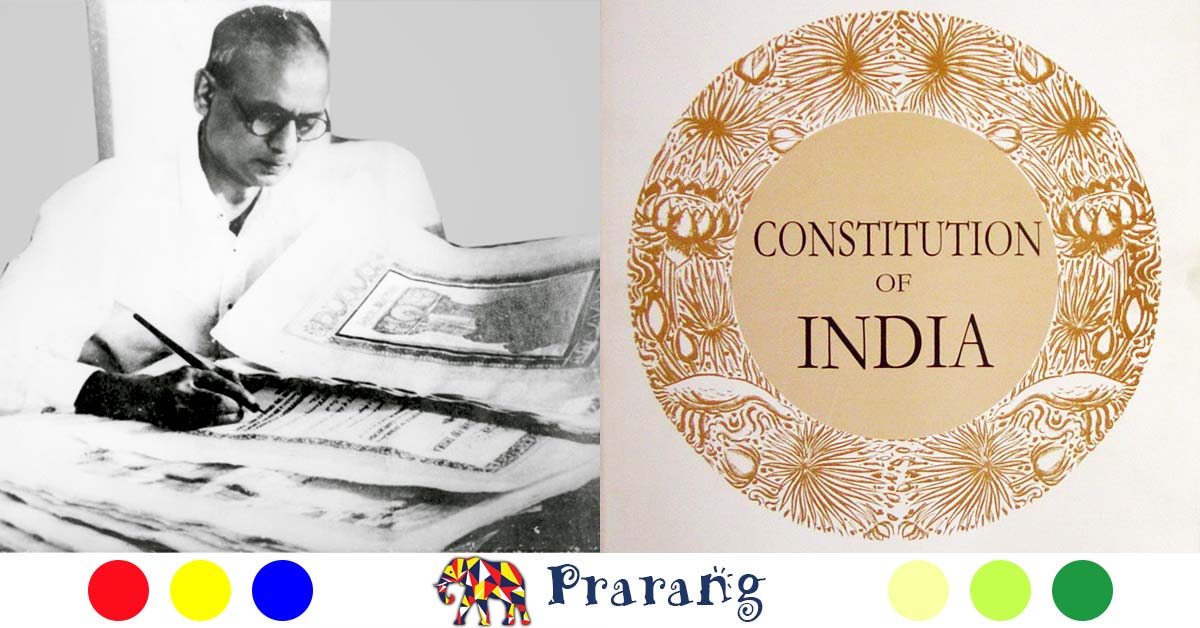



A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.
