
समय - सीमा 10
मानव और उनकी इंद्रियाँ 10
मानव और उनके आविष्कार 10
भूगोल 10
जीव-जंतु 0

प्राचीन भारतीय संस्कृति से जुड़े ज्ञान के प्रसार में संग्रहालयों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, गुरुकुल कांगड़ी (सम विश्वविद्यालय), हरिद्वार के पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना गुरुकुल के आरंभिक वर्षों में, 1907-08 के दौरान, स्वामी श्रद्धानंदजी की प्रेरणा से की गई थी। यह संग्रहालय हरिद्वार में पवित्र गंगा के पूर्वी तट पर, कांगड़ी गाँव के पास पुण्यभूमि में, शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य छात्रों और आम लोगों को भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान देना था। संग्रहालय की इस उपयोगिता को यूनेस्को द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। यहाँ पर हड़प्पा काल की पकी मिट्टी (टेराकोटा) से बनी पुरावस्तुएं रखी गई हैं। इनमें मानव और पशु आकृतियाँ (मानव आकृतियाँ अधिकतर मातृ देवियों की हैं), विभिन्न प्रकार के मनके, चूड़ियों और अंगूठियों जैसे आभूषण, केक और मुष्टिकाएँ, तथा गोफन की गोलियाँ हैं। हड़प्पा काल की पत्थर की पुरावस्तुओं का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है, जिनमें विभिन्न आकारों की गोफन की गोलियाँ, चर्ट ब्लेड और शामिल हैं। यहां पर बाँट जैसी वजन मापन इकाइयां भी संरक्षित हैं! इसलिए आज हम भारत में मापन प्रणाली के प्रमुख मील के पत्थर की ऐतिहासिक समयरेखा को समझेंगे।
आइए सबसे पहले भारत में मापन के संक्षिप्त इतिहास को समझते हैं:
३३०० ईसा पूर्व – १७०० ईसा पूर्व (सिंधु घाटी सभ्यता): इस प्राचीन सभ्यता ने लंबाई, वज़न, आयतन और समय मापने में अच्छी सटीकता हासिल कर ली थी। उन्होंने सबसे पहले ज्ञात एक समान बाट और माप प्रणालियाँ तैयार कीं। वे अलग-अलग लंबाई के हाथ (क्यूबिट) का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें विभिन्न तरीकों से विभाजित किया गया था।
१७०० ईसा पूर्व – ५०० ईसा पूर्व (वैदिक काल): प्राचीन धर्मग्रंथों में समय और लंबाई के मापन पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस दौर में लंबाई मापने के लिए धनुष, कोस और योजन जैसी इकाइयों का प्रयोग होता था। वैदिक काल में खगोल विज्ञान का भी काफी विकास हुआ।
३२१ ईसा पूर्व – १८५ ईसा पूर्व (मौर्य साम्राज्य): कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कानूनी माप-तौल (मेट्रोलॉजी) के सिद्धांत और इकाइयाँ दर्ज की गईं। इस काल में धूपघड़ी और जलघड़ी की उपस्थिति के प्रमाण भी मिलते हैं।
३०० ईसा पूर्व – १२७९ ईस्वी (चोल राजवंश): चोल शासकों ने जहाजरानी तकनीक, नहरें और पानी की टंकियां विकसित कीं। इससे व्यापार और वाणिज्य को बहुत बढ़ावा मिला।
२३० ईसा पूर्व (सातवाहन साम्राज्य): इस साम्राज्य में सिक्कों के सटीक मानक खोजे गए। यह अन्य देशों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का प्रमाण देता है।
१८७ ईसा पूर्व (शुंग राजवंश): इस समय में पतंजलि के महाभाष्य की रचना हुई। कला और वास्तुकला, जिसमें मथुरा शैली भी शामिल है, ने प्रगति की।
६८ ईस्वी (कुषाण साम्राज्य): कुषाणों ने मीनारें, चैत्य, नगर और मूर्तियाँ बनवाईं। उन्होंने ही भारत में सोने के सिक्के चलाए।
२४० ईस्वी (गुप्त साम्राज्य): गुप्त काल में भूमि मापन प्रणालियाँ विकसित हुईं। यहाँ से कपड़ा, दवा, रत्न और धातुएँ निर्यात की जाती थीं। आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत में ज्यामिति, त्रिकोणमिति और ब्रह्मांड विज्ञान पर चर्चा की गई है।
६०० ईस्वी – १२०० ईस्वी (चालुक्य राजवंश): चालुक्यों ने ऐसे मंदिर बनवाए जिनमें जनता के संदर्भ के लिए माप के निशान अंकित थे। राजा सोमेश्वर तृतीय ने कला और विज्ञान का विश्वकोश 'मानसोल्लास' संकलित किया।
१२०६ – १५२६ ईस्वी (दिल्ली सल्तनत): इस काल में सटीक वास्तुकला का निर्माण हुआ। चिकित्सा विज्ञान ने उन्नति की और उसे प्रलेखित किया गया।
१३३६ – १५६५ ईस्वी (विजयनगर साम्राज्य): यहाँ की वास्तुकला में चालुक्य, होयसल, पांड्य और चोल शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है।
१५२६ – १८५७ ईस्वी (मुगल साम्राज्य): मुगलों ने एक समान माप प्रणाली शुरू की और उसका अभ्यास किया। उन्होंने लंबाई और क्षेत्रफल की इकाइयाँ विकसित कीं। उन्होने जंतर मंतर जैसी सटीक वास्तुशिल्प संरचनाएँ बनाई जिसमें धूपघड़ियाँ और खगोलीय उपकरण शामिल थे।
१६७४ ईस्वी (मराठा साम्राज्य): मराठा शासन में शहरी बुनियादी ढाँचे का विकास हुआ। पुणे में बांध, पुल और भूमिगत जल प्रणालियाँ बनाई गईं।
१८५८ – १९४७ ईस्वी (ब्रिटिश काल): अंग्रेजों ने इंच, फुट, यार्ड, मील और एकड़ को मानक इकाइयों के रूप में बढ़ावा दिया। १९१३ की समिति ने एक मिश्रित भारतीय-ब्रिटिश प्रणाली की सिफारिश की। उन्होंने सटीक क्षेत्रीय मानचित्रण की भी शुरुआत की।
१९४७ ईस्वी (स्वतंत्रता के बाद भारत): भारत के राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी संस्थान के रूप में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL) की स्थापना की गई। इसकी नींव १९४७ में नेहरू जी ने रखी थी और १९५० में सरदार वल्लभभाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया।
वर्तमान SI प्रणाली: मीट्रिक प्रणाली पर आधारित आधुनिक मापनविद्या की जड़ें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी हैं। मीट्रिक प्रणाली मापन की वह व्यवस्था है जो 1790 के दशक में फ्रांस में शुरू की गई मीटर आधारित दशमलव प्रणाली के बाद विकसित हुई। इसके बाद हुए ऐतिहासिक विकास और शोध कार्यों के परिणामस्वरूप SI इकाइयों की परिभाषाएँ विकसित हुईं। यह कार्य 'बाट और माप पर सामान्य सम्मेलन' (CGPM) के अधिकार के तहत और 'बाट और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति' (CIPM) की देखरेख में, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निकाय, 'अंतर्राष्ट्रीय बाट और माप ब्यूरो' (BIPM), के हिस्से के रूप में संपन्न हुआ।
तथा चे स्मर्यते....
योजनानां सहस्रे द्वे द्वे शते द्वे च योजने।
एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोऽस्तु ते॥
इसका अर्थ है, "यह स्मरणीय है कि... (हे सूर्यदेव), आपको नमन है जो आधे निमिष में 2202 योजन की दूरी तय करते हैं।" यह श्लोक स्पष्ट रूप से प्रकाश की गति का वर्णन करता है। इसे गणितीय रूप में व्यक्त करें तो, उपरोक्त श्लोक के अनुसार, प्रकाश की गति इस प्रकार होगी:
प्रकाश की गति = 2202 योजन / निमिषार्ध
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'योजन' का प्रयोग प्राचीन काल में लंबाई मापने की इकाई के रूप में होता था।
| इकाई | SI इकाइयों से संबंध (मीटर) |
| अंगुल | ≈ 16.764 × 10⁻³ |
| 96 अंगुल का एक धनुष | ≈ 1.609 |
| 108 अंगुल का एक धनुष | ≈ 1.810 |
| एक योजन = 8000 धनुष (प्रत्येक 108 अंगुल का) | ≈ 14.484 × 10³ |
एक नाक्षत्र दिवस वह समय होता है जिसमें तारों के समूह पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करते हैं। यह अवधि 23 घंटे, 56 मिनट और 4.1 सेकंड के बराबर होती है।
इस अगली तालिका में वैदिक काल में प्रयुक्त समय की विभिन्न इकाइयाँ दर्शाई गई हैं:
| इकाई | SI इकाइयों से संबंध (सेकंड) |
| परमाणु | ≈ 25 × 10⁻⁶ |
| अणु | ≈ 50 × 10⁻⁶ |
| त्रसरेणु | ≈ 151 × 10⁻⁶ |
| त्रुटि | ≈ 454 × 10⁻⁶ |
| वेध | ≈ 45 × 10⁻³ |
| लव | ≈ 0.14 |
| निमेष | ≈ 0.4 |
| क्षण | ≈ 1.22 |
| काष्ठा | ≈ 6 |
| लघु | ≈ 92 |
| दण्ड | ≈ 1.38 × 10³ |
| मुहूर्त | ≈ 2.76 × 10³ |
| अहोरात्रम् (दिन-रात) | ≈ 86.4 × 10³ |
| मास (महीना) | ≈ 2592 × 10³ |
| ऋतु (मौसम) | ≈ 5184 × 10³ |
| अयन | ≈ 5184 × 10³ |
| संवत्सर (वर्ष) | ≈ 31,104 × 10³ |
विष्णु पुराण की सहायता से 'निमिषार्ध' का मान ज्ञात करके प्राचीन समय इकाइयों को आधुनिक इकाइयों से जोड़ा जा सकता है।
इस प्रकार, निमिषार्ध = 86,164.1 / 810,000 सेकंड ≈ 0.1063754 सेकंड
अतः, वैदिक साहित्य में दी गई प्रकाश की गति की गणना इस प्रकार होती है:
प्रकाश की गति = (2202 × 14.484 × 10³) / 0.1063754 मी/से ≈ 2.998 × 10⁸ मी/से
स्वतंत्रता प्राप्ति (15 अगस्त 1947) से पूर्व भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा अपर्याप्त था। देश के नवनिर्माण और औद्योगिक प्रगति के लिए इस कमी को दूर करना अत्यंत महत्वपूर्ण था। स्वतंत्रता के पश्चात, इस चुनौती को समझते हुए देश के प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. शांति स्वरूप भटनागर ने एक दूरदर्शी कदम उठाया। उन्होंने तत्कालीन सरकार को यह सुझाव दिया कि देश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एक समर्पित 'औद्योगिक अनुसंधान कोष' की स्थापना की जानी चाहिए।
सरकार ने डॉ. भटनागर के इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को गंभीरता से लिया और इसे स्वीकृति प्रदान की। इस अनुसंधान कोष के प्रभावी प्रबंधन और देश भर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक स्वायत्त निकाय की आवश्यकता महसूस की गई। इसी के परिणामस्वरूप, 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्' (सीएसआईआर) का गठन किया गया। सीएसआईआर की स्थापना तत्कालीन केंद्रीय विधान सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से हुई थी। इसे कानूनी रूप से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया, ताकि यह बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और वैज्ञानिक अनुसंधान को नई दिशा दे सके।
वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ-साथ देश में व्यापार और उद्योग के लिए एक समान और मानक माप प्रणाली का होना भी आवश्यक था। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अप्रैल 1955 में उठाया गया, जब भारत की लोकसभा (द्विसदनीय संसद का निचला सदन) ने एक प्रस्ताव अपनाया। इस प्रस्ताव में सदन ने यह मत व्यक्त किया कि भारत सरकार को पूरे देश में मीट्रिक प्रणाली पर आधारित एक समान बाट और माप प्रणाली लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
इस संसदीय इच्छा को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए, वर्ष 1956 में केंद्र सरकार ने 'बाट और माप मानक अधिनियम, 1956' पारित किया। इस अधिनियम ने भारत सरकार को देश में मीट्रिक प्रणाली को लागू करने हेतु बाट और माप के मानक स्थापित करने का अधिकार दिया। मानकीकरण की इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने और राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए एक जिम्मेदार संस्था की आवश्यकता थी। वर्तमान में, 'विधिक मापविज्ञान नियम, 2011' के अध्याय III, धारा 23(1) में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय बाट और माप मानकों की सिद्धि, स्थापना, अभिरक्षा, रखरखाव, निर्धारण, पुनरुत्पादन और उन्हें अद्यतन रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL) की होगी। इस प्रकार, एनपीएल भारत में सटीक माप मानकों को बनाए रखने वाली सर्वोच्च संस्था है।
संदर्भ
https://tinyurl.com/2cnkb4xp
https://tinyurl.com/28y5ehvj



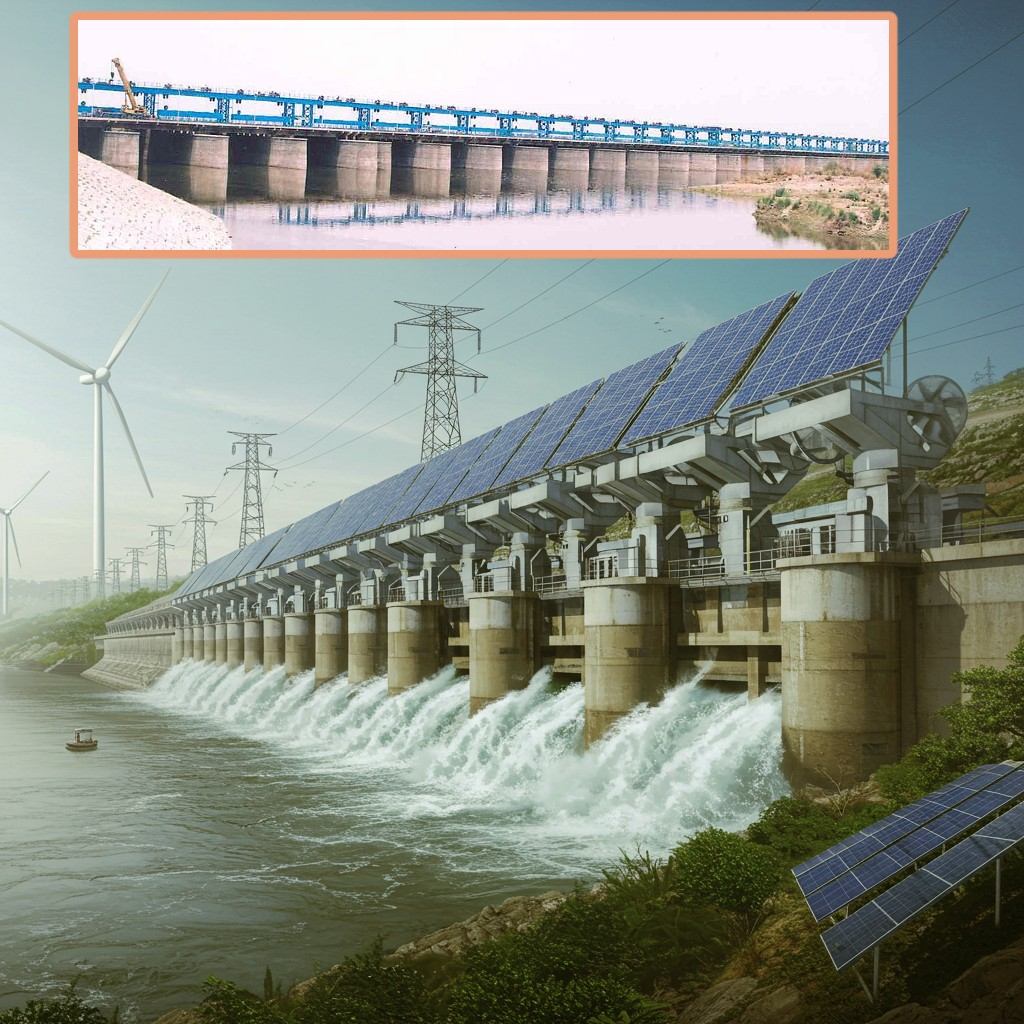

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.