
समय - सीमा 10
मानव और उनकी इंद्रियाँ 10
मानव और उनके आविष्कार 10
भूगोल 10
जीव-जंतु 0
समय - सीमा 10
मानव और उनकी इंद्रियाँ 10
मानव और उनके आविष्कार 10
भूगोल 10
जीव-जंतु 0

उत्तराखंड, एक शानदार हिमालयी राज्य है। इस राज्य को खनिजों और उपखनिजों का एक समृद्ध खजाना विरासत में मिला है। इसी प्रचुरता ने लंबे समय से यहाँ खनन गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया है! यह गतिविधियाँ राज्य की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती हैं। लेकिन, जैसे-जैसे मांग बढ़ी और खनन कार्य तेज हुए, इसके खूबसूरत परिदृश्य पर एक काला साया भी पड़ गया है। यह अपने साथ पर्यावरणीय तबाही और स्थानीय समुदायों के लिए गंभीर चुनौतियां लेकर आया है।
उत्तराखंड की भूवैज्ञानिक संपदा के केंद्र में प्रमुख और उपखनिज, दोनों के महत्वपूर्ण भंडार हैं। प्रमुख खनिजों में मैग्नेसाइट (magnesite), चूना पत्थर (limestone) और सोना, चांदी और सीसा जैसी आवश्यक बेस मेटल्स (base metals) शामिल हैं। उतने ही महत्वपूर्ण यहाँ के उपखनिज भी हैं, जिनमें सोपस्टोन (Soapstone), सिलिका सैंड (Silica Sand) और बैराइट (Baryte) जैसे स्थानीय चट्टानी खनिज आते हैं। इसके अलावा, राज्य की कई नदियाँ रेत, बजरी और बड़े पत्थरों जैसे मूल्यवान नदी-तल खनिजों का एक बड़ा स्रोत हैं। ये संसाधन बेहद ज़रूरी हैं! उदाहरण के तौर पर सोपस्टोन का इस्तेमाल पेंट (paint), कागज और कॉस्मेटिक्स (cosmetics) बनाने में होता है। उत्तराखंड में खनन किया जाने वाला चूना पत्थर (निर्माण और कृषि में एक महत्वपूर्ण घटक) चूना बनाने के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है।
इन खनन गतिविधियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी कई अलग-अलग संस्थाओं में बंटी हुई है। वन क्षेत्रों में स्थित नदी-तल खनन की देखरेख उत्तराखंड वन विकास निगम करता है। वहीं, राजस्व नदी क्षेत्रों (revenue river areas) के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम जिम्मेदार हैं। निजी व्यक्ति भी अपनी निजी भूमि पर खनन कार्य करते हैं।
इन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, राज्य सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत नियमों का एक व्यापक ढाँचा बनाया है। इसमें उत्तराखंड उपखनिज (रियायत) नियमावली, 2023 शामिल है, जो उपखनिज खनन को नियंत्रित करती है। साथ ही, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए विशेष रूप से उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2021 बनाई गई है। इसके अलावा, व्यवस्थित और कानूनी संचालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड स्टोन क्रशर (Stone Crusher), स्क्रीनिंग प्लांट (Screening Plant), पल्वराइज़र प्लांट (Pulverizer Plant), हॉट मिक्स प्लांट (Hot Mix Plant), रेडी मिक्स प्लांट (Ready Mix Plant) लाइसेंस पॉलिसी-2021 (License Policy-2021) और उत्तराखंड नदी निकर्षण (Dredging) नीति-2021 जैसी नीतियां भी लागू की गई हैं।
हालाँकि इन कानूनी ढाँचों के बावजूद, अवैध खनन पहाड़ों में एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरा है। यह कमजोर क्षेत्रों पर अपना एक लंबा साया डाल रही है। हरिद्वार के पास, खासकर कांगड़ी गाँव में, गंगा में होने वाले अवैध खनन के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन एक अध्ययन का विषय रहा है। हरिद्वार में 'अवैध गंगा खनन' पर एक अध्ययन इस बात पर ज़ोर देता है कि रेत और बजरी जैसे नदी-तल खनिजों के अनियंत्रित खनन को लेकर चिंता कितनी गंभीर है, जो उत्तराखंड की नदियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। राज्य द्वारा अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए बनाए गए नियम इस बात को साफ तौर पर स्वीकार करते हैं कि ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों से निपटने की सख्त ज़रूरत है।
उत्तराखंड में अनियंत्रित और बढ़ते खनन से होने वाले गंभीर पर्यावरणीय परिणामों को पूरी तरह समझने के लिए, बागेश्वर जिले में सामने आ रही भयावह स्थिति को देखा जा सकता है। हाल के वर्षों में बड़ी कंपनियों के आने और हाथ के काम की जगह मशीनों के इस्तेमाल से यहाँ सोपस्टोन खनन बहुत बढ़ गया है। इस तेज़ी ने विनाशकारी प्रभाव डाले हैं, जिससे ग्रामीणों का जीवन और यहाँ का पूरा परिदृश्य ही बदल गया है।
टल्ला ढपोली, कांडे कन्याल और दबती विजयपुर जैसे गाँवों में इसके परिणाम साफ दिखाई देते हैं। घरों, सड़कों और खेतों में खतरनाक दरारें आ गई हैं, जिससे निवासियों को डर है कि उनकी ज़मीन कभी भी धँस जाएगी। टल्ला ढपोली गाँव के केसर सिंह का दर्द इन शब्दों में झलकता है, "सोपस्टोन की खदानें एक अभिशाप बन गई हैं और हम अपना पूरा गाँव खो देंगे। गाँव के कई घरों में दरारें आ चुकी हैं।" दबती विजयपुर के कई निवासी तो पहले ही पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। लगातार धूल और शोर के प्रदूषण ने रोजमर्रा की ज़िंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया है, जिसके कारण ज़्यादातर घर खाली पड़े हैं। पहाड़ी ढलानों के लिए ज़रूरी सीढ़ीदार खेती करना भी इन प्रभावित क्षेत्रों में बेहद मुश्किल हो गया है।
पर्यावरणीय नुकसान सिर्फ ढाँचों के टूटने और प्रदूषण तक ही सीमित नहीं है। ढपोली गाँव के कृपाल सिंह बताते हैं कि खनन के लिए ज़रूरी सड़कें बनाने के लिए गाँव के वन पंचायत की अनुमति के बिना ही बाँज के पेड़ों को काट दिया गया है, जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। बागेश्वर से होकर बहने वाली पुंघर नदी भी साफ तौर पर प्रदूषित हो गई है। स्थानीय निवासियों ने देखा है कि इसका जल स्तर तो बढ़ा है, लेकिन विडंबना यह है कि पिछले कुछ वर्षों में साफ पानी की उपलब्धता कम हो गई है।
मवेशी भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। रीमा घाटी के निवासी बताते हैं कि कैसे खनन की धूल उन पौधों और पत्तियों पर जम जाती है, जिन्हें खाकर जानवर बीमार पड़ रहे हैं। अब कई लोगों को अपने जानवरों के लिए साफ चारा सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी गाँवों से चारा खरीदना पड़ता है या दूर-दराज के इलाकों में खेती करनी पड़ती है।
बागेश्वर की स्थिति की गंभीरता पर न्यायिक संस्थाओं का भी ध्यान गया है। सितंबर में, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) ने इस मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया। ट्रिब्यूनल (Tribunal) ने सभी संबंधित पक्षों को इस पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ, एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह जवाब जिले भर में खनन के कारण इमारतों और ज़मीनों में पड़ रही दरारों की खबरों पर मांगा गया है। ये कानूनी हस्तक्षेप इस बात पर ज़ोर देते हैं कि अब जवाबदेही तय करने और उत्तराखंड के खनन प्रभावित क्षेत्रों में फैल रही इस पर्यावरणीय आपदा को रोकने के लिए असरदार उपायों की तत्काल ज़रूरत है।
बागेश्वर के ये उदाहरण एक गंभीर चेतावनी हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में गहन और संभावित रूप से अनियंत्रित खनन की कितनी बड़ी पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ सकती है। पारंपरिक, हाथ से होने वाले खनन, (जिससे कभी स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलता था!) से हटकर बड़े पैमाने पर मशीनीकृत खनन की ओर जाने से नुकसान और भी तेज हो गया है। इसमें पारिस्थितिक संतुलन की जगह सिर्फ खनिज निकालने को प्राथमिकता दी गई है।
हालांकि राज्य सरकार ने खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने और अवैध कार्यों पर रोक लगाने के लिए कई नीतियां और नियम लागू किए हैं, लेकिन ज़मीन धँसने, प्रदूषण और लोगों के विस्थापन की लगातार आती खबरें एक बड़ी सच्चाई बयां करती हैं। ये खबरें नियमों को लागू करने और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन (sustainable resource management) में बनी हुई चुनौतियों को साफ तौर पर उजागर करती हैं। हरिद्वार के कांगड़ी गाँव जैसे इलाकों में 'पर्यावरणीय प्रभाव आकलन' (environmental impact assessment) की लगातार ज़रूरत यह बताती है कि ये क्षेत्र भी खनिज खनन के प्रभावों के प्रति उतने ही संवेदनशील हैं, खासकर नदी-तलों से होने वाले खनन को लेकर जो पारिस्थितिक संतुलन के लिए बेहद ज़रूरी हैं।
उत्तराखंड की खनिज संपदा और उसकी पर्यावरणीय विरासत में तालमेल बैठाने के लिए एक ठोस और एकजुट प्रयास की आवश्यकता है। यह एक ऐसा प्रयास होना चाहिए जिसमें नियमों का कड़ाई से पालन, व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, सामुदायिक भागीदारी और टिकाऊ खनन प्रथाओं के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता हो। इसी से आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ज़मीन और यहाँ के लोगों की आजीविका, दोनों को बचाया जा सकता है। उत्तराखंड के अनूठे परिदृश्य का भविष्य इसी नाजुक संतुलन पर टिका है।
संदर्भ



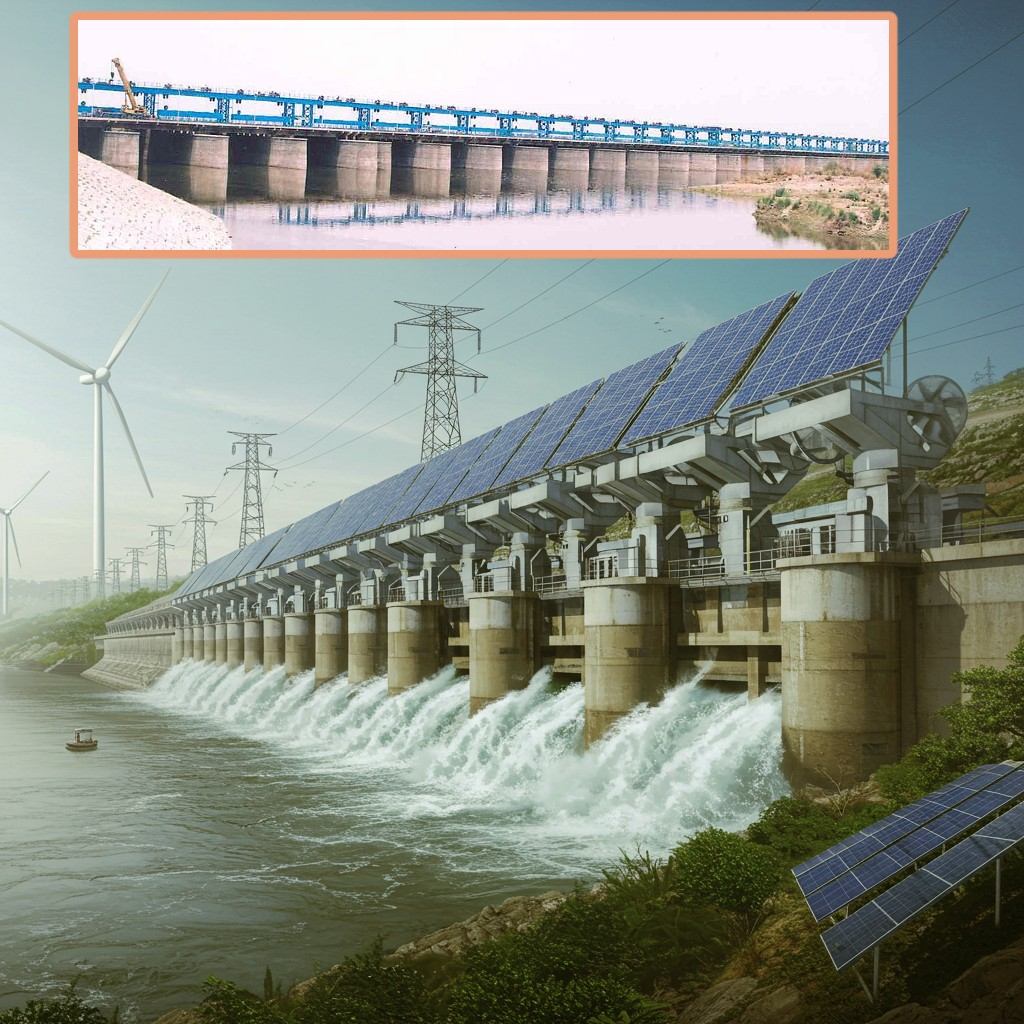

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.
