
समयसीमा 258
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1042
मानव व उसके आविष्कार 824
भूगोल 238
जीव - जन्तु 302
समयसीमा 258
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1042
मानव व उसके आविष्कार 824
भूगोल 238
जीव - जन्तु 302

लखनऊवासियो, गंगा-जमुनी तहज़ीब का यह शहर हमेशा से अपनी अनोखी पहचान और साझा संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ का हर त्योहार सिर्फ़ एक धार्मिक अवसर भर नहीं होता, बल्कि सामूहिक उल्लास, आस्था और भाईचारे का जीवंत प्रतीक बनकर सामने आता है। इन्हीं त्योहारों में से एक है दशहरा, जो लखनऊ की आत्मा से गहराई से जुड़ा हुआ है। दशहरे की रौनक पुराने समय से लेकर आज तक इस शहर की धड़कनों में बसती आई है। नवाबों के दौर में भी यह पर्व पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जाता था, और तब से लेकर अब तक इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। आज भी जब शहर की गलियाँ, मैदान और मोहल्ले दशहरे के रंगों में रंग उठते हैं, तो यह साफ़ दिखता है कि लखनऊ का दशहरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आपसी मेलजोल और मोहब्बत की मिसाल है। यही वजह है कि लखनऊ का दशहरा हमेशा कुछ ख़ास माना जाता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि त्योहारों की असली खूबसूरती तब नज़र आती है, जब पूरा समाज एक साथ मिलकर उन्हें मनाए - बिना किसी भेदभाव के, सिर्फ़ खुशी और अपनत्व के साथ।
आज हम इस लेख में चार बातों को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले, जानेंगे कि लखनऊ में दशहरे का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप कैसा है। फिर देखेंगे कि रामलीला और रावण दहन की परंपराएँ किस तरह पीढ़ी-दर-पीढ़ी जीवित हैं। उसके बाद रावण के दस सिर से जुड़ी मान्यताओं और उनके प्रतीकात्मक अर्थ को समझेंगे। अंत में, हम रावण से जुड़ी सीख और गीता के संदेश पर विचार करेंगे, जो हमारे जीवन के लिए आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।

लखनऊ में दशहरे का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप
लखनऊ का दशहरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शहर की आत्मा में रचा-बसा उत्सव है। यहाँ दशहरे ने समय के साथ सिर्फ़ मंदिरों और पूजा स्थलों में नहीं, बल्कि गलियों और चौबारों में भी अपनी छाप छोड़ी है। यह वह पर्व है जिसने लोगों के दिलों को जोड़ा और एक साझा उत्सव का रूप लिया। नवाबों के दौर से ही इस पर्व ने लखनऊ की गंगा-जमुनी तहज़ीब में अपनी पहचान बना ली थी। नवाब सादात अली खान और बाद में वाजिद अली शाह जैसे शासकों ने दशहरे के आयोजनों को न केवल सराहा, बल्कि स्वयं इसमें शामिल होकर इसे एक साझा उत्सव का स्वरूप दिया। जब शासक खुद इसमें शामिल होते थे, तो यह केवल धर्म का नहीं, बल्कि संस्कृति और मोहब्बत का भी जश्न बन जाता था। यही वजह है कि दशहरा धार्मिक सीमाओं से निकलकर एक बड़े सामाजिक जश्न में बदल गया। इस जश्न में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय पूरे मन से शिरकत करते थे। लोग एक-दूसरे के घर आते-जाते, खुशियाँ बाँटते और त्योहार को मिल-जुलकर मनाते। इन आयोजनों ने यह साबित किया कि त्योहार केवल पूजा-पाठ या धार्मिक मान्यताओं के लिए नहीं होते। वे इंसानियत, भाईचारे और आपसी मेलजोल को मज़बूत करने का ज़रिया भी हैं। यही कारण है कि लखनऊ का दशहरा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि साझा संस्कृति और आपसी मोहब्बत की जीवित मिसाल बन चुका है।

रामलीला और रावण दहन की परंपराएँ
दशहरे की बात हो और लखनऊ की ऐशबाग रामलीला का नाम न लिया जाए, तो मानो पूरा चित्र अधूरा रह जाता है। ऐशबाग की रामलीला दशकों से भव्य और जीवंत रूप में आयोजित की जाती रही है। हर साल कलाकार जब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की भूमिकाओं में मंच पर उतरते हैं, तो दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुँच जाता है। छोटे-बड़े, अमीर-गरीब, सभी दर्शक बिना भेदभाव के इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस रामलीला का सबसे बड़ा आकर्षण 121 फीट ऊँचे रावण के पुतले का दहन है। जब वह पुतला आग की लपटों में घिरकर धराशायी होता है और आतिशबाज़ी की चमक आसमान को रोशन करती है, तो पूरा शहर एक साथ उस पल को जीता है। बच्चे तालियाँ बजाते हैं, बुज़ुर्ग प्रसन्नता से झूम उठते हैं और युवाओं के चेहरे रोमांच और ख़ुशी से दमक उठते हैं। यह क्षण केवल प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि एक सामूहिक अनुभव बन जाता है। सिर्फ़ ऐशबाग ही नहीं, बल्कि मौसमगंज, सदर, राजाजीपुरम और झूलेलाल घाट जैसी जगहों पर भी दशहरे की धूम देखने लायक होती है। हर मोहल्ले और हर मैदान में रामलीला और रावण दहन की वही ऊर्जा और वही उत्साह महसूस किया जा सकता है। इन परंपराओं की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये हमें यह संदेश देती हैं - त्योहार तभी ज़िंदा रहते हैं जब लोग उन्हें दिल से अपनाते हैं। जब समाज इन्हें जीता है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं और हमेशा ताज़ा बने रहते हैं।

रावण के दस सिर का वास्तविक अर्थ और मान्यताएँ
रावण का नाम सुनते ही हमारे सामने एक अहंकारी और शक्तिशाली राक्षस की छवि उभर आती है। लेकिन उसके दस सिर केवल ताक़त या डर का प्रतीक नहीं थे। इन सिरों के पीछे गहरी प्रतीकात्मकता छिपी हुई थी। शास्त्रों के अनुसार, यह दस सिर उसकी विद्वत्ता और गहन ज्ञान का प्रतीक थे। रावण न केवल एक योद्धा था, बल्कि चार वेदों और छह शास्त्रों का ज्ञाता भी था। उसके पास अपार ज्ञान और विद्या का खजाना था, जिसकी मिसाल शायद ही किसी और पात्र में मिलती है। यह पहलू हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हर शक्तिशाली शख़्स केवल बुरा ही नहीं होता, उसमें अच्छाई और प्रतिभा भी होती है। दूसरी ओर, एक मान्यता यह भी कहती है कि रावण के दस सिर इंसानी अवगुणों का प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार, भय और असंवेदनशीलता - ये सभी अवगुण हमें भीतर से खोखला करते हैं। यह मान्यता हमें यह सिखाती है कि असली रावण हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा है। जब तक हम इन अवगुणों से नहीं लड़ेंगे, तब तक बाहरी रावण के पुतले जलाने का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। इस तरह, दशहरे का रावण केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं है, बल्कि आत्ममंथन का प्रतीक भी है। वह हमें अपने भीतर झाँकने और अपनी कमज़ोरियों को पहचानने की प्रेरणा देता है।

रावण से जुड़ी सीख और आध्यात्मिक संदेश
रामायण का सबसे बड़ा और कालजयी संदेश यही है कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली, विद्वान और समृद्ध क्यों न हो, अगर वह अपने अहंकार और बुराइयों को नहीं छोड़ता, तो उसका पतन निश्चित है। रावण इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। ज्ञान और शक्ति के बावजूद वह अपने भीतर के अहंकार और मोह से परास्त हो गया और विनाश की ओर बढ़ा। गीता भी यही कहती है कि जब इंसान अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण खो देता है, तो वह क्रोध और मोह में फँसकर अपना संतुलन खो बैठता है। यही स्थिति रावण की भी थी। वह अपनी बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल सही दिशा में नहीं कर पाया और अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो बैठा। इसलिए दशहरा हमें हर साल यह याद दिलाता है कि त्योहार का असली अर्थ केवल पुतला जलाने तक सीमित नहीं है। यह हमें भीतर झाँकने का अवसर देता है। हमें यह समझना होगा कि असली विजयदशमी तब है जब हम अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को परास्त करें। जब हम अपने जीवन को संयम, दया और सेवा-भाव से रोशन करते हैं, तभी हम रावण पर असली जीत हासिल कर पाते हैं। यही दशहरे का आध्यात्मिक संदेश है - बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम अच्छाई को अपनाएँ, तो विजय हमारी ही होगी।
संदर्भ-
https://short-link.me/18IE4
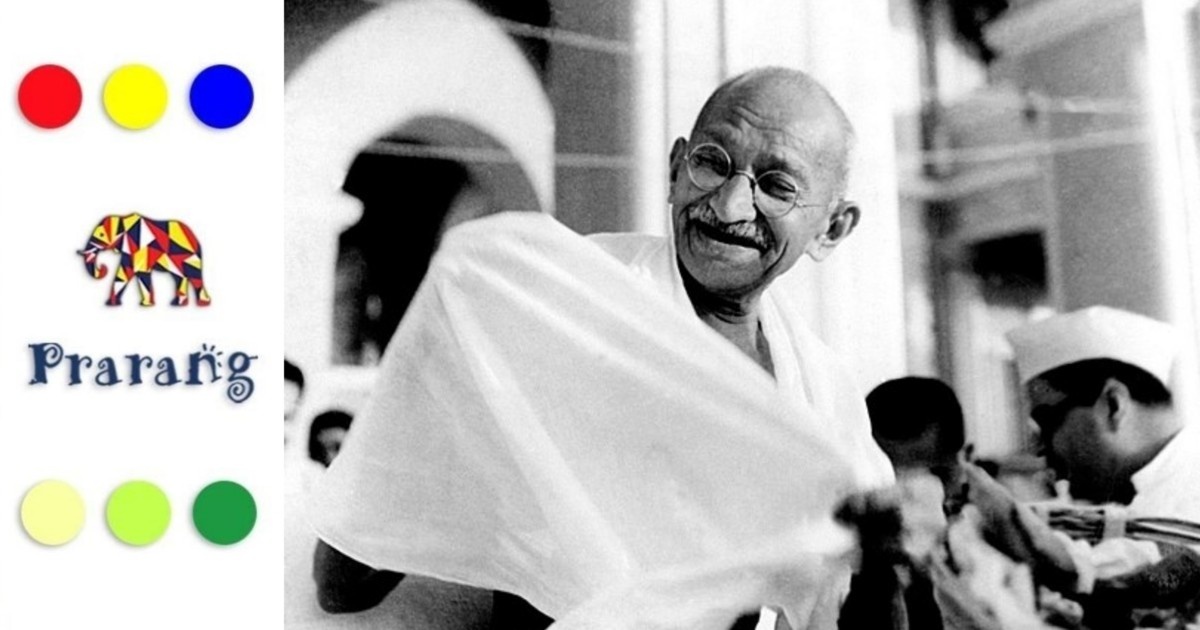
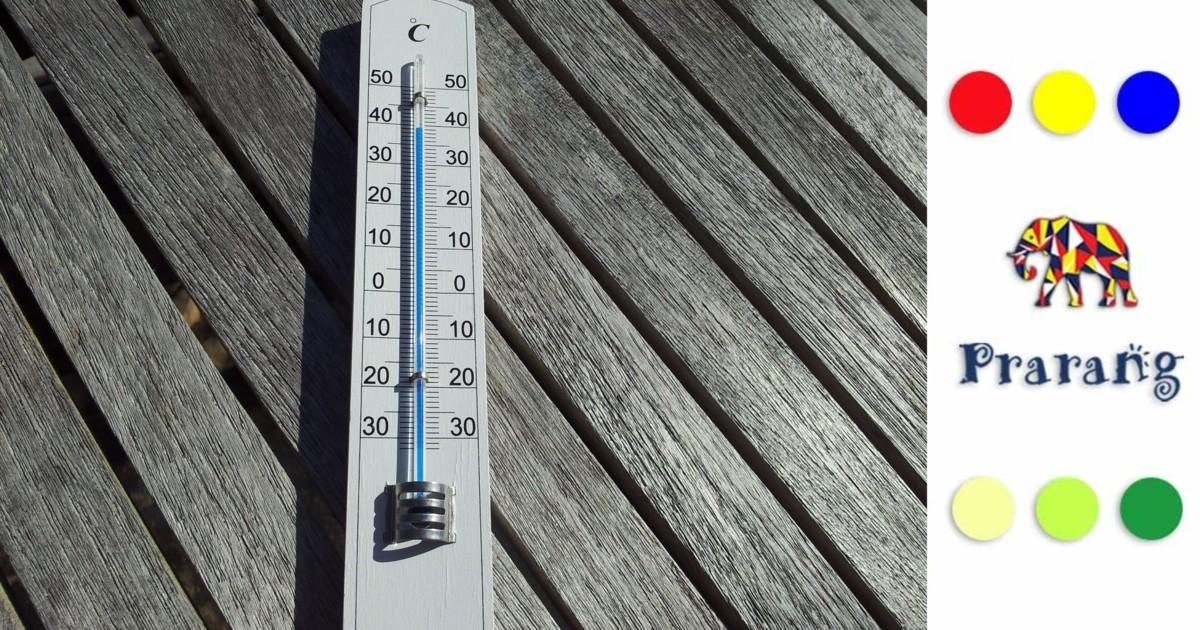


A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.
