
समय - सीमा 289
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1064
मानव और उनके आविष्कार 837
भूगोल 267
जीव-जंतु 321
| Post Viewership from Post Date to 26- May-2024 (31st Day) | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 2699 | 111 | 0 | 2810 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

भारत में पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण करने वाले संवैधानिक संशोधन को चिह्नित करने के लिए, हम हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। हम जानते हैं कि, केंद्र और राज्य सरकारों के बाद पंचायती राज भारत में शासन का तीसरा स्तर है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर शासन के लिए ज़िम्मेदार हैं। यह दिन 24 अप्रैल, 1993 को भारत में पहली पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का भी प्रतीक है। तो आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर आइए देखें कि, भारत में पंचायती राज का विकास कैसे हुआ और यह भारत जैसे देश में क्यों महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यह भी जानें कि, दो और तीन स्तरीय पंचायती राज के बीच क्या अंतर है। भारत के प्रशासनिक इतिहास के पटल पर, पंचायती राज का मुद्दा लचीलेपन, परिवर्तन और ग्रामीण स्तर पर सशक्तिकरण की कहानी सुनाता है। प्राचीन प्रणालियों से संवैधानिक मान्यता तक, इसकी यात्रा विकेंद्रीकृत शासन के लिए एक सामूहिक प्रयास को दर्शाती है। पंचायती राज के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर 1992 में हुआ संवैधानिक संशोधन हैं। इस 73वें संवैधानिक संशोधन ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को संस्थागत बनाया, जिसमें प्रत्येक स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और ज़िला परिषदें शामिल हैं। इस संवैधानिक मान्यता ने भारत की शासन विकेंद्रीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया है।
भारत के प्रशासनिक इतिहास के पटल पर, पंचायती राज का मुद्दा लचीलेपन, परिवर्तन और ग्रामीण स्तर पर सशक्तिकरण की कहानी सुनाता है। प्राचीन प्रणालियों से संवैधानिक मान्यता तक, इसकी यात्रा विकेंद्रीकृत शासन के लिए एक सामूहिक प्रयास को दर्शाती है। पंचायती राज के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर 1992 में हुआ संवैधानिक संशोधन हैं। इस 73वें संवैधानिक संशोधन ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को संस्थागत बनाया, जिसमें प्रत्येक स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और ज़िला परिषदें शामिल हैं। इस संवैधानिक मान्यता ने भारत की शासन विकेंद्रीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया है।
भारत की लगभग 69% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए पंचायती राज संस्थाएं विकासात्मक नीतियों को ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे सरकार और ग्रामीण समुदायों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं; स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, और सतत विकास पहल चलाते हैं। .jpg ) हालांकि, पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावशीलता पर्याप्त संसाधनों, क्षमता निर्माण, राजनीतिक समर्थन और सामुदायिक सहभागिता सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इनके प्रदर्शन और प्रभाव का आकलन करने के लिए वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि है। इ ग्राम स्वराज(eGramSwaraj) और ऑनलाइन ऑडिट प्लेटफ़ॉर्म(Online audit platforms) जैसी डिजिटल पहलों के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद भी, इन संस्थाओं के सामने चुनौतियां बनी हुई हैं। अतः इन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और स्थानीय सरकारी वित्त में मौजूदा डेटा अंतराल को संबोधित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।
हालांकि, पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावशीलता पर्याप्त संसाधनों, क्षमता निर्माण, राजनीतिक समर्थन और सामुदायिक सहभागिता सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इनके प्रदर्शन और प्रभाव का आकलन करने के लिए वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि है। इ ग्राम स्वराज(eGramSwaraj) और ऑनलाइन ऑडिट प्लेटफ़ॉर्म(Online audit platforms) जैसी डिजिटल पहलों के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद भी, इन संस्थाओं के सामने चुनौतियां बनी हुई हैं। अतः इन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और स्थानीय सरकारी वित्त में मौजूदा डेटा अंतराल को संबोधित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।
फिर भी, स्थानीय सरकार के एक भाग के रूप में भारत में पंचायत प्रणाली का निम्नलिखित महत्व है।
• लोगों की भागीदारी: ग्रामीण स्तर पर काम करने वाली ये संस्थाएं, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी का अवसर सुनिश्चित करते हैं।
• महिला सशक्तिकरण: पंचायत राज प्रणालियों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण के प्रावधान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है।
• एससी और एसटी आरक्षण: अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करके समाज के दलित वर्गों का सशक्तिकरण भी हुआ है।
• अधिनियम की अनुसूची 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से, पंचायतों को कृषि विकास, भूमि विकास, ग्रामीण विकास आदि स्थानीय शासन की जिम्मेदारियां दी गई हैं।
• ज़िला योजना समिति विकास गतिविधियों की संपूर्ण योजना सुनिश्चित करती है।.jpg ) आइए अब, दो स्तरीय तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणालियों के बीच अंतर को समझते हैं। दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसमें स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों के दो स्तरों, अर्थात् ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का गठन शामिल है।
यह प्रणाली दो स्तरों से बनी है: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (ग्राम परिषद) और ब्लॉक या तालुका स्तर पर पंचायत समिति (ब्लॉक परिषद)। ग्राम पंचायतें व्यवस्था के मूलभूत घटक हैं, जो गांवों या गांवों के समूहों पर शासन करने के प्रभारी हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत सीधे निर्वाचित सरपंच और अन्य लोगों द्वारा निर्वाचित सदस्यों से बनी होती है।
आइए अब, दो स्तरीय तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणालियों के बीच अंतर को समझते हैं। दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसमें स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों के दो स्तरों, अर्थात् ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का गठन शामिल है।
यह प्रणाली दो स्तरों से बनी है: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (ग्राम परिषद) और ब्लॉक या तालुका स्तर पर पंचायत समिति (ब्लॉक परिषद)। ग्राम पंचायतें व्यवस्था के मूलभूत घटक हैं, जो गांवों या गांवों के समूहों पर शासन करने के प्रभारी हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत सीधे निर्वाचित सरपंच और अन्य लोगों द्वारा निर्वाचित सदस्यों से बनी होती है।
1992 में पारित हुए भारतीय संविधान के 73वें संशोधन ने स्थानीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाने और लोगों को स्थानीय स्तर पर अधिक नियंत्रण देने के हेतु से दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की थी। इसने सरकारी प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है।.jpg ) दूसरी ओर, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एक प्रकार की विकेंद्रीकृत सरकार है। इसमें स्थानीय स्वशासन के लिए, संस्थानों के तीन स्तर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास अद्वितीय कर्तव्य और अधिकार होते हैं। यह प्रणाली, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (ग्राम परिषद), ब्लॉक या तालुका स्तर पर पंचायत समिति (ब्लॉक परिषद) तथा ज़िला स्तर पर ज़िला परिषद के गठन से बनती है।
दूसरी ओर, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एक प्रकार की विकेंद्रीकृत सरकार है। इसमें स्थानीय स्वशासन के लिए, संस्थानों के तीन स्तर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास अद्वितीय कर्तव्य और अधिकार होते हैं। यह प्रणाली, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (ग्राम परिषद), ब्लॉक या तालुका स्तर पर पंचायत समिति (ब्लॉक परिषद) तथा ज़िला स्तर पर ज़िला परिषद के गठन से बनती है।
ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है, और एक गांव या गांवों के समूह का शासन संभालता है। इसके प्राथमिक कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
१. अपने अधिकार क्षेत्र में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और योजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करना।
२. सड़क, जल आपूर्ति प्रणाली और सार्वजनिक भवनों जैसी सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव और विकास करना।
३. सरकारी कल्याण कार्यक्रम जैसे मनरेगा, एकीकृत बाल विकास सेवाएं आदि को लागू करना।
४. गांव में उत्पन्न होने वाले विवादों एवं झगड़ों का समाधान करना।
५. राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कर और शुल्क एकत्र करना।
६. गांव में जन्म, मृत्यु और विवाह के रिकॉर्ड और रजिस्टर बनाए रखना।
पंचायत समिति, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, और एक ब्लॉक या तालुका के भीतर ग्राम पंचायतों के एक समूह पर शासन करती है।
इसके प्राथमिक कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
१. अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की विकास गतिविधियों का समन्वय करना।
२. ब्लॉक-स्तरीय विकास कार्यक्रमों और योजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करना।
३. ग्राम पंचायतों को उनकी विकास गतिविधियों में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना।
४. ब्लॉक स्तर पर सरकारी कल्याण कार्यक्रमों का प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना।
५. ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाना।
६.अपने अधिकार क्षेत्र में जन्म, मृत्यु और विवाह के रिकॉर्ड और रजिस्टर बनाए रखना।
जबकि, पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर, जिला परिषद जिला-स्तरीय प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च स्तर के रूप में कार्य करती है। यह पंचायत समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी होती है, और पूरे जिले की समग्र प्रगति और विकास की देखरेख के प्रति जिम्मेदार है। जिला परिषद एक प्रधान संस्था के रूप में कार्य करती है, जो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली पंचायत समितियों के संचालन का समन्वय और निगरानी करती है। इसके अलावा, यह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित जिले की जरूरतों को पूरा करने वाली विविध प्रकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार और क्रियान्वित करती है।
आइए अब दो स्तरीय व त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणालियों के बीच तुलना करते हैं।
समानताएं–
•दोनों प्रणालियों का लक्ष्य ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है।
•दोनों प्रणालियों में गांव या वार्ड स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं।
•दोनों प्रणालियों में महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।
अंतर-
•दो-स्तरीय प्रणाली में ग्राम स्तर और ब्लॉक स्तर सरकार के केवल दो स्तर हैं। दूसरी ओर, त्रिस्तरीय संरचना में तीन स्तर होते हैं: गांव, ब्लॉक और जिला।
•दो-स्तरीय प्रणाली में कम निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में दो-स्तरीय प्रणाली में प्रति गांव केवल दो प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन, केरल में त्रि-स्तरीय प्रणाली में प्रति गांव चार प्रतिनिधि होते हैं।
•दो-स्तरीय प्रणाली में तीन-स्तरीय संरचना की तुलना में कम प्रशासनिक कर्तव्य होते हैं। उदाहरण के लिए, दो-स्तरीय प्रणाली में ब्लॉक स्तर पर केवल थोड़ी संख्या में प्रशासनिक कर्तव्य होते हैं, जबकि, त्रि-स्तरीय प्रणाली में, ब्लॉक स्तर बड़ी संख्या में प्रशासनिक कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार होता है।
दो-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के फायदे और त्रुटियां:
लाभ:
•त्रि-स्तरीय प्रणाली की तुलना में, दो-स्तरीय प्रणाली सरल और लागू करने में आसान है।
•कम निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासनिक कर्तव्यों के कारण, द्वि-स्तरीय प्रणाली त्रि-स्तरीय प्रणाली की तुलना में अधिक किफायती है।
•दो-स्तरीय दृष्टिकोण की बदौलत स्थानीय समुदाय निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं, और अधिक सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं।
त्रुटि:
•जिन बड़े राज्यों को सत्ता के अधिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है, उन्हें दो-स्तरीय संरचना अप्रभावी लग सकती है।
•उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता की मांग करने वाली जटिल समस्याओं से निपटने के दौरान, दो-स्तरीय संरचना प्रभावी नहीं हो सकती है।
•निर्वाचित सदस्यों की कम संख्या के कारण, संसाधनों के न्यायसंगत आवंटन की गारंटी देने में दो-स्तरीय प्रणाली उतनी प्रभावी नहीं हो सकती है।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के फायदे और त्रुटियां:
लाभ:
•सत्ता का व्यापक विकेन्द्रीकरण और कुशल स्थानीय प्रबंधन त्रि-स्तरीय संरचना द्वारा संभव हुआ है।
•त्रि-स्तरीय दृष्टिकोण उन जटिल समस्याओं से निपटने के लिए उपयोगी है, जिनके लिए उच्च स्तर की प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकता होती है।
•चुंकि त्रिस्तरीय प्रणाली के तहत अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए संसाधनों का अधिक समान आवंटन होता है।
त्रुटि:
•दो-स्तरीय प्रणाली की तुलना में, तीन-स्तरीय प्रणाली स्थापित करना अधिक कठिन और महंगा है।
•सरकार के विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच संघर्ष त्रि-स्तरीय प्रणाली के परिणामस्वरूप हो सकता है।
•शासन के अधिक स्तर होने के कारण, त्रि-स्तरीय संरचना स्थानीय भागीदारी और जमीनी स्तर के लोकतंत्र को बढ़ावा देने में सहायक नहीं हो सकती है।
संदर्भ
https://tinyurl.com/mr4d5par
https://tinyurl.com/mr3rrxec
https://tinyurl.com/bdddyhts
चित्र संदर्भ
1. मध्य प्रदेश के एक गाँव में बैठी पंचायत को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
2. भारत की शासन संरचना को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. एक मंदिर परिसर को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. कालूपुर ग्राम पंचायत को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
5. ग्रामीणों की बैठक को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)




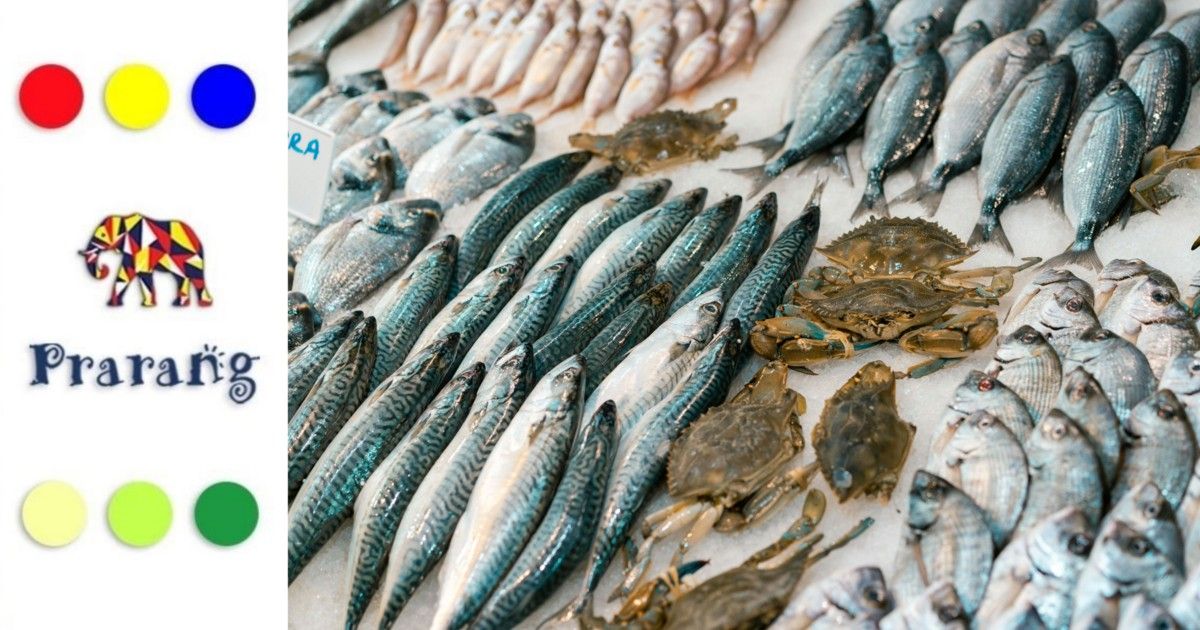
A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.