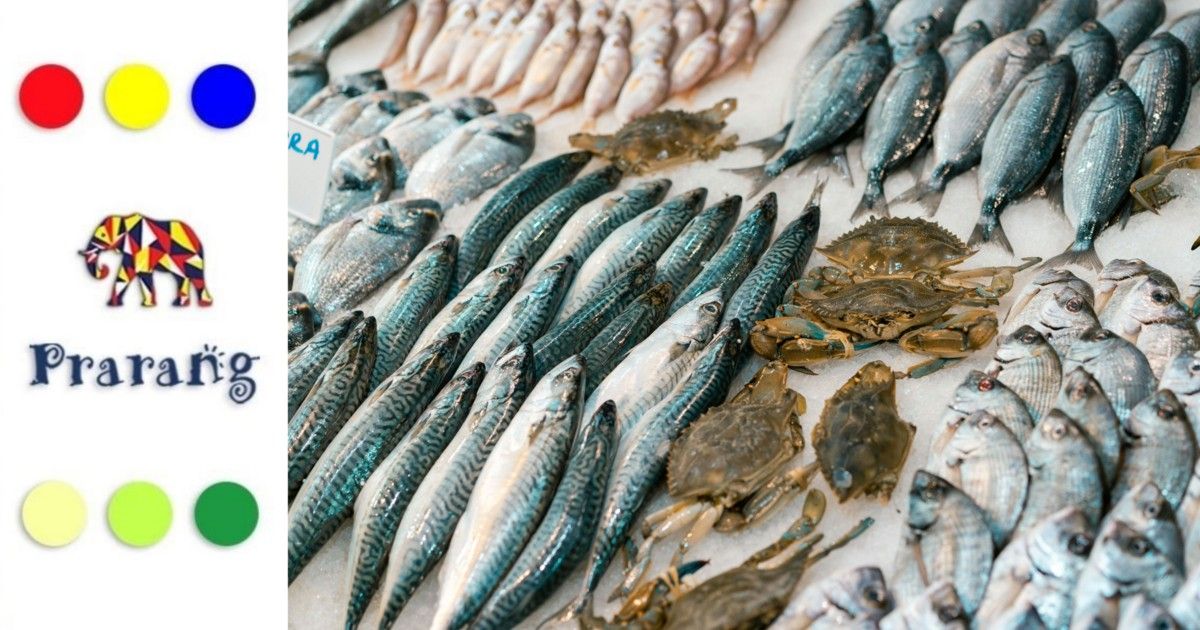हमारे मेरठ शहर में, कुछ लोगों को, पंजाबी बोलते हुए सुनना, कोई असामान्य बात नहीं है। आखिरकार, पंजाबी भाषा, भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार(Indo-European language family) के अंतर्गत, इंडो-आर्यन उपसमूह(Indo-Aryan subgroup) की एक भाषा है। सबसे प्रारंभिक पंजाबी लेखन, 9वीं और 14वीं शताब्दी के बीच, ‘नाथ योगी युग’ का है। यह अनूठी भाषा, दुनिया भर में, 100 मिलियन (Million) से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इनमें से, लगभग 90 मिलियन पंजाबी भाषी, भारत और पाकिस्तान में स्थित हैं, जबकि, शेष 10 मिलियन पंजाबी भाषी समुदाय, कनाडा(Canada), यूनाइटेड किंगडम(United Kingdom), संयुक्त राज्य अमेरिका(United States of America), मलेशिया(Malaysia), दक्षिण अफ़्रीका (South Africa), संयुक्त अरब अमीरात(United Arab Emirates) और अन्य जगहों पर फैले हुए हैं। भारत में, पंजाबी भाषा, ‘गुरुमुखी लिपि’ में लिखी जाती है, जो सिख धर्म से जुड़ी है। तो आइए, आज पंजाबी भाषा, इसकी उत्पत्ति और इसके प्रारंभिक विकास के बारे में जानें। फिर, हम इसकी गुरुमुखी लिपि के बारे में, विस्तार से बात करेंगे। आगे, हम गुरुमुखी लिपि की विशेषताओं का भी पता लगाएंगे।
प्राकृत और अपभ्रंश के, मध्यवर्ती चरणों के माध्यम से, संस्कृत से पंजाबी की यात्रा, भारतीय उपमहाद्वीप के, एक व्यापक भाषाई विकास को प्रतिबिंबित करती है। प्राकृत भाषाएं, जो अपनी सरलता और स्पष्टता के लिए जानी जाती हैं, आम लोगों द्वारा व्यापक रूप से बोली जाती थीं। यह विद्वानों और धार्मिक संदर्भों में प्रयुक्त, अभिजात्य संस्कृत से भिन्न थीं।
.jpg)
7वीं शताब्दी ईस्वी तक, उत्तरी भारत के भाषाई परिदृश्य में, महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दिखने लगे । इस कारण, क्षेत्रीय बोलियों को प्रमुखता मिलने लगी। इसी परिवेश में, पंजाबी भाषा ने स्थानीय बोलियों और विदेशी आक्रमणों के प्रभाव से, अपनी पहचान बनानी शुरू की। इससे नए भाषाई तत्व, सामने आए। 10वीं शताब्दी तक, पंजाबी, एक विशिष्ट भाषा के रूप में उभरी थी, जो अपनी अनूठी ध्वन्यात्मक, वाक्य-विन्यास और शाब्दिक विशेषताओं द्वारा चिह्नित थी। यह अवधि, पंजाबी के इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि, इस समय, पंजाबी समृद्ध साहित्यिक परंपरा के लिए एक मंच तैयार हुआ ।
गुरुमुखी लिपि, का शाब्दिक अर्थ – “गुरु के मुख से” है। 16वीं शताब्दी में, दूसरे सिख गुरु – गुरु अंगद देव जी, द्वारा इस लिपि को विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य, पंजाबी लोगों को, उनकी मूल भाषा के लिए, एक सुलभ और मानकीकृत लेखन प्रणाली प्रदान करना था। गुरुमुखी लिपि, न केवल सिख धर्म की पवित्र पुस्तक, गुरु ग्रंथ साहिब का प्राथमिक माध्यम बन गई, बल्कि, इसने समृद्ध पंजाबी साहित्य और लोककथाओं को संरक्षित करने में भी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पंजाबी सुलेख के संदर्भ में, गुरुमुखी लिपि, अपने सुरुचिपूर्ण घुमाव और विशिष्ट पात्रों के साथ, इस कला रूप को खूबसूरती से प्रस्तुत करती है।
गुरुमुखी लिपि में, पंजाबी सुलेख की कला, प्रलेखित साहित्यिक और आध्यात्मिक परंपराओं के साथ-साथ विकसित हुई। सुलेखकों ने, अपना जीवन इस लिपि की बारीकियों में महारत हासिल करने और दृश्यमान पांडुलिपियों को बनाने के लिए, समर्पित कर दिया।
.jpg ) गुरुमुखी लिपि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
गुरुमुखी लिपि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
1.) वर्णमाला: गुरुमुखी वर्णमाला में, पैंतीस अलग-अलग अक्षर हैं। पहले तीन अक्षर अद्वितीय हैं, क्योंकि, वे स्वरों का आधार बनते हैं, और व्यंजन नहीं हैं। ‘ऐरा’ को छोड़कर, पहले तीन वर्णों का, कभी भी, अपने आप उपयोग नहीं किया जाता है। इनके अलावा, व्यंजन के जोड़े पर, बिंदी लगाने से छह व्यंजन बनते हैं। हालांकि, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में मौजूद नहीं हैं।
2.) स्वर: गुरुमुखी, अन्य ब्राह्मी लिपियों के समान अवधारणाओं का पालन करती है, और इस तरह, सभी व्यंजनों के बाद एक अंतर्निहित “ए” ध्वनि आती है (जब तक कि, किसी शब्द के अंत में, “ए” हटा नहीं दिया जाता है)। इस अंतर्निहित स्वर ध्वनि को, आश्रित स्वर संकेतों का उपयोग करके बदला जा सकता है, जो एक असरदार व्यंजन से जुड़ते हैं। स्वतंत्र स्वरों का निर्माण, तीन वाहक वर्णों का उपयोग करके किया जाता है: उरा (ੳ), ऐरा (ਅ) और इरी (ੲ)। ऐरा (जो स्वर “ए” का प्रतिनिधित्व करता है) के अपवाद के साथ, उनका उपयोग कभी भी, अतिरिक्त स्वर चिह्नों के बिना नहीं किया जाता है।
3.) हलंत: पंजाबी को, गुरुमुखी में लिखते समय, हलंत (੍) वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है। हालांकि, इसका उपयोग, कभी-कभी संस्कृत रचित पाठ, या शब्दकोशों में अतिरिक्त ध्वन्यात्मक जानकारी के लिए, किया जा सकता है। जब हलंत का उपयोग किया जाता है, तो, यह अंतर्निहित स्वर के, दमन का प्रतिनिधित्व करता है।
इसका प्रभाव नीचे दिखाया गया है:
ਕ – का
ਕ੍ – के
4.) अंक:
गुरुमुखी के पास, अंकों का अपना समूह है, जो हिंदू-अरबी अंकों की तरह दिखता है। इनका उपयोग, पुराने ग्रंथों में, बड़े पैमाने पर किया गया है। आधुनिक संदर्भों में, उन्हें, मानक लैटिन (Standard Latin) अंकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, हालांकि, वे अभी भी व्यापक उपयोग में हैं।
0-੦
1 – ੧
2 – ੨
3 – ੩
4 – ੪
5 – ੫
6 – ੬
7 – ੭
8 – ੮
9 – ੯
5.) अन्य चिह्न: बिंदी (ਂ) और टिप्पी (ੰ) का उपयोग, अनुनासिकीकरण के लिए किया जाता है। सामान्य तौर पर, ओंकार (ੁ) और दुलांकार (ੂ), अपने शुरुआती रूपों में, बिंदी लेते हैं, और व्यंजन के बाद इस्तेमाल होने पर टिप्पी लेते हैं। अन्य सभी छोटे स्वर, टिप्पी लेते हैं, और अन्य सभी लंबे स्वर बिंदी लेते हैं। पुराने पाठ, इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। अद्दक (ੱ) का प्रयोग, दर्शाता है कि, निम्नलिखित व्यंजन श्रेष्ठ है। इसका मतलब यह है कि, बाद के व्यंजन को, दुगना या प्रबलित किया जाता है।
6.) विसर्ग: विसर्ग प्रतीक (ਃ) का प्रयोग, गुरुमुखी में कभी-कभी किया जाता है। यह, या तो एक संक्षिप्त नाम का प्रतिनिधित्व कर सकता है, या किसी संस्कृत विसर्ग की तरह कार्य कर सकता है; जहां स्वर के बाद, एक ध्वनिहीन ‘ह’ का उच्चारण किया जाता है।
7.) एक ओंकार: एक ओंकार (ੴ), गुरुमुखी में प्रतीक है, जिसका प्रयोग, अक्सर ही, सिख साहित्य में किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ – “एक ईश्वर” है।
संदर्भ
https://tinyurl.com/2k92jzxh
https://tinyurl.com/muwahsad
https://tinyurl.com/mv3swzx6
चित्र संदर्भ
1. गुरु ग्रंथ साहिब को संदर्भित करता एक चित्रण (snl)
2. गुरुमुखी लिपि की आधुनिक वर्णमाला को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. गुरु अर्जन की लिखावट में, 17वीं सदी के मूल मंतर को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
.jpg )
.jpg )
.jpg)
.jpg )