
समय - सीमा 288
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1058
मानव और उनके आविष्कार 829
भूगोल 262
जीव-जंतु 317

मुद्रण (Printing) व्यवसाय में मेरठ भारत के अग्र शहरों में से एक है लेकिन आज इस स्थान में काफी तेज़ी से गिरावट आ रही है। मुद्रण मतलब प्रतिमा और लेखन की प्रतिलिपि बनाने का इतिहास काफी पुराना और रंजक है। आईये हम आज विश्व में मुद्रण व्यवसाय के बारे में जानें और मेरठ में इसकी शुरुवात कब हुई इसका लेखा जोखा लें।
3000 ईसा पूर्व और उससे पहले:
मेसोपोटेमिया संस्कृति के लोग लंबगोलाकार मुहरों का इस्तेमाल मिट्टी की पट्टीयों पर चित्र छापने के लिए इस्तेमाल करते थे। मिस्र और चीन की संस्कृति में कपड़े पर छोटे ठप्पों से छपाई करते थे।
दूसरी शताब्दी ईस्वी:
चीन के त्से लुन (Ts’ai Lun) नामक इंसान ने कागज़ का शोध लगाया।
सातवीं शताब्दी ईस्वी:
संत जॉन की धर्मदीक्षा लिखी हुई एक छोटी पुस्तिका संत कुथबर्ट की कब्र में रखी गयी। उसे सन 1104 में ब्रिटेन में स्थित डरहम के प्रधान गिरिजाघर में रखी हुई उनकी कब्र से निकाला गया। आज कुथबर्ट धर्मदीक्षा के नाम से जाने जाने वाली यह पुस्तिका सबसे पुरानी यूरोपीय पुस्तिका मानी जाती है।
ग्यारहवीं शताब्दी ईस्वी:
चलत मुद्रण के लिए चीन के पाई शेंग (Pi Sheng) ने कठिन मिट्टी का इस्तेमाल कर कुछ वर्णाक्षर बनाए लेकिन उसके थोड़े मृदु पदार्थ के इस्तेमाल की वजह से यह तकनीक इतनी इस्तेमाल नहीं हुई।
बारहवीं शताब्दी ईस्वी:
कागज़ बनाने की तकनीक युरोप पहुंची।
तेरहवी शताब्दी ईस्वी:
जापान, कोरिया और चीन में कांसे का इस्तेमाल कर वर्णाक्षर प्रकार बनाए गए। इस तकनीक का इस्तेमाल कर बनाई हुई सबसे पुरानी किताब का नाम बौद्ध साधू और सिओन गुरुओं की चुनी हुई तालीम (Selected Teachings of Buddhist Sages and Seon Masters) है जो एक कोरियन बौद्ध किताब है।
15 वीं शती:
क्योंकि जापान और चीन में वुडकट (Woodcut) यानी लकड़ी पर रेखांकन कर बनाए चित्रों का इस्तेमाल मुद्रण के लिए सदियों से चला आ रहा था लेकिन यूरोप में इस तकनीक का सबसे पुराना साक्ष्य 15वीं शती से है। इस तकनीक में लकड़ी पर चाकू अथवा छुरी से रेखांकन किया जाता है जिसमें चित्र और शब्द को उभरी हुई नक्काशी में तब्दील किया जाता है, बाकी का भाग निकाल दिया जाता है। फिर इसपर स्याही लगाई जाती है और अवस्तर को इसपर दबाया जाता है। इसकी स्याही तेल के दियों पर जमने वाले कालिख से बनाई जाती है जिसे रोगन अथवा अलसी के तेल में उबालकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस समय में किताबें फिर भी बहुत कम मिलती हैं क्योंकि उन्हें हाथ से ही लिखा जाता था। कैंब्रिज विश्वविद्यालय जो यूरोप के सबसे बड़े लाइब्रेरी में से एक का धनी है उसमें भी सिर्फ 122 किताबें हैं।
सन 1436 में गुटेनबर्ग ने अपने मुद्रण यन्त्र पर काम करना शुरु कर दिया था, इस कार्य को पूरा करने में उन्हें चार साल लग गए जिसमें उन्होंने लकड़ी के मुद्रण यन्त्र में छपाई के लिए धातु की चलत-पट्टीयाँ इस्तेमाल की। उन्होंने सबसे पहले बाइबल छापना शुरू किया, प्रथम आवृत्ति में एक पन्ने पर 40 पंक्तियाँ थी तथा दूसरी बार में उन्होंने 42 पंक्तियों वाले दो खंड छपवाए। प्रस्तुत चित्र में गुटेनबर्ग को अपनी प्रेस पर काम करते हुए देखा जा सकता है। सुखी बिंदु उत्कीर्णन द्वारा नक्काशी बनाने का शोध एक दक्षिण जर्मनी के कलाकार हाउसबुक मास्टर को जाता है। इस तकनीक में तांबे की प्लेट पर एसिड के बिना उत्कीर्णन के लिए किसी भी धातु की सुई अथवा हीरे की नोंक की छेनी का इस्तेमाल किया जाता है।
वेनिस में स्थित स्पेलर के जॉन और वेंडेलीन ने उत्तम तरीके से रोमन प्रकार के मुद्रण के लिए इस्तेमाल किया जिसमें किताबों में मुद्रित शब्द हाथ की लिखावट के जैसे दिख रहे थे।
सन 1476 में विलियम काक्सटन ने नेदरलैंड से सामान मंगवाकर इंग्लैंड के वेस्टमिन्स्टर पर पहला छापखाना खोला तथा इसी साल पहली बार तांबे की पट्टिका का नक्काशी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह शती समाप्त होते-होते यूरोप में 250 के ऊपर मुद्रणालय शुरू हो गए थे और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से पुस्तक मेले लगने लगे जिसमें से फ़्रंकफ़र्ट का पुस्तक मेला सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
16वीं शती:
एलडस मैनुटलस नाम के मुद्रक ने पहली बार छोटी, सुवाहय़ क़िताबें प्रस्तुत की तथा उसी ने पहले इटैलिक (Italic) शब्द लिखने के तरीका का इस्तेमाल किया, यह परिकल्पना वेनिस-निवासी फ्रांसेस्को ग्रिफ्फो की थी।
सन 1507 में लुकास क्रानाख ने किआरोस्कूरो वुडकट (Chiaroscuro Woodcut) का इस्तेमाल किया जिसमें दो य अधिक लकड़ी के टुकड़ों पर अलग अलग रंग लगाकर चित्र मुद्रित किये जाते थे।
17वीं शती:
क्रिस्टोफ प्लांटीन इस शती का सबसे प्रसिद्ध मुद्रक था, उसी ने पहली प्रतिच्छाया मुद्रित की। उसका मुद्रित किया हुआ काम तथा उसने इस्तेमाल की हुई उपकरण सामग्री प्लांटीन-मोरेटस संग्रहालय में रखी गयी है।
इस शती में इसाई धर्म प्रसार का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा था जिस वजह से बहुतायता से मुद्रणालय बाइबल आदि धार्मिक किताबों का सबसे ज्यादा मुद्रण करते थे।
इस समय का एक वाक्या कुछ इस प्रकार है कि राजा चार्ल्स प्रथम और कैंटरबरी के मुख्य धर्माध्यक्ष के समय में सन 1634 में मुद्रक रोबर्ट बार्कर एवं मार्टिन लुकास के मुद्रणालय में मुद्रित राजा जेम्स की बाइबल छपवाई गयी। लेकिन उसमें निर्गमन 20:14 में जब भगवान मोसेस को कहता है कि तुम परस्त्रीगमन नहीं करोगे, तो इसमें वे यह शब्द मुद्रित करना भूल गए। इस वजह से उन्हें जुरमाना तो भरना पड़ा ही साथ में उनका मुद्रण का अनुज्ञापत्र रद्द कर दिया गया। इस बाइबल को आज दुष्ट/ व्यभिचारी/पातकी बाइबल कहा जाता है।
सन 1690 में पहला अमरीकी काग़ज़ का कारखाना खुला। सन 1642 में लडविग फौन सीगन ने मेज़ोटिंट (Mezzotint) नामक तकनीक का आविष्कार किया, इस तकनीक में एक तांबे की पट्टी पर धातु के छोटे दांत वाले ‘रॉकर’ (Rocker) नाम के साधन से हजारों छोटे-छोटे बिंदु का इस्तेमाल कर उसे खुरखुरा करके आंशिक रंग निकाला जाता था। पट्टी को साफ़ करने पर यह छोटे बिंदु स्याही को पकड़े रखते थे।
18वीं शती:
सन 1710 में जर्मन कलाकार और नक़्क़ाश जकोब क्रिस्टोफ ले ब्लोन ने मेज़ोटिंट तकनीक का इस्तेमाल कर रंगीन चित्र की नक़्क़ाशी बनाई, इस लिए उसने एक के बजाय तीन पट्टियों का इस्तेमाल किया, लाल पीला और नीला जो न्यूटन के हिसाब से रंगवाली के सभी रंगों को बनाने वाले प्राथमिक रंग हैं, जो हमारे प्रारंग के भी रंग हैं।
विलियम कैसलोन का ढलाईघर लंदन से 200 साल तक कार्यरत था, उसने ढाला हुआ कैसलोन रोमन ओल्ड फेस (Caslon Roman Old Face) यह डच अक्षरों जैसा प्रकार जो सन 1716 और 1728 के बीच तैयार किया गया था तथा बाकी के उसने बनाए हुए टंकित अक्षर प्रकार आज भी इस्तेमाल किये जाते हैं और वे काफी प्रसिद्ध हैं।
सन 1732 में बेंजामिन फ्रेंक्लिन ने खुदका मुद्रणालय शुरू किया। सन 1796 में अलोइस सेनेफेल्डर ने शिलामुद्रण का आविष्कार किया, इस तकनीक में कई बदलाव आये हैं लेकिन आज भी यह तकनीक इस्तेमाल की जाती है। गिआमबसट्टीटा बोड़ोनी नाम के इटली के मुद्रक द्वारा बनाए हुए अक्षर प्रकार आज भी इस्तेमाल में हैं।
19वीं शती:
सन 1800 में चार्ल्स स्टानहोप ने ऐसा मुद्रण यन्त्र बनाया जिसका ढांचा लकड़ी के बजाय लोहे का बना था। इसके बाद गोट्टलोब कोनिग और अन्द्रेअस फ्रेडरिश बाऊएर ने पहले सिलिंडर (Cylinder) अर्थात दो गोलों का बना मुद्रण यन्त्र बनाया। यह दोनों तकनीक आज भी इस्तेमाल में है तथा कोनिग और बाऊएर की कंपनी आज भी के.बी.ए. (KBA) नाम से कार्यरत है।
सन 1837 में गॉडफ्रे एंगेलमैन को रंगीतशिलामुद्रण के लिए आविष्कार के लिए एकस्व (पेटेंट-Patent) अधिकार दिया गया।
इसी समय के आस-पास अमेरिकी अन्वेषक रिचर्ड मार्च हो ने पहला घूमनेवाला शिलामुद्रण यंत्र बनाया।
चेक कलाकार कारेल क्लिक ने सन 1878 में फोटोग्रावुर (Photogravure) तकनीक का आविष्कार किया, इसमें आप धातु पर फ़ोटो निगेटिव की सहायता से चित्र का प्रतिरूप जैसे का तैसा बना सकते हैं। सन 1886 में ओट्टमार मेरगेनथालेर ने लीनोटाइप अक्षर प्रकार बनाने की मशीन का आविष्कार किया। सन 1890 में बिब्बी, बैरन और सन्स ने फ्लेक्सोग्रफिक (Flexographic) मुद्रण का शोध लगाया, इसमें रबड़ की पट्टिका पर उभरी हुई नक्काशी पर चित्र लगाके मुद्रण किया जाता है।
20वीं शती:
सन 1903 में अमेरिकी मुद्रक इरा वाशिंगटन रूबेल ने शिलामुद्रण में आफसेट (Offset) मुद्रण यंत्र बनाया। सन 1907 में इंग्लैंड के सामुएल साइमन को रेशम का मुद्रण पटल के आविष्कार के लिए एकस्व (पेटेंट-Patent) अधिकार दिया गया। सन 1915 में हॉलमार्क ने पहला क्रिसमस शुभकामना पत्र तैयार किया, इसी काल में सन 1888 में नेशनल जियोग्राफिक (National Geographic), सन 1883 में लाइफ (Life), सन 1923 में टाइम (Time), सन 1892 में वोग (Vogue) और सन 1920 में रीडर्स डाइजेस्ट (Reader’s Digest) यह पत्रिकाएँ लोगो तक पहुँचने लगी।
कोनिग और बाऊएर ने सन 1923 में चार रंगों का इस्तेमाल करने वाला आईरिस (Iris) मुद्रण यंत्र बनाया।
सन 1935 में इंग्लैंड के पेंग्विन किताब प्रकाशक ने कागज़ी पृष्ठ की किताबें छापना शुरू किया, उन्होंने जर्मन प्रकाशक अल्बाट्रोस किताब प्रकाशक की कल्पनाओं का इस प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया।
सन 1938 से लेकर 1959 तक ज़ेरोग्राफ़ी (Xerography) ज़ेरॉक्स मतलब स्याही के बिना प्रतिलिपि बनाने की तकनीक में बहुत परवतन आये।
सन 1948 में जापानी कंपनी शिनोहारा ने फ्लैटबेड लैटरप्रेस मशीन (Flatbed Letterpress Machine) बनाना शुरू किया।
सन 1967 में आय.एस.बी.एन. (ISBN) मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या की निर्मित्ति हुई। यह व्यावासिक पुस्तकों को दी जाने वाली संख्या है जिस से उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सन 1975 में पहले लेज़र (Laser) मुद्रण यन्त्र बाज़ार में आये। सन 1993 में आधुनिक मुद्रण की शुरुवात हुई।
21वीं शती:
इस समय में आफसेट (Offset) मुद्रण यंत्र का विकासशील गति से उत्क्रांत हुआ। इंकजेट (Inkjet) तकनीक की शुरुवात भी 21वीं शताब्दी में ही शुरू हुई।
सन 1790 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेरामपोर, कलकत्ता में मुद्रणालय शुरू किया। जब वारेन हास्टिंग्स ने अवध राज्य हथिया लिया और वे दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे तब उन्होंने मेरठ की बेगम समरू के किराये के सिपाहियों का इस्तेमाल किया। इन सभी वाक्यों की वजह से मेरठ में अंग्रेजों का एवं ब्रितानी सिपाहियों का बसेरा बढ़ गया साथ ही मेरठ की छावनी एवं बहुत से गिरिजाघरों की स्थापना हुई, बेगम समरू और इसाई धर्म प्रचारकों की वजह से मेरठ में इसाई धर्म का प्रसार हुआ। धर्म प्रचार और प्रसार के लिए मेरठ में इसाई-धर्मगुरु यहाँ पर पहली बार मुद्रण यन्त्र लाये।
1. https://www.prepressure.com/printing/history
2. http://prarang.in/Meerut/180104697
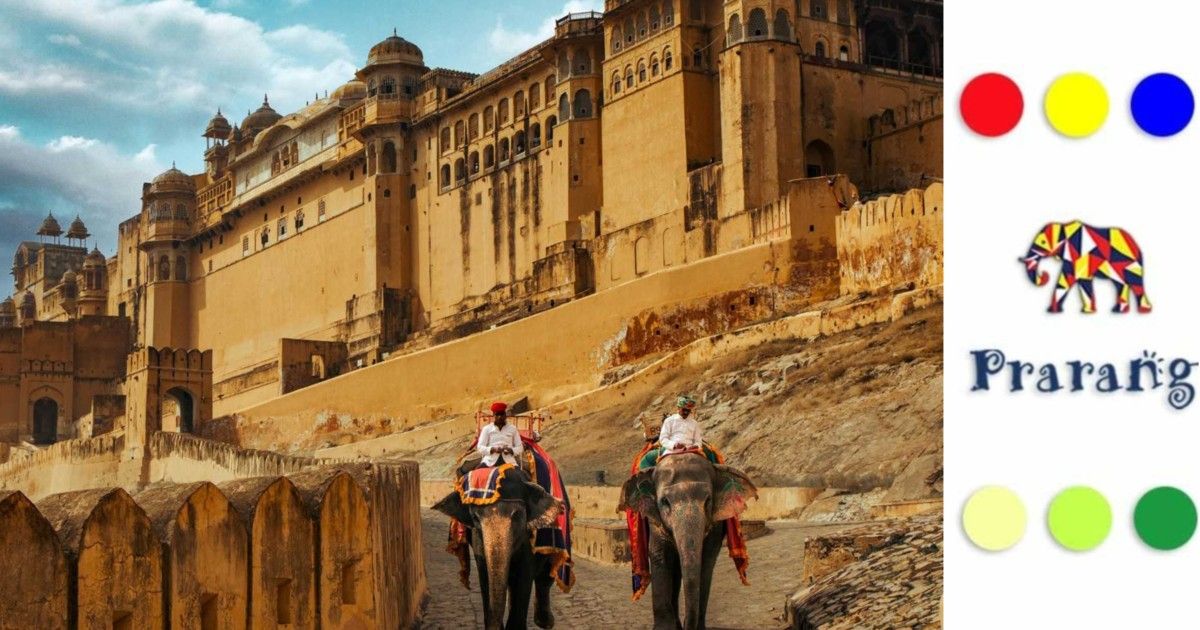
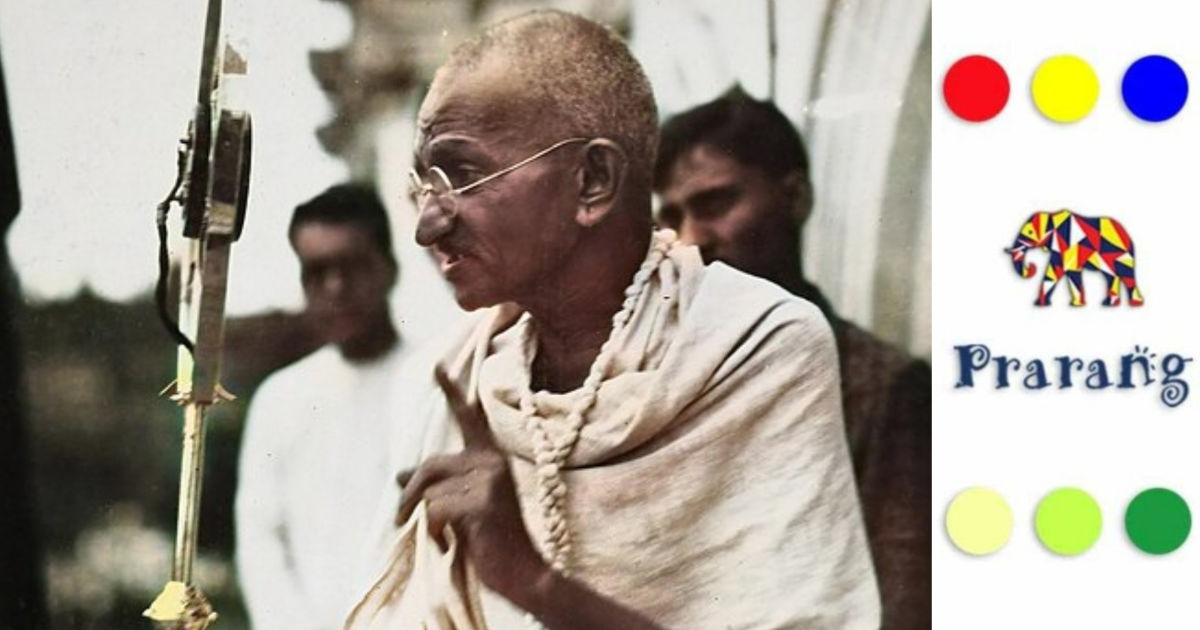



A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.