
समय - सीमा 289
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1064
मानव और उनके आविष्कार 837
भूगोल 267
जीव-जंतु 321
| Post Viewership from Post Date to 29- Dec-2025 (31st) Day | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 2754 | 88 | 6 | 2848 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

मेरठवासियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन विशाल हाथियों को हम प्राचीन भारत की कथाओं, मंदिरों की मूर्तियों और मेलों में सम्मान के प्रतीक के रूप में देखते हैं, वे आज विज्ञान की प्रयोगशालाओं में भी अध्ययन का विषय बन चुके हैं? धरती के इन सबसे बुद्धिमान जीवों के अस्तित्व पर आज बड़ा संकट मंडरा रहा है - लेकिन उम्मीद की किरण है “संरक्षण आनुवंशिकी” (Conservation Genetics)। यह आधुनिक विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों के डीएनए (DNA) और जीनों के माध्यम से उनके अस्तित्व को बचाने की दिशा में काम कर रही है। जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार और आवास विनाश से जूझते हाथियों के लिए यह शोध किसी पुनर्जागरण से कम नहीं। यही वह क्षेत्र है जहाँ विज्ञान, संवेदना और संरक्षण एक साथ खड़े दिखाई देते हैं - और यही प्रयास भविष्य की पीढ़ियों को इन अद्भुत जीवों के दर्शन का अवसर देगा।
आज के इस लेख में हम जानेंगे कि संरक्षण आनुवंशिकी क्या होती है और यह हाथियों की जैव विविधता को बचाने में क्यों महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, हम हाथियों की प्राचीन वंशावली और नई आनुवंशिक खोजों पर भी नज़र डालेंगे। आगे, हम आईआईएससी (IISc) और आईआईएसईआर (IISER) जैसे भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों की भूमिका समझेंगे, जो हाथियों के जीन अध्ययन में अहम योगदान दे रहे हैं। अंत में, हम हाथियों की घटती संख्या, सरकारी पहलों जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट (Project Elephant), और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
संरक्षण आनुवंशिकी: एक आधुनिक वैज्ञानिक क्रांति
संरक्षण आनुवंशिकी विज्ञान का वह क्षेत्र है जो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जीन और डीएनए के अध्ययन का उपयोग करता है। यह विधा यह समझने में मदद करती है कि किस प्रकार किसी प्रजाति की आनुवंशिक विविधता घटने पर वह धीरे-धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ती है। जब किसी प्रजाति के भीतर जीनों में विविधता कम हो जाती है, तो उसकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता और पर्यावरणीय अनुकूलन क्षमता दोनों घट जाती हैं। संरक्षण आनुवंशिकी इन जोखिमों को पहचानकर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करती है। आज यह विज्ञान “इकोलॉजी” (Ecology) और “जीनोमिक्स” (Genomics) को जोड़कर एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर रहा है - जिसमें न केवल प्रजातियों का संरक्षण होता है, बल्कि यह भी समझा जा सकता है कि कौन सी आबादी किस आनुवंशिक कारण से अधिक संवेदनशील या लुप्तप्राय है। यही कारण है कि अब विलुप्ति से पहले ही आनुवंशिक स्तर पर सुधार की रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, जैसे नियंत्रित प्रजनन और जीनोमिक विविधता का संरक्षण।

हाथियों की प्राचीन वंशावली और नई आनुवंशिक खोजें
हाथी, पृथ्वी के सबसे प्राचीन और बुद्धिमान जीवों में से एक हैं। लंबे समय तक वैज्ञानिक मानते थे कि केवल दो ही प्रमुख प्रजातियाँ हैं - अफ्रीकी और एशियाई हाथी। लेकिन आधुनिक आनुवंशिक अनुसंधान ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। डीएनए विश्लेषण से पता चला कि अफ्रीकी हाथियों की दो अलग-अलग प्रजातियाँ हैं - अफ्रीकी वन हाथी और अफ्रीकी सवाना हाथी। इसके अलावा, एक विलुप्त प्रजाति पैलियोलोक्सोडोन एंटीकस (Palaeoloxodon Antiquus) (सीधे दाँत वाला हाथी) भी अस्तित्व में थी, जो अफ्रीकी वन हाथी से आनुवंशिक रूप से काफी निकट पाई गई। इन खोजों ने हाथियों के विकासवादी इतिहास की हमारी समझ को नया आयाम दिया। यह स्पष्ट हुआ कि हाथियों की वंशावली केवल अफ्रीका तक सीमित नहीं थी, बल्कि यूरोप और एशिया में भी उनके आनुवंशिक निशान मौजूद थे। यह वैज्ञानिक प्रमाण यह भी दिखाता है कि हाथियों में हजारों वर्षों से निरंतर जीन प्रवाह होता रहा है, जिसने उन्हें पर्यावरणीय बदलावों के बावजूद टिके रहने में मदद की।

आधुनिक वैज्ञानिक शोध और भारतीय संस्थानों की भूमिका
भारत इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) पुणे के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एशियाई हाथियों के जीनोम का अनुक्रमण किया है। इस अध्ययन से यह पता चला कि एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के बीच कई आनुवंशिक अंतर हैं, खासकर उन जीनों में जो गंध की पहचान और पर्यावरणीय अनुकूलन से जुड़े हैं। इस शोध से यह समझने में मदद मिली है कि एशियाई हाथियों ने अपने पर्यावरण के अनुरूप खुद को किस तरह ढाला। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये आनुवंशिक भिन्नताएँ न केवल उनके व्यवहार और अनुकूलन की क्षमता को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे अनुसंधान भारत को वैश्विक संरक्षण प्रयासों में एक वैज्ञानिक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं।

विलुप्ति की ओर बढ़ते हाथी: वैश्विक और भारतीय परिदृश्य
आज जब दुनिया के कई हिस्सों में हाथियों की गर्जना धीरे-धीरे कम हो रही है, तो यह चेतावनी का संकेत है। आईयूसीएन (IUCN) के अनुसार, पिछले सौ वर्षों में अफ्रीकी सवाना हाथियों की आबादी में 60% और अफ्रीकी वन हाथियों में 86% की गिरावट दर्ज की गई है। भारत में भी मानव गतिविधियों, शहरीकरण और वन क्षेत्र घटने के कारण एशियाई हाथियों के लिए स्थान कम होता जा रहा है। हाथियों की यह घटती आबादी केवल पर्यावरणीय हानि नहीं, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन के लिए खतरा है। ये प्राणी बीज फैलाव, जंगल पुनर्जीवन और जल स्रोतों के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनका विलुप्त होना पृथ्वी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है।

डीएनए प्रोफाइलिंग और प्रोजेक्ट एलिफेंट: भारत की बड़ी पहल
भारत सरकार ने 1992 में “प्रोजेक्ट एलिफेंट” की शुरुआत की, जो अब हाथी संरक्षण की दिशा में एक मॉडल परियोजना बन चुकी है। इस पहल के तहत हाल ही में 270 हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग (DNA Profiling) पूरी की गई है। यह प्रक्रिया हर हाथी की एक अनूठी पहचान बनाने में मदद करती है - ठीक वैसे जैसे मनुष्यों के लिए ‘आधार कार्ड’। साथ ही, “गज सूचना मोबाइल एप्लिकेशन” के माध्यम से बंदी हाथियों की देखभाल, स्थानांतरण और निगरानी आसान हुई है। इस तकनीक के ज़रिए अधिकारियों को न केवल प्रत्येक हाथी की स्वास्थ्य स्थिति का डेटा मिलता है, बल्कि अवैध शिकार और तस्करी पर भी नियंत्रण संभव हुआ है। यह पहल दर्शाती है कि भारत संरक्षण आनुवंशिकी को व्यवहारिक रूप में अपनाने वाला अग्रणी देश बन रहा है।
मानव-हाथी संघर्ष और संरक्षण की भविष्य दिशा
विकास और प्रकृति का संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। जैसे-जैसे मानव बस्तियाँ हाथियों के प्राकृतिक गलियारों में फैल रही हैं, वैसे-वैसे संघर्ष बढ़ रहा है। यह न केवल हाथियों के लिए खतरनाक है, बल्कि ग्रामीण समुदायों के लिए भी चुनौती है। संरक्षण का भविष्य तभी संभव है जब स्थानीय समुदाय, सरकार और वैज्ञानिक संस्थान एक साझा दृष्टिकोण से काम करें। डीएनए-आधारित पहचान प्रणाली, हाथियों के प्रवासन पैटर्न का विश्लेषण, और सुरक्षित कॉरिडोर बनाना - ये सभी पहल मानव-हाथी सह-अस्तित्व की दिशा में ठोस कदम हैं। मेरठ जैसे शहरी क्षेत्र के नागरिक भी इस प्रयास का हिस्सा बन सकते हैं - जागरूकता, समर्थन और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के ज़रिए।
संदर्भ-
https://tinyurl.com/54h7nh7v
https://tinyurl.com/2x6wve6b
https://tinyurl.com/49j5wchh
https://tinyurl.com/bdmw8v3p
https://tinyurl.com/4tphy3jf
https://tinyurl.com/ypupb7mt



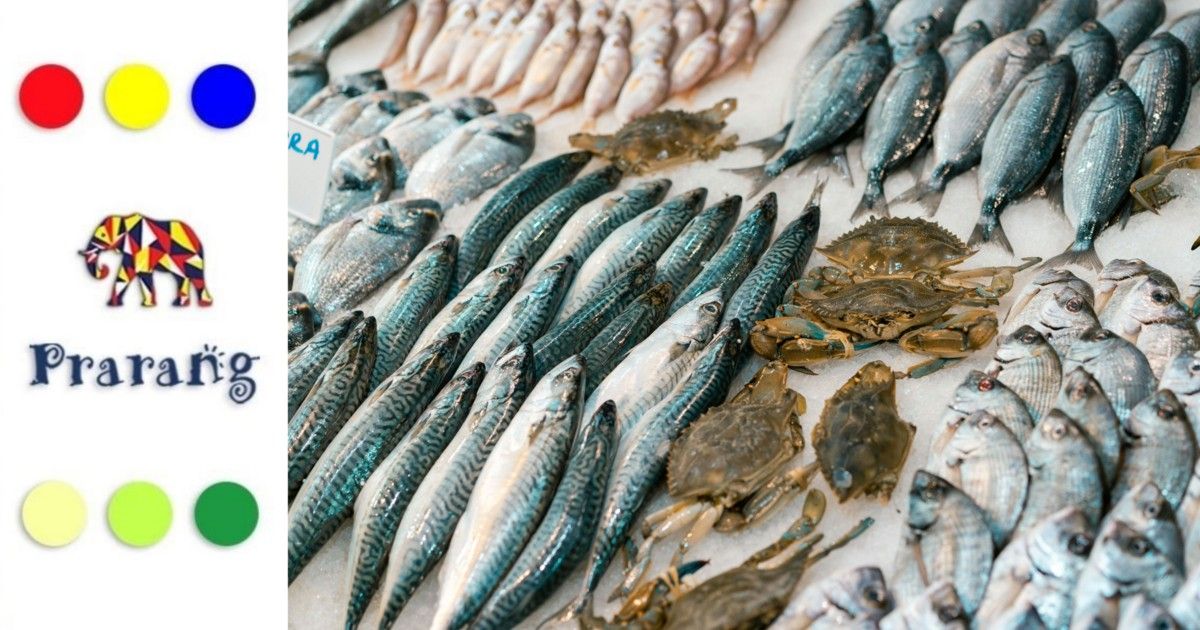

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.