
समय - सीमा 288
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1058
मानव और उनके आविष्कार 829
भूगोल 262
जीव-जंतु 317
समय - सीमा 288
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1058
मानव और उनके आविष्कार 829
भूगोल 262
जीव-जंतु 317

चीनी उद्योग भारत का एक महत्वपूर्ण कृषि-आधारित उद्योग है, जो लाखों गन्ना किसानों और चीनी मिलों में नियोजित कर्मियों की आजीविका को प्रभावित करता है। साथ ही साथ ये परिवहन, मशीनरी (Machinery) की व्यापार सेवाओं और कृषि आदानों की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न सहायक गतिविधियों में भी रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। इसके लिए आधारभूत कच्चा माल गन्ना है। परंतु जैसे-जैसे दुनिया भर में चीनी की मांग और कीमतों में गिरावट आ रही है उससे देश के गन्ना किसानों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा मेरठ जिले पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है, जिसकी अर्थव्यवस्था गन्ने पर अत्यधिक निर्भर है।
वर्तमान में भारत में चीनी उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। वैश्विक व घरेलु बाज़ार में चीनी के दामों में भारी गिरावट आई है जिससे उत्पादकों के उत्साह में भी कमी आई है। 2019 में आम चुनाव आने के साथ, चीनी बाजारों का प्रबंधन करना और चीनी मिलों तथा गन्ना उत्पादकों के हितों को संतुलित करना भारत सरकार के लिए एक गंभीर नीतिगत चुनौती बन गई है। फसल वर्ष 2017-18 में उच्च गन्ना उत्पादन ने इस समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादकों को 180 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाना शेष है। अधिक उत्पादन होने के बाद भी बाज़ार में क़ीमत कम होने के कारण चीनी उत्पादक अपेक्षित मुनाफ़ा नहीं कमा पा रहे हैं।
भारत चीनी उत्पादन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और इसके अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार चीनी की कीमतों में गिरावट का सामना कर रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा चीनी उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अब तक कई कदम उठाये गए हैं। परंतु जब वैश्विक बाज़ार में चीनी के दामों में भारी गिरावट आई हो तो चीनी निर्यात बढ़ाना आसान नहीं होता है। इसके अलावा वैश्विक बाज़ार में मुख्य चीनी उत्पादक देश, जिनमें ब्राज़ील और थाईलैंड शामिल हैं, भारत के प्रतियोगी हैं, इसलिए भारतीय चीनी निर्यातकों को वैश्विक बाजार में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
विश्व बैंक के अनुसार, 2018 में वैश्विक बाजार में चीनी की कीमत 25.95 रू. प्रति किलो थी और यदि घरेलू बाजार की बात करे तो सितंबर 2017 में चीनी की कीमत 44.89 रू. प्रति किलो थी जो कि 2018 में 14 प्रतिशत घटकर 37.88 रू. प्रति किलो रह गई। सरकार के कृषि सांख्यिकी विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया था कि फसल वर्ष 2017-18 में चीनी का उत्पादन 35 मिलियन मेट्रिक टन (Million Metric Tonne) से अधिक होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक था। इस तरह से यह प्रतिवर्ष बढ़ता जायेगा जिस कारण मिल मालिकों के लिए गन्ना किसानों का भुगतान करना मुश्किल हो जाएगा।
इस समस्या से निपटने के लिये इथेनॉल (Ethanol) उत्पादन वैकल्पिक समाधान हो सकता है। इथेनॉल एक कृषि आधारित उत्पाद है जो चीनी उद्योग के सह-उत्पाद शीरा से निकाला गया मौलिक उत्पाद है। गन्ने के अधिशेष उत्पादन वाले वर्षों में, जब चीनी की कीमतें काफी कम हो जाती हैं तो चीनी उद्योग किसानों के गन्ने की कीमत का भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं। परंतु इथेनॉल उत्पादन से इस नुकसान को कम किया जा सकता है। कई सरकारी कार्यक्रम चीनी मिलों को इथेनॉल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल न केवल प्रदूषण को कम करता है वरन् यह गन्ने के उपयोग के लिए एक अन्य स्त्रोत भी प्रदान करता है।
गन्ने को आमतौर पर जैव ईंधन (इथेनॉल) के उत्पादन के लिए बायोमास (Biomass) के सबसे महत्वपूर्ण और पर्याप्त स्रोतों में से एक माना जाता है। यह खाद्य पदार्थों जैसे फाइबर (Fibre) और ऊर्जा का विशेष स्रोत होने के साथ-साथ बिजली उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में इथेनॉल की वैश्विक मांग में काफी वृद्धि हुई है जो ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रीनहाउस गैस (Greenhouse Gas) उत्सर्जन में कमी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायक है।
वर्तमान में विश्व स्तर पर, यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 15 प्रतिशत गन्ना फसलों को इथेनॉल में बदल दिया जाता है। इसके अलावा रिपोर्टों (Reports) से पता चलता है कि जैव ऊर्जा से वैश्विक ऊर्जा की मांग को 30 प्रतिशत से अधिक मात्रा तक पूरा किया जा सकता है। कुछ विकासशील देशों, विशेष रूप से ब्राज़ील, भारत, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और संभवतः कई अफ्रीकी देशों, जैसे तंजानिया या मोज़ाम्बिक, ने भूमि और प्राकृतिक संसाधनों (जैसे कोयला आदि) के उपयोग को कम कर दिया है। इनका उपयोग केवल तब किया जायेगा जब तेल की कीमतें अधिक होंगी या भविष्य में और भी बढ़ेंगी।
प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार, इथेनॉल के उत्पादन कार्यक्रम में 22.6 करोड़ खर्च होंगे और ये संभवतः किसानों को भुगतान करने में मदद करेंगे। सरकार पेट्रोलियम (Petroleum) ईंधन के साथ इथेनॉल के मिश्रण को भी अनिवार्य कर रही है, जो 2020 तक 20 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। हालांकि, 2016 तक यह मात्रा केवल 3.3 प्रतिशत थी। इस मामले में हमें ब्राज़ील से कुछ सीखना चाहिये। ब्राज़ील कई दशकों तक दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक रहा है, और इसने 1970 की शुरुआत में गन्ना आधारित इथेनॉल का उत्पादन शुरू किया, और अपने वैश्विक कर्ज को सीमित करने के लिए राष्ट्रीय ईंधन एल्कोहॉल कार्यक्रम की शुरूआत की, जिसे प्रोलकूल (Proálcool) के रूप में जाना जाता है। ब्राज़ील की इथेनॉल उत्पादन प्रणाली अद्वितीय है। इस देश की अधिकांश चीनी मिलें चीनी और इथेनॉल दोनों का उत्पादन करने में सक्षम हैं।
यदि भारत ब्राज़ील के गन्ना-इथेनॉल मॉडल को अपनाता है तो लाभ अर्जित कर सकता है। जिस हिसाब से चीनी उद्योग को बेहद कम कीमतों का सामना करना पड़ रहा है और वैश्विक तेल संकट घरेलू पेट्रोलियम कीमतों को बढ़ा रहा है, उसमें इथेनॉल उत्पादन इस समस्या को कम कर सकता है। भारत का इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम चीनी कीमतों को स्थिर करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण सिद्ध हो सकता है। साथ ही साथ यह विदेशी कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने में भी मदद कर सकता है। आज सरकार को गंभीरता से तत्काल नीतियों और कार्यक्रमों पर विचार करना चाहिए जो इथेनॉल उत्पादन की क्षमता विकसित करने में समर्थन करें।
भारत में, पहली बार 2001 में इथेनॉल का ईंधन के रूप में उपयोग किया गया था। सरकार ने तीन ईबीपी पायलट प्रोजेक्ट (EBP pilot project) लॉन्च किए, पहला उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद दो अन्य महाराष्ट्र में। देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2003 में 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल के साथ 5 प्रतिशत इथेनॉल के सम्मिश्रण को अनिवार्य किया। बाद में नवंबर 2006 में उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों और (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 5 प्रतिशत सम्मिश्रण को अनिवार्य किया गया।
मेरठ में गन्ने के उत्पादन और उसकी स्थिति के विषय में अधिक जानने के लिए प्रारंग के निचे दिए गये लिंकों पर क्लिक करें
https://meerut.prarang.in/posts/1029/postname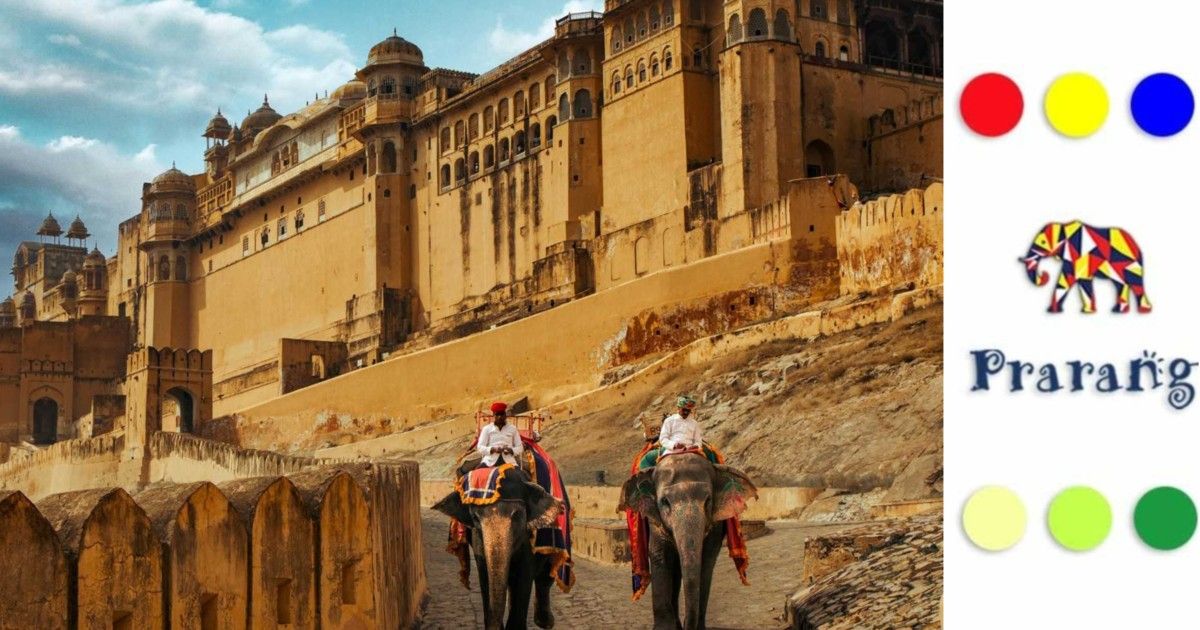
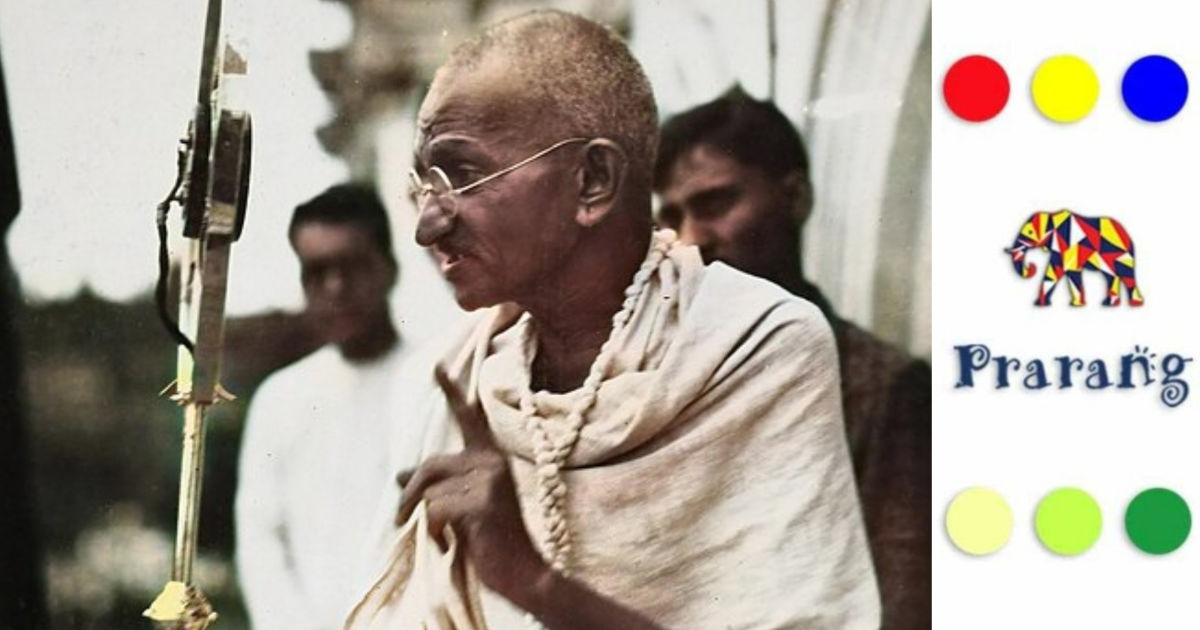



A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.