
समय - सीमा 288
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1058
मानव और उनके आविष्कार 829
भूगोल 262
जीव-जंतु 317

भारत 121 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश है, जो दुनिया की आबादी का 17% से अधिक है। भारत में जनगणना के अनुसार, युवा (15-24 वर्ष) भारत की कुल जनसंख्या का एक बटे पाँचवाँ (19.1%) हिस्सा है। वहीं भारत में 2020 के अंत तक दुनिया की 34.33% युवा आबादी होने की संभावना है। इस तरह के कारक और साक्षरता दर युवाओं के बीच 74% के राष्ट्रीय औसत से 9% अधिक पाई गई है। किसी राष्ट्र के युवा उस राष्ट्र के निर्माता होते हैं, ये हमेशा राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी विकास में मदद करते हैं। युवा, उत्साही, जीवंत, प्रकृति में अभिनव और गतिशील होता है, जो जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण खंड है। युवा का दृढ़ जोश, प्रेरणा और इच्छा शक्ति, उन्हें राष्ट्र के आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे मूल्यवान मानव संसाधन बनाते हैं। किसी देश की वृद्धि की क्षमता उसकी युवा आबादी के आकार से निर्धारित होती है। एक राष्ट्र की रक्षा क्षमता के निर्माण में उनकी भूमिका निर्विवाद रूप से प्रथम श्रेणी में है। किसी देश का विकास उस देश की शिक्षा से होता है, भारत में शिक्षा सार्वजनिक स्कूलों और निजी स्कूलों (तीन स्तरों द्वारा नियंत्रित और वित्तपोषित: केंद्रीय, राज्य और स्थानीय) द्वारा प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान के विभिन्न लेखों के तहत, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। भारत में पब्लिक स्कूलों में निजी स्कूलों का अनुमानित अनुपात 7: 5 है। भारत ने प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति दर बढ़ाने में प्रगति की है। 2011 में, लगभग 75% आबादी, जिनकी आयु 7 से 10 वर्ष के बीच थी, साक्षर थी। भारत की बेहतर शिक्षा प्रणाली को अक्सर इसके आर्थिक विकास के मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। अधिकांश प्रगति, विशेष रूप से उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों को श्रेय दिया गया है।
किसी देश का विकास उस देश की शिक्षा से होता है, भारत में शिक्षा सार्वजनिक स्कूलों और निजी स्कूलों (तीन स्तरों द्वारा नियंत्रित और वित्तपोषित: केंद्रीय, राज्य और स्थानीय) द्वारा प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान के विभिन्न लेखों के तहत, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। भारत में पब्लिक स्कूलों में निजी स्कूलों का अनुमानित अनुपात 7: 5 है। भारत ने प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति दर बढ़ाने में प्रगति की है। 2011 में, लगभग 75% आबादी, जिनकी आयु 7 से 10 वर्ष के बीच थी, साक्षर थी। भारत की बेहतर शिक्षा प्रणाली को अक्सर इसके आर्थिक विकास के मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। अधिकांश प्रगति, विशेष रूप से उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों को श्रेय दिया गया है।  गरीबी और भूख को कम करने और निरंतर, समावेशी और समान आर्थिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने में शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा सुलभता, गुणवत्ता और सामर्थ्य के प्रति बढ़े हुए प्रयास, वैश्विक विकास प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुनिया भर में, 10.6% युवा निरक्षर हैं, जिनमें बुनियादी संख्यात्मक और पढ़ने के कौशल की कमी है और इस तरह की कमी के कारण वे पूर्ण और सभ्य रोजगार के माध्यम से जीवन निर्वाह करने में सक्षम नहीं होते हैं। वहीं दुनिया भर में लगातार उच्च स्तर पर युवा बेरोजगारी और बेरोजगारी के साथ अन्य कई काम कर रहे गरीबों के पास प्राथमिक स्तर की शिक्षा का भी अभाव है, ऐसे युवा बेरोजगारी और बेरोजगारी की दर, सामाजिक समावेश, सामंजस्य और स्थिरता को खतरे में डालते हैं। 2013 में, लगभग 225 मिलियन युवाओं में से 20% निष्क्रिय (न ही शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण) थे। ज्ञान और शिक्षा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में युवाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी के प्रमुख कारक हैं।
गरीबी और भूख को कम करने और निरंतर, समावेशी और समान आर्थिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने में शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा सुलभता, गुणवत्ता और सामर्थ्य के प्रति बढ़े हुए प्रयास, वैश्विक विकास प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुनिया भर में, 10.6% युवा निरक्षर हैं, जिनमें बुनियादी संख्यात्मक और पढ़ने के कौशल की कमी है और इस तरह की कमी के कारण वे पूर्ण और सभ्य रोजगार के माध्यम से जीवन निर्वाह करने में सक्षम नहीं होते हैं। वहीं दुनिया भर में लगातार उच्च स्तर पर युवा बेरोजगारी और बेरोजगारी के साथ अन्य कई काम कर रहे गरीबों के पास प्राथमिक स्तर की शिक्षा का भी अभाव है, ऐसे युवा बेरोजगारी और बेरोजगारी की दर, सामाजिक समावेश, सामंजस्य और स्थिरता को खतरे में डालते हैं। 2013 में, लगभग 225 मिलियन युवाओं में से 20% निष्क्रिय (न ही शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण) थे। ज्ञान और शिक्षा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में युवाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी के प्रमुख कारक हैं।
शिक्षा में निरंतर लिंग अंतर युवा विकास में बाधा डालता है। शिक्षा में लैंगिक असमानता, अन्य संवेदनशील चीजों, लिंग संवेदनशील शैक्षिक बुनियादी ढांचे, सामग्रियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहुंच और उपलब्धता के साथ-साथ माध्यमिक विद्यालय की वृद्ध लड़कियों के बीच उच्च निर्गम पात की दर को दर्शाती है। समाज के वंचित वर्ग के बीच खराब गुणवत्ता की शिक्षा अधिक सामान्य है, जिसमें शिक्षा विशेष रूप से विशेष समूहों के सांस्कृतिक और भाषाई संदर्भों के अनुकूल है। समान रूप से महत्वपूर्ण, खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण युवाओं को रोजगार के अवसरों के साथ-साथ परिणामी कमाई और जीवन की गुणवत्ता में सुधार से वंचित करता है।  अंतत: खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा असमानताओं को मजबूत करती है और अंतर-पीढ़ीगत गरीबी और पार्श्वीकरण को बनाए रखती है। कई शिक्षा प्रशिक्षण प्रणाली युवा लोगों को पलायन और बेरोजगारी के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल प्रदान नहीं करती हैं, तब भी जब वे औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना जारी रखते हैं। गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम इस अंतर को सीखने और कौशल विकास के अवसर प्रदान करके भरना चाहते हैं, जो उस संदर्भ के लिए प्रासंगिक हैं जिसमें युवा लोग अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं। कई शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली गरीबी और बेरोजगारी से बचने के लिए युवाओं को आवश्यक बुनियादी कौशल प्रदान नहीं करते हैं। गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम इस अंतर को भरने और कौशल विकास के अवसर प्रदान करते हैं। गैर-औपचारिक शिक्षा (अक्सर युवाओं और समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से प्रदान की जाती है) विशेष रूप से वंचित और हाशिए वाले समूहों के लिए जीवन-प्रासंगिक ज्ञान और कौशल सीखने की सुविधा प्रदान करती है।
अंतत: खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा असमानताओं को मजबूत करती है और अंतर-पीढ़ीगत गरीबी और पार्श्वीकरण को बनाए रखती है। कई शिक्षा प्रशिक्षण प्रणाली युवा लोगों को पलायन और बेरोजगारी के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल प्रदान नहीं करती हैं, तब भी जब वे औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना जारी रखते हैं। गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम इस अंतर को सीखने और कौशल विकास के अवसर प्रदान करके भरना चाहते हैं, जो उस संदर्भ के लिए प्रासंगिक हैं जिसमें युवा लोग अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं। कई शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली गरीबी और बेरोजगारी से बचने के लिए युवाओं को आवश्यक बुनियादी कौशल प्रदान नहीं करते हैं। गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम इस अंतर को भरने और कौशल विकास के अवसर प्रदान करते हैं। गैर-औपचारिक शिक्षा (अक्सर युवाओं और समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से प्रदान की जाती है) विशेष रूप से वंचित और हाशिए वाले समूहों के लिए जीवन-प्रासंगिक ज्ञान और कौशल सीखने की सुविधा प्रदान करती है।
2012 से 2014 की अवधि के लिए वैश्विक युवा बेरोजगारी दर 13.0% है। कुल मिलाकर, पाँच में से दो (42.6 प्रतिशत) आर्थिक रूप से सक्रिय युवा अभी भी या तो बेरोजगार हैं या गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। 2014 तक, 73.3 मिलियन युवा बेरोजगार थे, जिनका वैश्विक बेरोजगारों का प्रतिशत 36.7 था। हालांकि, कुल बेरोजगारी में युवाओं की हिस्सेदारी धीरे-धीरे कम हो रही है। अपनी आबादी को पर्याप्त और उचित रोजगार प्रदान करने के लिए किसी देश की क्षमता उसकी अर्थव्यवस्था और नीति के वातावरण की ताकत और प्रकृति पर निर्भर करती है। किसी देश में पर्याप्त रोजगार होने से न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, बल्कि इससे उसकी आबादी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है। इसके विपरीत, उच्च बेरोजगारी दर का सामाजिक और राजनीतिक अशांति पर सीधा असर पड़ता है। दुनिया भर में कई राजनीतिक उथल-पुथल को उच्च बेरोजगारी दर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। उच्च बेरोजगारी दर से भुखमरी, प्रवासन, आपराधिक गतिविधि, आत्महत्या की प्रवृत्ति, मानसिक विकार आदि भी हो सकते हैं।
भारत युवा देश है, यहाँ लगभग 65% आबादी युवा पीढ़ी की है। हमारी बढ़ती हुई कार्यशील आबादी की मदद से आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। जैसे-जैसे अन्य बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को तेजी से वृद्ध हो रही आबादी का सामना करना पड़ रहा है, भारत की युवा आबादी दुनिया भर में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा कर सकती है। हालांकि, यदि भारत इस बढ़ती युवा आबादी को रोजगार और कौशल प्रदान करने में विफल होता है तो ये जनसांख्यिकी अवसर किसी काम का नहीं होगा। देश के युवाओं में सूचना की अधिक पहुंच और बढ़ती आकांक्षाओं के साथ, भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले रोजगार की गुणवत्ता मात्रा के रूप में महत्वपूर्ण साबित होगी। वहीं अधिकांश राष्ट्र नीतिगत उपायों और पारंपरिक कार्यक्रमों के माध्यम से बेरोजगारी को कम करने या समाप्त करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में अधिकांश देशों में मुख्यतः सभी क्षेत्रों में युवा रोजगार की नीति को प्राथमिकता दी जाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसे युवा रोजगार के लिए एक वैश्विक रणनीति के विकास में अनुवाद किया जा रहा है और सतत विकास लक्ष्यों के तहत 2030 के विकास के कार्यसूची में शामिल किया गया है।
दूसरी ओर भारत में नई प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से मोबाइल के उद्भव ने सामाजिक परिवर्तन को जन्म दिया है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया की पहुंच और वृद्धि को मात्राबद्ध किया जा सकता है, लेकिन उन रुझानों के साथ सामाजिक मूल्यों और जीवनशैली में बदलाव का वर्णन करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। भारत में प्रौद्योगिकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम संयोजकता रहा है, जिसने सूचना तक अभूतपूर्व पहुंच बनाई है। लाखों लोग जिनके पास राष्ट्रीय प्रवचन में शामिल होने के लिए बहुत कम साधन थे, वे अब अपने आसपास की दुनिया में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को फसल के भावों का पता रहता है।
उत्पाद और सेवा की गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता वैश्विक मानकों को समझता है। ग्रामीण भारतीय अपने लिए उपलब्ध अवसरों और अपने शहरी समकक्षों के लिए उपलब्ध अवसरों के बीच अंतर को पहचानते हैं और नागरिकों के पास अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मंच है। इस संपर्क क्रांति का मूलमंत्र भारतीयों का सशक्तिकरण है। वहीं यदि युवाओं की ऊर्जा और लगन अगर सही तरीके से उपयोग की जाए तो समाज में भारी सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है और राष्ट्र भी प्रगति कर सकता है। युवा अपने समुदायों में रचनात्मक डिजिटल अन्वेषक हैं और सक्रिय नागरिकों के रूप में भाग लेते हैं, जो सतत विकास में सकारात्मक योगदान के लिए उत्सुक हैं। जनसंख्या के इस हिस्से को एक देश के लिए तेजी से प्रगति लाने के लिए दोहन, प्रेरित, कुशल और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
चित्र सन्दर्भ :
मुख्य चित्र में देश की भविष्य भावी पीढ़ी को दिखाया गया है। (Publicdomainpictures)
दूसरे चित्र में एक कार्यालय में व्यस्त युवाओं के झुण्ड का व्यंग्य चित्रण है। (Youtube)
तीसरे चित्र में डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते छात्र और उनकी शिक्षिका को दिखाया गया है। (Picseql)
अंतिम चित्र में युवाओं की भीड़ को दिखाया गया है। (Pexels)
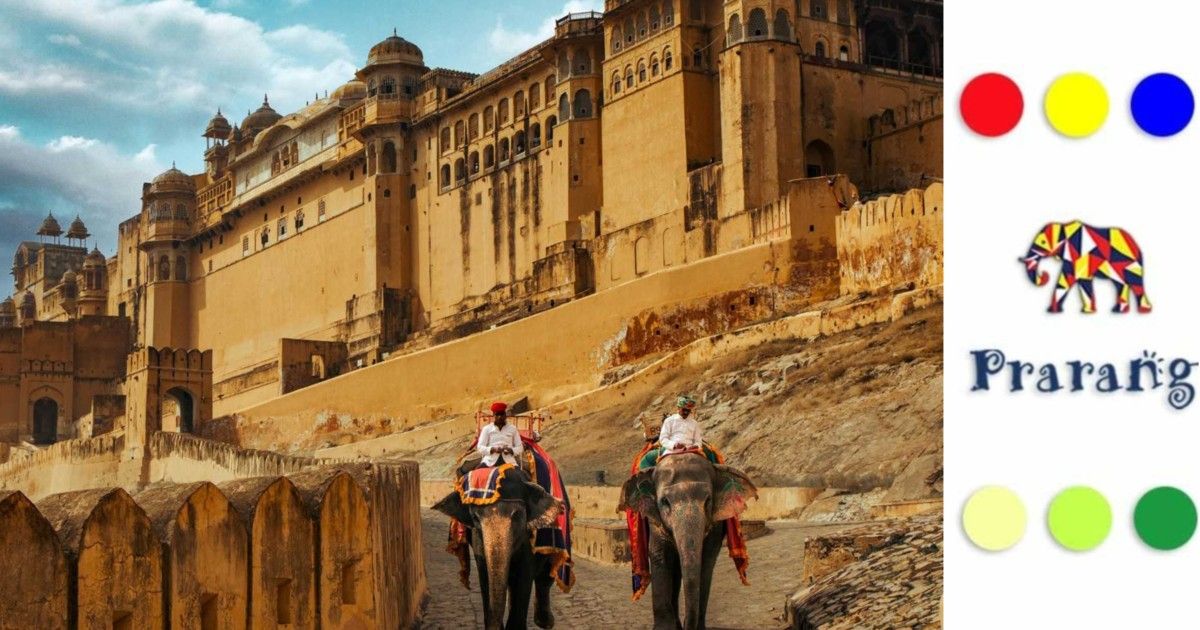
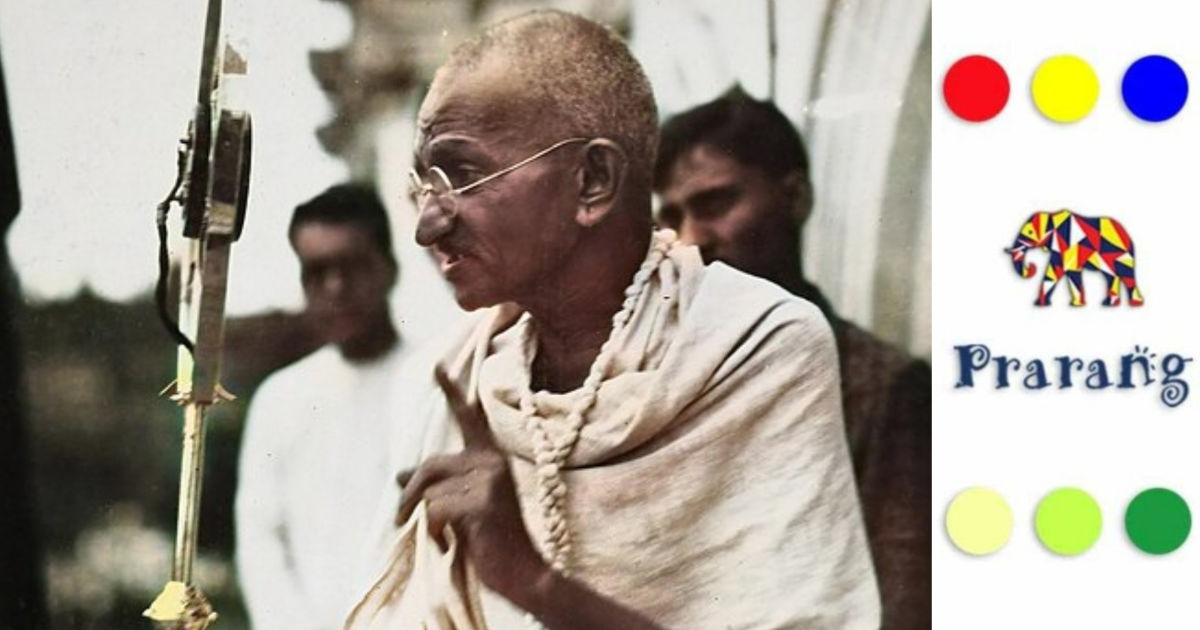



A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.