
समय - सीमा 288
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1058
मानव और उनके आविष्कार 829
भूगोल 262
जीव-जंतु 317
| Post Viewership from Post Date to 28- Nov-2021 (30th Day) | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 1411 | 109 | 0 | 1520 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

संगीत उन कुछ चीजों में से एक है जो विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ता है और संचार के माध्यम के रूप में
आचरण करता है। मनुष्य द्वारा निर्मित और अक्सर परमात्मा के लिए गाया जाता है, इस विश्व में हर कोई
इस स्वर की मधुरता की भाषा को समझता है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो लोगों की भावनाओं को
छूता है और उन्हें संशय, और अवरोधों से मुक्त दुनिया में पहुंचाता है।सदियों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में
लोग अपनी बेटियों की शादी का जश्न मनाने के लिए 'लाडली दो दो चीके डालन' (हमारी लड़की के पास अब दो
घर हैं) गाते रहे हैं। लेकिन आज नई पीढ़ी अपने यंत्र, प्रौद्योगिकी और क्षण भर के मनोरंजन की दुनिया में
व्यस्त होने के कारण ऐसे गाने हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर हैं।
भारत, एक सांस्कृतिक रूप से विविध देश, लोक संगीत की व्यापक विविधता के लिए पहचाना जाता है। यहां के
लोक गीत प्राचीन समय से यहां मौजूद हैं।उनमें से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर बड़े शहरों तक फैले हैं, और
मनोरंजन और धार्मिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के स्रोत के रूप में प्रत्येक भारतीय के जीवन का एक
अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं।भारत में लगभग हर क्षेत्र का अपना लोक संगीत है, जो उनके जीवन के तरीके का
अनुकरण करता है। लोक संगीत खेती और ऐसे अन्य व्यवसायों से निकटता से जुड़ा हुआ है और सांसारिक
जीवन की एकरसता को दूर करने के लिए विकसित हुआ है।  भारतीय लोक संगीत के प्रारंभिक अभिलेख वैदिक साहित्य में 1500 ईसा पूर्व के हैं। कुछ शिक्षाविदों का प्रस्ताव
है कि भारतीय लोक संगीत उतना ही पुराना हो सकता है जितना कि स्वयं राज्य। उदाहरण के लिए, मध्य
भारत के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय लोक संगीत का एक टुकड़ा पांडवानी, महाकाव्य महाभारत जितना पुराना
माना जाता है। यह अविश्वसनीय शीर्षक इस तथ्य से समर्थित है कि पांडवानी का विषय महाभारत के नायकों
में से एक भीम की वीरता से संबंधित है।लोक गीतों का व्यापक रूप से मनोरंजक उद्देश्यों के लिए उपयोग
किया जाता था और जैसे कि शादियों, बच्चे के जन्म, त्योहारों आदि सहित विशेष आयोजनों को मनाने के लिए।
लोक गीतों का उपयोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रमुख जानकारी देने के लिए भी किया जाता था। चूंकि
लोगों के पास प्राचीन जानकारी को संरक्षित करने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं थी, इसलिए महत्वपूर्ण
सूचनाओं को गीतों के रूप में प्रसारित करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था।इसलिए लोक गीतों को स्वदेशी
लोगों द्वारा सराहा गया क्योंकि यह न केवल मनोरंजन प्रदान करता था बल्कि दैनिक जीवन में उपयोग की
जाने वाली अनिवार्य जानकारी भी प्रदान करता था।
अधिकांश लोक गीतों को महान कवियों और लेखकों द्वारा लिखा और रचा गया था जो देश के विभिन्न हिस्सों
और विभिन्न युगों से संबंधित थे। उदाहरण के लिए, बंगाल के रवींद्र संगीत या टैगोर गीत उन गीतों का एक
संग्रह है जो मूल रूप से रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए थे।आदि शंकराचार्य जैसे धार्मिक नेताओं ने अपने
संदेश को पूरे देश में फैलाने के लिए गीतों का इस्तेमाल किया। इसी तरह, अन्य धार्मिक नेताओं द्वारा गाए गए
लोक गीतों ने उन गांवों को विशिष्टता प्रदान की, जहां वे मूल रूप से आए थे और उत्तरोत्तर, इन गीतों को लोगों
ने अपने-अपने क्षेत्रों में अपनी पहचान के रूप में सराहा और प्रसिद्धि दिलाई।यह स्पष्ट है कि लोक संगीत ने
इस प्रकार भारत के कई हिस्सों में सामाजिक-धार्मिक सुधार लाने में मदद की है।
उत्तर प्रदेश लोक संगीत का खजाना है, जिसमें प्रत्येक जिले में अद्वितीय संगीत परंपराएं हैं।इस राज्य को
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 'पुबैया अंग' का गढ़ माना जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार, ‘लोक
संगीत में, पृथ्वी गाती है, पहाड़ गाते हैं, नदियां गाती हैं, फसल गाती हैं’। लोक गीतों ने सामूहिक जीवन और
सामूहिक श्रम को अधिक सुखद बनाया और स्थानीय बोलियों और भाषाओं के माध्यम से समाज में एकीकृत हो
गए। इन्हे आमतौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से संचरित किया जाता था, किंतु कई स्थानीय
बोलियों के विलुप्त होने के साथ लोक संगीत का पूरा वर्ग समाप्त होता जा रहा है, जिससे इस परंपरा में अब
भारी गिरावट को देखा जा सकता है। पारंपरिक लोक संगीत को कई तरीकों से परिभाषित किया गया है: जैसे
संगीत मौखिक रूप से प्रसारित होता है, अज्ञात संगीतकारों के साथ संगीत, या लंबे समय तक प्रचलन द्वारा
प्रस्तुत संगीत। इसकी तुलना व्यावसायिक और शास्त्रीय शैलियों से भी की गई है।स्थानीय बोलियां, लोक गीतों
का मुख्य आधार होती हैं, क्योंकि इनके बोल प्रायः स्थानीय बोली में होते हैं और गाये जाते हैं।
भारतीय लोक संगीत के प्रारंभिक अभिलेख वैदिक साहित्य में 1500 ईसा पूर्व के हैं। कुछ शिक्षाविदों का प्रस्ताव
है कि भारतीय लोक संगीत उतना ही पुराना हो सकता है जितना कि स्वयं राज्य। उदाहरण के लिए, मध्य
भारत के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय लोक संगीत का एक टुकड़ा पांडवानी, महाकाव्य महाभारत जितना पुराना
माना जाता है। यह अविश्वसनीय शीर्षक इस तथ्य से समर्थित है कि पांडवानी का विषय महाभारत के नायकों
में से एक भीम की वीरता से संबंधित है।लोक गीतों का व्यापक रूप से मनोरंजक उद्देश्यों के लिए उपयोग
किया जाता था और जैसे कि शादियों, बच्चे के जन्म, त्योहारों आदि सहित विशेष आयोजनों को मनाने के लिए।
लोक गीतों का उपयोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रमुख जानकारी देने के लिए भी किया जाता था। चूंकि
लोगों के पास प्राचीन जानकारी को संरक्षित करने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं थी, इसलिए महत्वपूर्ण
सूचनाओं को गीतों के रूप में प्रसारित करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था।इसलिए लोक गीतों को स्वदेशी
लोगों द्वारा सराहा गया क्योंकि यह न केवल मनोरंजन प्रदान करता था बल्कि दैनिक जीवन में उपयोग की
जाने वाली अनिवार्य जानकारी भी प्रदान करता था।
अधिकांश लोक गीतों को महान कवियों और लेखकों द्वारा लिखा और रचा गया था जो देश के विभिन्न हिस्सों
और विभिन्न युगों से संबंधित थे। उदाहरण के लिए, बंगाल के रवींद्र संगीत या टैगोर गीत उन गीतों का एक
संग्रह है जो मूल रूप से रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए थे।आदि शंकराचार्य जैसे धार्मिक नेताओं ने अपने
संदेश को पूरे देश में फैलाने के लिए गीतों का इस्तेमाल किया। इसी तरह, अन्य धार्मिक नेताओं द्वारा गाए गए
लोक गीतों ने उन गांवों को विशिष्टता प्रदान की, जहां वे मूल रूप से आए थे और उत्तरोत्तर, इन गीतों को लोगों
ने अपने-अपने क्षेत्रों में अपनी पहचान के रूप में सराहा और प्रसिद्धि दिलाई।यह स्पष्ट है कि लोक संगीत ने
इस प्रकार भारत के कई हिस्सों में सामाजिक-धार्मिक सुधार लाने में मदद की है।
उत्तर प्रदेश लोक संगीत का खजाना है, जिसमें प्रत्येक जिले में अद्वितीय संगीत परंपराएं हैं।इस राज्य को
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 'पुबैया अंग' का गढ़ माना जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार, ‘लोक
संगीत में, पृथ्वी गाती है, पहाड़ गाते हैं, नदियां गाती हैं, फसल गाती हैं’। लोक गीतों ने सामूहिक जीवन और
सामूहिक श्रम को अधिक सुखद बनाया और स्थानीय बोलियों और भाषाओं के माध्यम से समाज में एकीकृत हो
गए। इन्हे आमतौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से संचरित किया जाता था, किंतु कई स्थानीय
बोलियों के विलुप्त होने के साथ लोक संगीत का पूरा वर्ग समाप्त होता जा रहा है, जिससे इस परंपरा में अब
भारी गिरावट को देखा जा सकता है। पारंपरिक लोक संगीत को कई तरीकों से परिभाषित किया गया है: जैसे
संगीत मौखिक रूप से प्रसारित होता है, अज्ञात संगीतकारों के साथ संगीत, या लंबे समय तक प्रचलन द्वारा
प्रस्तुत संगीत। इसकी तुलना व्यावसायिक और शास्त्रीय शैलियों से भी की गई है।स्थानीय बोलियां, लोक गीतों
का मुख्य आधार होती हैं, क्योंकि इनके बोल प्रायः स्थानीय बोली में होते हैं और गाये जाते हैं। क्षेत्र की कई स्थानीय बोलियां जैसे- जाटू, गुर्जरी, अहिरी और ब्रज भाषा मुख्य धारा से बाहर होते नजर आ रहे
हैं, जिसका मतलब है कि इन भाषाओं में लिखे लोक गीतों की परंपरा भी खत्म कर रही है। उदाहरण के लिए
ऐसे बहुत कम कलाकार बचे हैं, जो आल्हाउदल, रागिनी, स्वांग और ढोला जैसी प्रस्तुतियाँ दे सकते हैं। इस तेजी
से लुप्त होती परंपरा को बचाए रखने के लिए, सेंटर फॉर आर्म्ड फोर्सेस हिस्टोरिकल रिसर्च (Centre for Armed
Forces Historical Research) ने एकल कलाकार की आवाज़ में, 33 कहानियों का दस्तावेजीकरण किया है।
इसके साथ, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्ति के
दस्तावेजीकरण का काम कर रहा है।
क्षेत्र की कई स्थानीय बोलियां जैसे- जाटू, गुर्जरी, अहिरी और ब्रज भाषा मुख्य धारा से बाहर होते नजर आ रहे
हैं, जिसका मतलब है कि इन भाषाओं में लिखे लोक गीतों की परंपरा भी खत्म कर रही है। उदाहरण के लिए
ऐसे बहुत कम कलाकार बचे हैं, जो आल्हाउदल, रागिनी, स्वांग और ढोला जैसी प्रस्तुतियाँ दे सकते हैं। इस तेजी
से लुप्त होती परंपरा को बचाए रखने के लिए, सेंटर फॉर आर्म्ड फोर्सेस हिस्टोरिकल रिसर्च (Centre for Armed
Forces Historical Research) ने एकल कलाकार की आवाज़ में, 33 कहानियों का दस्तावेजीकरण किया है।
इसके साथ, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्ति के
दस्तावेजीकरण का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत के अंतर्गत हर मनोदशा और हर अवसर के लिए कोई न कोई गीत है। यहां के लोक
संगीतों की बात करें तो सोहर (Sohar), कहारवा (Kaharwa), चनायनी (Chanayni), नौका झक्कड (Nauka
Jhakkad), बंजारा और नजवा (Banjara and Njava), कजली या कजरी (Kajli or Kajri), जरेवा और सदवाजरा
सारंगा (Jarewa and Sadavajra Saranga) आदि हैं। सोहर एक ऐसा रूप है जो जीवन-चक्र के प्रदर्शनों का
हिस्सा है। इसे एक बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए गाया जाने वाला गीत बताया गया है। कहारवा
विवाह के समय कहार जाति द्वारा गाया जाता है। चनायनी एक प्रकार का नृत्य संगीत है। नौका झक्कड नाई
समुदाय में बहुत लोकप्रिय है और इसे नाई गीत के रूप में जाना जाता है। बंजारा और नजवा रात के समय
तेली समुदाय के लोगों द्वारा गाया जाता है। कजली या कजरी महिलाओं द्वारा सावन के महीने में गाया जाता
है। यह अर्ध-शास्त्रीय गायन के रूप में भी विकसित हुआ और इसकी गायन शैली बनारस घराने से निकटता से
जुड़ी हुई है। संगीत का जरेवा और सदवाजरासरंगा रूप लोक-पत्थरों के लिए गाया जाता है। इन लोक गीतों के
अलावा, ग़ज़ल और ठुमरियाँ अवध क्षेत्र में काफी लोकप्रिय रही हैं तथा कव्वालियाँ और मार्सियस (Marsiyas)
दोनों उत्तर प्रदेश के लोक संगीत के एक मजबूत प्रभाव को दर्शाते हैं। इनके अलावा आल्हाउदल, रागिनी, स्वांग
और ढोला भी लोक संगीत के अन्य रूप हैं। ये सभी लोक गीत विभिन्न अवसरों जैसे विभिन्न मौसमों की
शुरुआत को संदर्भित करने के लिए मौसमी त्योहारों या उत्सवों, धार्मिक और साथ ही विवाह समारोहों का एक
अभिन्न हिस्सा थे।
उत्तर प्रदेश के लोक संगीत के अंतर्गत हर मनोदशा और हर अवसर के लिए कोई न कोई गीत है। यहां के लोक
संगीतों की बात करें तो सोहर (Sohar), कहारवा (Kaharwa), चनायनी (Chanayni), नौका झक्कड (Nauka
Jhakkad), बंजारा और नजवा (Banjara and Njava), कजली या कजरी (Kajli or Kajri), जरेवा और सदवाजरा
सारंगा (Jarewa and Sadavajra Saranga) आदि हैं। सोहर एक ऐसा रूप है जो जीवन-चक्र के प्रदर्शनों का
हिस्सा है। इसे एक बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए गाया जाने वाला गीत बताया गया है। कहारवा
विवाह के समय कहार जाति द्वारा गाया जाता है। चनायनी एक प्रकार का नृत्य संगीत है। नौका झक्कड नाई
समुदाय में बहुत लोकप्रिय है और इसे नाई गीत के रूप में जाना जाता है। बंजारा और नजवा रात के समय
तेली समुदाय के लोगों द्वारा गाया जाता है। कजली या कजरी महिलाओं द्वारा सावन के महीने में गाया जाता
है। यह अर्ध-शास्त्रीय गायन के रूप में भी विकसित हुआ और इसकी गायन शैली बनारस घराने से निकटता से
जुड़ी हुई है। संगीत का जरेवा और सदवाजरासरंगा रूप लोक-पत्थरों के लिए गाया जाता है। इन लोक गीतों के
अलावा, ग़ज़ल और ठुमरियाँ अवध क्षेत्र में काफी लोकप्रिय रही हैं तथा कव्वालियाँ और मार्सियस (Marsiyas)
दोनों उत्तर प्रदेश के लोक संगीत के एक मजबूत प्रभाव को दर्शाते हैं। इनके अलावा आल्हाउदल, रागिनी, स्वांग
और ढोला भी लोक संगीत के अन्य रूप हैं। ये सभी लोक गीत विभिन्न अवसरों जैसे विभिन्न मौसमों की
शुरुआत को संदर्भित करने के लिए मौसमी त्योहारों या उत्सवों, धार्मिक और साथ ही विवाह समारोहों का एक
अभिन्न हिस्सा थे। वहीं इस सांस्कृतिक विरासत के नुकसान को रोकने के लिए, ग्रेटर नोएडा के शिव नादर विश्वविद्यालय में
पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र, प्राकृतिक विज्ञान स्कूल के तीन विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा
गौतमबुद्ध नगर जिले की दादरी तहसील के छितरा ग्राम पंचायत के लोकगीतों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया। वे
लोक गीतों सहित पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, चितारा ग्राम पंचायत के विभिन्न 'मोहल्लों',
जिनकी कुल आबादी 7,656 है और भौगोलिक क्षेत्र 770.78 हेक्टेयर है।
लोक गीतों और लोक भाषाओं को संरक्षित करने के कई तरीकें हो सकते हैं। पहला ये कि हम सुनिश्चित करें
कि दूसरे लोग उन्हें सीखें और गायें। लोक गीतों और लोक भाषाओं को अनुकूलित किया जा सकता है। अधिक
आधुनिक घटनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए लोक गीतों को अपडेट (Update) करने से गीत के भीतर धुनों
और सामान्य संदेश को जीवित रखने में मदद की जा सकती है। सामान्य संगीत संकेतन और आसानी से पढे
जाने वाले विषय इस प्रकार से लिखे या उपलब्ध होने चाहिए, जिनका उपयोग भविष्य की पीढ़ियों द्वारा
आसानी से किया जा सके। परिणामी पुस्तक को यह सुनिश्चित करते हुए प्रकाशित किया जाना चाहिए कि
इसकी कुछ प्रतियां आसपास मौजूद या उपलब्ध हों।लोक गीतों को संरक्षित करने के लिए उन्हें फिर से रिकॉर्ड
(Record) किया जा सकता है और यह कुछ दीर्घकालिक इलेक्ट्रॉनिक (Electronic) प्रारूप में होना चाहिए। यदि
हम इन अद्भुत लोक संगीतों को नियमित रूप से गाते या सुनते हैं, तो हम निश्चित ही इनके संरक्षण में
सक्षम हो पाएंगे।
वहीं इस सांस्कृतिक विरासत के नुकसान को रोकने के लिए, ग्रेटर नोएडा के शिव नादर विश्वविद्यालय में
पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र, प्राकृतिक विज्ञान स्कूल के तीन विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा
गौतमबुद्ध नगर जिले की दादरी तहसील के छितरा ग्राम पंचायत के लोकगीतों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया। वे
लोक गीतों सहित पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, चितारा ग्राम पंचायत के विभिन्न 'मोहल्लों',
जिनकी कुल आबादी 7,656 है और भौगोलिक क्षेत्र 770.78 हेक्टेयर है।
लोक गीतों और लोक भाषाओं को संरक्षित करने के कई तरीकें हो सकते हैं। पहला ये कि हम सुनिश्चित करें
कि दूसरे लोग उन्हें सीखें और गायें। लोक गीतों और लोक भाषाओं को अनुकूलित किया जा सकता है। अधिक
आधुनिक घटनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए लोक गीतों को अपडेट (Update) करने से गीत के भीतर धुनों
और सामान्य संदेश को जीवित रखने में मदद की जा सकती है। सामान्य संगीत संकेतन और आसानी से पढे
जाने वाले विषय इस प्रकार से लिखे या उपलब्ध होने चाहिए, जिनका उपयोग भविष्य की पीढ़ियों द्वारा
आसानी से किया जा सके। परिणामी पुस्तक को यह सुनिश्चित करते हुए प्रकाशित किया जाना चाहिए कि
इसकी कुछ प्रतियां आसपास मौजूद या उपलब्ध हों।लोक गीतों को संरक्षित करने के लिए उन्हें फिर से रिकॉर्ड
(Record) किया जा सकता है और यह कुछ दीर्घकालिक इलेक्ट्रॉनिक (Electronic) प्रारूप में होना चाहिए। यदि
हम इन अद्भुत लोक संगीतों को नियमित रूप से गाते या सुनते हैं, तो हम निश्चित ही इनके संरक्षण में
सक्षम हो पाएंगे।
संदर्भ :-
https://bit.ly/3mltKZJ
https://bit.ly/3BmgKqM
https://bit.ly/3jJg7St
https://bit.ly/3nymFnP
https://bit.ly/3EmWYNR
चित्र संदर्भ
1. पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते बुजुर्ग का एक चित्रण (Videvo)
2. एकतारे से संगीत बजाते स्थानीय गायकों का एक चित्रण (wikimedia)
3. अपने अनुयाइयों के साथ बैठे आदिगुरु शंकराचार्य का एक चित्रण (wikimedia)
4. लोक संगीत गायक घर-घर जाकर अपनी आजीविका चलते हैं जिनको संदर्भित करता एक चित्रण (youtube)
5. ठुमरी गायकी के मुख्य पृष्ठ को संदर्भित करता एक चित्रण (
Exotic India Art)
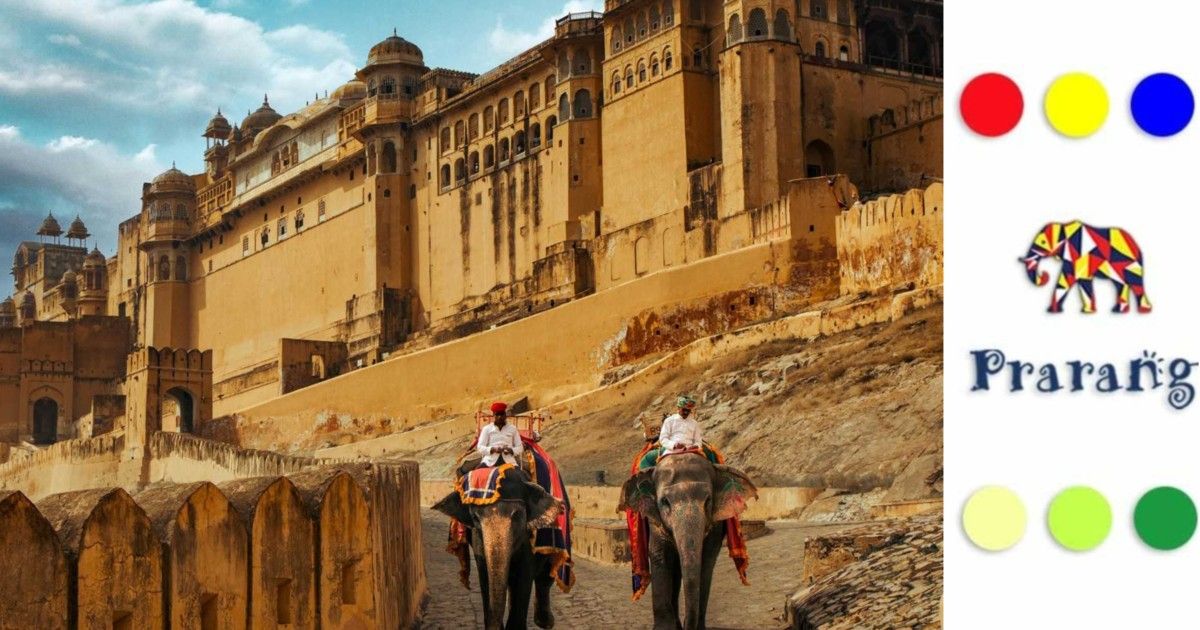
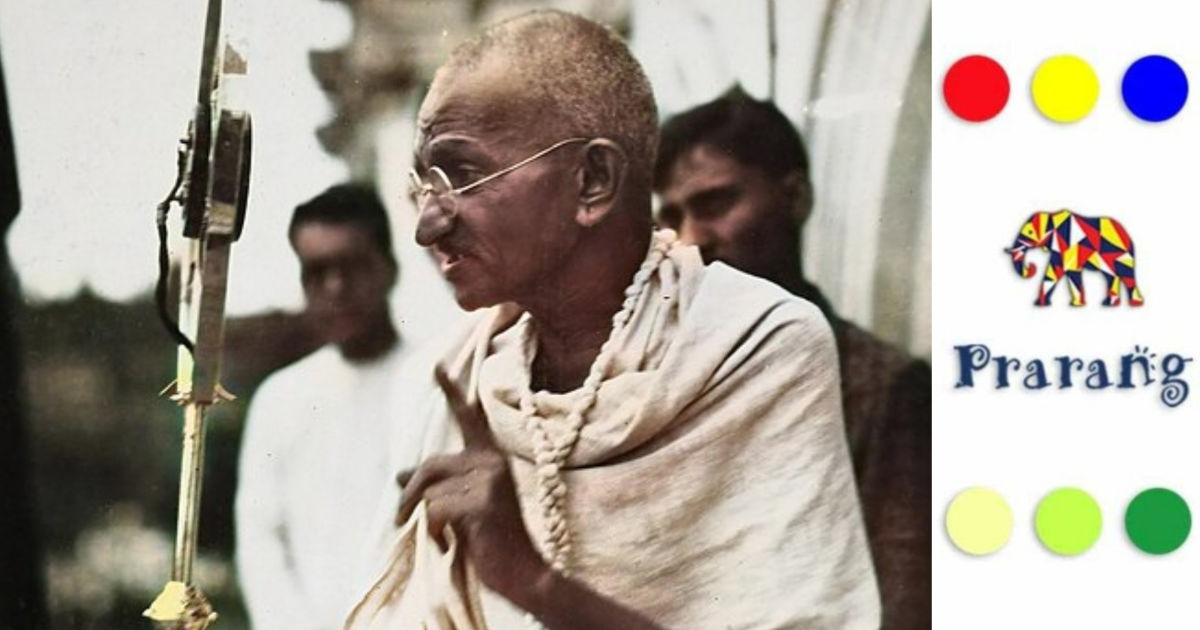



A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.