
समय - सीमा 288
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1058
मानव और उनके आविष्कार 829
भूगोल 262
जीव-जंतु 317
| Post Viewership from Post Date to 03- Apr-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 885 | 111 | 0 | 996 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

आधुनिक समय में पुरूष तथा महिलाओं, मुख्यत: श्रमिक वर्ग में काम करने वाली
महिलाओं, के वेतन के मध्य अंतर को समझने के लिए आवश्यक है कि हम इसके
ऐतिहासिक मूल पर नजर डालें। औपनिवेशिक युग की पितृसत्तात्मक मानसिकता के
परिणामस्वरूप,जिसमें यह धारणा शामिल थी कि महिलाओं का काम पुरुषों की तुलना में
कम कुशल या कम मूल्यवान है, और उनके लिए सार्वजनिक श्रम में सम्मान का अभाव था,
जिसने महिला कारीगरों और औद्योगिक श्रमिकों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाला।
उन्नीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी के शहरी भारत में कारखानों और कार्यशालाओं के
कपड़ा उत्पादन पर हावी होने से पहले, कपड़ा उत्पादन की मुख्य साइटें घर ही हुआ करती
थी। जबकि कामकाजी परिवारों की महिलाओं और बच्चों ने सूत और कपड़े के उत्पादन में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पुरुष आमतौर पर एक बुनकर हुआ करते थे, इन्होंने घरेलु
उत्पादन में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। युवा महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की भूमिका
अक्सर सहायक प्रक्रियाओं में पुरुषों की सहायता के रूप में तैयार की गयी थी, जबकि पुरुष
बच्चों ने शिल्प सीखा और पिता की मदद की। साथ ही, जैसा कि आज भी कई समाजों में
होता है, महिलाओं ने घरेलू श्रम और देखभाल के कामों का बड़ा हिस्सा अपने कंधों पर उठा
रखा था। एक औपनिवेशिक अधिकारी, भाषाविद् और भारतीय संस्कृति के पर्यवेक्षक जॉर्ज ग्रियर्सन
(George Grierson) ने कताई और बुनाई की प्रक्रिया के दौरान लिंग की धुरी पर श्रम
विभाजन को दर्ज किया। 1879 में मधुबनी क्षेत्र के बारे में लिखते हुए, ग्रियर्सन ने उल्लेख
किया कि कपास को खेतों से एकत्र किया जाता है और उसे धूप में सुखाया जाता है, इसे
'बूढ़ी महिलाओं' द्वारा 2 से 3 दिनों तक साफ किया गया।जबकि कताई की प्रक्रिया आमतौर
पर परिवार की महिलाओं द्वारा की जाती थी, बुनाई आमतौर पर पुरुषों द्वारा की जाती थी।
यद्यपि महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं को प्राथमिक के बजाय सहायक के रूप में तैयार
किया गया था - उनका महत्वपूर्ण श्रम अंतिम उत्पाद और इससे मिलने वाली कीमत में
अंतर्निहित था।
उन्नीसवीं सदी के मध्य तक, अंग्रेजी मिलों से निर्मित कपड़ों के आयात से भारतीय वस्त्र
कमजोर हो गए थे। कई बुनकर शहरों में चले गए जहां कारखानों, कपड़ा मिलों, रेलवे, प्रिंटिंग
प्रेस, यांत्रिक प्रतिष्ठानों और शहरी अर्थव्यवस्था ने इन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए।
महिलाएं गांवों और कारीगरों के पूर्व शहरी केंद्रों दोनों में पीछे रह गईं। औपनिवेशिक नीति के
परिणामस्वरूप इस आर्थिक अव्यवस्था ने कमाने वाले पुरूषों की विचारधारा बदल दी।
इतिहासकार समिता सेन का तर्क है कि पुरुष मजदूरी को श्रेष्ठ माना जाने लगा, जबकि
महिलाओं के श्रम का अवमूल्यन किया गया और उनकी कमाई को 'पूरक आय' के रूप में
वर्गीकृत किया गया। महिलाओं के कम वेतन को उचित ठहराने के लिए उन्हें कमजोर, कम
उत्पादक और घरेलू प्रबंधन के 'स्वाभाविक' कर्तव्यों के तर्क दिए गए।
औद्योगिक और औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं में, कारखानों में महिलाओं के कम वेतन वाले
काम ने भी पुरुष श्रमिकों के अधिकार को खतरे में डाल दिया। ब्रिटेन (Britain) में, पुरुष-
प्रधान व्यापारिक इकाईयों ने पुरुष श्रमिकों के हितों और मजदूरी की रक्षा करने की कोशिश
की। औपनिवेशिक बंबई में इसी तरह के संघर्ष हुए, जहां 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक
कपड़ा उद्योग में महिलाओं की श्रम शक्ति का लगभग 20% हिस्सा बन गया था और कभी-
कभी पुरुष श्रमिकों की मजदूरी के लिए खतरा माना जाता था।पुरुषों ने इस खतरे को
संबोधित करने का एक तरीका घरेलूता की पितृसत्तात्मक विचारधारा के माध्यम से किया,
जिसने महिलाओं को घर और मातृत्व से बांध दिया, हालांकि विभिन्न वर्गों और सामाजिक
समूहों के सदस्यों ने इस विचारधारा का अलग-अलग इस्तेमाल किया। राधा कुमार बताते हैं
कि पूंजीपतियों के लिए, कामकाजी महिला की आकृति को उस माँ के रूप में चिह्नित किया
गया था, जिसने स्वस्थ श्रमिकों की नई पीढ़ियों को जन्म दिया।
एक औपनिवेशिक अधिकारी, भाषाविद् और भारतीय संस्कृति के पर्यवेक्षक जॉर्ज ग्रियर्सन
(George Grierson) ने कताई और बुनाई की प्रक्रिया के दौरान लिंग की धुरी पर श्रम
विभाजन को दर्ज किया। 1879 में मधुबनी क्षेत्र के बारे में लिखते हुए, ग्रियर्सन ने उल्लेख
किया कि कपास को खेतों से एकत्र किया जाता है और उसे धूप में सुखाया जाता है, इसे
'बूढ़ी महिलाओं' द्वारा 2 से 3 दिनों तक साफ किया गया।जबकि कताई की प्रक्रिया आमतौर
पर परिवार की महिलाओं द्वारा की जाती थी, बुनाई आमतौर पर पुरुषों द्वारा की जाती थी।
यद्यपि महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं को प्राथमिक के बजाय सहायक के रूप में तैयार
किया गया था - उनका महत्वपूर्ण श्रम अंतिम उत्पाद और इससे मिलने वाली कीमत में
अंतर्निहित था।
उन्नीसवीं सदी के मध्य तक, अंग्रेजी मिलों से निर्मित कपड़ों के आयात से भारतीय वस्त्र
कमजोर हो गए थे। कई बुनकर शहरों में चले गए जहां कारखानों, कपड़ा मिलों, रेलवे, प्रिंटिंग
प्रेस, यांत्रिक प्रतिष्ठानों और शहरी अर्थव्यवस्था ने इन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए।
महिलाएं गांवों और कारीगरों के पूर्व शहरी केंद्रों दोनों में पीछे रह गईं। औपनिवेशिक नीति के
परिणामस्वरूप इस आर्थिक अव्यवस्था ने कमाने वाले पुरूषों की विचारधारा बदल दी।
इतिहासकार समिता सेन का तर्क है कि पुरुष मजदूरी को श्रेष्ठ माना जाने लगा, जबकि
महिलाओं के श्रम का अवमूल्यन किया गया और उनकी कमाई को 'पूरक आय' के रूप में
वर्गीकृत किया गया। महिलाओं के कम वेतन को उचित ठहराने के लिए उन्हें कमजोर, कम
उत्पादक और घरेलू प्रबंधन के 'स्वाभाविक' कर्तव्यों के तर्क दिए गए।
औद्योगिक और औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं में, कारखानों में महिलाओं के कम वेतन वाले
काम ने भी पुरुष श्रमिकों के अधिकार को खतरे में डाल दिया। ब्रिटेन (Britain) में, पुरुष-
प्रधान व्यापारिक इकाईयों ने पुरुष श्रमिकों के हितों और मजदूरी की रक्षा करने की कोशिश
की। औपनिवेशिक बंबई में इसी तरह के संघर्ष हुए, जहां 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक
कपड़ा उद्योग में महिलाओं की श्रम शक्ति का लगभग 20% हिस्सा बन गया था और कभी-
कभी पुरुष श्रमिकों की मजदूरी के लिए खतरा माना जाता था।पुरुषों ने इस खतरे को
संबोधित करने का एक तरीका घरेलूता की पितृसत्तात्मक विचारधारा के माध्यम से किया,
जिसने महिलाओं को घर और मातृत्व से बांध दिया, हालांकि विभिन्न वर्गों और सामाजिक
समूहों के सदस्यों ने इस विचारधारा का अलग-अलग इस्तेमाल किया। राधा कुमार बताते हैं
कि पूंजीपतियों के लिए, कामकाजी महिला की आकृति को उस माँ के रूप में चिह्नित किया
गया था, जिसने स्वस्थ श्रमिकों की नई पीढ़ियों को जन्म दिया। अंततः, यहां तक कि जब घर में काम करने के लिए अत्यधिक समय और कौशल की
आवश्यकता होती थी, तब भी इसे औपनिवेशिक प्रशासकों और क्षेत्रीय पूंजीपतियों द्वारा
पारिवारिक आय के प्राथमिक रूप में नहीं देखा गया था। औपनिवेशिक काल के दौरान,
महिला कारीगरों और मजदूरों को 'अदृश्य' किया गया, उनका यौन शोषण किया गया और
उन्हें औपनिवेशिक पितृसत्तात्मक विचारधाराओं और नीतियों द्वारा पर्याप्त मजदूरी हासिल
करने से रोका गया। यहां तक कि जब कुलीन महिलाओं और पुरुषों ने 19वीं सदी के अंत
और 20वीं सदी की शुरुआत में पितृसत्ता के कुछ पहलुओं पर बहस और चुनौती देना शुरू
किया, तब भी कारीगरों और मेहनतकश महिलाओं के अनुभवों की अनदेखी की गई, उनके
कौशल को कम आंका गया और उनके काम का कम भुगतान किया गया। समान स्थिति21वीं सदी के वर्तमान चरण में भी देखी जा सकती है, जहां महिलाएं आज भी इस
असमानता का सामना कर रहीं हैं। हाल के वर्षों में भारतीय महिला श्रमिकों की एक रिर्पोट
तैयार की गयी। जिसमें हमारा मेरठ शहर भी शामिल था जिसकी रिर्पोट इस प्रकार है:
अंततः, यहां तक कि जब घर में काम करने के लिए अत्यधिक समय और कौशल की
आवश्यकता होती थी, तब भी इसे औपनिवेशिक प्रशासकों और क्षेत्रीय पूंजीपतियों द्वारा
पारिवारिक आय के प्राथमिक रूप में नहीं देखा गया था। औपनिवेशिक काल के दौरान,
महिला कारीगरों और मजदूरों को 'अदृश्य' किया गया, उनका यौन शोषण किया गया और
उन्हें औपनिवेशिक पितृसत्तात्मक विचारधाराओं और नीतियों द्वारा पर्याप्त मजदूरी हासिल
करने से रोका गया। यहां तक कि जब कुलीन महिलाओं और पुरुषों ने 19वीं सदी के अंत
और 20वीं सदी की शुरुआत में पितृसत्ता के कुछ पहलुओं पर बहस और चुनौती देना शुरू
किया, तब भी कारीगरों और मेहनतकश महिलाओं के अनुभवों की अनदेखी की गई, उनके
कौशल को कम आंका गया और उनके काम का कम भुगतान किया गया। समान स्थिति21वीं सदी के वर्तमान चरण में भी देखी जा सकती है, जहां महिलाएं आज भी इस
असमानता का सामना कर रहीं हैं। हाल के वर्षों में भारतीय महिला श्रमिकों की एक रिर्पोट
तैयार की गयी। जिसमें हमारा मेरठ शहर भी शामिल था जिसकी रिर्पोट इस प्रकार है:
.webp) मेरठ एक प्राचीन शहर है जो सिंधु नदी सभ्यता से ही अस्तिव में है। कुछ वर्ष पहले
शोधकर्ताओं ने मेरठ शहर के आसपास के गांवों में 122 श्रमिकों का दस्तावेजीकरण किया।
सभी कार्यकर्ता महिलाएं थीं। मेरठ के आसपास की महिला श्रमिकों को किसी भी अन्य शहर
के औसत आठ घंटे के बराबर वेतन $0.73 ($0.09 प्रति घंटा) मिलता था, जो उत्तर प्रदेश
राज्य के न्यूनतम वेतन से लगभग 85% कम है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत 11.5%
श्रमिक जबरन मजदूरी की स्थिति में मेहनतकश पाए गए, और जिनमें 12.3% बाल मजदूर
थे। हालांकि मेरठ में बाल मजदूरी होती है किंतु यहां के कुछ स्कूलों में उपस्थिति दर उत्तरी
भारत के सभी शहरों से उच्चतम है।. मेरठ में साक्षरता दर (43.4%) उत्तर भारत के किसी
भी शहर की साक्षरता दर से अधिक थी। उच्च साक्षरता दर के कारण उत्तरी भारत में
कामगारों के बीच रिकॉर्ड रखने की दर भी सबसे अधिक (34.4%) रही। किसी भी शहर का
औसत वेतन सबसे कम होने के बावजूद, मेरठ में श्रमिकों के वेतन भुगतान में देरी की दर
सबसे कम थी (7.4%), चाहे वह उत्तरी भारत हो या दक्षिणी भारत।
मेरठ एक प्राचीन शहर है जो सिंधु नदी सभ्यता से ही अस्तिव में है। कुछ वर्ष पहले
शोधकर्ताओं ने मेरठ शहर के आसपास के गांवों में 122 श्रमिकों का दस्तावेजीकरण किया।
सभी कार्यकर्ता महिलाएं थीं। मेरठ के आसपास की महिला श्रमिकों को किसी भी अन्य शहर
के औसत आठ घंटे के बराबर वेतन $0.73 ($0.09 प्रति घंटा) मिलता था, जो उत्तर प्रदेश
राज्य के न्यूनतम वेतन से लगभग 85% कम है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत 11.5%
श्रमिक जबरन मजदूरी की स्थिति में मेहनतकश पाए गए, और जिनमें 12.3% बाल मजदूर
थे। हालांकि मेरठ में बाल मजदूरी होती है किंतु यहां के कुछ स्कूलों में उपस्थिति दर उत्तरी
भारत के सभी शहरों से उच्चतम है।. मेरठ में साक्षरता दर (43.4%) उत्तर भारत के किसी
भी शहर की साक्षरता दर से अधिक थी। उच्च साक्षरता दर के कारण उत्तरी भारत में
कामगारों के बीच रिकॉर्ड रखने की दर भी सबसे अधिक (34.4%) रही। किसी भी शहर का
औसत वेतन सबसे कम होने के बावजूद, मेरठ में श्रमिकों के वेतन भुगतान में देरी की दर
सबसे कम थी (7.4%), चाहे वह उत्तरी भारत हो या दक्षिणी भारत।
संदर्भ:
https://bit.ly/3Hq81XB
https://bit.ly/33WGejV
चित्र संदर्भ
1. कपडा उद्द्योग में महिला कारीगरों को दर्शाता एक चित्रण (cdn4.picryl)
2. भारतीय कताई मिल में प्रसंस्करण से पहले कपास को मैन्युअल रूप से कीटाणुरहित करने की प्रक्रिया को दर्शाता चित्रण (wikimedia)
3. महिला कपड़ा कारीगर को दर्शाता चित्रण (Max Pixel)
4. गारमेंट्स फैक्ट्री को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
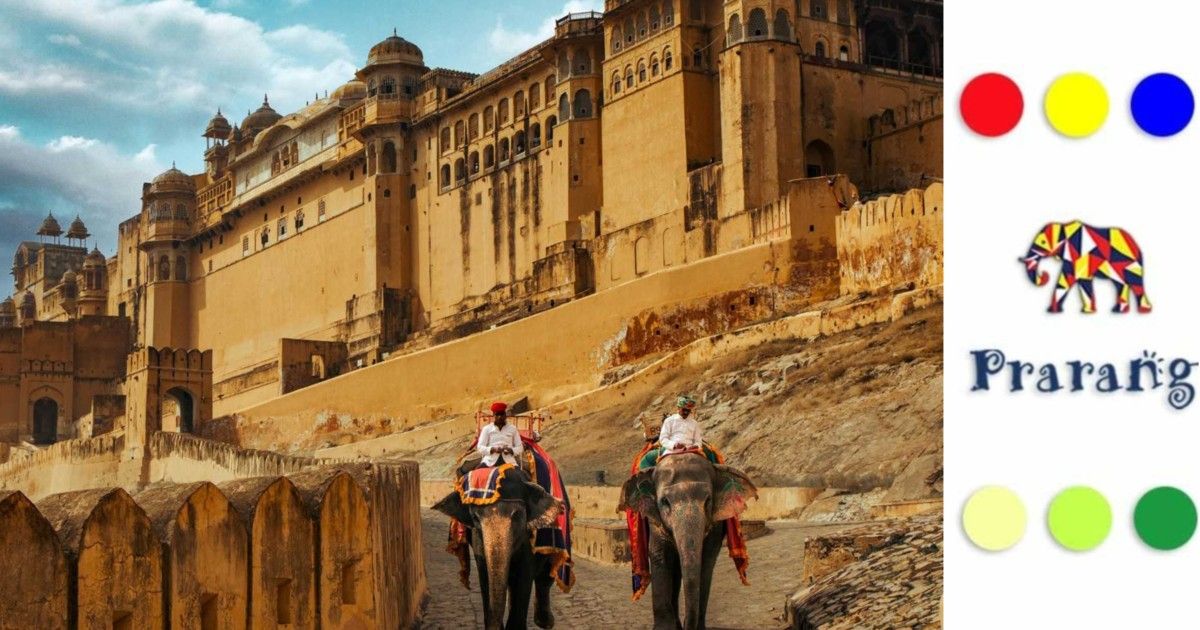
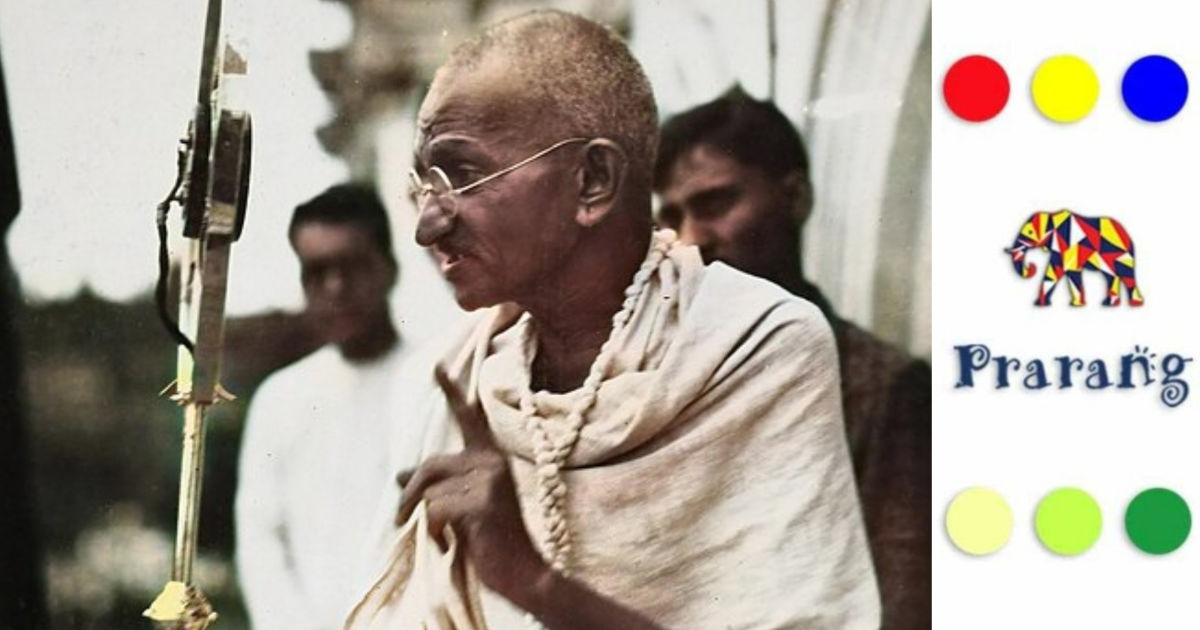



A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.