
समय - सीमा 289
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1064
मानव और उनके आविष्कार 837
भूगोल 267
जीव-जंतु 321
| Post Viewership from Post Date to 26- Jul-2022 (30th Day) | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 2855 | 10 | 0 | 2865 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

1971 की जनगणना के बाद, भारत सरकार ने कहा था कि, देश में 10,000 से कम लोगों द्वारा
बोली जाने वाली किसी भी स्वदेशी भाषा को, अब भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची में
शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से भारत में स्वदेशी आदिवासी समूहों जैसे
वाडारी, कोल्हाटी, गोला, गिसारी आदि की मूल भाषाओं के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया!
दुर्भाग्य से आज हम कई भारतीय आदिवासी और अलिखित भाषाओं को पूरी तरह से खो चुके हैं!
लेकिन बची हुई भाषाओं को बचाने में डिजिटल उपकरण हमारी सहायता जरूर कर सकते हैं! चलिए
जानते हैं कैसे?
पूरी दुनिया में लगभग 7,000 जीवित भाषाएं हैं, लेकिन इनमें से लगभग 3,000 भाषाओँ को
'लुप्तप्राय' माना जाता है। इसका मतलब है कि ग्रह की वर्तमान भाषाई विविधता का लगभग आधा
हिस्सा वलुप्ति की कगार पर खड़ा है। भारत में स्थिति और भी चिंताजनक है! हमारे देश में लगभग 197 भाषाएं संकट के विभिन्न चरणों में हैं, जो दुनिया के किसी भी देश की
तुलना में अधिक है। गुजरात के तेजगढ़ में भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर (Bhasha Research
and Publication Center), वडोदरा तथा आदिवासी अकादमी के संस्थापक-निदेशक गणेश एन
देवी के अनुसार, “संभव है की भारत ने 1961 से 220 भाषाओं को खो दिया हो। भाषाई विशेषज्ञ डेवी
ने 780 जीवित भाषाओं का दस्तावेजीकरण किया और दावा किया कि उनमें से 400 के विलुप्त
होने का खतरा है।
हमारे देश में लगभग 197 भाषाएं संकट के विभिन्न चरणों में हैं, जो दुनिया के किसी भी देश की
तुलना में अधिक है। गुजरात के तेजगढ़ में भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर (Bhasha Research
and Publication Center), वडोदरा तथा आदिवासी अकादमी के संस्थापक-निदेशक गणेश एन
देवी के अनुसार, “संभव है की भारत ने 1961 से 220 भाषाओं को खो दिया हो। भाषाई विशेषज्ञ डेवी
ने 780 जीवित भाषाओं का दस्तावेजीकरण किया और दावा किया कि उनमें से 400 के विलुप्त
होने का खतरा है।
भारत में पांच आदिवासी भाषाएं पूरी तरह से विलुप्त होने की ओर बढ़ रही हैं। भाषाविद् विशेषज्ञों
का कहना है कि, सबसे बड़ा खतरा सिक्किम में मांझी भाषा को है। पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ
इंडिया (People's Linguistic Survey of India) द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार, वर्तमान
में केवल चार लोग हैं जो मांझी बोलते हैं, और वे सभी एक ही परिवार के हैं। इसी तरह, पूर्वी भारत में
महली भाषा, अरुणाचल प्रदेश में कोरो, गुजरात में सिदी और असम में दीमासा भी विलुप्ति का
सामना कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक, यूनेस्को ने असुर, बिरहोर और कोरवा को दुनिया की
लुप्तप्राय भाषाओं की सूची में रखा था, जिसमें बिरहोर को 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' के रूप में
वर्गीकृत किया गया था, जिसके केवल 2,000 वक्ता ही बचे थे। यूनेस्को (UNESCO) के अनुसार, 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली कोई भी भाषा
संभावित रूप से संकटग्रस्त श्रेणी के अंदर आती है। लेकिन भारत में, 1971 की जनगणना के बाद,
सरकार ने फैसला किया कि 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा को
भाषाओं की आधिकारिक सूची में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। 1971 के बाद से,
जनगणना में केवल उन भाषाओं की गिनती की जा रही है, जिसके 10,000 से अधिक वक्ता हैं।
इसके परिणामस्वरूप 1971 की जनगणना में भाषाओं की सूची में 108 भाषाओं की गिरावट आई,
जबकि एक दशक पहले यह 1,652 थी।
यूनेस्को (UNESCO) के अनुसार, 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली कोई भी भाषा
संभावित रूप से संकटग्रस्त श्रेणी के अंदर आती है। लेकिन भारत में, 1971 की जनगणना के बाद,
सरकार ने फैसला किया कि 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा को
भाषाओं की आधिकारिक सूची में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। 1971 के बाद से,
जनगणना में केवल उन भाषाओं की गिनती की जा रही है, जिसके 10,000 से अधिक वक्ता हैं।
इसके परिणामस्वरूप 1971 की जनगणना में भाषाओं की सूची में 108 भाषाओं की गिरावट आई,
जबकि एक दशक पहले यह 1,652 थी।
परिमाण इतना बुरा है की आज भारत में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक लुप्तप्राय भाषाएँ
हैं:
1. भारत 197
2. यूएस 191
3. ब्राजील 190
4. चीन 144
5. इंडोनेशिया 143
6. मेक्सिको 143
7. रूस 131
8. ऑस्ट्रेलिया 108
 भाषा विशेषज्ञ मानते है की “जनजातीय भाषाएं एक क्षेत्र के वनस्पतियों, जीवों और औषधीय पौधों
के बारे में ज्ञान का खजाना हैं। आमतौर पर, यह जानकारी पीढ़ी-दर-पीढ़ी पारित की जाती है।
लेकिन जब किसी भाषा का ह्रास होता है, तो वह ज्ञान प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो जाती है।
भाषा की हानि के साथ संस्कृति में सब कुछ खो जाता है!
आठवीं अनुसूची में शामिल दो प्रमुख जनजातीय भाषाओं, अर्थात् बोडो और संताली में भी गिरावट
देखी गई है। असम में बोडो बोलने वालों की संख्या 2011 में घटकर कुल जनसंख्या का 4.53
प्रतिशत हो गई, जो 2001 में 4.86 प्रतिशत थी।
भाषा विशेषज्ञ मानते है की “जनजातीय भाषाएं एक क्षेत्र के वनस्पतियों, जीवों और औषधीय पौधों
के बारे में ज्ञान का खजाना हैं। आमतौर पर, यह जानकारी पीढ़ी-दर-पीढ़ी पारित की जाती है।
लेकिन जब किसी भाषा का ह्रास होता है, तो वह ज्ञान प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो जाती है।
भाषा की हानि के साथ संस्कृति में सब कुछ खो जाता है!
आठवीं अनुसूची में शामिल दो प्रमुख जनजातीय भाषाओं, अर्थात् बोडो और संताली में भी गिरावट
देखी गई है। असम में बोडो बोलने वालों की संख्या 2011 में घटकर कुल जनसंख्या का 4.53
प्रतिशत हो गई, जो 2001 में 4.86 प्रतिशत थी।
ओडिशा में भारत की सबसे विविध आदिवासी आबादी निवास करती है, जिसमें 62 जनजातियां हैं,
जिनमें 13 विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह भी शामिल हैं। यहां 21 आदिवासी भाषाएँ और
74 बोलियाँ हैं, जो राज्य की भाषाई विविधता में अत्यधिक योगदान देती हैं। इन भाषाओं के
विलुप्त होने के खतरे देखते हुए, ओडिशा सरकार ने आदिवासी बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली
भाषा बाधाओं के मुद्दे को हल करने के लिए 2006 में शुरू किए गए बहुभाषी शिक्षा (एमएलई)
कार्यक्रम के लिए 3,385 आदिवासी भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की थी।
पिछले 60 वर्षों में, अंडमान में बो भाषा और सिक्किम में मांझी भाषा सहित लगभग 250 भाषाएं
देश में गायब हो गईं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब कोई भाषा मर जाती है, तो आसपास की
ज्ञान प्रणाली भी मर जाती है और विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार दुनिया को पीछे मुड़कर देखने का
अनोखा तरीका भी खो जाता है। भाषा खो जाने के साथ, वक्ता विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों में
पलायन करना शुरू कर देते हैं। ऐसा अनुमान है कि यदि कुछ नहीं किया गया, तो आज बोली जाने
वाली 6,000 से अधिक भाषाओं में से आधी, इस सदी के अंत तक लुप्त हो जाएंगी।
पिछले कई वर्षों में, देश ने कई भाषाओं और बोलियों की मृत्यु या अपूरणीय क्षति का सामना किया
है। भाषाओं की हानि हमेशा न केवल किसी देश की विरासत के लिए बल्कि पूरे मानव इतिहास के
लिए एक सांस्कृतिक क्षति होती है।
भाषाओं के लुप्तप्राय होने के कारण:
1. अक्सर, एक भाषा तब गायब हो जाती है जब उसके वक्ता गायब हो जाते हैं या जब वे एक
अधिक शक्तिशाली समूह द्वारा उपयोग की जाने वाली एक बड़ी या दूसरी भाषा बोलने के लिए
स्थानांतरित हो जाते हैं।
2. बाहरी स्रोतों से खतरा: भाषाओं को बाहरी ताकतों जैसे सैन्य, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा
शैक्षिक अधीनता, या आंतरिक ताकतों जैसे किसी समुदाय की अपनी भाषा के प्रति नकारात्मक
दृष्टिकोण से खतरा होता है।
3. बढ़ते प्रवास और तेजी से बढता शहरीकरण अक्सर जीवन के पारंपरिक तरीकों के नुकसान और
एक प्रमुख भाषा बोलने के लिए एक मजबूत दबाव के साथ उभरते हैं।
4. राजनीतिक-आर्थिक और सांस्कृतिक अधीनता: किसी भी समूह द्वारा सामाजिक प्रभुत्व उस
समूह की भाषा को उस समाज में अधिक लोकप्रिय बना देता है। उदाहरण के लिए, संस्कृत बोलने
वालों के सामाजिक वर्चस्व के कारण प्राचीन भारत में संस्कृत लोकप्रिय हो गई। या औपनिवेशिक
शासन के कारण अंग्रेजी लोकप्रिय हो गई है।
5. आर्थिक लाभ: जब कोई भाषा बाज़ार में उपयोगी हो जाती है, तो उस भाषा को अधिक मुद्रा प्राप्त
होती है।
6. भाषा वर्चस्व: अंग्रेजी और अन्य प्रमुख भाषाएं ज्ञान और रोजगार की भाषा के साथ-साथ इंटरनेट
की प्राथमिक भाषा भी बन गई हैं। डिजिटल क्षेत्र की प्रमुख सामग्री अब अंग्रेजी में है, और इसलिए,
अन्य भाषाओं को हाशिए पर डाल दिया गया है।
लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण के लिए योजनाएं एवं उपाय:
1. भारत सरकार ने "भारत की लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण नामक” एक योजना शुरू की है। यह
2013 में शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा स्थापित की गई थी! इस योजना का एकमात्र
उद्देश्य देश की उन भाषाओं का दस्तावेजीकरण और संग्रह करना है जिनके निकट भविष्य में
लुप्तप्राय या संकटग्रस्त होने की संभावना है। इस योजना की निगरानी कर्नाटक के मैसूर में स्थित
केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) द्वारा की जाती है। इस मिशन के लिए CIIL ने भारत भर के
विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ सहयोग किया है। वर्तमान में, प्रलेखन के लिए
117 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। लगभग 500 कम ज्ञात भाषाओं के व्याकरण, शब्दकोश
और जातीय-भाषाई प्रोफाइल के रूप में प्रलेखन आने वाले वर्षों में पूरा होने का अनुमान है।
चूंकि इसमें महत्वपूर्ण कारक
वक्ता समुदाय का अपनी भाषा के प्रति दृष्टिकोण भी है, इसलिए हमें एक सामाजिक और
राजनीतिक वातावरण बनाना आवश्यक है जो बहुभाषावाद और अल्पसंख्यक भाषाओं के सम्मान
को प्रोत्साहित करे ताकि ऐसी भाषा बोलना एक दायित्व के बजाय एक संपत्ति साबित हो जाए।
अतीत में डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट के अभाव में, पाठ के माध्यम से प्रलेखन इतिहास,
संस्कृति, कला और यहां तक कि भाषाओं के संरक्षण का एकमात्र माध्यम था। फिर डिजिटल
उपकरण आए, जिसके साथ इतिहास, संस्कृति, कला और यहां तक कि (लिपियों की)
भाषाओं की तस्वीरें खींची और संरक्षित की जा सकती थीं। और अब हमारे पास दृश्य-श्रव्य प्रारूप हैं,
जो किसी भाषा को दस्तावेज या संरक्षित करने के लिए एक स्क्रिप्ट की आवश्यकता को समाप्त
करते हैं।नेशनल ज्योग्राफिक के एंड्योरिंग वॉयस प्रोजेक्ट (National Geographic's
Enduring Voice Project) के भाषाविदों ने संघर्षरत भाषाओं के दस्तावेज के लिए पहले ही आठ
टॉकिंग डिक्शनरी (Eight Talking Dictionary) तैयार कर ली हैं। आठ लुप्तप्राय भाषाओं में
32,000 शब्द प्रविष्टियों के अलावा, शब्दकोशों में देशी वक्ताओं की 24,000 से अधिक ऑडियो
रिकॉर्डिंग हैं - जिनमें से कई अपनी मूल भाषा में अंतिम धाराप्रवाह व्यक्तियों शब्दों और वाक्यों का
उच्चारण, और सांस्कृतिक वस्तुओं की तस्वीरें में से हैं। इस पहल के तहत पहली परियोजना 2010
में अरुणाचल प्रदेश में एक हजार से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली चीन-तिब्बती भाषा कोरो का
दस्तावेज़ीकरण भी शुरू किया गया था।
यूनेस्को का दावा है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया, तो आज बोली जाने वाली 7,000 से
अधिक भाषाओं में से आधी इस सदी के अंत तक गायब हो जाएंगी। इस प्रकार यह आवश्यक है कि
दस्तावेज़ भाषाओं के लिए ऑडियो-विज़ुअल (audio-visual) का उपयोग करने के लिए और
अधिक प्रयास किए जाएं. क्योंकि यह विशेष माध्यम शोधकर्ताओं और भाषा के प्रति उत्साही लोगों
को एक भाषा को समझने की अनुमति देता है, भले ही वे स्क्रिप्ट नहीं जानते हों। दस्तावेज़ीकरण
(पाठ्य बनाम श्रव्य-दृश्य) के माध्यम में यह अंतर वास्तव में एक भाषा को संरक्षित कर सकता है,
भले ही इसके मूल वक्ताओं/लेखकों के लंबे समय तक चले गए हों।
 जहां कुछ भाषाओं पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, वहीं कई अन्य भाषाएँ फल-फूल भी रही
हैं। उदाहरण के लिए, गोंडी (ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में बोली जाने वाली), भीली (महाराष्ट्र,
राजस्थान, गुजरात), मिजो (मिजोरम), गारो और खासी (मेघालय) और कोकबोरोक (त्रिपुरा) एक
ऊपर की ओर रुझान दिखा रहे हैं, क्योंकि इन समुदायों में शिक्षित लोगों ने लिखने के लिए इन
भाषाओं का प्रयोग शुरू कर दिया है। “वे इन भाषाओं में कविताएँ प्रकाशित करते हैं, नाटक लिखते
हैं और उनका प्रदर्शन भी करते हैं। कुछ भाषाओं में तो फिल्में भी बन रही हैं। उदाहरण के लिए,
उन्होंने गोंडी और भोजपुरी फिल्म उद्योग आज फल-फूल रहा है।
जहां कुछ भाषाओं पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, वहीं कई अन्य भाषाएँ फल-फूल भी रही
हैं। उदाहरण के लिए, गोंडी (ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में बोली जाने वाली), भीली (महाराष्ट्र,
राजस्थान, गुजरात), मिजो (मिजोरम), गारो और खासी (मेघालय) और कोकबोरोक (त्रिपुरा) एक
ऊपर की ओर रुझान दिखा रहे हैं, क्योंकि इन समुदायों में शिक्षित लोगों ने लिखने के लिए इन
भाषाओं का प्रयोग शुरू कर दिया है। “वे इन भाषाओं में कविताएँ प्रकाशित करते हैं, नाटक लिखते
हैं और उनका प्रदर्शन भी करते हैं। कुछ भाषाओं में तो फिल्में भी बन रही हैं। उदाहरण के लिए,
उन्होंने गोंडी और भोजपुरी फिल्म उद्योग आज फल-फूल रहा है।
संदर्भ
https://bit.ly/3zqYw9Y
https://bit.ly/3B6vkpV
https://bit.ly/3cnXeDy
https://bit.ly/2Jy5Q79
चित्र संदर्भ
1. विश्व में संकटग्रस्त भाषाओँ को दर्शाता एक चित्रण (Quora)
2. मानव भाषा परिवारों का वर्तमान वितरण को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. भारत- गुर्जर खानाबदोश जनजाति को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
4. स्कूल की गतिविधियों में भाग लेते छात्रों को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
5. दुनिया भर की भाषाओँ को दर्शाता एक चित्रण (Openclipart)
6. दस्तावेज़ भाषाओं के लिए ऑडियो-विज़ुअल (audio-visual) का उपयोग करने को दर्शाता एक चित्रण (Picryl)



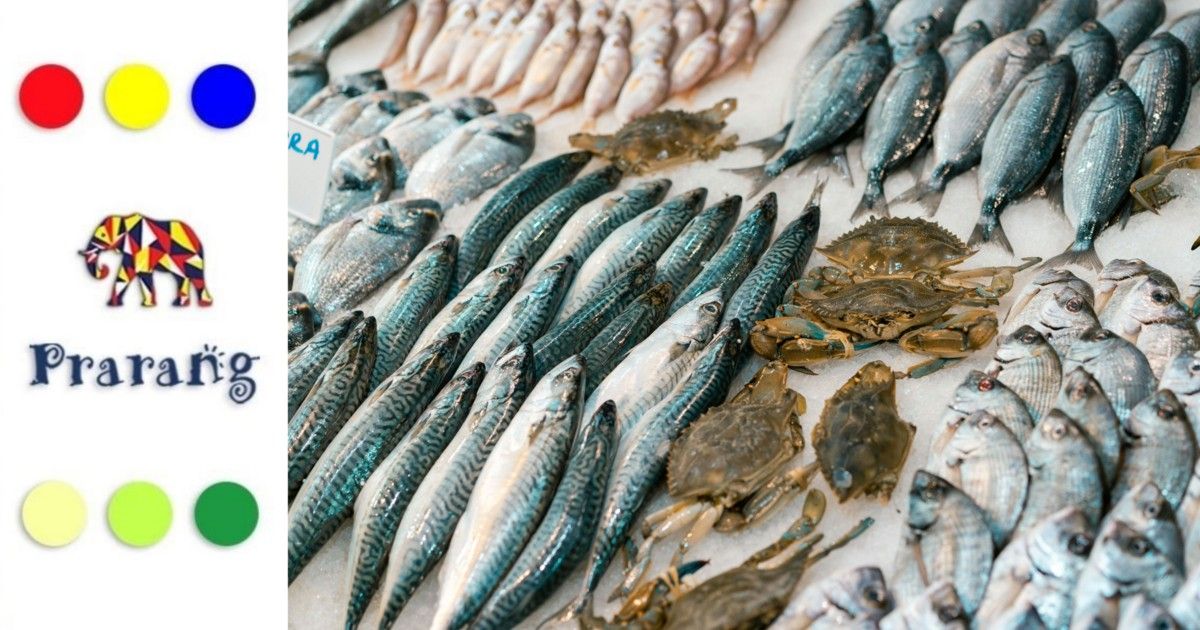
A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.