
समय - सीमा 288
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1058
मानव और उनके आविष्कार 829
भूगोल 262
जीव-जंतु 317
| Post Viewership from Post Date to 28- Jul-2022 (30th Day) | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 2678 | 16 | 0 | 2694 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ्य ग्रह छोड़ने की आवश्यकता को देखते हुए प्रत्येक
वर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस को आयोजित किया जाता है। यह दिन एक स्थिर
और स्वस्थ समाज को बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण
की आवश्यकता पर जोर देता है। विलुप्त होने के खतरे का सामना करने वाले पौधों और जानवरों को
बचाना विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक है।
इसके अलावा, उत्सव प्रकृति के
विभिन्न घटकों जैसे वनस्पतियों, जीवों, ऊर्जा संसाधनों, मिट्टी, पानी और हवा को बरकरार रखने पर
जोर देता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पिछली शताब्दी के दौरान मानवीय गतिविधियों का
प्राकृतिक वनस्पति और अन्य संसाधनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण
की तलाश और लगातार बढ़ती आबादी के लिए जगह बनाने के लिए वनों के आवरण में कटौती ने
जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों को उत्पन्न किया है। पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण
संरक्षण के बारे में जितनी जागरूकता बढ़ी है, इन सकारात्मक कदमों के परिणाम को देखने के लिए
अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। हाल के दिनों में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और
अधिक स्पष्ट हो गई है।संसाधनों के निरंतर मानव अतिदोहन ने असामान्य मौसम स्वरूप, वन्यजीवों
के आवासों का विनाश, प्रजातियों के विलुप्त होने और जैव विविधता के नुकसान को जन्म दिया है।
अफसोस की बात है कि यह विश्व भर में प्रचलित है।इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ
(International Union for Conservation of Nature) जैसे संगठन महत्वपूर्ण हैं।अपने अस्तित्व के पहले
दशक में, संगठन ने यह जांचने पर ध्यान केंद्रित किया कि मानव गतिविधियों ने प्रकृति को कैसे
प्रभावित किया। इसने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के उपयोग को भी बढ़ावा दिया, जिसे व्यापक रूप
से उद्योगों में अपनाया गया है।वहीं 1960 और 1970 के दशक में, प्रकृति के कार्य के संरक्षण के
लिए अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण की ओर निर्देशित थे।
पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण
संरक्षण के बारे में जितनी जागरूकता बढ़ी है, इन सकारात्मक कदमों के परिणाम को देखने के लिए
अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। हाल के दिनों में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और
अधिक स्पष्ट हो गई है।संसाधनों के निरंतर मानव अतिदोहन ने असामान्य मौसम स्वरूप, वन्यजीवों
के आवासों का विनाश, प्रजातियों के विलुप्त होने और जैव विविधता के नुकसान को जन्म दिया है।
अफसोस की बात है कि यह विश्व भर में प्रचलित है।इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ
(International Union for Conservation of Nature) जैसे संगठन महत्वपूर्ण हैं।अपने अस्तित्व के पहले
दशक में, संगठन ने यह जांचने पर ध्यान केंद्रित किया कि मानव गतिविधियों ने प्रकृति को कैसे
प्रभावित किया। इसने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के उपयोग को भी बढ़ावा दिया, जिसे व्यापक रूप
से उद्योगों में अपनाया गया है।वहीं 1960 और 1970 के दशक में, प्रकृति के कार्य के संरक्षण के
लिए अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण की ओर निर्देशित थे।
1964
में, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की
खतरे की प्रजातियों की लाल सूची की स्थापना, जो वर्तमान में प्रजातियों के वैश्विक रूप से विलुप्त
होने के जोखिम पर विश्व भरका सबसे व्यापक विवरण स्रोत है।2000 के दशक में, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति
संरक्षण संघ ने 'प्रकृति आधारित समाधान' पेश किए। ये ऐसे कार्य हैं जो जलवायु परिवर्तन, भोजन
और पानी की सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हुए प्रकृति का
संरक्षण करते हैं।अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध
पर्यावरण संघ है। प्राचीन साहित्य पर्यावरणीय क्षरण के अवांछनीय प्रभावों का पूर्ण ज्ञान प्रकट करता है, चाहे वह
प्राकृतिक कारकों के कारण हो या मानवीय गतिविधियों के कारण। हिंदू दर्शन हमेशा से ही पर्यावरण
के अनुकूल रहा है और वे पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील थे। महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद,
भगवद गीता और पुराण पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण के संदेशों से भरे हुए
हैं।पर्यावरण की सुरक्षा को पृथ्वी माता की सुरक्षा से निकटता से संबंधित समझा जाता था।इसलिए
ऋग्वेद के कई सूक्तों में दिव्य पृथ्वी का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, अर्थात वे स्वर्ग और
पृथ्वी का एक साथ वर्णन करते हैं।ऋग्वेद में मित्र, वरुण, इंद्र, मरुत और आदित्य जैसे देवताओं की
पूजा करता है, जो प्रकृति की सभी वस्तुओं के संचालन में आवश्यक संतुलन बनाए रखने के लिए
जिम्मेदार हैं, चाहे वह पहाड़, झील, स्वर्ग और पृथ्वी, जंगल या जल हो।
प्राचीन साहित्य पर्यावरणीय क्षरण के अवांछनीय प्रभावों का पूर्ण ज्ञान प्रकट करता है, चाहे वह
प्राकृतिक कारकों के कारण हो या मानवीय गतिविधियों के कारण। हिंदू दर्शन हमेशा से ही पर्यावरण
के अनुकूल रहा है और वे पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील थे। महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद,
भगवद गीता और पुराण पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण के संदेशों से भरे हुए
हैं।पर्यावरण की सुरक्षा को पृथ्वी माता की सुरक्षा से निकटता से संबंधित समझा जाता था।इसलिए
ऋग्वेद के कई सूक्तों में दिव्य पृथ्वी का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, अर्थात वे स्वर्ग और
पृथ्वी का एक साथ वर्णन करते हैं।ऋग्वेद में मित्र, वरुण, इंद्र, मरुत और आदित्य जैसे देवताओं की
पूजा करता है, जो प्रकृति की सभी वस्तुओं के संचालन में आवश्यक संतुलन बनाए रखने के लिए
जिम्मेदार हैं, चाहे वह पहाड़, झील, स्वर्ग और पृथ्वी, जंगल या जल हो।
वहीं भविष्यद्रष्टा द्वारा माना गया कि अविवेकपूर्ण मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले
परिवर्तनों के परिणामस्वरूप मौसम, वर्षा स्वरूप, फसलों और वातावरण में असंतुलन हो सकता है
और जल, वायु और पृथ्वी संसाधनों की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है।पांच मूल स्थूल तत्वों या
प्रकृति के पंच महाभूत का आशीर्वाद पाने के लिए कई भजन भी मौजूद हैं: वायु, अग्नि, तेजस, जल,
और पृथ्वी। प्राचीन समय से ही लोग ऐसी गतिविधियों को करने से परहेज करते थे जो प्रकृति के
उपहारों को नुकसान पहुंचा सकती हो।वे मानते थे कि धरती माता की भलाई पर्यावरण के संरक्षण
और पालन-पोषण पर निर्भर करती है। यदि अनजाने में पृथ्वी को नुकसान पहुंचा देने वाला कार्य कर
दिया जाता था तो उनके द्वारा क्षमा के लिए प्रार्थना की जाती थी। साथ ही ऋग्वेद में एक
सुरक्षात्मक परत की उपस्थिति का स्पष्ट संदर्भ भी मौजूद है, जिसे हम अब ओजोन (Ozone) परत
के रूप में जानते हैं, जो सूर्य की हानिकारक किरणों को फ़िल्टर कर पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करती
है। ऋग्वेद के एक भजन में द्रष्टा अश्विनों से प्रार्थना करते हैं कि वे पृथ्वी के तापमान को प्रभावित
करने वाले किसी भी अत्यधिक सौर ज्वाला से सुरक्षा के लिए कृपा बनाए रखें। सभी चार प्रमुख वेद
ऋग्, साम, यजुर और अथर्ववेद, मौसम के चक्रों के रखरखाव के महत्व को पहचानते हैं जो अनुचित
मानव कार्यों के कारण जलवायु परिवर्तन के कारण बदल सकते हैं। ऋग्वेद का एक श्लोक कहता है, "हजारों और सैकड़ों वर्ष यदि आप जीवन के फल और सुख का
आनंद लेना चाहते हैं तो वृक्षों का व्यवस्थित रोपण करें।"हिंदू धर्म मानता है कि मानव शरीर इन
पांच तत्वों से बना है और उनसे संबंधित है, और प्रत्येक तत्व को पांच इंद्रियों में से एक से जोड़ता
है। मनुष्य की नाक का संबंध पृथ्वी से, जीभ का जल से, आंखों का आग से, त्वचा से वायु का और
कान का अंतरिक्ष से संबंध है। हमारी इंद्रियों और तत्वों के बीच की यह कड़ी प्राकृतिक दुनिया के
साथ हमारे मानवीय संबंधों की नींव है। वहीं महाभारत से संकेत प्राप्त होता है कि प्रकृति के मूल
तत्व ब्रह्मांडीय अस्तित्व का गठन करते हैं - पर्वत उनकी हड्डियाँ, पृथ्वी उनका मांस, समुद्र उनका
रक्त, आकाश उनका पेट, वायु उनकी सांस और अग्नि उनकी ऊर्जा। प्राचीन हिंदू शास्त्रों का पूरा जोर
यही है कि मनुष्य अपने आप को प्राकृतिक परिवेश से अलग नहीं कर सकता है और पृथ्वी का
मनुष्य के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि मां का अपने बच्चे के साथ है।
ऋग्वेद का एक श्लोक कहता है, "हजारों और सैकड़ों वर्ष यदि आप जीवन के फल और सुख का
आनंद लेना चाहते हैं तो वृक्षों का व्यवस्थित रोपण करें।"हिंदू धर्म मानता है कि मानव शरीर इन
पांच तत्वों से बना है और उनसे संबंधित है, और प्रत्येक तत्व को पांच इंद्रियों में से एक से जोड़ता
है। मनुष्य की नाक का संबंध पृथ्वी से, जीभ का जल से, आंखों का आग से, त्वचा से वायु का और
कान का अंतरिक्ष से संबंध है। हमारी इंद्रियों और तत्वों के बीच की यह कड़ी प्राकृतिक दुनिया के
साथ हमारे मानवीय संबंधों की नींव है। वहीं महाभारत से संकेत प्राप्त होता है कि प्रकृति के मूल
तत्व ब्रह्मांडीय अस्तित्व का गठन करते हैं - पर्वत उनकी हड्डियाँ, पृथ्वी उनका मांस, समुद्र उनका
रक्त, आकाश उनका पेट, वायु उनकी सांस और अग्नि उनकी ऊर्जा। प्राचीन हिंदू शास्त्रों का पूरा जोर
यही है कि मनुष्य अपने आप को प्राकृतिक परिवेश से अलग नहीं कर सकता है और पृथ्वी का
मनुष्य के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि मां का अपने बच्चे के साथ है।
साथ ही अधिकांश धार्मिक
कार्यों में वृक्षारोपण और संरक्षण को पवित्र बनाया जाता है। हिन्दू धर्म में प्रकृति के तत्वों को
भगवान का दर्जा दिया गया है, जैसे : पृथ्वी को धरती माता या पृथ्वी माँ के रूप में माना जाता है;
आग के देवता को अग्नि के रूप में जाना जाता है; वरुण देव को समुद्र के देवता का दर्जा प्राप्त है;
हवा के देवता को वायु देवता के रूप में जाना जाता है; इन्द्र देव बारिश, बिजली और गरज के देवता
हैं; और जंगलों और उसके भीतर रहने वाले जानवर की देवी को अरण्यानि के नाम से जाना जाता है। हमारे पूर्वज लंबे समय से प्रकृति संतुलन के सबसे मुखर रक्षकों में से रहे हैं। प्राचीन समय से इस
बात पर जोर दिया गया है कि प्रकृति पवित्र है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसकी
देखभाल की जानी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय पारिस्थितिकी और
स्थिरता के बारे में बहुत अधिक जागरूक थे। यह विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में
मदद करता है और उस समय स्थिरता के आधुनिक सिद्धांतों को अपनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से हम उन सुनहरे सिद्धांतों को भूल गए हैं जो आज के समय में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। एक संतुलित, शांतिपूर्ण जीवन के लिए हमें अपने परिवेश में अशांति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। हमें पेड़ लगाने, मिट्टी का संरक्षण, जैविक विविधता की रक्षा करने, और प्राकृतिक ऊर्जा के उत्पादन के नए तरीके खोजने में व्यापक प्रयास करने चाहिए, जिससे हमारी वर्तमान दुनिया में एक संतुलित पर्यावरमय स्थिरता के आधुनिक सिद्धांतों को अपनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से हम उन सुनहरे सिद्धांतों को भूल गए हैं जो आज के समय में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। एक संतुलित, शांतिपूर्ण जीवन के लिए हमें अपने परिवेश में अशांति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। हमें पेड़ लगाने, मिट्टी का संरक्षण, जैविक विविधता की रक्षा करने, और प्राकृतिक ऊर्जा के उत्पादन के नए तरीके खोजने में व्यापक प्रयास करने चाहिए, जिससे हमारी वर्तमान दुनिया में एक संतुलित पर्यावरणीय सद्भाव बनाए रखने में काफी हद तक मदद मिल सकती है।
हमारे पूर्वज लंबे समय से प्रकृति संतुलन के सबसे मुखर रक्षकों में से रहे हैं। प्राचीन समय से इस
बात पर जोर दिया गया है कि प्रकृति पवित्र है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसकी
देखभाल की जानी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय पारिस्थितिकी और
स्थिरता के बारे में बहुत अधिक जागरूक थे। यह विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में
मदद करता है और उस समय स्थिरता के आधुनिक सिद्धांतों को अपनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से हम उन सुनहरे सिद्धांतों को भूल गए हैं जो आज के समय में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। एक संतुलित, शांतिपूर्ण जीवन के लिए हमें अपने परिवेश में अशांति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। हमें पेड़ लगाने, मिट्टी का संरक्षण, जैविक विविधता की रक्षा करने, और प्राकृतिक ऊर्जा के उत्पादन के नए तरीके खोजने में व्यापक प्रयास करने चाहिए, जिससे हमारी वर्तमान दुनिया में एक संतुलित पर्यावरमय स्थिरता के आधुनिक सिद्धांतों को अपनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से हम उन सुनहरे सिद्धांतों को भूल गए हैं जो आज के समय में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। एक संतुलित, शांतिपूर्ण जीवन के लिए हमें अपने परिवेश में अशांति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। हमें पेड़ लगाने, मिट्टी का संरक्षण, जैविक विविधता की रक्षा करने, और प्राकृतिक ऊर्जा के उत्पादन के नए तरीके खोजने में व्यापक प्रयास करने चाहिए, जिससे हमारी वर्तमान दुनिया में एक संतुलित पर्यावरणीय सद्भाव बनाए रखने में काफी हद तक मदद मिल सकती है।
संदर्भ :-
https://bit.ly/3OGeOju
https://bit.ly/3OFofzU
https://bit.ly/3OB4jxX
चित्र संदर्भ
1. हाथ में पर्वत उठाये कृष्ण एवं बौद्ध साधुओं को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
2. जंगल में चर्चा करते लोगों को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
3. बंटेय श्रेई मंदिर की पेडिमेंट नक्काशियों में ऐरावत को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
4. वैदिक ज्योतिषी पाराशर, भृगु, वराहमिहिर और जैमिनी दक्षिणामूर्ति को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
5. वैदिक साहित्य को दर्शाता एक चित्रण (enoughscience)
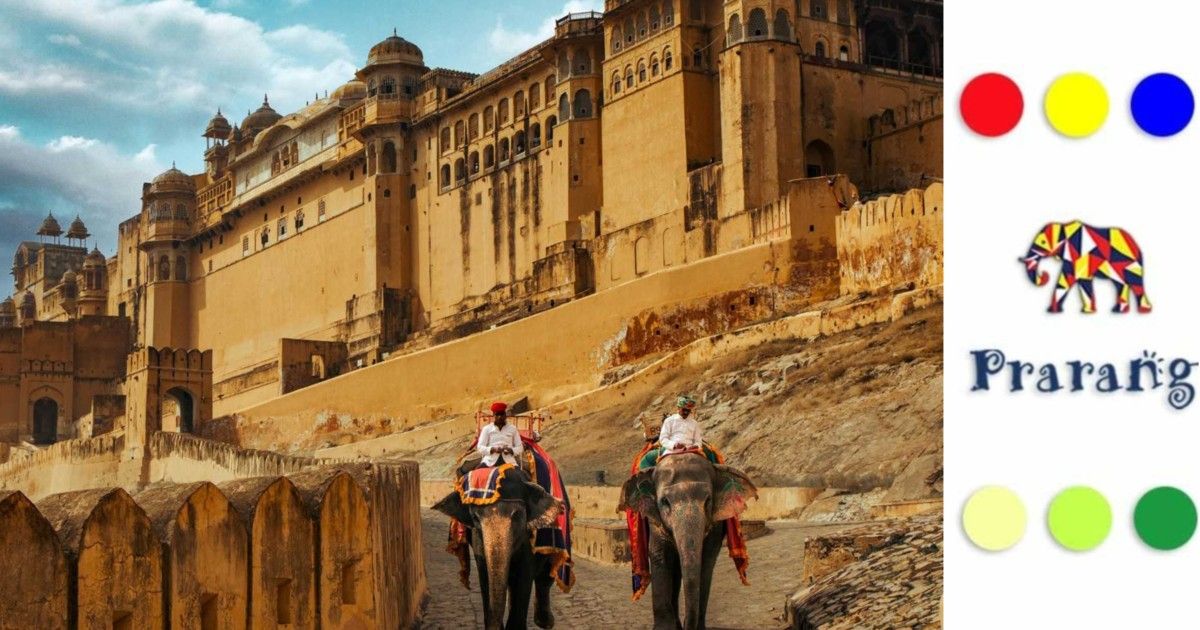
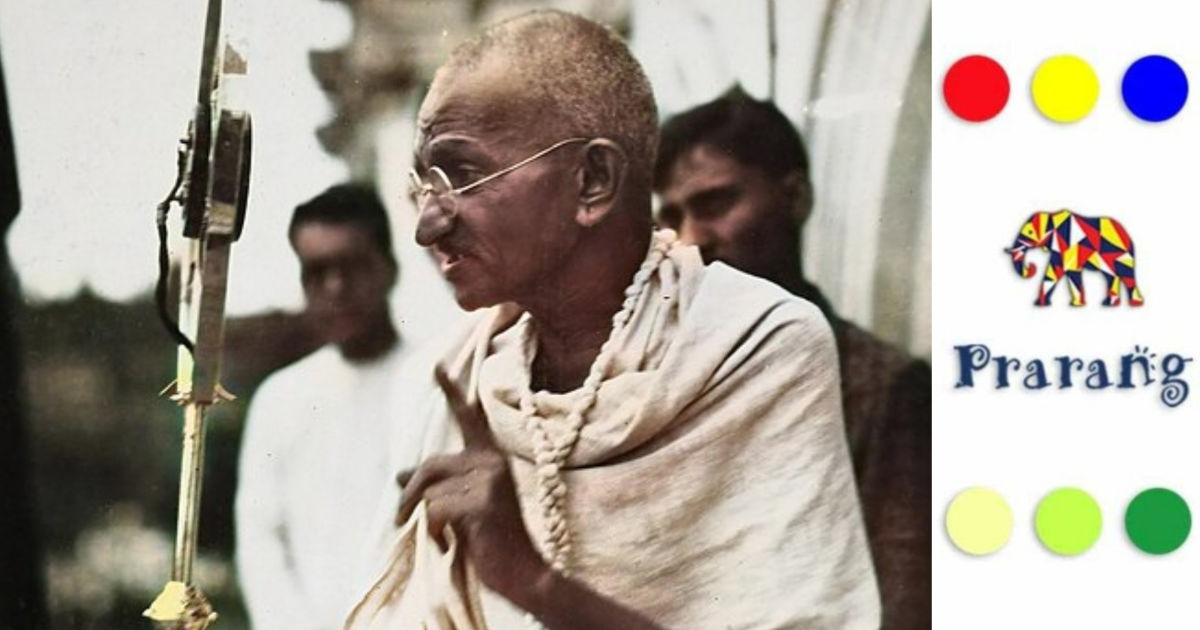



A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.