
समय - सीमा 289
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1064
मानव और उनके आविष्कार 837
भूगोल 267
जीव-जंतु 321
समय - सीमा 289
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1064
मानव और उनके आविष्कार 837
भूगोल 267
जीव-जंतु 321
| Post Viewership from Post Date to 15- Sep-2022 (30th Day) | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 4391 | 50 | 0 | 4441 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

मध्यनूतन काल आदिम वानरों के उद्विकास के लिए विशेष रहा था। इस अवधि में, वानर और पुराने
जगत के बंदरों ने विचलन किया और इन वानरों ने तब एक अनुकूली विकिरण को पार कर लिया।
ऐसे ही शिवपिथेकस (एक प्रकार का वानर, जिसे पहले रामपिथेकस के नाम से जाना जाता था) के
जीवाश्म वानर प्रजाति के अंतिम अवशेष हैं।
ये हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले में, मेरठ से ज्यादा दूर
नहीं, शिवालिक पर्वत की निचली श्रेणियों में भारी मात्रा में पाए गए हैं।शिवालिक पर्वत में
प्रागैतिहासिक काल के बड़े जानवरों के जीवाश्म समृद्ध रूप से मौजूद हैं, इन जीवाश्मों से यह भी
पता चलता है कि इन पहाड़ियों में सभी प्रकार के जानवर रहते थे। विलुप्त एशियाई शुतुरमुर्ग,
ड्रोमाईस सिवलेंसिस (Dromaius sivalensis) और हाइपसेलोर्निस (Hypselornis) सहित शिवालिक
पहाड़ियों से कई जीवाश्म रैटाइट (Ratite) पाए गए।  हालांकि, बाद की दो प्रजातियों का नाम केवल
पैर की उंगलियों की हड्डियों से रखा गया था, जिन्हें बाद में क्रमशः एक अनगिनत स्तनपायी और
एक मगरमच्छ से संबंधित के रूप में पहचाना गया। इसमें प्रागैतिहासिक कशेरुकी जीवाश्मों और
कंकालों का एक संग्रह है जो सुकेती में ऊपरी और मध्य शिवालिक के बलुआ पत्थरों और चीनी
मिट्टी के भूगर्भीय संरचनाओं से प्राप्त हुए हैं। पार्क में प्लियो-प्लीस्टोसिन युग (Plio- Pleistocene
- लगभग 2.5 मिलियन वर्ष) के रहने वाले विलुप्त हो चुके स्तनधारियों के खोजे गए जीवाश्म के छह
आदमकद फाइबरग्लास (Fiberglass) के मॉडल (Model)को खुले मैदान में प्राकृतिक रूप से प्रदर्शित
किया गया है।
शिवपिथेकस प्रागैतिहासिक प्राइमेट (Primate) विकासवादी चक्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं।
यह पतला, पांच फुट लंबा वानर उस समय को चिह्नित करता है जब शुरुआती प्राइमेट पेड़ों के
आरामदायक आश्रय से उतर कर चौड़े खुले घास के मैदानों का समन्वेषण करने लगे थे।
हालांकि, बाद की दो प्रजातियों का नाम केवल
पैर की उंगलियों की हड्डियों से रखा गया था, जिन्हें बाद में क्रमशः एक अनगिनत स्तनपायी और
एक मगरमच्छ से संबंधित के रूप में पहचाना गया। इसमें प्रागैतिहासिक कशेरुकी जीवाश्मों और
कंकालों का एक संग्रह है जो सुकेती में ऊपरी और मध्य शिवालिक के बलुआ पत्थरों और चीनी
मिट्टी के भूगर्भीय संरचनाओं से प्राप्त हुए हैं। पार्क में प्लियो-प्लीस्टोसिन युग (Plio- Pleistocene
- लगभग 2.5 मिलियन वर्ष) के रहने वाले विलुप्त हो चुके स्तनधारियों के खोजे गए जीवाश्म के छह
आदमकद फाइबरग्लास (Fiberglass) के मॉडल (Model)को खुले मैदान में प्राकृतिक रूप से प्रदर्शित
किया गया है।
शिवपिथेकस प्रागैतिहासिक प्राइमेट (Primate) विकासवादी चक्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं।
यह पतला, पांच फुट लंबा वानर उस समय को चिह्नित करता है जब शुरुआती प्राइमेट पेड़ों के
आरामदायक आश्रय से उतर कर चौड़े खुले घास के मैदानों का समन्वेषण करने लगे थे।
विलुप्त हो
चुके मध्यनव शिवपिथेकस के लचीली टखनों के साथ चिंपैंजी जैसे पैर हुआ करते थे,लेकिन अन्यथा
यह एक ऑरंगुटान (Orangutan) जैसा दिखता था।यह भी संभव है कि शिवपिथेकस की ओरंगुटन
जैसी विशेषताएं अभिसरण विकास की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न हुई हों, क्योंकि समान
पारिस्थितिकी प्रणालियों में जानवरों की समान विशेषताओं को विकसित करने की प्रवृत्ति मौजूद होती
है।जीवाश्म विज्ञानियों के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण, शिवपिथेकस के दांतों का आकार था।
शिवपिथेकस की तीन नामित प्रजातियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की समय-सीमा थोड़ी भिन्न है। 19वीं
शताब्दी के अंत में भारत में खोजी गई प्रजाति, एस. इंडिकस (S. indicus), लगभग 12 मिलियन से 10
मिलियन वर्ष पहले जीवित थी;एक दूसरी प्रजाति, एस. सिवलेंसिस (S. sivalensis), जो 1930 के दशक
की शुरुआत में उत्तरी भारत और पाकिस्तान (Pakistan) में खोजी गई थी, लगभग नौ से आठ मिलियन
वर्ष पहले तक जीवित थी; और एक तीसरी प्रजाति, एस. परवाडा (S. parvada), जिसे 1970 के दशक में
भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया था, अन्य दो की तुलना में काफी बड़े थे और आधुनिक ओरंगुटान
के साथ शिवपिथेकस में वंशज समानता को इनसे ही प्राप्त हुई। 
संदर्भ :-
https://bit.ly/3ztGRxg
https://bit.ly/3SoppTh
https://bit.ly/3zUhypu
https://bit.ly/3zw8zth
https://bit.ly/3SrFurI
चित्र संदर्भ
1. शिवालिक फॉसिलपार्क (Shivalik Fossil Park) स्थित हाथियों के मॉडल को दर्शाता चित्रण (youtube)
2. शिवालिक पहाड़ियों के नक़्शे को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. विलुप्त विशालकाय कछुए मेगालोचेली एटलस के मॉडल को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
4. शिवपिथेकस सिवलेन्सिस को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)




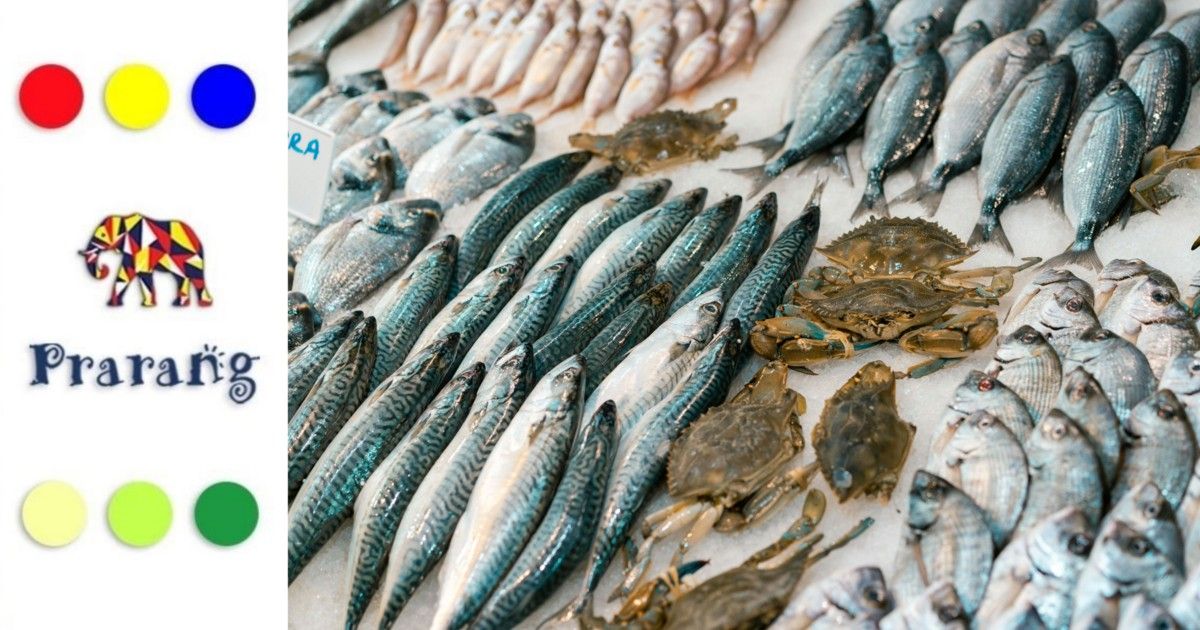
A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.