
समय - सीमा 289
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1064
मानव और उनके आविष्कार 837
भूगोल 267
जीव-जंतु 321
| Post Viewership from Post Date to 04- Feb-2023 (5th Day) | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 1411 | 1036 | 0 | 2447 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

यदि आप यह सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन या प्रदूषण बढ़ने से केवल अंटार्कटिका (Antarctica) की बर्फ टूटेगी या मुंबई के ‘जुहू बीच’ (Juhu Beach) का जलस्तर बढ़ेगा अथवा लोगों की केवल सेहत पर ही बुरा असर पड़ेगा, तो आप यह जानकर बेहद हैरान हो सकते है कि जलवायु परिवर्तन आर्थिक पहलू से भी बेहद महँगी आपदा साबित हो सकता है, जहां यह 2100 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद को लगभग 2.6% तक कम कर सकता है।
पिछले तीन दशकों में, भारत ने आम नागरिकों की आय और जीवन स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि, भारत पहले से ही अत्यधिक गर्मी, भारी वर्षा, भयंकर बाढ़, विनाशकारी तूफान और समुद्र के बढ़ते स्तर के रूप में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का सामना कर रहा है।ये सभी आपदाएं मिलकर देश भर में जीवन, आजीविका और संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही हैं।
अनुमानों के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन के कारण 2100 तक भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद में सालाना 3 से 10 प्रतिशत की कमी देख सकता है, और 2040 तक देश में गरीबी दर 3.5 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।  बढ़ती गर्मी अगले तीन दशकों में श्रम कार्यबल की बाहरी गतिविधियों की क्षमता को काफी कम कर देगी, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि खतरे में पड़ जाएगी। वर्तमान में ही लगभग 75 प्रतिशत श्रम शक्ति (लगभग 380 मिलियन लोग) गर्मी से संबंधित तनावों से जूझ रहे हैं। वहीं आने वाले वर्षों में अनुकूलन और शमन उपायों के अभाव में, भारी गर्मी के बीच खुले में काम करना काफी मुश्किल हो जायेगा। 2030 तक गर्मी और आर्द्रता का बढ़ता स्तर 160 मिलियन से 200 मिलियन भारतीयों तक को भयंकर गर्मी के थपेड़ों का सामना करने पर मजबूर कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप अनाज की कीमतों में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में घटती मजदूरी, और जलवायु परिवर्तन के कारण आर्थिक विकास की धीमी दर के संयोजन से 2040 में भारत की राष्ट्रीय गरीबी दर 3.5% तक बढ़ सकती है।
बढ़ती गर्मी अगले तीन दशकों में श्रम कार्यबल की बाहरी गतिविधियों की क्षमता को काफी कम कर देगी, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि खतरे में पड़ जाएगी। वर्तमान में ही लगभग 75 प्रतिशत श्रम शक्ति (लगभग 380 मिलियन लोग) गर्मी से संबंधित तनावों से जूझ रहे हैं। वहीं आने वाले वर्षों में अनुकूलन और शमन उपायों के अभाव में, भारी गर्मी के बीच खुले में काम करना काफी मुश्किल हो जायेगा। 2030 तक गर्मी और आर्द्रता का बढ़ता स्तर 160 मिलियन से 200 मिलियन भारतीयों तक को भयंकर गर्मी के थपेड़ों का सामना करने पर मजबूर कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप अनाज की कीमतों में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में घटती मजदूरी, और जलवायु परिवर्तन के कारण आर्थिक विकास की धीमी दर के संयोजन से 2040 में भारत की राष्ट्रीय गरीबी दर 3.5% तक बढ़ सकती है।
भारत में जलवायु परिवर्तन का एक और बड़ा दुष्प्रभाव मुंबई में विनाशकारी बाढ़ के रूप में भी देखा जा सकता है। ग्रेटर मुंबई में (Greater Mumbai) 20 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं और यह दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। वाणिज्यिक और व्यापारिक आधार होने के कारण मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन तटीय शहर का अधिकांश हिस्सा समुद्र तल से 15 मीटर से भी कम ऊपर स्थित हैं, जो कि इसे दुनिया के सबसे कमजोर बंदरगाह शहरों में से एक बनाता है एवं जिसके कारण इसे तूफान की वृद्धि, बाढ़, तटीय कटाव और समुद्र के स्तर में वृद्धि सहित जलवायु संबंधी जोखिमों की एक विस्तृत श्रृंखला का सामना करना पड़ सकता है।  मुंबई, जो कि पहले से ही विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहा है, में कांक्रीटीकरण और डामरीकरण में वृद्धि और वृक्षों के आवरण में कमी के कारण पानी जमीन के भीतर नहीं जा पा रहा है। साथ ही खराब सीवेज और जल निकासी व्यवस्था के कारण बाढ़ से स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ जाते हैं, जिनमें मलेरिया, डायरिया और लेप्टोस्पायरोसिस (Leptospirosis) जैसी बीमारियाँ भी शामिल हैं। मुंबई 284 मिलियन डॉलर के वार्षिक नुकसान के साथ बाढ़ जोखिम के संबंध में दुनिया में पांचवें स्थान पर है। अनुमान है कि 2050 में बाढ़ के कारण शहर का वार्षिक नुकसान 6.1 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगा।
मुंबई, जो कि पहले से ही विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहा है, में कांक्रीटीकरण और डामरीकरण में वृद्धि और वृक्षों के आवरण में कमी के कारण पानी जमीन के भीतर नहीं जा पा रहा है। साथ ही खराब सीवेज और जल निकासी व्यवस्था के कारण बाढ़ से स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ जाते हैं, जिनमें मलेरिया, डायरिया और लेप्टोस्पायरोसिस (Leptospirosis) जैसी बीमारियाँ भी शामिल हैं। मुंबई 284 मिलियन डॉलर के वार्षिक नुकसान के साथ बाढ़ जोखिम के संबंध में दुनिया में पांचवें स्थान पर है। अनुमान है कि 2050 में बाढ़ के कारण शहर का वार्षिक नुकसान 6.1 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगा।
जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव भौगोलिक रूप से भिन्न होते हैं और इनकी सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। 2018 के एक अध्ययन में पाया गया कि यदि सभी देश पेरिस समझौते (Paris Agreement) में निर्धारित 2 °C तापमान कम करने के लक्ष्य का अनुपालन करने के लिए शमन रणनीतियों को लागू करते हैं, तो 2100 तक पूरी दुनिया को प्रति वर्ष 17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास संभावित आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि, फ़िलहाल 1970 के दशक से ही चरम मौसम की घटनाओं के कारण वैश्विक नुकसान तेजी से बढ़ रहा है। अध्ययन में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन से अकेले कृषि क्षेत्र को 2050 तक 208 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो जायेगा।
2021 में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि कई देशों में युवाओं को जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी नौकरी खोने का डर है, जबकि कई अन्य लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की पहलों का रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा।  यूरोपीय संघ (European Union), ब्रिटेन (Britain), अमेरिका (America) और चीन(China) में अधिकांश व्यक्ति भी जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने का समर्थन करते हैं। हालांकि, आने वाले वर्षों में, कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के दौरान, कार्बन-गहन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को अपनी नौकरी खोने का खतरा बढ़ सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में हुई 1.5 डिग्री की अनुमानित वृद्धि से 80 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों में कमी आएगी।
यूरोपीय संघ (European Union), ब्रिटेन (Britain), अमेरिका (America) और चीन(China) में अधिकांश व्यक्ति भी जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने का समर्थन करते हैं। हालांकि, आने वाले वर्षों में, कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के दौरान, कार्बन-गहन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को अपनी नौकरी खोने का खतरा बढ़ सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में हुई 1.5 डिग्री की अनुमानित वृद्धि से 80 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों में कमी आएगी।
भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। भारत में तीन प्रमुख खाद्य फसलों (चावल, मक्का और गेहूं), बिजली उत्पादन और लोगों के स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन का विशेष प्रभाव पड़ेगा। अध्ययन का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से होने वाली मौतों में वृद्धि हो सकती है, और 2100 तक वैश्विक निष्क्रियता की लागत, भारत की जीडीपी के 1.17% तक पहुंच सकती है।  पिछले 20 वर्षों में, चरम मौसम की घटनाओं के परिणामस्वरूप अनुमानित 500,000 लोग मारे गए हैं और 3.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। 2020 के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि यदि जलवायु परिवर्तन को कम करने की वर्तमान प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया गया, तो जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक आर्थिक नुकसान 2100 तक 127 ट्रिलियन से 616 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकता है। हालांकि, अगर जलवायु परिवर्तन को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखा जाता है तो इन नुकसानों को कम किया जा सकता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं का अनुकूलन करना भी जरूरी हो गया है।
पिछले 20 वर्षों में, चरम मौसम की घटनाओं के परिणामस्वरूप अनुमानित 500,000 लोग मारे गए हैं और 3.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। 2020 के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि यदि जलवायु परिवर्तन को कम करने की वर्तमान प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया गया, तो जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक आर्थिक नुकसान 2100 तक 127 ट्रिलियन से 616 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकता है। हालांकि, अगर जलवायु परिवर्तन को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखा जाता है तो इन नुकसानों को कम किया जा सकता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं का अनुकूलन करना भी जरूरी हो गया है।
संदर्भ
https://bit.ly/2VfrqDs
https://bit.ly/3XQlXTu
https://bit.ly/40c3bbp
चित्र संदर्भ
1. बाढ़ आने पर टूट चुके मकानों को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
2. भूस्खलन क्षेत्र को संदर्भित करता एक चित्रण (USC News)
3. बस को धक्का लगाते लोगों को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
4. बाढ़ के दृश्य को संदर्भित करता एक चित्रण (flickr)
5. मुंबई की बाढ़ को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)




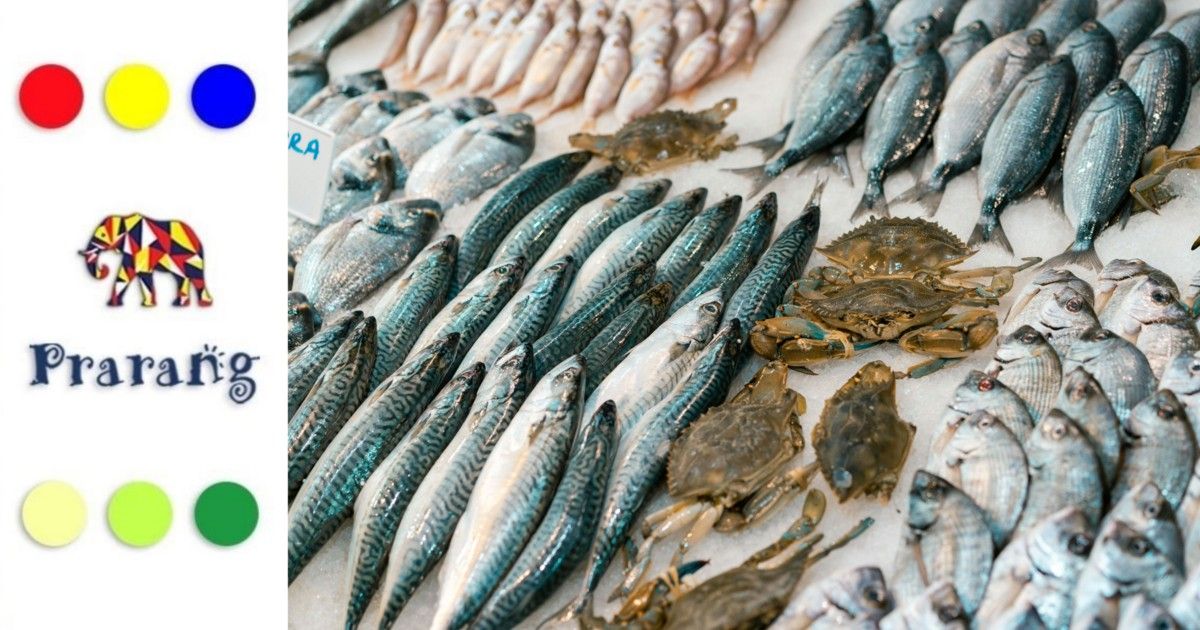
A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.