
समय - सीमा 289
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1064
मानव और उनके आविष्कार 837
भूगोल 267
जीव-जंतु 321
| Post Viewership from Post Date to 04- Jan-2024 (31st Day) | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 3134 | 256 | 0 | 3390 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

सदियों से ही, पूर्वी भारत में, फटी हुई साड़ियों, लूंगी एवं धोती जैसे पुराने कपड़ों से, मुलायम ‘कांथा’ रजाई बनाई जाती आ रही हैं। इसमें कपड़े परतदार और एक साथ सिले हुए होते हैं। कांथा तकनीक से गलीचे भी बनाए जाते थे।
माना जाता है कि, कांथा कढ़ाई एक हजार वर्ष से भी अधिक पुरानी है, जो प्राचीन भारत में पूर्व-वैदिक काल(1500 ईसा पूर्व से पहले) की है।यद्यपि, पारंपरिक रूप से इस कढ़ाई की एक उपयोगितावादी एवं कार्यात्मक शैली थी, लेकिन, यह आज भी जीवंत है।
कांथा, सिलाई की शैली के साथ तैयार कपड़े एवं कढ़ाई तकनीक दोनों को संदर्भित करता है। यह शिल्प, मुख्य रूप से पूर्वी बंगाल (वर्तमान बांग्लादेश) और पश्चिम बंगाल में प्रचलित था।तब सभी उम्र की महिलाएं, उपयोग में आने वाले, मुलायम और जीर्ण कपड़े लेती थीं तथा उन्हें सरल टांके के साथ परतदार बनाती थी। साथ ही, पुरानी साड़ियों की किनारी से लिए गए धागे का उपयोग करके, उन्होंने रजाई, बिस्तर कवर और फर्नीचर कवर, जैसी अन्य उपयोगी वस्तुएं भी बनाईं। टांके की कई पंक्तियों के कारण,कांथा का तैयार वस्त्र आमतौर पर, थोड़ा झुर्रीदार और लहरदार दिखता था। जबकि, मूल कांथा दो तरफा था, जिसमें दोनों तरफ डिजाइन समान दिखाई देता था। समय के साथ, इसकी नक्शी कांथा, वगैरह शैलियां भी उभरी, जिनमें अधिक जटिल कढ़ाई वाले स्वरूप शामिल थे। हालांकि, इस सिलाई के लिए कोई विशिष्ट डिज़ाइन नहीं हैं, मुख्य रूप से, कमल के फूल, पक्षी, मछली, पौधे, फूल और अन्य प्रासंगिक डिज़ाइन नक्शी कांथा में उपयोग किए जाते हैं।नक्शीकांथा धर्म, संस्कृति और उन्हें सिलने वाली महिलाओं के जीवन से प्रभावित रूपांकनों से बना होता है।
टांके की कई पंक्तियों के कारण,कांथा का तैयार वस्त्र आमतौर पर, थोड़ा झुर्रीदार और लहरदार दिखता था। जबकि, मूल कांथा दो तरफा था, जिसमें दोनों तरफ डिजाइन समान दिखाई देता था। समय के साथ, इसकी नक्शी कांथा, वगैरह शैलियां भी उभरी, जिनमें अधिक जटिल कढ़ाई वाले स्वरूप शामिल थे। हालांकि, इस सिलाई के लिए कोई विशिष्ट डिज़ाइन नहीं हैं, मुख्य रूप से, कमल के फूल, पक्षी, मछली, पौधे, फूल और अन्य प्रासंगिक डिज़ाइन नक्शी कांथा में उपयोग किए जाते हैं।नक्शीकांथा धर्म, संस्कृति और उन्हें सिलने वाली महिलाओं के जीवन से प्रभावित रूपांकनों से बना होता है।
दरअसल, कांथा यह नाम,‘कोंथा’ के नाम पर रखा गया है, जो कि, चिथड़ों के लिए एक संस्कृत शब्द है। इसका उल्लेख सबसे पहले बंगाली कवि कृष्णदास कविराज की 500 साल पुरानी पुस्तक,‘चैतन्य चरितामृत’ में किया गया था। पुस्तक में उल्लेखित वृतांत में संत चैतन्य महाप्रभु की मां, कुछ यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के माध्यम से, अपने बेटे को अपने हाथों से सिला हुआ कांथा वस्त्र भेजती हैं। आज, यह कांथा पुरी के गंभीरा मंदिर में प्रदर्शित किया गया है।
‘कन्था’ का अर्थ ‘गला’ भी है, जो भगवान शिव की कहानी को संदर्भित करता है। उन्हें ‘नील कंठ’ यह नाम इसी से मिला है। इस किंवदंती के आधार पर, प्राचीन कांथा रजाई पर अनुष्ठानिक प्रतीक और जानवरों के रुपांकन बनाए गए थे, और इन वस्त्रों को अक्सर ही, बच्चे के जन्म और विवाह के दौरान उपयोग में लाया जाता था।
मूलतः कांथा पुराने कपड़ों को पुनर्चक्रित करने और उन्हें नया जीवन देने के बारे में था। लेकिन, यह शिल्प महिलाओं के लिए अपनी कलात्मक प्रतिभा को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करता था। और आमतौर पर, गांव की हर महिला अपने घर में इसका अभ्यास करती थी। मुख्य रूप से यह कढ़ाई सामग्री की उपलब्धता, दैनिक आवश्यक वस्तु, जलवायु, स्थान और आर्थिक स्थिति जैसे कारकों से प्रभावित थी।जबकि, इस पर बने पैटर्न(Pattern)या डिजाइन अक्सर निर्माता के प्रियजनों के प्रति स्नेह का प्रतीक होते थे। साथ ही, यह भी माना जाता था कि, वे पहनने वाले या उपयोगकर्ता को बुरी नज़र से बचाते हैं।  हिंदू घरों में कांथा अक्सर ही, धार्मिक प्रतीकात्मकता और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को चित्रित करते थे।जबकि, मुस्लिम घरों में इस्लामी और फारसी डिजाइन प्रभाव अधिक थे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में, महिलाएं ज्यामितीय पैटर्न वाले कांथा के, एक विशेष रूप पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिसे ‘पार तोला’ कहा जाता है। यह पारंपरिक इस्लामी कला की तर्ज पर विकसित हुआ है, जिसे कुरान द्वारा हतोत्साहित किया गया है। इस कांथा की खूबसूरती यह है कि, इसका आकार केवल एक सतह पर धागों को फंसाकर बनाया जाता है। इसलिए, कपड़े का उल्टा भाग सीधी, चलने वाली सिलाई का एक साधारण कांथा बना रहता है, जबकि सामने का भाग एक जटिल ज्यामितीय पैटर्न होता है।
हिंदू घरों में कांथा अक्सर ही, धार्मिक प्रतीकात्मकता और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को चित्रित करते थे।जबकि, मुस्लिम घरों में इस्लामी और फारसी डिजाइन प्रभाव अधिक थे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में, महिलाएं ज्यामितीय पैटर्न वाले कांथा के, एक विशेष रूप पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिसे ‘पार तोला’ कहा जाता है। यह पारंपरिक इस्लामी कला की तर्ज पर विकसित हुआ है, जिसे कुरान द्वारा हतोत्साहित किया गया है। इस कांथा की खूबसूरती यह है कि, इसका आकार केवल एक सतह पर धागों को फंसाकर बनाया जाता है। इसलिए, कपड़े का उल्टा भाग सीधी, चलने वाली सिलाई का एक साधारण कांथा बना रहता है, जबकि सामने का भाग एक जटिल ज्यामितीय पैटर्न होता है।
वैसे, कांथा कभी भी एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी, बल्कि यह एक घरेलू शिल्प थी। महिलाएं इसका अभ्यास, अपने घर चलाने तथा पशुधन और बच्चों की देखभाल के बीच करती थीं। प्रारंभिक कांथा कार्य में लाल, काला और नीला रंग प्रचलित थे, हालांकि, अब यह सभी रंगों में उपलब्ध है।
आज, कांथा का अभ्यास बांग्लादेश तथा हमारे देश भारत के पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार राज्यों के कुछ हिस्सों में किया जाता है। अन्य देशों में भी पुराने कपड़ों को सिलाई के साथ, परतदार बनाने की समान संस्कृति है, जैसे की, जापान(Japan) में बोरो(Boro) शैली। कांथा को ‘सुजानी’ के नाम से भी जाना जाता है, जो सिलाई या सुई के लिए एक शब्द है, और मध्य एशिया की सुजानी कढ़ाई(Suzani embroidery) से संबंधित है।
कांथा में जबकि, सरल टांके या रनिंग स्टिच(Running Stitch) का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, इसमें कभी-कभी कंबल सिलाई और चेन स्टिच(Chain Stitch) का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, कांथा कढ़ाई में क्रॉस-सिलाई(cross-stitch), डार्निंग सिलाई(darning stitch), साटन(satin) और लूप टांके(loop stitches) का भी उपयोग किया जाता है। अधिकांश पारंपरिक कांथा वस्त्रों में, केंद्रीय तौर पर सूर्य या कमल की छवि होती थी। लेकिन,कांथा में प्रयुक्त रूपांकनों में बहुत भिन्नता भी है। इसमें लोककथाओं और पौराणिक कथाओं के पात्र, प्रकृति के तत्व और वे चीजें शामिल हैं, जो निर्माताओं ने उनके आसपास देखीं होती थी।
भारतीय प्रेरणाओं के साथ-साथ,कांथा औपनिवेशिक शासन और पुर्तगाली व्यापारियों से भी प्रभावित था। रेशमी धागों वाला कांथा पुर्तगाली संरक्षण में बनाया गया था, जिसमें नौकायन जहाज तथा हथियारों के कोट जैसे रूपांकन थे। नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में 19वीं सदी के एक कांथा में ताश के पत्ते, साहिब और मेमसाहब, झूमर और रानी विक्टोरिया(Queen Victoria) के पदकों के रूपांकन हैं। साथ ही, इसमें हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य भी हैं।
अधिकांश पारंपरिक कांथा वस्त्रों में, केंद्रीय तौर पर सूर्य या कमल की छवि होती थी। लेकिन,कांथा में प्रयुक्त रूपांकनों में बहुत भिन्नता भी है। इसमें लोककथाओं और पौराणिक कथाओं के पात्र, प्रकृति के तत्व और वे चीजें शामिल हैं, जो निर्माताओं ने उनके आसपास देखीं होती थी।
भारतीय प्रेरणाओं के साथ-साथ,कांथा औपनिवेशिक शासन और पुर्तगाली व्यापारियों से भी प्रभावित था। रेशमी धागों वाला कांथा पुर्तगाली संरक्षण में बनाया गया था, जिसमें नौकायन जहाज तथा हथियारों के कोट जैसे रूपांकन थे। नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में 19वीं सदी के एक कांथा में ताश के पत्ते, साहिब और मेमसाहब, झूमर और रानी विक्टोरिया(Queen Victoria) के पदकों के रूपांकन हैं। साथ ही, इसमें हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य भी हैं।
एक ओर, कांथा विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिन्हें उनकी उपयोगिता के आधार पर आसानी से पृथक किया जा सकता है।
अर्शिलता एक संकीर्ण आयताकार आकार का आवरण होता है, जिसका उपयोग दर्पण, कंघी या स्नान सामग्री के लिए किया जाता है। बेटन(Bayton) किताबों और अन्य समान वस्तुओं के लिए, एक चौकोर आकार का कवर होता है, जो पीले, नीले, हरे और लाल जैसे रंगीन धागों का उपयोग करके बनाया जाता है।दुर्जनी, जिसे ‘थालिया’ के नाम से भी जाना जाता है, एक चौकोर आकार का कांथा होता है, जो बटुए को ढकने के लिए बनाया जाता है। इसे एक लिफाफे की तरह एक साथ सिल दिया जाता है, जिसके साथ एक लटकन या डोरी जुड़ी होती है। लेप कांथा एक मोटी रजाई होती है, जिसका उपयोग सर्दियों के दौरान किया जाता है। आमतौर पर, इस कांथा पर ज्यामितीय डिज़ाइन सिले जाते हैं।ओअर एक आयताकार आकार की कांथा रजाई है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से तकिये के कवर के रूप में किया जाता है।जबकि,कांथा का सबसे लोकप्रिय प्रकार–सुजानी, कढ़ाई वाले कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा होता है, जिसका उपयोग समारोहों के दौरान किया जाता है।
कांथा कढ़ाई 19वीं सदी की शुरुआत में, लगभग लुप्त हो गई थी। लेकिन, रवींद्रनाथ टैगोर की बहू ने, विनम्रतापूर्वक इसे फिर से जीवंत कर दिया। जिन महिलाओं ने कांथा कढ़ाई का उपयोग करके वस्त्रों की सिलाई की थी, उन्होंने प्राप्तकर्ता या परिवार के सदस्य के अनुरोध के अनुसार अपने डिजाइनों को अनुकूलित किया था। जबकि, परंपरा को जीवित रखते हुए, यह कढ़ाई तकनीक एक स्त्री से दूसरी स्त्री को हस्तांतरित की गई है।
साथ ही, वर्ष 1947 में भारत के विभाजन और भारत तथा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान(अब बांग्लादेश) के बीच आगामी संघर्ष के दौरान, कांथा का पुनरुद्धार फिर से बाधित हो गया था। अंततः, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध (1971) के बाद से, कांथा का एक अत्यधिक मूल्यवान और बहुप्रतीक्षित कला-शिल्प के रूप में, पुनर्जन्म हुआ है। आज भी, यदि आप बंगाल में यात्रा करते हैं, तो आपको अभी भी पारंपरिक कांथा रजाई की आधुनिक पुनरावृत्तियां मिलेंगी। लेकिन, देशज स्तर पर और निर्यात बाजार के लिए, अब अधिकांश कांथावस्त्र व्यावसायिक खपत के लिए बनाएं जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से, यह एक अच्छी बात है। क्योंकि, बंगाल की ग्रामीण महिलाएं, जो आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कारकों के कारण अपने घरों के बाहर लाभकारी रोजगार खोजने से सीमित थीं, अब इस बाजार के लिए पर्याप्त कांथा का उत्पादन करने के लिए खुद को उच्च मांग में पाती हैं।
आज भी, यदि आप बंगाल में यात्रा करते हैं, तो आपको अभी भी पारंपरिक कांथा रजाई की आधुनिक पुनरावृत्तियां मिलेंगी। लेकिन, देशज स्तर पर और निर्यात बाजार के लिए, अब अधिकांश कांथावस्त्र व्यावसायिक खपत के लिए बनाएं जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से, यह एक अच्छी बात है। क्योंकि, बंगाल की ग्रामीण महिलाएं, जो आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कारकों के कारण अपने घरों के बाहर लाभकारी रोजगार खोजने से सीमित थीं, अब इस बाजार के लिए पर्याप्त कांथा का उत्पादन करने के लिए खुद को उच्च मांग में पाती हैं।
संदर्भ
https://tinyurl.com/yc58ze92
https://tinyurl.com/bdfb4nnj
https://tinyurl.com/58k4n9kw
चित्र संदर्भ
1. ‘कांथा’ कढ़ाई करती महिला को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
2. नक्शी कांथा को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. 18वीं-19वीं शताब्दी के कांथा वस्त्र को दर्शाता एक चित्रण (GetArchive)
4. बारीक ‘कांथा’ कढ़ाई को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
5. चादर में की गई कांथा कड़ाई को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)



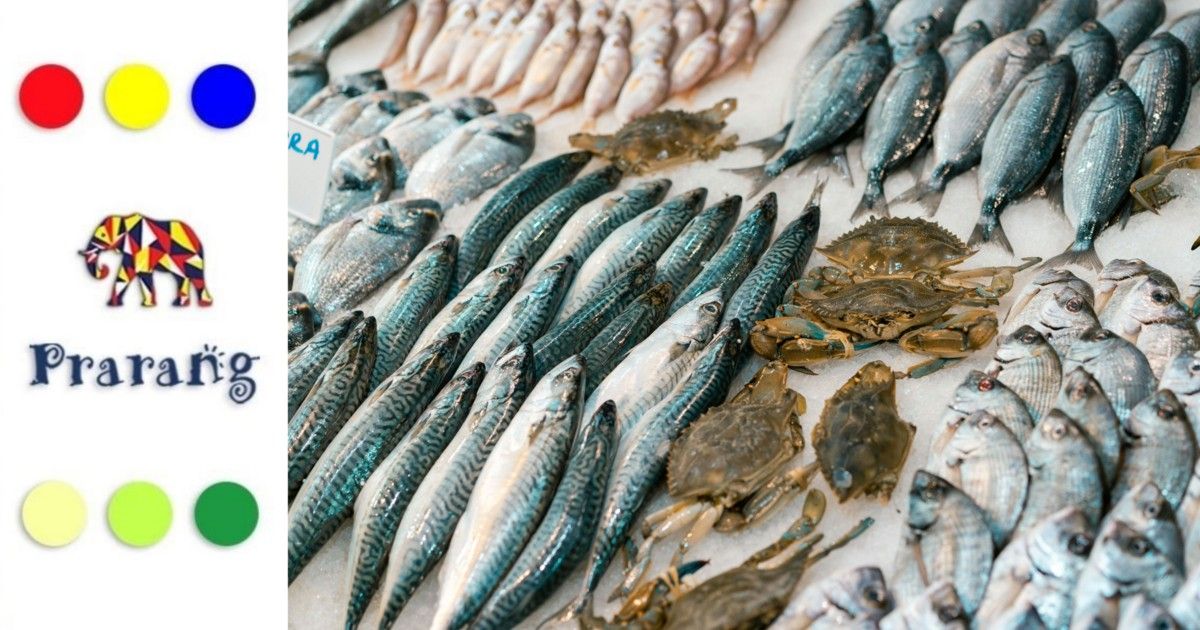
A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.