
समय - सीमा 289
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1064
मानव और उनके आविष्कार 837
भूगोल 267
जीव-जंतु 321
| Post Viewership from Post Date to 11- Feb-2024 (31st Day) | ||||
|---|---|---|---|---|
| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |
| 1771 | 241 | 0 | 2012 | |
| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

भारत में पुलिस के काम को संचालित या नियंत्रित करने वाला कानूनी और संस्थागत ढांचा हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है। वर्तमान भारत में पुलिस, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की राज्य सूची के अंतर्गत आती है।
भारतीय संविधान द्वारा पुलिस के निम्नलिखित कर्तव्य सुनिश्चित किये गए हैं:
- प्राथमिक कर्तव्य:
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना।
- आपराधिक जांच करना।
- द्वितीयक कर्तव्य:
- वीवीआईपी (VVIP) गतिविधि में पुलिस बल का शामिल होना।  हालांकि संविधान द्वारा पुलिस के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से प्राथमिक और द्वितीयक कर्तव्यों के रूप में विभाजित किया गया है। लेकिन वर्तमान में पुलिस की छवि इसके बिल्कुल विपरीत मानी जाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि पुलिस और राजनीतिक संबंधों और हस्तक्षेप के कारण पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य गौण (secondary) हो जाता है। इसके साथ ही भारतीय पुलिस का जनता के साथ रवैया भी मित्रवत होने के स्थान पर भयपूर्ण समझा जाता है। पुलिस की इसी छवि को सुधारने के लिए कई बार पुलिस सुधार समितियां एवं आयोग गठित किए गए हैं।
हालांकि संविधान द्वारा पुलिस के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से प्राथमिक और द्वितीयक कर्तव्यों के रूप में विभाजित किया गया है। लेकिन वर्तमान में पुलिस की छवि इसके बिल्कुल विपरीत मानी जाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि पुलिस और राजनीतिक संबंधों और हस्तक्षेप के कारण पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य गौण (secondary) हो जाता है। इसके साथ ही भारतीय पुलिस का जनता के साथ रवैया भी मित्रवत होने के स्थान पर भयपूर्ण समझा जाता है। पुलिस की इसी छवि को सुधारने के लिए कई बार पुलिस सुधार समितियां एवं आयोग गठित किए गए हैं।
पुलिस सुधारों का उद्देश्य पुलिस संगठनों के मूल्यों, संस्कृति, नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन लाना है ताकि पुलिस लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और कानून के शासन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। इसका उद्देश्य अन्य विभागों जैसे कि सुरक्षा क्षेत्र, अदालतें और सुधार विभाग, या प्रबंधन या निरीक्षण जिम्मेदारियों वाले कार्यकारी, संसदीय या स्वतंत्र प्राधिकरण के साथ पुलिस के समन्वय को सुनिश्चित करना भी है।
क्या आप जानते हैं कि भारत में पुलिस सुधार की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में ही हो चुकी थी? 1861 का ‘भारतीय पुलिस अधिनियम’ ब्रिटिश भारत के तहत पुलिस सुधार की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण विकास था। इस अधिनियम का उद्देश्य एक पेशेवर पुलिस बल की स्थापना करना था क्योंकि इससे पूर्व भारत में एक संगठित संस्था के रूप में पुलिस बल मौजूद नहीं था।
इस अधिनियम द्वारा पुलिस बल के संगठन और संरचना के लिए दिशानिर्देश प्रदान किये गए। साथ ही इसके द्वारा पुलिस अधिकारियों की शक्तियों और जिम्मेदारियों के साथ साथ अधिनियम में भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रिया को भी परिभाषित किया गया। वास्तव में इस अधिनियम द्वारा पुलिस संचालन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया। इसने भारत में पुलिस व्यवस्था की नींव रखी। स्वतंत्रता से पहले 1902-1903 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार ‘फ्रेज़र आयोग’ (Fraser Commission), की स्थापना के साथ पुलिस सुधारों की शुरुआत की गई थी। फ्रेज़र आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर 1902-1903 के पुलिस आयोग के रूप में जाना जाता है, को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में पुलिस प्रशासन में सुधारों की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसका नेतृत्व सर एंड्रयू फ़्रेज़र (Sir Andrew Fraser) और डेविड बेले (David Bayley) द्वारा किया गया था। आयोग द्वारा पुलिस संगठन, प्रशिक्षण, भर्ती में सुधार और मुंबई (तत्कालीन बॉम्बे), कलकत्ता और चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) जैसे प्रमुख शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली की स्थापना जैसे सुझाव दिये गए थे। जिसका उद्देश्य पुलिस दक्षता, व्यावसायिकता और जवाबदेही को बढ़ाना था, हालाँकि ग्रामीण, कृषि आबादी वाले क्षेत्रों में जिला पुलिस प्रणाली बरकरार रखी गई थी।
स्वतंत्रता से पहले 1902-1903 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार ‘फ्रेज़र आयोग’ (Fraser Commission), की स्थापना के साथ पुलिस सुधारों की शुरुआत की गई थी। फ्रेज़र आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर 1902-1903 के पुलिस आयोग के रूप में जाना जाता है, को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में पुलिस प्रशासन में सुधारों की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसका नेतृत्व सर एंड्रयू फ़्रेज़र (Sir Andrew Fraser) और डेविड बेले (David Bayley) द्वारा किया गया था। आयोग द्वारा पुलिस संगठन, प्रशिक्षण, भर्ती में सुधार और मुंबई (तत्कालीन बॉम्बे), कलकत्ता और चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) जैसे प्रमुख शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली की स्थापना जैसे सुझाव दिये गए थे। जिसका उद्देश्य पुलिस दक्षता, व्यावसायिकता और जवाबदेही को बढ़ाना था, हालाँकि ग्रामीण, कृषि आबादी वाले क्षेत्रों में जिला पुलिस प्रणाली बरकरार रखी गई थी।
जबकि आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार पुलिस सुधारों के लिए 1977 में एक समिति "राष्ट्रीय पुलिस आयोग" का गठन किया गया, यह पुलिस संस्था पर रिपोर्ट देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय स्तर पर पहली समिति थी। NCP द्वारा 1979 और 1981 के बीच मौजूदा पुलिस व्यवस्था में व्यापक सुधारों के लिए कई सुझाव दिए गए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण सुझावों में से एक मॉडल पुलिस अधिनियम के विषय में था, लेकिन यह सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। 1996 में उत्तर प्रदेश के एक पूर्व पुलिस महानिदेशक द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पुलिस सुधार की मांग की गई। जिसके तहत सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस सुधार लाने का निर्देश दिया था। इस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सात बाध्यकारी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। उत्तम न्यायालय द्वारा दिए गए ये सात निर्देश निम्नलिखित हैं:
उत्तम न्यायालय द्वारा दिए गए ये सात निर्देश निम्नलिखित हैं:
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव न डाले।
- राज्य सरकार सुनिश्चित करें कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति योग्यता-आधारित, पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जाए और न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए।
- सभी अधिकारियों के लिये न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए।
- जांच और कानून व्यवस्था बनाए रखने के पुलिस के कार्यों को अलग रखा जाए।
- पुलिस उपाधीक्षक और उससे नीचे के स्तर के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और अन्य सेवा-संबंधी मामलों पर निर्णय लेने और सिफारिशें करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली स्थापित की जाए।
- प्रत्येक राज्य में एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित किया जाए।
- केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए एक चयन आयोग स्थापित किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए इन सात निर्देशों की समीक्षा के लिए फिर से जस्टिस थॉमस समिति की स्थापना की गई, लेकिन दुर्भाग्यवश इस समिति द्वारा कोई सुधार और समीक्षा नहीं की गई। 2012-2013 में आपराधिक कानून में संशोधन की सिफारिश करने के लिए न्यायाधीश जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया ताकि निर्भया कांड के बाद महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने के आपराधिक आरोपियों के लिए त्वरित सुनवाई और बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया जा सके। इस समिति ने पुलिस में सुधार के लिए कुछ कदमों की सिफारिश की। इस समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि एक राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री या गृह मंत्री द्वारा की जानी चाहिए, जिससे राज्य सरकार राज्य पुलिस को प्रभावित न कर सके। लेकिन, दुर्भाग्यवश इतनी समितियों के गठन और सुझावों के बावजूद अब तक कोई पुलिस सुधार नहीं हुआ है। आधुनिक युग में, भारतीय पुलिस को विभिन्न प्रकार के मुद्दों से संबंधित बहुआयामी चुनौतियों जैसे कि सांप्रदायिक अशांति, वामपंथी उग्रवाद, मादक द्रव्य आतंकवाद, मानव तस्करी, आतंकवाद के विभिन्न रूप और सीमा पार के खतरे आदि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों का बढ़ता उपयोग पुलिस की चुनौतियों में एक और चुनौती को शामिल करता है।
इसलिए इन सभी चुनौतियों से निपटने एवं जनता के बीच अपनी छवि को सुधारने के लिए वर्तमान समय में भारत में पुलिस सुधारों की आवश्यकता है, जिससे जनता पुलिस की ओर अपने सहायक के रूप में देख सके।
आधुनिक युग में, भारतीय पुलिस को विभिन्न प्रकार के मुद्दों से संबंधित बहुआयामी चुनौतियों जैसे कि सांप्रदायिक अशांति, वामपंथी उग्रवाद, मादक द्रव्य आतंकवाद, मानव तस्करी, आतंकवाद के विभिन्न रूप और सीमा पार के खतरे आदि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों का बढ़ता उपयोग पुलिस की चुनौतियों में एक और चुनौती को शामिल करता है।
इसलिए इन सभी चुनौतियों से निपटने एवं जनता के बीच अपनी छवि को सुधारने के लिए वर्तमान समय में भारत में पुलिस सुधारों की आवश्यकता है, जिससे जनता पुलिस की ओर अपने सहायक के रूप में देख सके।
संदर्भ
https://shorturl.at/uHOR2
https://shorturl.at/pDJQ9
https://shorturl.at/oCHI8
चित्र संदर्भ
1. एक ब्राह्मण पर नजर रखते पुलिस अधिकारीयों और महिला पुलिस अधिकारी को दर्शाता एक चित्रण (picryl, Pexels)
2. उपद्रवी को पकड़ कर ले जाती पुलीस को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. भारतीय सैनिकों के मार्च पास्ट के दौरान, एक महिला एक सैनिक के अंगरखा पर फूल लगाती है। को दर्शाता एक चित्रण (picryl)
4. नई दिल्ली में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन के दौरान भारतीय छात्रों और पुलिस के बीच झड़प को दर्शाता एक चित्रण (picryl)
5. भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द को 2018 में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के साथ दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)



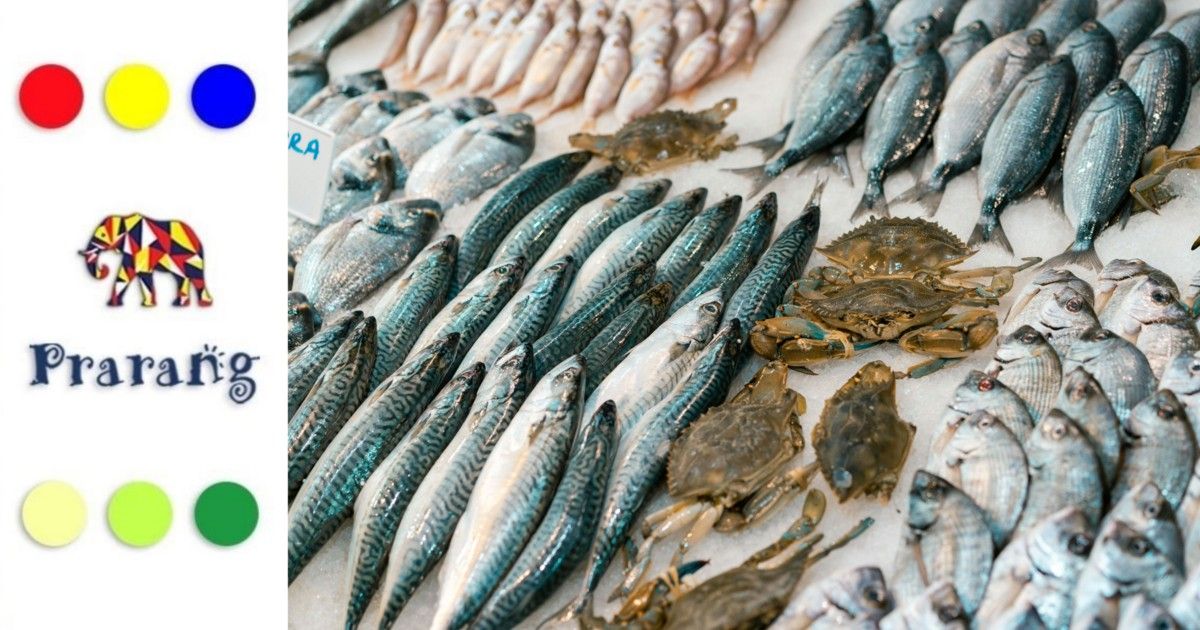
A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.
B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.
C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.
D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.
E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.